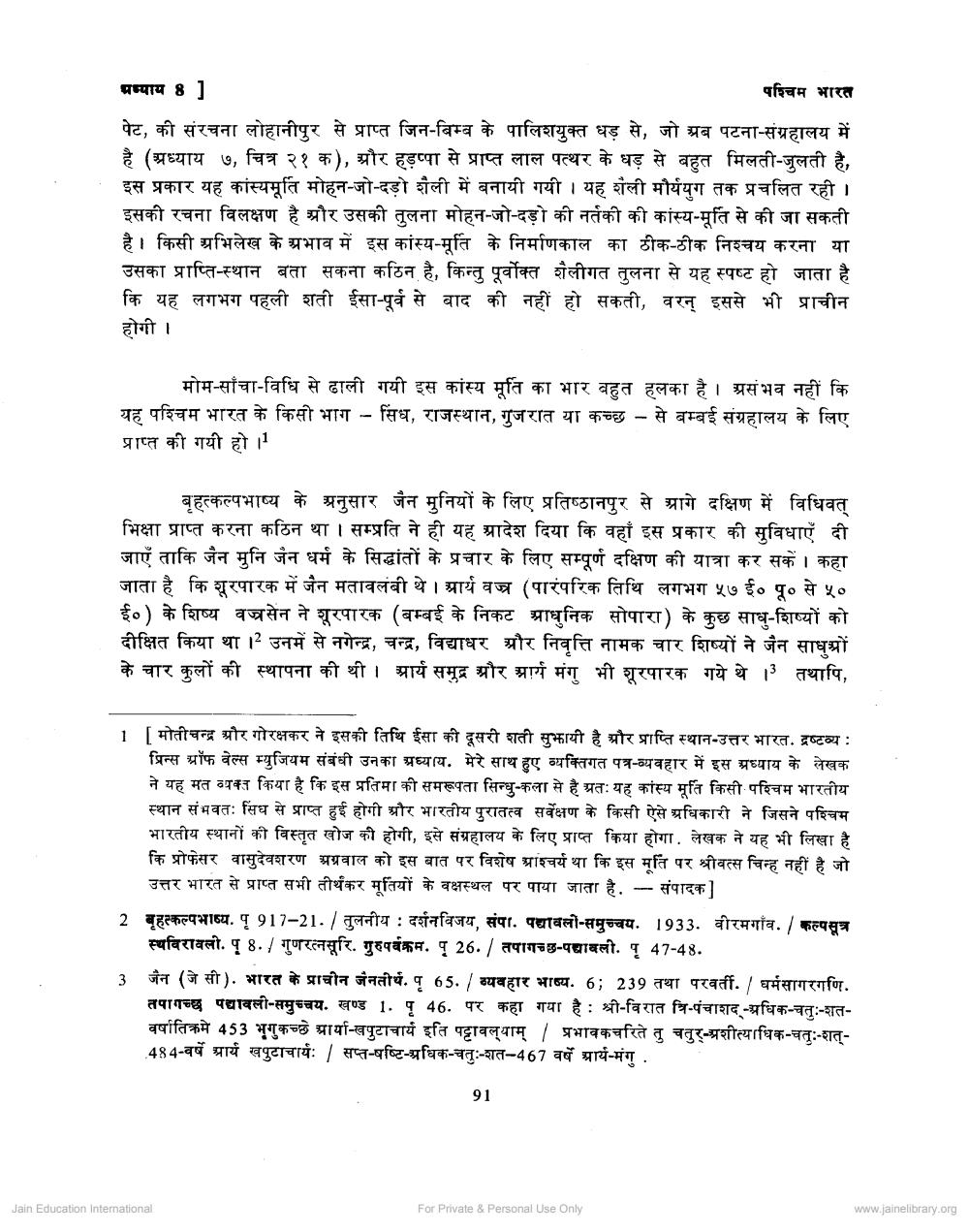________________
अध्याय 8 ]
पश्चिम भारत
पेट, की संरचना लोहानीपुर से प्राप्त जिन-बिम्ब के पालिशयुक्त धड़ से, जो अब पटना-संग्रहालय में है (अध्याय ७, चित्र २१ क), और हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर के धड़ से बहुत मिलती-जुलती है, इस प्रकार यह कांस्यमूर्ति मोहन-जो-दड़ो शैली में बनायी गयी । यह शैली मौर्ययुग तक प्रचलित रही। इसकी रचना विलक्षण है और उसकी तुलना मोहन-जो-दड़ो की नर्तकी की कांस्य-मूर्ति से की जा सकती है। किसी अभिलेख के अभाव में इस कांस्य-मूर्ति के निर्माणकाल का ठीक-ठीक निश्चय करना या उसका प्राप्ति-स्थान बता सकना कठिन है, किन्तु पूर्वोक्त शैलीगत तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लगभग पहली शती ईसा-पूर्व से बाद की नहीं हो सकती, वरन् इससे भी प्राचीन होगी।
मोम-साँचा-विधि से ढाली गयी इस कांस्य मूर्ति का भार बहुत हलका है। असंभव नहीं कि यह पश्चिम भारत के किसी भाग - सिंध, राजस्थान, गुजरात या कच्छ - से बम्बई संग्रहालय के लिए प्राप्त की गयी हो।।
बृहत्कल्पभाष्य के अनुसार जैन मुनियों के लिए प्रतिष्ठानपूर से प्रागे दक्षिण में विधिवत भिक्षा प्राप्त करना कठिन था । सम्प्रति ने ही यह आदेश दिया कि वहाँ इस प्रकार की सुविधाएँ दी जाएँ ताकि जैन मुनि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए सम्पूर्ण दक्षिण की यात्रा कर सकें। कहा जाता है कि शुरपारक में जैन मतावलंबी थे। आर्य वज्र (पारंपरिक तिथि लगभग ५७ ई० पू० से ५० ई.) के शिष्य वज्रसेन ने शूरपारक (बम्बई के निकट आधुनिक सोपारा) के कुछ साधु-शिष्यों को दीक्षित किया था। उनमें से नगेन्द्र, चन्द्र, विद्याधर और निवृत्ति नामक चार शिष्यों ने जैन साधुओं के चार कुलों की स्थापना की थी। आर्य समुद्र और आर्य मंगु भी शूरपारक गये थे । तथापि,
1 [ मोतीचन्द्र और गोरक्षकर ने इसकी तिथि ईसा की दूसरी शती सुझायी है और प्राप्ति स्थान-उत्तर भारत. द्रष्टव्य :
प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युजियम संबंधी उनका अध्याय. मेरे साथ हुए व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार में इस अध्याय के लेखक ने यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रतिमा की समरूपता सिन्धु-कला से है अतः यह कांस्य मूर्ति किसी पश्चिम भारतीय स्थान संभवतः सिंध से प्राप्त हुई होगी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किसी ऐसे अधिकारी ने जिसने पश्चिम भारतीय स्थानों की विस्तृत खोज की होगी, इसे संग्रहालय के लिए प्राप्त किया होगा. लेखक ने यह भी लिखा है कि प्रोफेसर वासुदेवशरण अग्रवाल को इस बात पर विशेष प्राश्चर्य था कि इस मूर्ति पर श्रीवत्स चिन्ह नहीं है जो
उत्तर भारत से प्राप्त सभी तीर्थंकर मूर्तियों के वक्षस्थल पर पाया जाता है. - संपादक] 2 बृहत्कल्पभाष्य. पृ 917-21./ तुलनीय : दर्शनविजय, संपा. पद्यावलो-समुच्चय. 1933. वीरमगाँव. / कल्पसूत्र
स्थविरावली. पृ8./गुणरत्नसूरि. गुरुपर्वक्रम. पृ 26./ तपागच्छ-पद्यावली. पृ 47-48. 3 जैन (जे सी). भारत के प्राचीन जैनतीर्थ. पृ 65. / व्यवहार भाष्य. 6; 239 तथा परवी. / धर्मसागरगणि.
तपागच्छ पद्यावली-समुच्चय. खण्ड 1. पृ 46. पर कहा गया है : श्री-विरात त्रि-पंचाशद -अधिक-चतुः-शतवर्षातिक्रमे 453 भुगुकच्छे पार्या-खपुटाचार्य इति पट्टावल्याम् । प्रभावकचरिते तु चतुर्-प्रशीत्याधिक-चतुः-शत्484-वर्षे प्रार्य खपुटाचार्यः | सप्त-षष्टि-अधिक-चतुः-शत-467 वर्षे प्रार्य-मंगु .
91
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org