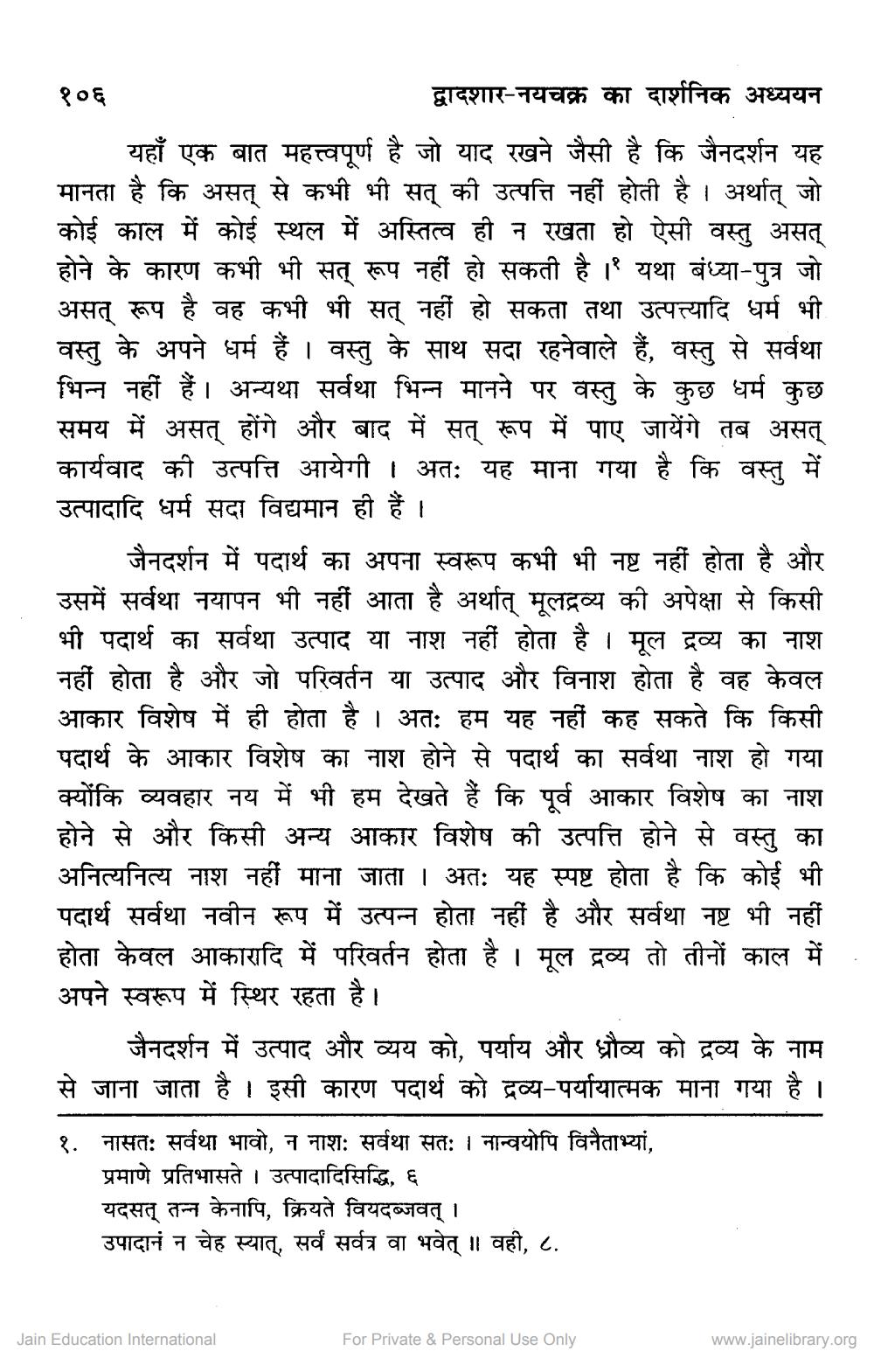________________
१०६
द्वादशार-नयचक्र का दार्शनिक अध्ययन यहाँ एक बात महत्त्वपूर्ण है जो याद रखने जैसी है कि जैनदर्शन यह मानता है कि असत् से कभी भी सत् की उत्पत्ति नहीं होती है । अर्थात् जो कोई काल में कोई स्थल में अस्तित्व ही न रखता हो ऐसी वस्तु असत् होने के कारण कभी भी सत् रूप नहीं हो सकती है । यथा बंध्या-पुत्र जो असत् रूप है वह कभी भी सत् नहीं हो सकता तथा उत्पत्त्यादि धर्म भी वस्तु के अपने धर्म हैं । वस्तु के साथ सदा रहनेवाले हैं, वस्तु से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। अन्यथा सर्वथा भिन्न मानने पर वस्तु के कुछ धर्म कुछ समय में असत् होंगे और बाद में सत् रूप में पाए जायेंगे तब असत् कार्यवाद की उत्पत्ति आयेगी । अतः यह माना गया है कि वस्तु में उत्पादादि धर्म सदा विद्यमान ही हैं ।
जैनदर्शन में पदार्थ का अपना स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता है और उसमें सर्वथा नयापन भी नहीं आता है अर्थात् मूलद्रव्य की अपेक्षा से किसी भी पदार्थ का सर्वथा उत्पाद या नाश नहीं होता है । मूल द्रव्य का नाश नहीं होता है और जो परिवर्तन या उत्पाद और विनाश होता है वह केवल आकार विशेष में ही होता है । अतः हम यह नहीं कह सकते कि किसी पदार्थ के आकार विशेष का नाश होने से पदार्थ का सर्वथा नाश हो गया क्योंकि व्यवहार नय में भी हम देखते हैं कि पूर्व आकार विशेष का नाश होने से और किसी अन्य आकार विशेष की उत्पत्ति होने से वस्तु का अनित्यनित्य नाश नहीं माना जाता । अतः यह स्पष्ट होता है कि कोई भी पदार्थ सर्वथा नवीन रूप में उत्पन्न होता नहीं है और सर्वथा नष्ट भी नहीं होता केवल आकारादि में परिवर्तन होता है । मूल द्रव्य तो तीनों काल में . अपने स्वरूप में स्थिर रहता है।
जैनदर्शन में उत्पाद और व्यय को, पर्याय और ध्रौव्य को द्रव्य के नाम से जाना जाता है । इसी कारण पदार्थ को द्रव्य-पर्यायात्मक माना गया है । १. नासतः सर्वथा भावो, न नाशः सर्वथा सतः । नान्वयोपि विनैताभ्यां,
प्रमाणे प्रतिभासते । उत्पादादिसिद्धि, ६ यदसत् तन्न केनापि, क्रियते वियदब्जवत् । उपादानं न चेह स्यात्, सर्वं सर्वत्र वा भवेत् ॥ वही, ८.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org