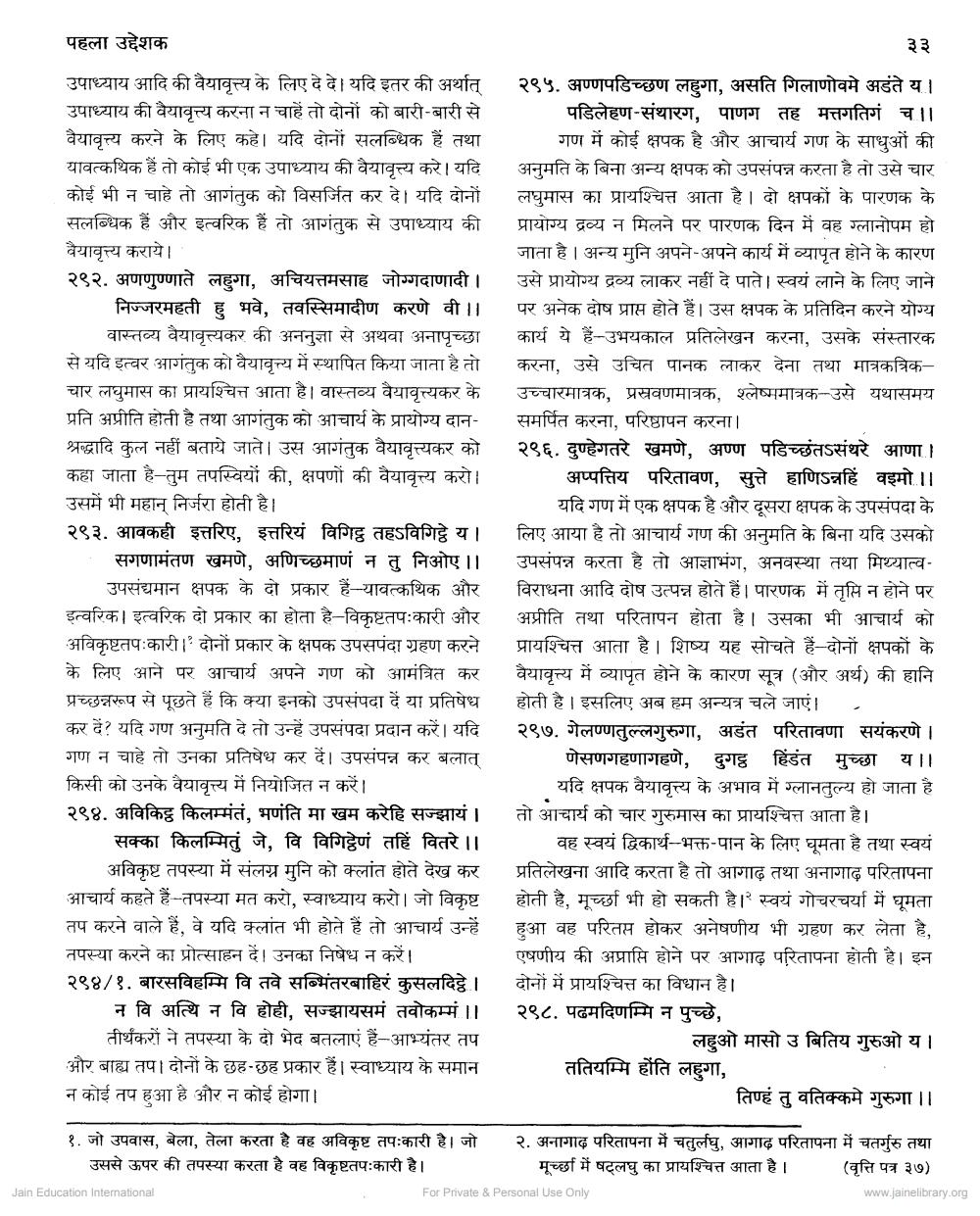________________
पहला उद्देशक
३३
उपाध्याय आदि की वैयावृत्त्य के लिए दे दे। यदि इतर की अर्थात् उपाध्याय की वैयावृत्त्य करना न चाहें तो दोनों को बारी-बारी से वैयावृत्त्य करने के लिए कहे। यदि दोनों सलब्धिक हैं तथा यावत्कथिक हैं तो कोई भी एक उपाध्याय की वैयावृत्त्य करे। यदि कोई भी न चाहे तो आगंतुक को विसर्जित कर दे। यदि दोनों सलब्धिक हैं और इत्वरिक हैं तो आगंतुक से उपाध्याय की वैयावृत्त्य कराये। २९२. अणणुण्णाते लहुगा, अचियत्तमसाह जोग्गदाणादी।
निज्जरमहती हु भवे, तवस्सिमादीण करणे वी।।
वास्तव्य वैयावृत्त्यकर की अननुज्ञा से अथवा अनापृच्छा से यदि इत्वर आगंतुक को वैयावृत्त्य में स्थापित किया जाता है तो चार लघुमास का प्रायश्चित्त आता है। वास्तव्य वैयावृत्त्यकर के प्रति अप्रीति होती है तथा आगंतुक को आचार्य के प्रायोग्य दानश्रद्धादि कुल नहीं बताये जाते। उस आगंतुक वैयावृत्त्यकर को कहा जाता है-तुम तपस्वियों की, क्षपणों की वैयावृत्त्य करो। उसमें भी महान् निर्जरा होती है। २९३. आवकही इत्तरिए, इत्तरियं विगिट्ठ तहऽविगिटे य।
सगणामंतण खमणे, अणिच्छमाणं न तु निओए।।
उपसंद्यमान क्षपक के दो प्रकार हैं-यावत्कथिक और इत्वरिक। इत्वरिक दो प्रकार का होता है-विकृष्टतपःकारी और अविकृष्टतपःकारी। दोनों प्रकार के क्षपक उपसपंदा ग्रहण करने के लिए आने पर आचार्य अपने गण को आमंत्रित कर प्रच्छन्नरूप से पूछते हैं कि क्या इनको उपसंपदा दें या प्रतिषेध कर दें? यदि गण अनुमति दे तो उन्हें उपसंपदा प्रदान करें। यदि गण न चाहे तो उनका प्रतिषेध कर दें। उपसंपन्न कर बलात् किसी को उनके वैयावृत्त्य में नियोजित न करें। २९४. अविकिट्ठ किलम्मतं, भणंति मा खम करेहि सज्झायं।
सक्का किलम्मितुं जे, वि विगिटेणं तहिं वितरे ।।
अविकृष्ट तपस्या में संलग्न मुनि को क्लांत होते देख कर आचार्य कहते हैं-तपस्या मत करो, स्वाध्याय करो। जो विकृष्ट तप करने वाले हैं, वे यदि क्लांत भी होते हैं तो आचार्य उन्हें तपस्या करने का प्रोत्साहन दें। उनका निषेध न करें। २९४/१. बारसविहम्मि वि तवे सब्भितरबाहिरं कुसलदिढे। __ न वि अत्थि न वि होही, सज्झायसमं तवोकम्मं ।।
तीर्थंकरों ने तपस्या के दो भेद बतलाएं हैं-आभ्यंतर तप और बाह्य तप। दोनों के छह-छह प्रकार हैं। स्वाध्याय के समान न कोई तप हुआ है और न कोई होगा।
२९५. अण्णपडिच्छण लहुगा, असति गिलाणोवमे अडते य ।
पडिलेहण-संथारग, पाणग तह मत्तगतिगं च ।।
गण में कोई क्षपक है और आचार्य गण के साधुओं की अनुमति के बिना अन्य क्षपक को उपसंपन्न करता है तो उसे चार लघुमास का प्रायश्चित्त आता है। दो क्षपकों के पारणक के प्रायोग्य द्रव्य न मिलने पर पारणक दिन में वह ग्लानोपम हो जाता है। अन्य मुनि अपने-अपने कार्य में व्याप्त होने के कारण उसे प्रायोग्य द्रव्य लाकर नहीं दे पाते। स्वयं लाने के लिए जाने पर अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उस क्षपक के प्रतिदिन करने योग्य कार्य ये हैं-उभयकाल प्रतिलेखन करना, उसके संस्तारक करना, उसे उचित पानक लाकर देना तथा मात्रकत्रिकउच्चारमात्रक, प्रस्रवणमात्रक, श्लेष्ममात्रक-उसे यथासमय समर्पित करना, परिष्ठापन करना। २९६. दुण्हेगतरे खमणे, अण्ण पडिच्छंतऽसंथरे आणा।
अप्पत्तिय परितावण, सुत्ते हाणिऽन्नहिं वइमो.।।
यदि गण में एक क्षपक है और दूसरा क्षपक के उपसंपदा के लिए आया है तो आचार्य गण की अनुमति के बिना यदि उसको उपसंपन्न करता है तो आज्ञाभंग, अनवस्था तथा मिथ्यात्वविराधना आदि दोष उत्पन्न होते हैं। पारणक में तृप्ति न होने पर अप्रीति तथा परितापन होता है। उसका भी आचार्य को प्रायश्चित्त आता है। शिष्य यह सोचते हैं-दोनों क्षपकों के वैयावृत्त्य में व्याप्त होने के कारण सूत्र (और अर्थ) की हानि होती है। इसलिए अब हम अन्यत्र चले जाएं। . २९७. गेलण्णतुल्लगुरुगा, अडंत परितावणा सयंकरणे ।
णेसणगहणागहणे, दुगट्ठ हिंडंत मुच्छा य ।।
यदि क्षपक वैयावृत्त्य के अभाव में ग्लानतुल्य हो जाता है तो आचार्य को चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है।
वह स्वयं द्विकार्थ-भक्त-पान के लिए घूमता है तथा स्वयं प्रतिलेखना आदि करता है तो आगाढ़ तथा अनागाढ़ परितापना होती है, मूर्छा भी हो सकती है। स्वयं गोचरचर्या में घूमता हुआ वह परितप्त होकर अनेषणीय भी ग्रहण कर लेता है, एषणीय की अप्राप्ति होने पर आगाढ़ परितापना होती है। इन दोनों में प्रायश्चित्त का विधान है। २९८. पढमदिणम्मि न पुच्छे,
लहुओ मासो उ बितिय गुरुओ य । ततियम्मि होति लहुगा,
तिण्हं तु वतिक्कमे गुरुगा ।।
१. जो उपवास, बेला, तेला करता है वह अविकृष्ट तपःकारी है। जो २. अनागाढ़ परितापना में चतुर्लघु, आगाढ़ परितापना में चतर्गुरु तथा उससे ऊपर की तपस्या करता है वह विकृष्टतपःकारी है।
मूर्छा में षट्लघु का प्रायश्चित्त आता है। (वृत्ति पत्र ३७) Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org