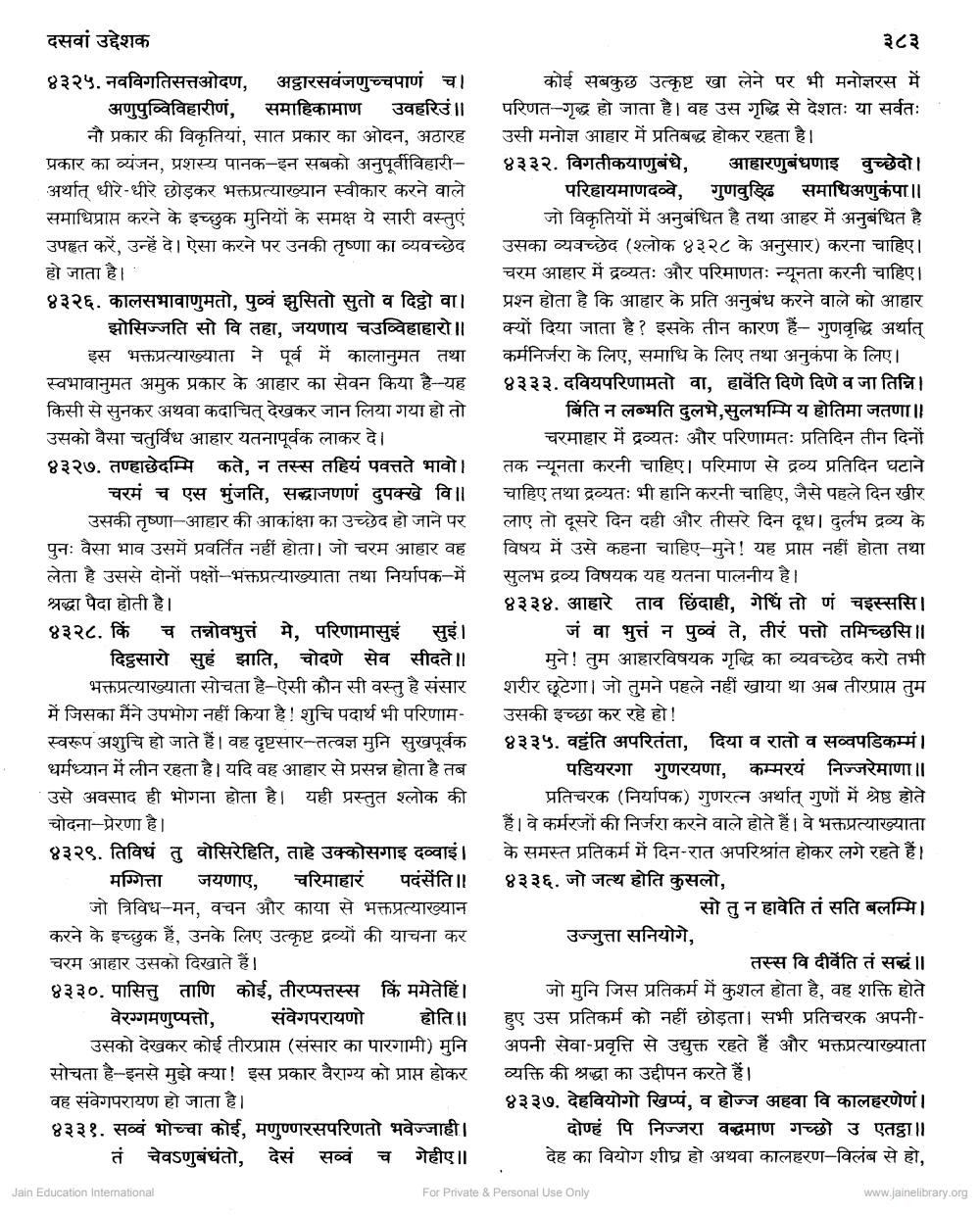________________
दसवां उद्देशक
४३२५. नवविगतिसत्तओदण, अट्ठारसवंजणुच्चपाणं च।
अणुपुव्विविहारीणं, समाहिकामाण उवहरिउं॥
नौ प्रकार की विकृतियां, सात प्रकार का ओदन, अठारह प्रकार का व्यंजन, प्रशस्य पानक-इन सबको अनुपूर्वीविहारी- अर्थात् धीरे-धीरे छोड़कर भक्तप्रत्याख्यान स्वीकार करने वाले समाधिप्राप्त करने के इच्छुक मुनियों के समक्ष ये सारी वस्तुएं उपहृत करें, उन्हें दे। ऐसा करने पर उनकी तृष्णा का व्यवच्छेद हो जाता है। ४३२६. कालसभावाणुमतो, पुव्वं झुसितो सुतो व दिट्ठो वा।
झोसिज्जति सो वि तहा, जयणाय चउब्विहाहारो॥ इस भक्तप्रत्याख्याता ने पूर्व में कालानुमत तथा स्वभावानुमत अमुक प्रकार के आहार का सेवन किया है यह किसी से सुनकर अथवा कदाचित् देखकर जान लिया गया हो तो उसको वैसा चतुर्विध आहार यतनापूर्वक लाकर दे। ४३२७. तण्हाछेदम्मि कते, न तस्स तहियं पवत्तते भावो।
__ चरमं च एस भुंजति, सद्धाजणणं दुपक्खे वि॥
उसकी तृष्णा-आहार की आकांक्षा का उच्छेद हो जाने पर पुनः वैसा भाव उसमें प्रवर्तित नहीं होता। जो चरम आहार वह लेता है उससे दोनों पक्षों-भक्तप्रत्याख्याता तथा निर्यापक-में श्रद्धा पैदा होती है। ४३२८. किं च तन्नोवभुत्तं मे, परिणामासुई सुई।
दिवसारो सुहं झाति, चोदणे सेव सीदते॥
भक्तप्रत्याख्याता सोचता है-ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जिसका मैंने उपभोग नहीं किया है ! शुचि पदार्थ भी परिणामस्वरूप अशुचि हो जाते हैं। वह दृष्टसार-तत्वज्ञ मुनि सुखपूर्वक धर्मध्यान में लीन रहता है। यदि वह आहार से प्रसन्न होता है तब उसे अवसाद ही भोगना होता है। यही प्रस्तुत श्लोक की चोदना-प्रेरणा है। ४३२९. तिविधं तु वोसिरेहिति, ताहे उक्कोसगाइ दव्वाइं।
मग्गित्ता जयणाए, चरिमाहारं पदंसेंति॥
जो त्रिविध-मन, वचन और काया से भक्तप्रत्याख्यान करने के इच्छुक हैं, उनके लिए उत्कृष्ट द्रव्यों की याचना कर चरम आहार उसको दिखाते हैं। ४३३०. पासित्तु ताणि कोई, तीरप्पत्तस्स किं ममेतेहिं।
__ वेरग्गमणुप्पत्तो, संवेगपरायणो होति।
उसको देखकर कोई तीरप्राप्त (संसार का पारगामी) मुनि सोचता है-इनसे मुझे क्या! इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वह संवेगपरायण हो जाता है। ४३३१. सव्वं भोच्चा कोई, मणुण्णरसपरिणतो भवेज्जाही।
तं चेवडणुबंधंतो, देसं सव्वं च गेहीए॥
३८३ कोई सबकुछ उत्कृष्ट खा लेने पर भी मनोज्ञरस में परिणत-गृद्ध हो जाता है। वह उस गृद्धि से देशतः या सर्वतः उसी मनोज्ञ आहार में प्रतिबद्ध होकर रहता है। ४३३२. विगतीकयाणुबंधे, आहारणुबंधणाइ वुच्छेदो।
__परिहायमाणदव्वे, गुणवुढि समाधिअणुकंपा।।
जो विकृतियों में अनुबंधित है तथा आहर में अनुबंधित है उसका व्यवच्छेद (श्लोक ४३२८ के अनुसार) करना चाहिए। चरम आहार में द्रव्यतः और परिमाणतः न्यूनता करनी चाहिए। प्रश्न होता है कि आहार के प्रति अनुबंध करने वाले को आहार क्यों दिया जाता है? इसके तीन कारण हैं-गुणवृद्धि अर्थात् कर्मनिर्जरा के लिए, समाधि के लिए तथा अनुकंपा के लिए। ४३३३. दवियपरिणामतो वा, हावेंति दिणे दिणे व जा तिन्नि।
बिंति न लब्भति दुलभे,सुलभम्मि य होतिमा जतणा।
चरमाहार में द्रव्यतः और परिणामतः प्रतिदिन तीन दिनों तक न्यूनता करनी चाहिए। परिमाण से द्रव्य प्रतिदिन घटाने चाहिए तथा द्रव्यतः भी हानि करनी चाहिए, जैसे पहले दिन खीर लाए तो दूसरे दिन दही और तीसरे दिन दूध। दुर्लभ द्रव्य के विषय में उसे कहना चाहिए-मुने! यह प्राप्त नहीं होता तथा सुलभ द्रव्य विषयक यह यतना पालनीय है। ४३३४. आहारे ताव छिंदाही, गेधिं तो णं चइस्ससि।
जं वा भुत्तं न पुव्वं ते, तीरं पत्तो तमिच्छसि। मुने! तुम आहारविषयक गृद्धि का व्यवच्छेद करो तभी शरीर छूटेगा। जो तुमने पहले नहीं खाया था अब तीरप्रास तुम उसकी इच्छा कर रहे हो! ४३३५. वटुंति अपरितंता, दिया व रातो व सव्वपडिकम्म।
पडियरगा गुणरयणा, कम्मरयं निज्जरेमाणा।।
प्रतिचरक (निर्यापक) गुणरत्न अर्थात् गुणों में श्रेष्ठ होते हैं। वे कर्मरजों की निर्जरा करने वाले होते हैं। वे भक्तप्रत्याख्याता के समस्त प्रतिकर्म में दिन-रात अपरिश्रांत होकर लगे रहते हैं। ४३३६. जो जत्थ होति कुसलो,
सो तु न हावेति तं सति बलम्मि। उज्जुत्ता सनियोगे,
तस्स वि दीवेंति तं सद्धं । जो मुनि जिस प्रतिकर्म में कुशल होता है, वह शक्ति होते हुए उस प्रतिकर्म को नहीं छोड़ता। सभी प्रतिचरक अपनीअपनी सेवा-प्रवृत्ति से उद्युक्त रहते हैं और भक्तप्रत्याख्याता व्यक्ति की श्रद्धा का उद्दीपन करते हैं। ४३३७. देहवियोगो खिप्पं, व होज्ज अहवा वि कालहरणेणं।
दोण्हं पि निज्जरा वद्धमाण गच्छो उ एतट्ठा।। देह का वियोग शीघ्र हो अथवा कालहरण-विलंब से हो,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org