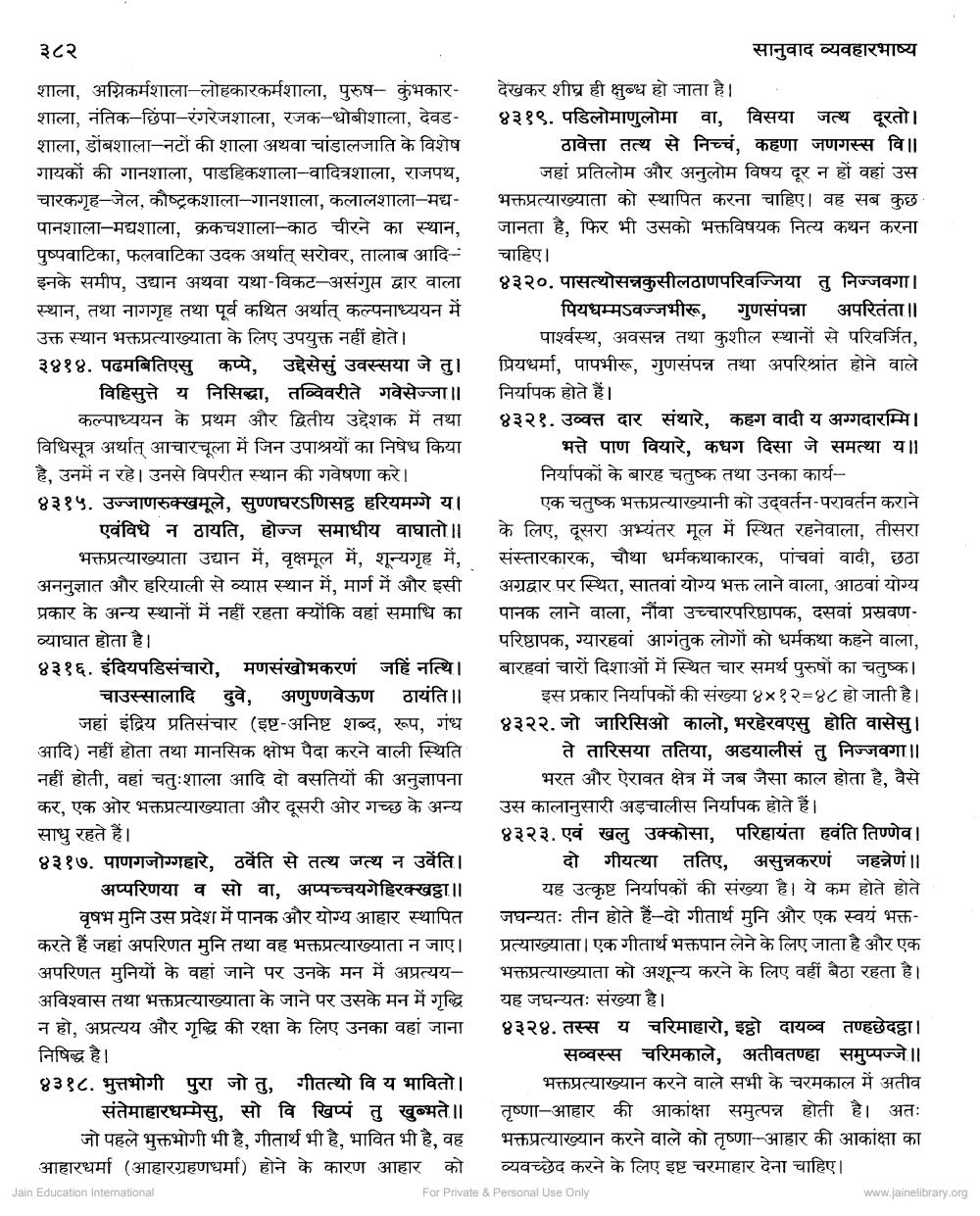________________
३८२
सानुवाद व्यवहारभाष्य
शाला, अग्निकर्मशाला-लोहकारकर्मशाला, पुरुष- कुंभकार- देखकर शीघ्र ही क्षुब्ध हो जाता है। शाला, नंतिक-छिपा-रंगरेजशाला, रजक-धोबीशाला, देवड- ४३१९. पडिलोमाणुलोमा वा, विसया जत्थ दूरतो। शाला, डोंबशाला-नटों की शाला अथवा चांडालजाति के विशेष
ठावेत्ता तत्थ से निच्चं, कहणा जणगस्स वि।। गायकों की गानशाला, पाडहिकशाला-वादित्रशाला, राजपथ, जहां प्रतिलोम और अनुलोम विषय दूर न हों वहां उस चारकगृह-जेल, कौष्ट्रकशाला-गानशाला, कलालशाला-मद्य- भक्तप्रत्याख्याता को स्थापित करना चाहिए। वह सब कुछ पानशाला-मद्यशाला, क्रकचशाला-काठ चीरने का स्थान, जानता है, फिर भी उसको भक्तविषयक नित्य कथन करना पुष्पवाटिका, फलवाटिका उदक अर्थात् सरोवर, तालाब आदि चाहिए। इनके समीप, उद्यान अथवा यथा-विकट-असंगुप्त द्वार वाला ४३२०. पासत्थोसन्नकुसीलठाणपरिवज्जिया तु निज्जवगा। स्थान, तथा नागगृह तथा पूर्व कथित अर्थात् कल्पनाध्ययन में
पियधम्मऽवज्जभीरू, गुणसंपन्ना अपरितंता ।। उक्त स्थान भक्तप्रत्याख्याता के लिए उपयुक्त नहीं होते।
पार्श्वस्थ, अवसन्न तथा कुशील स्थानों से परिवर्जित, ३४१४. पढमबितिएसु कप्पे, उद्देसेसुं उवस्सया जे तु। प्रियधर्मा, पापभीरू, गुणसंपन्न तथा अपरिश्रांत होने वाले
विहिसुत्ते य निसिद्धा, तब्विवरीते गवेसेज्जा॥ निर्यापक होते हैं।
कल्पाध्ययन के प्रथम और द्वितीय उद्देशक में तथा ४३२१. उव्वत्त दार संथारे, कहग वादी य अग्गदारम्मि। विधिसूत्र अर्थात् आचारचूला में जिन उपाश्रयों का निषेध किया
भत्ते पाण वियारे, कधग दिसा जे समत्था य॥ है, उनमें न रहे। उनसे विपरीत स्थान की गवेषणा करे।
निर्यापकों के बारह चतुष्क तथा उनका कार्य४३१५. उज्जाणरुक्खमूले, सुण्णघरऽणिसठ्ठ हरियमग्गे य। एक चतुष्क भक्तप्रत्याख्यानी को उद्वर्तन-परावर्तन कराने
एवंविधे न ठायति, होज्ज समाधीय वाघातो॥ के लिए, दूसरा अभ्यंतर मूल में स्थित रहनेवाला, तीसरा भक्तप्रत्याख्याता उद्यान में, वृक्षमूल में, शून्यगृह में, संस्तारकारक, चौथा धर्मकथाकारक, पांचवां वादी, छठा अननुज्ञात और हरियाली से व्याप्त स्थान में, मार्ग में और इसी अग्रद्वार पर स्थित, सातवां योग्य भक्त लाने वाला, आठवां योग्य प्रकार के अन्य स्थानों में नहीं रहता क्योंकि वहां समाधि का पानक लाने वाला, नौंवा उच्चारपरिष्ठापक, दसवां प्रस्रवणव्याघात होता है।
परिष्ठापक, ग्यारहवां आगंतुक लोगों को धर्मकथा कहने वाला, ४३१६. इंदियपडिसंचारो, मणसंखोभकरणं जहिं नत्थि। बारहवां चारों दिशाओं में स्थित चार समर्थ पुरुषों का चतुष्क।
चाउस्सालादि दुवे, अणुण्णवेऊण ठायंति।। इस प्रकार निर्यापकों की संख्या ४४१२-४८ हो जाती है। जहां इंद्रिय प्रतिसंचार (इष्ट-अनिष्ट शब्द, रूप, गंध ४३२२. जो जारिसिओ कालो, भरहेरवएसु होति वासेसु। आदि) नहीं होता तथा मानसिक क्षोभ पैदा करने वाली स्थिति
ते तारिसया ततिया, अडयालीसं तु निज्जवगा।। नहीं होती, वहां चतुःशाला आदि दो वसतियों की अनुज्ञापना भरत और ऐरावत क्षेत्र में जब जैसा काल होता है, वैसे कर, एक ओर भक्तप्रत्याख्याता और दूसरी ओर गच्छ के अन्य उस कालानुसारी अड़चालीस निर्यापक होते हैं। साधु रहते हैं।
४३२३. एवं खलु उक्कोसा, परिहार्यता हवंति तिण्णेव। ४३१७. पाणगजोग्गहारे, ठवेंति से तत्थ जत्थ न उर्वति।
दो गीयत्था ततिए, असुन्नकरणं जहन्नेणं ।। अप्परिणया व सो वा, अप्पच्चयगेहिरक्खट्ठा।। यह उत्कृष्ट निर्यापकों की संख्या है। ये कम होते होते
वृषभ मुनि उस प्रदेश में पानक और योग्य आहार स्थापित जघन्यतः तीन होते हैं-दो गीतार्थ मुनि और एक स्वयं भक्तकरते हैं जहां अपरिणत मुनि तथा वह भक्तप्रत्याख्याता न जाए। प्रत्याख्याता। एक गीतार्थ भक्तपान लेने के लिए जाता है और एक अपरिणत मुनियों के वहां जाने पर उनके मन में अप्रत्यय- भक्तप्रत्याख्याता को अशून्य करने के लिए वहीं बैठा रहता है। अविश्वास तथा भक्तप्रत्याख्याता के जाने पर उसके मन में गृद्धि यह जघन्यतः संख्या है। न हो, अप्रत्यय और गृद्धि की रक्षा के लिए उनका वहां जाना ४३२४. तस्स य चरिमाहारो, इट्ठो दायव्व तण्हछेदट्ठा। निषिद्ध है।
सव्वस्स चरिमकाले, अतीवतण्हा समुप्पज्जे।। ४३१८. भुत्तभोगी पुरा जो तु, गीतत्थो वि य भावितो। भक्तप्रत्याख्यान करने वाले सभी के चरमकाल में अतीव
संतेमाहारधम्मेसु, सो वि खिप्पं तु खुब्भते.॥ तृष्णा-आहार की आकांक्षा समुत्पन्न होती है। अतः
जो पहले भुक्तभोगी भी है, गीतार्थ भी है, भावित भी है, वह भक्तप्रत्याख्यान करने वाले को तृष्णा-आहार की आकांक्षा का आहारधर्मा (आहारग्रहणधर्मा) होने के कारण आहार को व्यवच्छेद करने के लिए इष्ट चरमाहार देना चाहिए। For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International