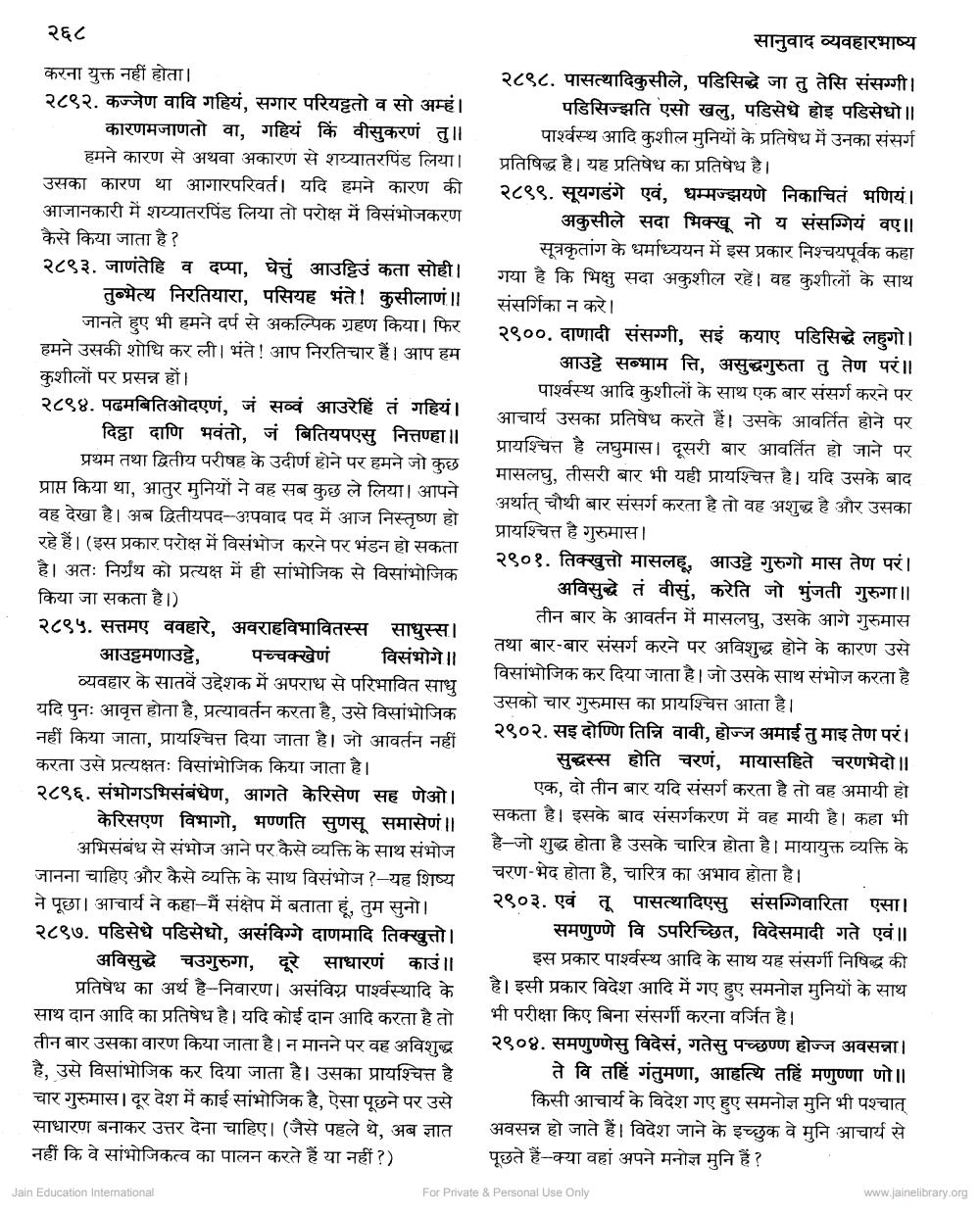________________
२६८
करना युक्त नहीं होता ।
२८९२. कज्जेण वावि गहियं, सगार परियट्टतो व सो अम्हं । कारणमजाणतो वा, गहियं किं वीसुकरणं तु ॥ हमने कारण से अथवा अकारण से शय्यातरपिंड लिया। उसका कारण था आगारपरिवर्त । यदि हमने कारण की आजानकारी में शय्यातरपिंड लिया तो परोक्ष में विसंभोजकरण कैसे किया जाता है ?
२८९३. जाणतेहि व दप्पा, घेत्तुं आउट्टिउं कता सोही ।
तुब्भेत्थ निरतियारा, पसियह भंते! कुसीलाणं ॥ जानते हु भी हमने दर्प से अकल्पिक ग्रहण किया। फिर हमने उसकी शोधि कर ली। भंते! आप निरतिचार हैं। आप हम कुशीलों पर प्रसन्न हों। २८९४. पढमबितिओदएणं, जं सव्वं आउरेहिं तं गहियं । दिट्ठा दाणि भवंतो, जं बितियपएसु नित्तण्हा ॥ प्रथम तथा द्वितीय परीषह के उदीर्ण होने पर हमने जो कुछ प्राप्त किया था, आतुर मुनियों ने वह सब कुछ ले लिया। आपने वह देखा है। अब द्वितीयपद - अपवाद पद में आज निस्तृष्ण हो रहे हैं। (इस प्रकार परोक्ष में विसंभोज करने पर भंडन हो सकता है । अतः निर्ग्रथ को प्रत्यक्ष में ही सांभोजिक से विसांभोजिक किया जा सकता है ।)
२८९५. सत्तम ववहारे, अवराहविभावितस्स साधुस्स । आउट्टमणाउट्टे पच्चक्खेणं विसंभोगे । व्यवहार के सातवें उद्देशक में अपराध से परिभावित साधु यदि पुनः आवृत्त होता है, प्रत्यावर्तन करता है, उसे विसांभोजिक नहीं किया जाता, प्रायश्चित्त दिया जाता है। जो आवर्तन नहीं करता उसे प्रत्यक्षतः विसांभोजिक किया जाता है। २८९६. संभोगऽभिसंबंधेण, आगते केरिसेण सह णेओ ।
केरिसएण विभागो, भण्णति सुणसू समासेणं ॥ अभिसंबंध से संभोज आने पर कैसे व्यक्ति के साथ संभोज जानना चाहिए और कैसे व्यक्ति के साथ विसंभोज ? -यह शिष्य ने पूछा। आचार्य ने कहा- मैं संक्षेप में बताता हूं, तुम सुनो। २८९७. पडिसेधे पडिसेधो, असंविग्गे दाणमादि तिक्खुत्तो ।
अविसुद्धे चउगुरुगा, दूरे साधारणं काउं ॥ प्रतिषेध का अर्थ है - निवारण असंविग्न पार्श्वस्थादि के साथ दान आदि का प्रतिषेध है। यदि कोई दान आदि करता है तो तीन बार उसका वारण किया जाता है। न मानने पर वह अविशुद्ध है, उसे विसांभोजिक कर दिया जाता है। उसका प्रायश्चित्त है चार गुरुमास । दूर देश में काई सांभोजिक है, ऐसा पूछने पर उसे साधारण बनाकर उत्तर देना चाहिए। (जैसे पहले थे, अब ज्ञात नहीं कि वे सांभोजकत्व का पालन करते हैं या नहीं ?)
Jain Education International
सानुवाद व्यवहारभाष्य
२८९८. पासत्थादिकुसीले, पडिसिद्धे जा तु तेसि संसग्गी । पडिसिज्झति एसो खलु, पडिसेधे होइ पडिसेधो ॥ पार्श्वस्थ आदि कुशील मुनियों के प्रतिषेध में उनका संसर्ग प्रतिषिद्ध है। यह प्रतिषेध का प्रतिषेध है ।
२८९९. सूयगडंगे एवं, धम्मज्झयणे निकाचितं भणियं । अकुसीले सदा भिक्खू नो य संसग्गियं वए || सूत्रकृतांग के धर्माध्ययन में इस प्रकार निश्चयपूर्वक कहा गया है कि भिक्षु सदा अकुशील रहें। वह कुशीलों के साथ संसर्गिका न करे।
२९००. दाणादी संसग्गी, सई कयाए पडिसिद्धे लहुगो ।
आउट्टे सब्भामत्ति, असुद्धगुरुता तु तेण परं ॥ पार्श्वस्थ आदि कुशीलों के साथ एक बार संसर्ग करने पर आचार्य उसका प्रतिषेध करते हैं। उसके आवर्तित होने पर प्रायश्चित्त है लघुमास। दूसरी बार आवर्तित हो जाने पर मासलघु, तीसरी बार भी यही प्रायश्चित्त है । यदि उसके बाद अर्थात् चौथी बार संसर्ग करता है तो वह अशुद्ध है और उसका प्रायश्चित्त है गुरुमास ।
२९०१. तिक्खुत्तो मासलहू, आउट्टे गुरुगो मास तेण परं । अविसुद्धे तं वीसुं, करेति जो भुंजती गुरुगा ॥ तीन बार के आवर्तन में मासलघु, उसके आगे गुरुमास तथा बार-बार संसर्ग करने पर अविशुद्ध होने के कारण उसे विसांभोजिक कर दिया जाता है। जो उसके साथ संभोज करता है उसको चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है। २९०२. सइ दोण्णि तिन्नि वावी, होज्ज अमाई तु माइ तेण परं ।
सुद्धस्स होति चरणं, मायासहिते चरणभेदो || एक, दो तीन बार यदि संसर्ग करता है तो वह अमायी हो सकता है। इसके बाद संसर्गकरण में वह मायी है। कहा भी है- जो शुद्ध होता है उसके चारित्र होता है। मायायुक्त व्यक्ति के चरण-भेद होता है, चारित्र का अभाव होता है। २९०३. एवं तू पासत्थादिएसु संसग्गिवारिता एसा ।
समणुणेवि परिच्छित, विदेसमादी गते एवं ॥ इस प्रकार पार्श्वस्थ आदि के साथ यह संसर्गी निषिद्ध की है । इसी प्रकार विदेश आदि में गए हुए समनोज्ञ मुनियों के साथ भी परीक्षा किए बिना संसर्गी करना वर्जित है । २९०४. समणुण्णेसु विदेसं, गतेसु पच्छण्ण होज्ज अवसन्ना । वि तहिं गंतुमणा, आहत्थि तहिं मणुण्णा णो ॥ किसी आचार्य के विदेश गए हुए समनोज्ञ मुनि भी पश्चात् अवसन्न हो जाते हैं। विदेश जाने के इच्छुक वे मुनि आचार्य से पूछते हैं-क्या वहां अपने मनोज्ञ मुनि हैं ?
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org