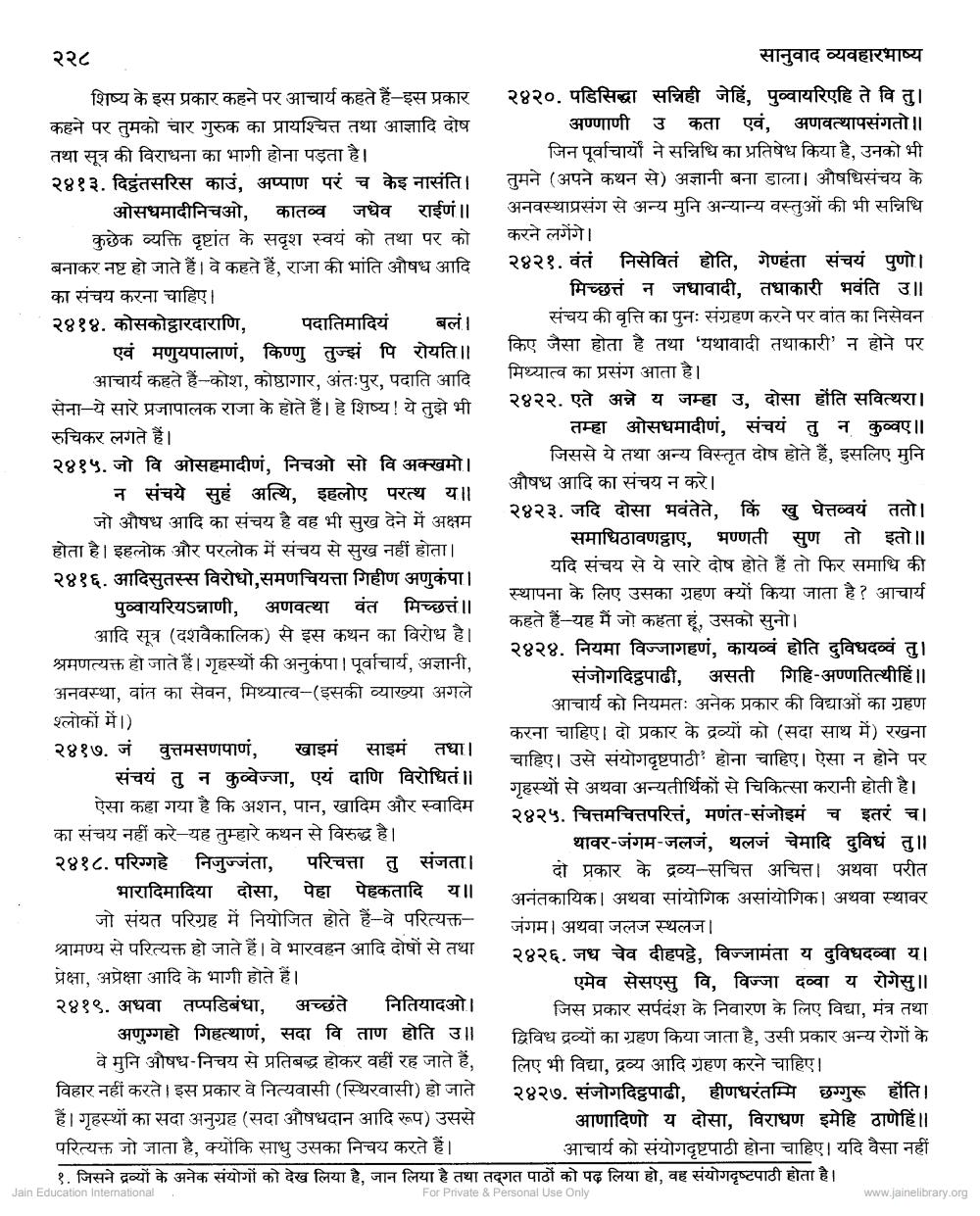________________
२२८
शिष्य के इस प्रकार कहने पर आचार्य कहते हैं - इस प्रकार कहने पर तुमको चार गुरुक का प्रायश्चित्त तथा आज्ञादि दोष तथा सूत्र की विराधना का भागी होना पड़ता है। २४१३. दिवंतसरिस काउं, अप्पाण परं च केइ नासंति । ओसधमादीनिचओ, कातव्व जधेव राईणं ॥ कुछेक व्यक्ति दृष्टांत के सदृश स्वयं को तथा पर को बनाकर नष्ट हो जाते हैं। वे कहते हैं, राजा की भांति औषध आदि का संचय करना चाहिए। २४१४. कोसकोट्ठारदाराणि,
पदातिमादियं बलं ।
एवं मणुयपालाणं, किण्णु तुज्झं पिरोयति ।। आचार्य कहते हैं - कोश, कोष्ठागार, अंतःपुर, पदाति आदि सेना- ये सारे प्रजापालक राजा के होते हैं। हे शिष्य ! ये तुझे भी रुचिकर लगते हैं।
सानुवाद व्यवहारभाष्य २४२०. पडिसिद्धा सन्निही जेहिं, पुव्वायरिएहि ते वि तु । अण्णाणी उ कता एवं अणवत्थापसंगतो ॥
जिन पूर्वाचार्यों ने सन्निधि का प्रतिषेध किया है, उनको भी तुमने (अपने कथन से) अज्ञानी बना डाला। औषधिसंचय के अनवस्थाप्रसंग से अन्य मुनि अन्यान्य वस्तुओं की भी सन्निधि करने लगेंगे।
२४२१. वंतं
निसेवितं होति, गेण्हंता संचयं पुणो । मिच्छत्तं न जधावादी, तधाकारी भवंति उ ॥ संचय की वृत्ति का पुनः संग्रहण करने पर वांत का निसेवन किए जैसा होता है तथा 'यथावादी तथाकारी' न होने पर मिथ्यात्व का प्रसंग आता है।
२४२२. एते अन्ने य जम्हा उ, दोसा होंति सवित्थरा ।
तम्हा ओसधमादीणं, संचयं तु न कुव्वए । जिससे ये तथा अन्य विस्तृत दोष होते हैं, इसलिए मुनि औषध आदि का संचय न करे।
२४१५. जो वि ओसहमादीणं, निचओ सो वि अक्खमो । न संचये सुहं अत्थि, इहलोए परत्थ य ।। जो औषध आदि का संचय है वह भी सुख देने में अक्षम होता है । इहलोक और परलोक में संचय से सुख नहीं होता । २४१६. आदिसुतस्स विरोधो, समणचियत्ता गिहीण अणुकंपा । पुव्वायरियऽन्नाणी, अणवत्था वंत मिच्छत्तं ॥ आदि सूत्र (दशवैकालिक) से इस कथन का विरोध है। श्रमणत्यक्त हो जाते हैं। गृहस्थों की अनुकंपा । पूर्वाचार्य, अज्ञानी, अनवस्था, वांत का सेवन, मिथ्यात्व - (इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में।)
२४१७. जं
वुत्तमसणपाणं,
खाइमं साइमं तथा । संचयं तु न कुव्वेज्जा, एयं दाणि विरोधितं ॥ ऐसा कहा गया है कि अशन, पान, खादिम और स्वादिम का संचय नहीं करे - यह तुम्हारे कथन से विरुद्ध है। २४१८. परिग्गहे निजुज्जंता,
परिचत्ता तु संजता । भारादिमादिया दोसा, पेहा पेहकतादि य ॥ जो संयत परिग्रह में नियोजित होते हैं-वे परित्यक्तश्रामण्य से परित्यक्त हो जाते हैं। वे भारवहन आदि दोषों से तथा प्रेक्षा, अपेक्षा आदि के भागी होते हैं। २४१९. अधवा तप्पडिबंधा, अच्छंते
नितियादओ । अणुग्गहो गिहत्थाणं, सदा वि ताण होति उ ॥ मुन औषध-निचय से प्रतिबद्ध होकर वहीं रह जाते हैं, विहार नहीं करते। इस प्रकार वे नित्यवासी (स्थिरवासी) हो जाते हैं। गृहस्थों का सदा अनुग्रह (सदा औषधदान आदि रूप) उससे परित्यक्त जो जाता है, क्योंकि साधु उसका निचय करते हैं। १. जिसने द्रव्यों के अनेक संयोगों को देख लिया है, जान लिया है तथा तद्गत पाठों को पढ़ लिया हो, वह संयोगदृष्टपाठी होता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
२४२३. जदि दोसा भवंतेते, किं खु घेत्तव्वयं ततो । समाधिठावणट्ठाए, भण्णती सुण तो इतो ॥
यदि संचय से ये सारे दोष होते हैं तो फिर समाधि की स्थापना के लिए उसका ग्रहण क्यों किया जाता है ? आचार्य कहते हैं - यह मैं जो कहता हूं, उसको सुनो।
२४२४. नियमा विज्जागहणं, कायव्वं होति दुविधदव्वं तु ।
संजोगदिट्ठपाढी, असती गिहि- अण्णतित्थीहिं ॥
आचार्य को नियमतः अनेक प्रकार की विद्याओं का ग्रहण करना चाहिए। दो प्रकार के द्रव्यों को (सदा साथ में) रखना चाहिए। उसे संयोगदृष्टपाठी' होना चाहिए। ऐसा न होने पर गृहस्थों से अथवा अन्यतीर्थिकों से चिकित्सा करानी होती है। २४२५. चित्तमचित्तपरित्तं, मणंत-संजोइमं च इतरं च ।
थावर-जंगम-जलजं, थलजं चेमादि दुविधं तु ॥ दो प्रकार के द्रव्य-सचित्त अचित्त । अथवा परीत अनंतकायिक । अथवा सांयोगिक असांयोगिक । अथवा स्थावर जंगम । अथवा जलज स्थलज ।
२४२६. जध चेव दीहपट्टे, विज्जामंता य दुविधदव्वा य । एमेव सेसएस वि, विज्जा दव्वा य रोगेसु ॥
जिस प्रकार सर्पदंश के निवारण के लिए विद्या, मंत्र तथा द्विविधद्रव्यों का ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार अन्य रोगों के लिए भी विद्या, द्रव्य आदि ग्रहण करने चाहिए।
२४२७. संजोगदिट्ठपाढी, हीणधरंतम्मि छग्गुरू होंति । आणादिणो य दोसा, विराधण इमेहि ठाणेहिं || आचार्य को संयोगदृष्टपाठी होना चाहिए। यदि वैसा नहीं
www.jainelibrary.org