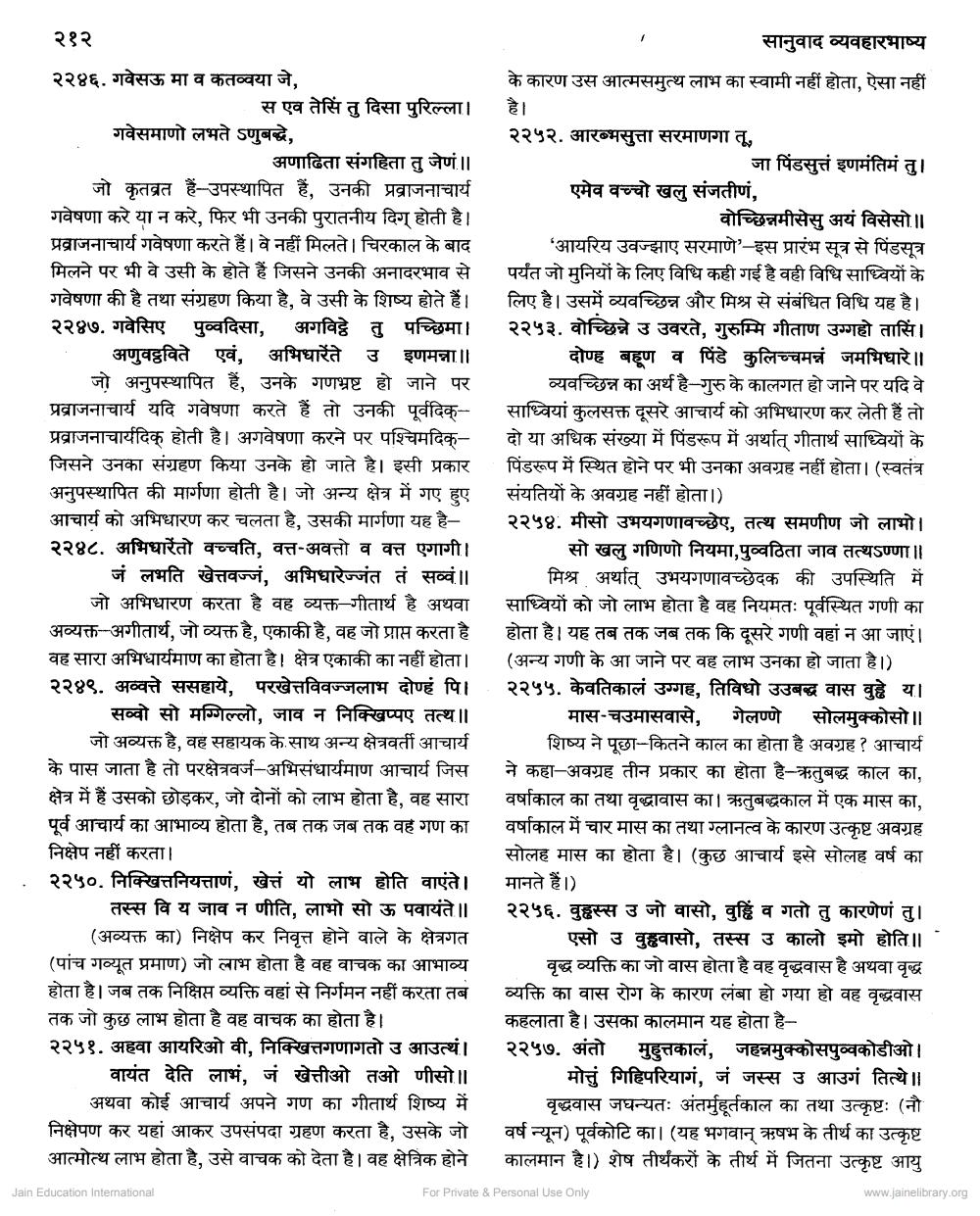________________
२१२
२२४६. गवेसऊ मा व कतव्वया जे,
स एव तेसिं तु दिसा पुरिल्ला। गवेसमाणो लभते ऽणुबद्धे,
अणाढिता संगहिता तु जेणं ।। जो कृतव्रत हैं-उपस्थापित हैं, उनकी प्रव्राजनाचार्य गवेषणा करे या न करे, फिर भी उनकी पुरातनीय दिग होती है। प्रव्राजनाचार्य गवेषणा करते हैं। वे नहीं मिलते। चिरकाल के बाद मिलने पर भी वे उसी के होते हैं जिसने उनकी अनादरभाव से गवेषणा की है तथा संग्रहण किया है, वे उसी के शिष्य होते हैं। २२४७. गवेसिए पुव्वदिसा, अगविढे तु पच्छिमा।
अणुवट्ठविते एवं, अभिधारेते उ इणमन्ना।
जो अनुपस्थापित हैं, उनके गणभ्रष्ट हो जाने पर प्रव्राजनाचार्य यदि गवेषणा करते हैं तो उनकी पूर्वदिक्- प्रव्राजनाचार्यदिक् होती है। अगवेषणा करने पर पश्चिमदिक्जिसने उनका संग्रहण किया उनके हो जाते है। इसी प्रकार अनुपस्थापित की मार्गणा होती है। जो अन्य क्षेत्र में गए हुए आचार्य को अभिधारण कर चलता है, उसकी मार्गणा यह है- २२४८. अभिधारेंतो वच्चति, वत्त-अवत्तो व वत्त एगागी।
जं लभति खेत्तवज्जं, अभिधारेज्जंत तं सव्वं ।।
जो अभिधारण करता है वह व्यक्त-गीतार्थ है अथवा अव्यक्त-अगीतार्थ, जो व्यक्त है, एकाकी है, वह जो प्राप्त करता है वह सारा अभिधार्यमाण का होता है। क्षेत्र एकाकी का नहीं होता। २२४९. अव्वत्ते ससहाये, परखेत्तविवज्जलाभ दोण्हं पि।
सव्वो सो मग्गिल्लो, जाव न निक्खिप्पए तत्थ ।।
जो अव्यक्त है, वह सहायक के साथ अन्य क्षेत्रवर्ती आचार्य के पास जाता है तो परक्षेत्रवर्ज-अभिसंधार्यमाण आचार्य जिस क्षेत्र में हैं उसको छोड़कर, जो दोनों को लाभ होता है, वह सारा पूर्व आचार्य का आभाव्य होता है, तब तक जब तक वह गण का निक्षेप नहीं करता। २२५०. निक्खित्तनियत्ताणं, खेत्तं यो लाभ होति वाएंते।
तस्स वि य जाव न णीति, लाभो सो ऊ पवायंते॥ (अव्यक्त का) निक्षेप कर निवृत्त होने वाले के क्षेत्रगत (पांच गव्यूत प्रमाण) जो लाभ होता है वह वाचक का आभाव्य होता है। जब तक निक्षिप्त व्यक्ति वहां से निर्गमन नहीं करता तब तक जो कुछ लाभ होता है वह वाचक का होता है। २२५१. अहवा आयरिओ वी, निक्खित्तगणागतो उ आउत्थं।
वायंत देति लाभ, जं खेत्तीओ तओ णीसो।।
अथवा कोई आचार्य अपने गण का गीतार्थ शिष्य में निक्षेपण कर यहां आकर उपसंपदा ग्रहण करता है, उसके जो आत्मोत्थ लाभ होता है, उसे वाचक को देता है। वह क्षेत्रिक होने
सानुवाद व्यवहारभाष्य के कारण उस आत्मसमुत्थ लाभ का स्वामी नहीं होता, ऐसा नहीं है। २२५२. आरब्मसुत्ता सरमाणगा तू,
जा पिंडसुत्तं इणमंतिमं तु। एमेव वच्चो खलु संजतीणं,
वोच्छिन्नमीसेसु अयं विसेसो॥ 'आयरिय उवज्झाए सरमाणे'-इस प्रारंभ सूत्र से पिंडसूत्र पर्यंत जो मुनियों के लिए विधि कही गई है वही विधि साध्वियों के लिए है। उसमें व्यवच्छिन्न और मिश्र से संबंधित विधि यह है। २२५३. वोच्छिन्ने उ उवरते, गुरुम्मि गीताण उग्गहो तासिं।
दोण्ह बहूण व पिंडे कुलिच्चमन्नं जमभिधारे॥ व्यवच्छिन्न का अर्थ है-गुरु के कालगत हो जाने पर यदि वे साध्वियां कुलसक्त दूसरे आचार्य को अभिधारण कर लेती हैं तो दो या अधिक संख्या में पिंडरूप में अर्थात् गीतार्थ साध्वियों के पिंडरूप में स्थित होने पर भी उनका अवग्रह नहीं होता। (स्वतंत्र संयतियों के अवग्रह नहीं होता।) २२५४. मीसो उभयगणावच्छेए, तत्थ समणीण जो लाभो।
सो खलु गणिणो नियमा,पुव्वठिता जाव तत्थऽण्णा॥ मिश्र अर्थात् उभयगणावच्छेदक की उपस्थिति में साध्वियों को जो लाभ होता है वह नियमतः पूर्वस्थित गणी का होता है। यह तब तक जब तक कि दूसरे गणी वहां न आ जाएं। (अन्य गणी के आ जाने पर वह लाभ उनका हो जाता है।) २२५५. केवतिकालं उग्गह, तिविधो उउबद्ध वास वुड्ढे य।
मास-चउमासवासे, गेलण्णे सोलमुक्कोसो॥ शिष्य ने पूछा-कितने काल का होता है अवग्रह ? आचार्य ने कहा-अवग्रह तीन प्रकार का होता है-ऋतुबद्ध काल का, वर्षाकाल का तथा वृद्धावास का। ऋतुबद्धकाल में एक मास का, वर्षाकाल में चार मास का तथा ग्लानत्व के कारण उत्कृष्ट अवग्रह सोलह मास का होता है। (कुछ आचार्य इसे सोलह वर्ष का मानते हैं।) २२५६. वुड्डस्स उ जो वासो, वुद्धिं व गतो तु कारणेणं तु।
एसो उ वुहृवासो, तस्स उ कालो इमो होति।।
वृद्ध व्यक्ति का जो वास होता है वह वृद्धवास है अथवा वृद्ध व्यक्ति का वास रोग के कारण लंबा हो गया हो वह वृद्धवास कहलाता है। उसका कालमान यह होता है२२५७. अंतो मुहुत्तकालं, जहन्नमुक्कोसपुव्वकोडीओ।
मोत्तुं गिहिपरियागं, जं जस्स उ आउगं तित्थे॥ वृद्धवास जघन्यतः अंतर्मुहूर्तकाल का तथा उत्कृष्टः (नौ वर्ष न्यून) पूर्वकोटि का। (यह भगवान् ऋषभ के तीर्थ का उत्कृष्ट कालमान है।) शेष तीर्थंकरों के तीर्थ में जितना उत्कृष्ट आयु
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org