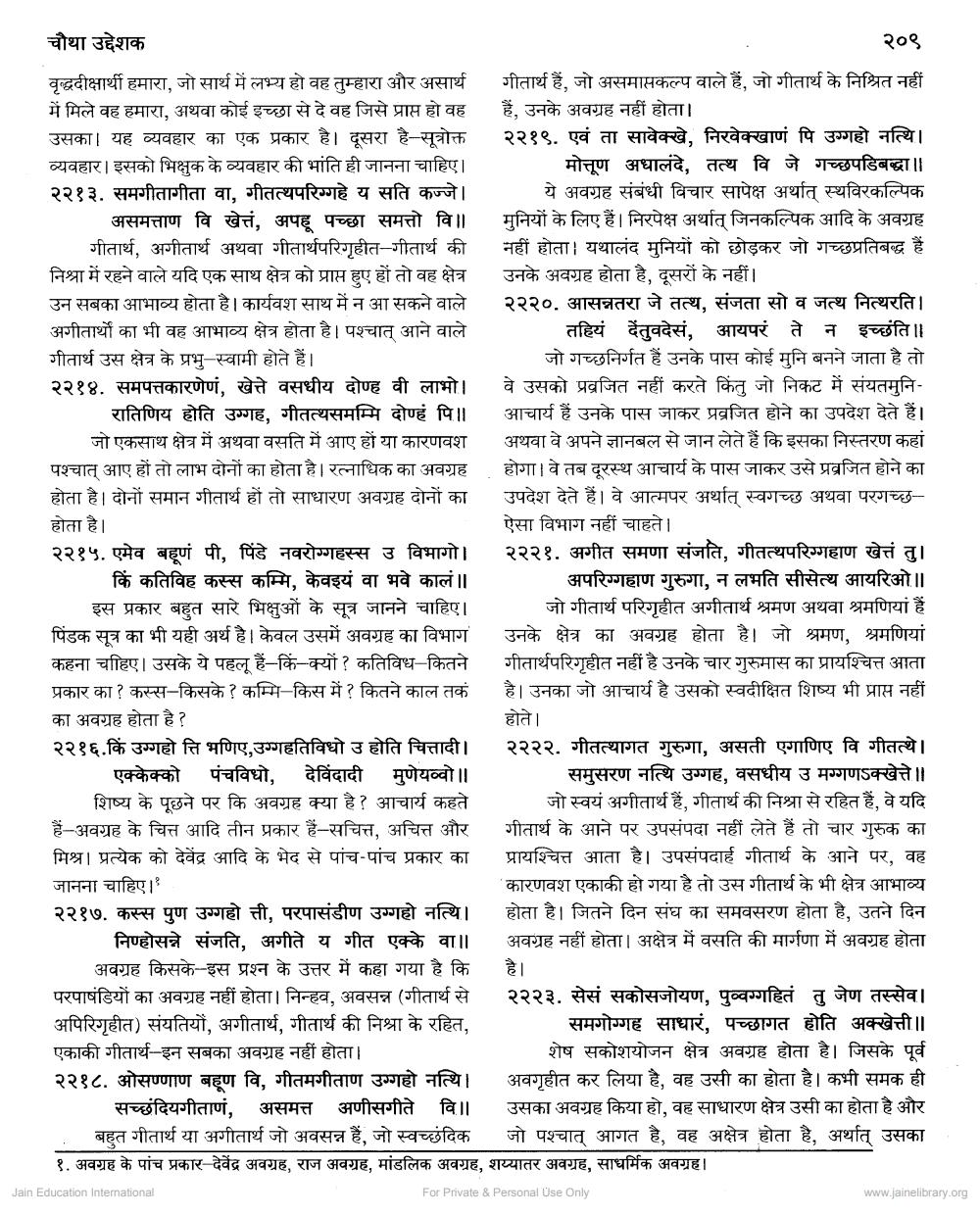________________
चौथा उद्देशक
२०९ वृद्धदीक्षार्थी हमारा, जो सार्थ में लभ्य हो वह तुम्हारा और असार्थ गीतार्थ हैं, जो असमाप्तकल्प वाले हैं, जो गीतार्थ के निश्रित नहीं में मिले वह हमारा, अथवा कोई इच्छा से दे वह जिसे प्राप्त हो वह हैं, उनके अवग्रह नहीं होता। उसका। यह व्यवहार का एक प्रकार है। दूसरा है-सूत्रोक्त २२१९. एवं ता सावेक्खे, निरवेक्खाणं पि उग्गहो नत्थि। व्यवहार। इसको भिक्षुक के व्यवहार की भांति ही जानना चाहिए।
मोत्तूण अधालंदे, तत्थ वि जे गच्छपडिबद्धा ।। २२१३. समगीतागीता वा, गीतत्थपरिग्गहे य सति कज्जे। ये अवग्रह संबंधी विचार सापेक्ष अर्थात् स्थविरकल्पिक
__ असमत्ताण वि खेत्तं, अपहू पच्छा समत्तो वि॥ मुनियों के लिए हैं। निरपेक्ष अर्थात् जिनकल्पिक आदि के अवग्रह
गीतार्थ, अगीतार्थ अथवा गीतार्थपरिगृहीत-गीतार्थ की नहीं होता। यथालंद मुनियों को छोड़कर जो गच्छप्रतिबद्ध हैं निश्रा में रहने वाले यदि एक साथ क्षेत्र को प्राप्त हुए हों तो वह क्षेत्र उनके अवग्रह होता है, दूसरों के नहीं। उन सबका आभाव्य होता है। कार्यवश साथ में न आ सकने वाले २२२०. आसन्नतरा जे तत्थ, संजता सो व जत्थ नित्थरति। अगीतार्थों का भी वह आभाव्य क्षेत्र होता है। पश्चात् आने वाले
तहियं देंतुवदेसं, आयपरं ते न इच्छंति।। गीतार्थ उस क्षेत्र के प्रभु-स्वामी होते हैं।
जो गच्छनिर्गत हैं उनके पास कोई मुनि बनने जाता है तो २२१४. समपत्तकारणेणं, खेत्ते वसधीय दोण्ह वी लाभो। वे उसको प्रवजित नहीं करते किंतु जो निकट में संयतमुनि
रातिणिय होति उग्गह, गीतत्थसमम्मि दोण्हं पि॥ आचार्य हैं उनके पास जाकर प्रवजित होने का उपदेश देते हैं।
जो एकसाथ क्षेत्र में अथवा वसति में आए हों या कारणवश अथवा वे अपने ज्ञानबल से जान लेते हैं कि इसका निस्तरण कहां पश्चात् आए हों तो लाभ दोनों का होता है। रत्नाधिक का अवग्रह . होगा। वे तब दूरस्थ आचार्य के पास जाकर उसे प्रवजित होने का होता है। दोनों समान गीतार्थ हों तो साधारण अवग्रह दोनों का उपदेश देते हैं। वे आत्मपर अर्थात् स्वगच्छ अथवा परगच्छहोता है।
ऐसा विभाग नहीं चाहते। २२१५. एमेव बहूणं पी, पिंडे नवरोग्गहस्स उ विभागो। २२२१. अगीत समणा संजति, गीतत्थपरिग्गहाण खेत्तं तु। किं कतिविह कस्स कम्मि, केवइयं वा भवे कालं॥
अपरिग्गहाण गुरुगा, न लभति सीसेत्थ आयरिओ। इस प्रकार बहुत सारे भिक्षुओं के सूत्र जानने चाहिए। जो गीतार्थ परिगृहीत अगीतार्थ श्रमण अथवा श्रमणियां हैं पिंडक सूत्र का भी यही अर्थ है। केवल उसमें अवग्रह का विभाग उनके क्षेत्र का अवग्रह होता है। जो श्रमण, श्रमणियां कहना चाहिए। उसके ये पहलू हैं-किं-क्यों ? कतिविध-कितने गीतार्थपरिगृहीत नहीं है उनके चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता प्रकार का ? कस्स-किसके ? कम्मि-किस में ? कितने काल तक है। उनका जो आचार्य है उसको स्वदीक्षित शिष्य भी प्राप्त नहीं का अवग्रह होता है?
होते। २२१६.किं उग्गहो त्ति भणिए,उग्गहतिविधो उ होति चित्तादी। २२२२. गीतत्थागत गुरुगा, असती एगाणिए वि गीतत्थे। एक्केक्को पंचविधो, देविंदादी मुणेयव्वो॥
समुसरण नत्थि उग्गह, वसधीय उ मग्गणऽक्खेत्ते॥ शिष्य के पूछने पर कि अवग्रह क्या है ? आचार्य कहते जो स्वयं अगीतार्थ हैं, गीतार्थ की निश्रा से रहित हैं, वे यदि हैं-अवग्रह के चित्त आदि तीन प्रकार हैं-सचित्त, अचित्त और गीतार्थ के आने पर उपसंपदा नहीं लेते हैं तो चार गुरुक का मिश्र। प्रत्येक को देवेंद्र आदि के भेद से पांच-पांच प्रकार का प्रायश्चित्त आता है। उपसंपदार्ह गीतार्थ के आने पर, वह जानना चाहिए।'
कारणवश एकाकी हो गया है तो उस गीतार्थ के भी क्षेत्र आभाव्य २२१७. कस्स पुण उग्गहो त्ती, परपासंडीण उग्गहो नत्थि। होता है। जितने दिन संघ का समवसरण होता है, उतने दिन
निण्होसन्ने संजति, अगीते य गीत एक्के वा॥ अवग्रह नहीं होता। अक्षेत्र में वसति की मार्गणा में अवग्रह होता
अवग्रह किसके इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि है। परपाषंडियों का अवग्रह नहीं होता। निन्हव, अवसन्न (गीतार्थ से २२२३. सेसं सकोसजोयण, पुव्वग्गहितं तु जेण तस्सेव। अपिरिगृहीत) संयतियों, अगीतार्थ, गीतार्थ की निश्रा के रहित,
समगोग्गह साधारं, पच्छागत होति अक्खेत्ती॥ एकाकी गीतार्थ-इन सबका अवग्रह नहीं होता।
शेष सकोशयोजन क्षेत्र अवग्रह होता है। जिसके पूर्व २२१८. ओसण्णाण बहूण वि, गीतमगीताण उग्गहो नत्थि। अवगृहीत कर लिया है, वह उसी का होता है। कभी समक ही
सच्छंदियगीताणं, असमत्त अणीसगीते वि॥ उसका अवग्रह किया हो, वह साधारण क्षेत्र उसी का होता है और __ बहुत गीतार्थ या अगीतार्थ जो अवसन्न हैं, जो स्वच्छंदिक जो पश्चात् आगत है, वह अक्षेत्र होता है, अर्थात् उसका
१. अवग्रह के पांच प्रकार देवेंद्र अवग्रह, राज अवग्रह, मांडलिक अवग्रह, शय्यातर अवग्रह, साधर्मिक अवग्रह। Jain Education International
www.jainelibrary.org
For Private & Personal Use Only