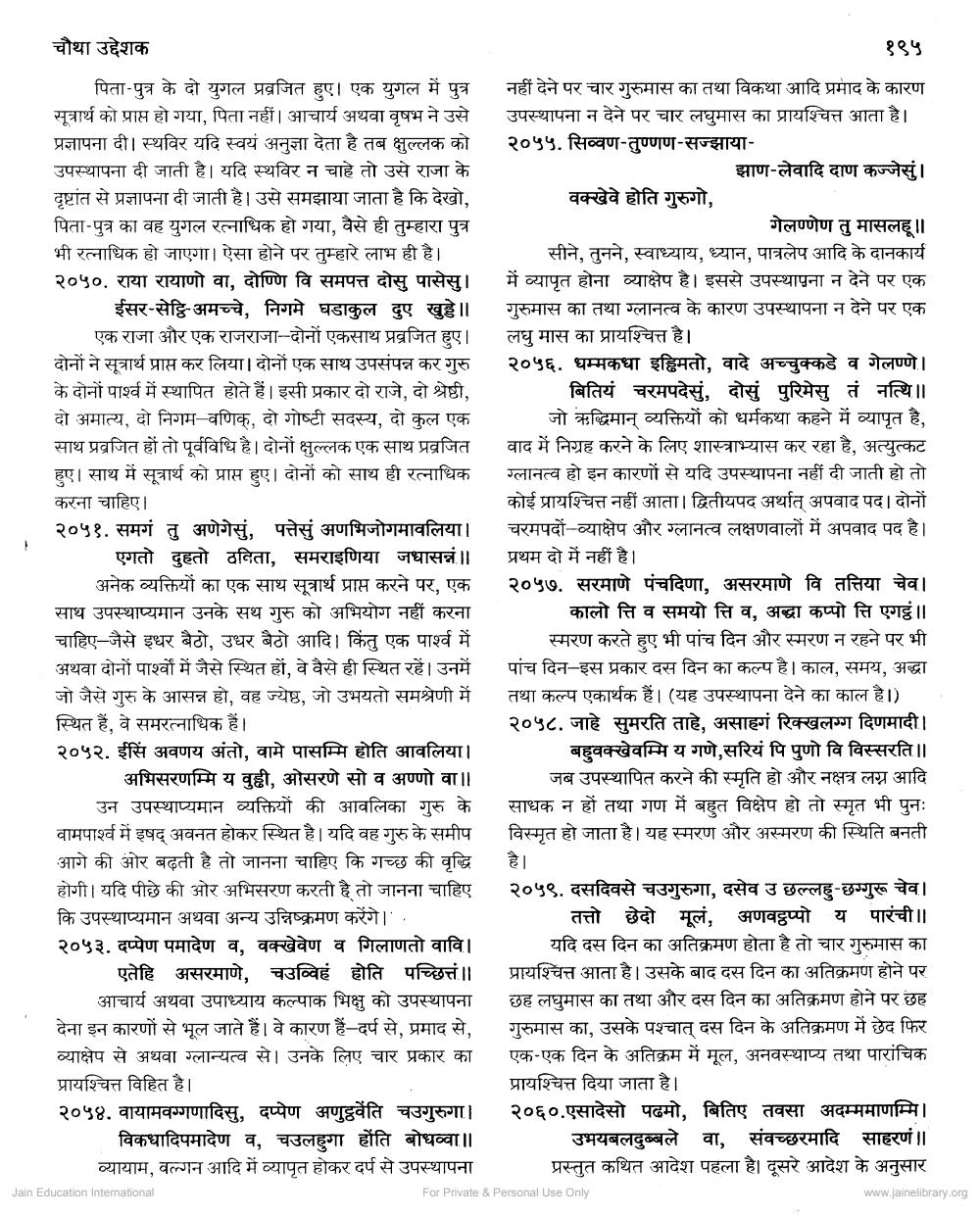________________
चौथा उद्देशक
पिता-पुत्र के दो युगल प्रब्रजित हुए एक युगल में पुत्र सूत्रार्थ को प्राप्त हो गया, पिता नहीं आचार्य अथवा वृषभ ने उसे प्रज्ञापना दी। स्थविर यदि स्वयं अनुज्ञा देता है तब क्षुल्लक को उपस्थापना दी जाती है। यदि स्थविर न चाहे तो उसे राजा के दृष्टांत से प्रज्ञापना दी जाती है। उसे समझाया जाता है कि देखो, पिता-पुत्र का वह युगल रत्नाधिक हो गया, वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी रत्नाधिक हो जाएगा। ऐसा होने पर तुम्हारे लाभ ही है। २०५०. राया रायाणो वा, दोण्णि वि समपत्त दोसु पासेसु । ईसर - सेट्ठि अमच्चे, निगमे घडाकुल दुए खुड्डे || एक राजा और एक राजराजा - दोनों एकसाथ प्रव्रजित हुए । दोनों ने सूत्रार्थ प्राप्त कर लिया। दोनों एक साथ उपसंपन्न कर गुरु के दोनों पार्श्व में स्थापित होते हैं। इसी प्रकार दो राजे, दो श्रेष्ठी, वो अमात्य, वो निगम वणिक, दो गोष्टी सदस्य, दो कुल एक साथ प्रव्रजित हों तो पूर्वविधि है। दोनों क्षुल्लक एक साथ प्रव्रजित हुए। साथ में सूत्रार्थ को प्राप्त हुए। दोनों को साथ ही रत्नाधिक करना चाहिए।
२०५१. समर्ग तु अणेगेसं
पत्तेसं अणभिजोगमावलिया । एगतो दुहतो ठविता, समराइणिया जधासन्नं ॥ अनेक व्यक्तियों का एक साथ सूत्रार्थ प्राप्त करने पर, एक साथ उपस्थाप्यमान उनके सथ गुरु को अभियोग नहीं करना चाहिए जैसे इधर बैठो, उधर बैठो आदि। किंतु एक पार्श्व में अथवा दोनों पार्श्वों में जैसे स्थित हों, वे वैसे ही स्थित रहें। उनमें जो जैसे गुरु के आसन्न हो, वह ज्येष्ठ, जो उभयतो समश्रेणी में स्थित हैं, वे समरत्नाधिक हैं।
२०५२. ईसिं अवणय अंतो, वामे पासम्मि होति आवलिया ।
अभिसरणम्मिय वुड्डी, ओसरणे सो व अण्णो वा ।। उन उपस्थाप्यमान व्यक्तियों की आवलिका गुरु के वामपार्श्व में इषद् अवनत होकर स्थित है। यदि वह गुरु के समीप आगे की ओर बढ़ती है तो जानना चाहिए कि गच्छ की वृद्धि होगी। यदि पीछे की ओर अभिसरण करती है तो जानना चाहिए कि उपस्थाप्यमान अथवा अन्य उन्निष्क्रमण करेंगे।. २०५३. दप्पेण पमादेण व वक्खेवेण व गिलाणतो वावि।
एतेहि असरमाणे, चउब्बिहं होति पच्छित्तं ॥ आचार्य अथवा उपाध्याय कल्पाक भिक्षु को उपस्थापना देना इन कारणों से भूल जाते हैं। वे कारण हैं-दर्प से, प्रमाद से, व्याक्षेप से अथवा ग्लान्यत्व से। उनके लिए चार प्रकार का प्रायश्चित्त विहित है ।
२०५४. वायामवग्गणादिसु, दप्पेण अणुट्ठवेंति चउगुरुगा । विकधादिपमादेण व, चउलहुगा होंति बोधव्वा ॥ व्यायाम, वल्गन आदि में व्यापृत होकर दर्प से उपस्थापना
Jain Education International
१९५
नहीं देने पर चार गुरुमास का तथा विकथा आदि प्रमाद के कारण उपस्थापना न देने पर चार लघुमास का प्रायश्चित्त आता है। २०५५. सिव्वण तुण्णण सज्झाया
झाण-लेवादि वाण कज्जेसुं ।
वक्खेवे होति गुरुगो,
गेलणेण तु मासलहू ॥
सीने, तुनने, स्वाध्याय, ध्यान, पात्रलेप आदि के दानकार्य में व्यापृत होना व्याक्षेप है। इससे उपस्थापना न देने पर एक गुरुमास का तथा ग्लानत्व के कारण उपस्थापना न देने पर एक लघु मास का प्रायश्चित्त है।
२०५६. धम्मकधा इड्डिमतो, वादे अच्चुक्कडे व गेलण्णे । बितियं चरमपदेसुं, दोसुं पुरिमेसु तं नत्थि ॥ जो ऋद्धिमान् व्यक्तियों को धर्मकथा कहने में व्यापृत है, वाद में निग्रह करने के लिए शास्त्राभ्यास कर रहा है, अत्युत्कट ग्लानत्व हो इन कारणों से यदि उपस्थापना नहीं दी जाती हो तो कोई प्रायश्चित्त नहीं आता। द्वितीयपद अर्थात् अपवाद पद दोनों चरमपदों-व्याक्षेप और ग्लानत्व लक्षणवालों में अपवाद पद है। प्रथम दो में नहीं है ।
२०५७. सरमाणे पंचदिणा, असरमाणे वि तत्तिया चेव ।
कालो त्ति व समयो त्ति व, अद्धा कप्पो त्ति एगद्वं ।। स्मरण करते हुए भी पांच दिन और स्मरण न रहने पर भी पांच दिन - इस प्रकार दस दिन का कल्प है। काल, समय, अद्धा तथा कल्प एकार्थक हैं। (यह उपस्थापना देने का काल है ।) २०५८. जाहे सुमरति ताहे, असाहगं रिक्खलग्ग दिणमादी ।
बहुवक्खेवम्मिय गणे, सरियं पि पुणो वि विस्सरति ॥ जब उपस्थापित करने की स्मृति हो और नक्षत्र लग्न आदि साधक न हों तथा गण में बहुत विक्षेप हो तो स्मृत भी पुनः विस्मृत हो जाता है। यह स्मरण और अस्मरण की स्थिति बनती है।
२०५९. दसदिवसे चउगुरुगा, दसेव उ छल्लहु-छग्गुरू चेव । तत्तो छेदो मूलं, अणवटुप्पो य पारंची ॥ यदि दस दिन का अतिक्रमण होता है तो चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है। उसके बाद दस दिन का अतिक्रमण होने पर छह लघुमास का तथा और दस दिन का अतिक्रमण होने पर उड़ गुरुमास का, उसके पश्चात् दस दिन के अतिक्रमण में छेद फिर एक-एक दिन के अतिक्रम में मूल, अनवस्थाप्य तथा पारांचिक प्रायश्चित्त दिया जाता है।
२०६०. एसावेसो पढमो, बितिए तवसा अदम्ममाणम्मि | उभयबलवुब्बले वा, संवच्छरमादि साहरणं ॥ प्रस्तुत कथित आदेश पहला है। दूसरे आदेश के अनुसार
www.jainelibrary.org
For Private & Personal Use Only