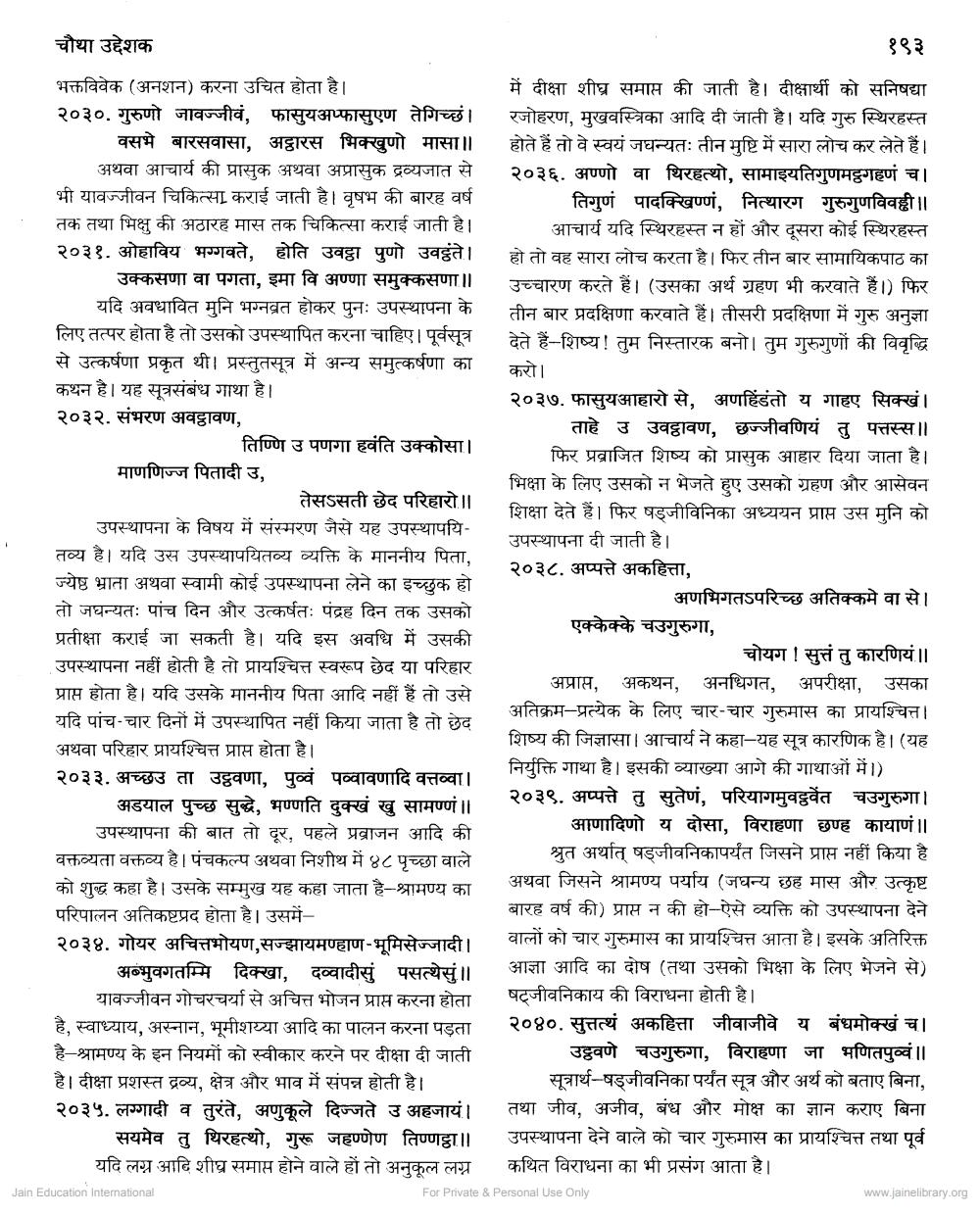________________
चौथा उद्देशक
१९३ भक्तविवेक (अनशन) करना उचित होता है।
में दीक्षा शीघ्र समाप्त की जाती है। दीक्षार्थी को सनिषद्या २०३०. गुरुणो जावज्जीवं, फासुयअफासुएण तेगिच्छं। रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि दी जाती है। यदि गुरु स्थिरहस्त
वसभे बारसवासा, अट्ठारस भिक्खुणो मासा॥ होते हैं तो वे स्वयं जघन्यतः तीन मुष्टि में सारा लोच कर लेते हैं।
अथवा आचार्य की प्रासुक अथवा अप्रासुक द्रव्यजात से २०३६. अण्णो वा थिरहत्थो, सामाइयतिगुणमट्ठगहणं च। भी यावज्जीवन चिकित्सा कराई जाती है। वृषभ की बारह वर्ष
तिगुणं पादक्खिण्णं, नित्थारग गुरुगुणविवड्डी।। तक तथा भिक्षु की अठारह मास तक चिकित्सा कराई जाती है। आचार्य यदि स्थिरहस्त न हों और दूसरा कोई स्थिरहस्त २०३१. ओहाविय भग्गवते, होति उवट्ठा पुणो उवट्ठते।
हो तो वह सारा लोच करता है। फिर तीन बार सामायिकपाठ का उक्कसणा वा पगता, इमा वि अण्णा समुक्कसणा॥
उच्चारण करते हैं। (उसका अर्थ ग्रहण भी करवाते हैं। फिर यदि अवधावित मुनि भग्नव्रत होकर पुनः उपस्थापना के
तीन बार प्रदक्षिणा करवाते हैं। तीसरी प्रदक्षिणा में गुरु अनुज्ञा लिए तत्पर होता है तो उसको उपस्थापित करना चाहिए। पूर्वसूत्र देते हैं-शिष्य! तम निस्तारक बनो। तम गुरुगृणों की विवृद्धि से उत्कर्षणा प्रकृत थी। प्रस्तुतसूत्र में अन्य समुत्कर्षणा का करो। कथन है। यह सूत्रसंबंध गाथा है।
२०३७. फासुयआहारो से, अणहिंडंतो य गाहए सिक्खं । २०३२. संभरण अवठ्ठावण,
ताहे उ उवट्ठावण, छज्जीवणियं तु पत्तस्स॥ तिण्णि उ पणगा हवंति उक्कोसा।
फिर प्रवाजित शिष्य को प्रासुक आहार दिया जाता है। माणणिज्ज पितादी उ,
भिक्षा के लिए उसको न भेजते हुए उसको ग्रहण और आसेवन तेसऽसती छेद परिहारो॥
शिक्षा देते हैं। फिर षड्जीविनिका अध्ययन प्राप्त उस मुनि को उपस्थापना के विषय में संस्मरण जैसे यह उपस्थापयि
उपस्थापना दी जाती है। तव्य है। यदि उस उपस्थापयितव्य व्यक्ति के माननीय पिता,
२०३८. अप्पत्ते अकहित्ता, ज्येष्ठ भ्राता अथवा स्वामी कोई उपस्थापना लेने का इच्छुक हो
अणभिगतऽपरिच्छ अतिक्कमे वा से। तो जघन्यतः पांच दिन और उत्कर्षतः पंद्रह दिन तक उसको
एक्केक्के चउगुरुगा, प्रतीक्षा कराई जा सकती है। यदि इस अवधि में उसकी
चोयग ! सुत्तं तु कारणियं॥ उपस्थापना नहीं होती है तो प्रायश्चित्त स्वरूप छेद या परिहार
अप्राप्त, अकथन, अनधिगत, अपरीक्षा, उसका प्राप्त होता है। यदि उसके माननीय पिता आदि नहीं हैं तो उसे
अतिक्रम-प्रत्येक के लिए चार-चार गुरुमास का प्रायश्चित्त। यदि पांच-चार दिनों में उपस्थापित नहीं किया जाता है तो छेद
शिष्य की जिज्ञासा। आचार्य ने कहा-यह सूत्र कारणिक है। (यह अथवा परिहार प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। २०३३. अच्छउ ता उट्ठवणा, पुव्वं पव्वावणादि वत्तव्वा ।
नियुक्ति गाथा है। इसकी व्याख्या आगे की गाथाओं में।) अडयाल पुच्छ सुद्धे, भण्णति दुक्खं खु सामण्णं ।।
२०३९. अप्पत्ते तु सुतेणं, परियागमुवट्ठवेंत चउगुरुगा। उपस्थापना की बात तो दूर, पहले प्रव्राजन आदि की
आणादिणो य दोसा, विराहणा छण्ह कायाणं ।। वक्तव्यता वक्तव्य है। पंचकल्प अथवा निशीथ में ४८ पृच्छा वाले
श्रुत अर्थात् षड्जीवनिकापर्यंत जिसने प्राप्त नहीं किया है को शुद्ध कहा है। उसके सम्मुख यह कहा जाता है-श्रामण्य का
अथवा जिसने श्रामण्य पर्याय (जघन्य छह मास और उत्कृष्ट परिपालन अतिकष्टप्रद होता है। उसमें
बारह वर्ष की) प्रास न की हो-ऐसे व्यक्ति को उपस्थापना देने २०३४. गोयर अचित्तभोयण,सज्झायमण्हाण-भूमिसेज्जादी।
वालों को चार गुरुमास का प्रायश्चित्त आता है। इसके अतिरिक्त अभवगतम्मि टिक्खा दवादी पसशे आज्ञा आदि का दोष (तथा उसको भिक्षा के लिए भेजने से)
यावजीवन गोचरचर्या असिन भोजन करना होगा षट्जीवनिकाय की विराधना होती है। है, स्वाध्याय, अस्नान, भूमीशय्या आदि का पालन करना पड़ता २०४०. सुत्तत्थं अकहित्ता जीवाजीवे य बंधमोक्खं च। है-श्रामण्य के इन नियमों को स्वीकार करने पर दीक्षा दी जाती
उट्ठवणे चउगुरुगा, विराहणा जा भणितपुव्वं ।। है। दीक्षा प्रशस्त द्रव्य, क्षेत्र और भाव में संपन्न होती है।
सूत्रार्थ-षड्जीवनिका पर्यंत सूत्र और अर्थ को बताए बिना, २०३५. लग्गादी व तुरंते, अणुकूले दिज्जते उ अहजायं। तथा जीव, अजीव, बंध और मोक्ष का ज्ञान कराए बिना
सयमेव तु थिरहत्थो, गुरू जहण्णेण तिण्णट्ठा॥ उपस्थापना देने वाले को चार गुरुमास का प्रायश्चित्त तथा पूर्व
यदि लग्न आदि शीघ्र समाप्त होने वाले हों तो अनुकूल लग्न कथित विराधना का भी प्रसंग आता है। Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org