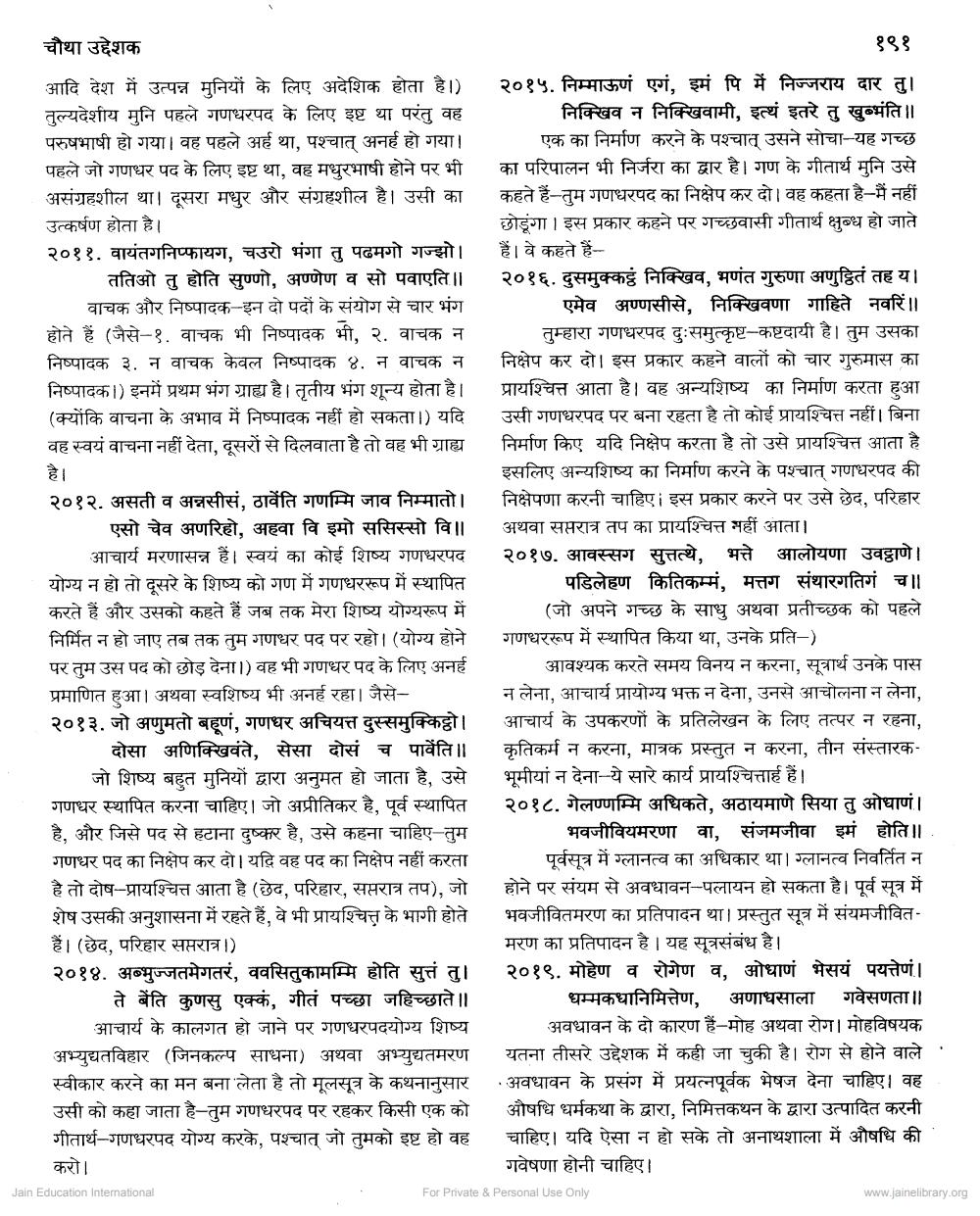________________
चौथा उद्देशक आदि देश में उत्पन्न मुनियों के लिए अदेशिक होता है।) २०१५. निम्माऊणं एगं, इमं पि में निज्जराय दार तु। तुल्यदेशीय मुनि पहले गणधरपद के लिए इष्ट था परंतु वह
निक्खिव न निक्खिवामी, इत्थं इतरे तु खुब्भंति॥ परुषभाषी हो गया। वह पहले अर्ह था, पश्चात् अनर्ह हो गया। एक का निर्माण करने के पश्चात् उसने सोचा-यह गच्छ पहले जो गणधर पद के लिए इष्ट था, वह मधुरभाषी होने पर भी का परिपालन भी निर्जरा का द्वार है। गण के गीतार्थ मुनि उसे असंग्रहशील था। दूसरा मधुर और संग्रहशील है। उसी का कहते हैं-तुम गणधरपद का निक्षेप कर दो। वह कहता है-मैं नहीं उत्कर्षण होता है।
छोडूंगा। इस प्रकार कहने पर गच्छवासी गीतार्थ क्षुब्ध हो जाते २०११. वायंतगनिप्फायग, चउरो भंगा तु पढमगो गज्झो। हैं। वे कहते हैं
ततिओ तु होति सुण्णो, अण्णेण व सो पवाएति॥ २०१६. दुसमुक्कट्ठ निक्खिव, भणंत गुरुणा अणुट्ठितं तह य। वाचक और निष्पादक-इन दो पदों के संयोग से चार भंग
एमेव अण्णसीसे, निक्खिवणा गाहिते नवरिं।। होते हैं (जैसे-१. वाचक भी निष्पादक भी, २. वाचक न तुम्हारा गणधरपद दुःसमुत्कृष्ट-कष्टदायी है। तुम उसका निष्पादक ३. न वाचक केवल निष्पादक ४. न वाचक न निक्षेप कर दो। इस प्रकार कहने वालों को चार गुरुमास का निष्पादक।) इनमें प्रथम भंग ग्राह्य है। तृतीय भंग शून्य होता है। प्रायश्चित्त आता है। वह अन्यशिष्य का निर्माण करता हुआ (क्योंकि वाचना के अभाव में निष्पादक नहीं हो सकता।) यदि उसी गणधरपद पर बना रहता है तो कोई प्रायश्चित्त नहीं। बिना वह स्वयं वाचना नहीं देता, दूसरों से दिलवाता है तो वह भी ग्राह्य । निर्माण किए यदि निक्षेप करता है तो उसे प्रायश्चित्त आता है है।
इसलिए अन्यशिष्य का निर्माण करने के पश्चात् गणधरपद की २०१२. असती व अन्नसीसं, ठावेंति गणम्मि जाव निम्मातो।। निक्षेपणा करनी चाहिए। इस प्रकार करने पर उसे छेद, परिहार
एसो चेव अणरिहो, अहवा वि इमो ससिस्सो वि॥ अथवा सप्तरात्र तप का प्रायश्चित्त महीं आता।
आचार्य मरणासन्न हैं। स्वयं का कोई शिष्य गणधरपद २०१७. आवस्सग सुत्तत्थे, भत्ते आलोयणा उवठ्ठाणे। योग्य न हो तो दूसरे के शिष्य को गण में गणधररूप में स्थापित
पडिलेहण कितिकम्म, मत्तग संथारगतिगं च॥ करते हैं और उसको कहते हैं जब तक मेरा शिष्य योग्यरूप में (जो अपने गच्छ के साधु अथवा प्रतीच्छक को पहले निर्मित न हो जाए तब तक तुम गणधर पद पर रहो। (योग्य होने गणधररूप में स्थापित किया था, उनके प्रति-) पर तुम उस पद को छोड़ देना।) वह भी गणधर पद के लिए अनर्ह आवश्यक करते समय विनय न करना, सूत्रार्थ उनके पास प्रमाणित हुआ। अथवा स्वशिष्य भी अनर्ह रहा। जैसे
न लेना, आचार्य प्रायोग्य भक्त न देना, उनसे आचोलना न लेना, २०१३. जो अणुमतो बहूणं, गणधर अचियत्त दुस्समुक्किट्ठो। आचार्य के उपकरणों के प्रतिलेखन के लिए तत्पर न रहना, __ दोसा अणिक्खिवंते, सेसा दोसं च पावेंति॥ कृतिकर्म न करना, मात्रक प्रस्तुत न करना, तीन संस्तारक
जो शिष्य बहुत मुनियों द्वारा अनुमत हो जाता है, उसे भूमीयां न देना-ये सारे कार्य प्रायश्चित्ताह हैं। गणधर स्थापित करना चाहिए। जो अप्रीतिकर है, पूर्व स्थापित २०१८. गेलण्णम्मि अधिकते, अठायमाणे सिया तु ओधाणं। है, और जिसे पद से हटाना दुष्कर है, उसे कहना चाहिए तुम
भवजीवियमरणा वा, संजमजीवा इमं होति॥ गणधर पद का निक्षेप कर दो। यदि वह पद का निक्षेप नहीं करता पूर्वसूत्र में ग्लानत्व का अधिकार था। ग्लानत्व निवर्तित न है तो दोष-प्रायश्चित्त आता है (छेद, परिहार, सप्तरात्र तप), जो होने पर संयम से अवधावन-पलायन हो सकता है। पूर्व सूत्र में शेष उसकी अनुशासना में रहते हैं, वे भी प्रायश्चित्त के भागी होते भवजीवितमरण का प्रतिपादन था। प्रस्तुत सूत्र में संयमजीवितहैं। (छेद, परिहार सप्तरात्र।)
मरण का प्रतिपादन है। यह सूत्रसंबंध है। २०१४. अब्भुज्जतमेगतरं, ववसितुकामम्मि होति सुत्तं तु। २०१९. मोहेण व रोगेण व, ओधाणं भेसयं पयत्तेणं । ते बेंति कुणसु एक्कं, गीतं पच्छा जहिच्छाते॥
धम्मकधानिमित्तेण, अणाधसाला गवसणता।। आचार्य के कालगत हो जाने पर गणधरपदयोग्य शिष्य अवधावन के दो कारण हैं-मोह अथवा रोग। मोहविषयक अभ्युद्यतविहार (जिनकल्प साधना) अथवा अभ्युद्यतमरण यतना तीसरे उद्देशक में कही जा चुकी है। रोग से होने वाले । स्वीकार करने का मन बना लेता है तो मूलसूत्र के कथनानुसार अवधावन के प्रसंग में प्रयत्नपूर्वक भेषज देना चाहिए। वह उसी को कहा जाता है-तुम गणधरपद पर रहकर किसी एक को औषधि धर्मकथा के द्वारा, निमित्तकथन के द्वारा उत्पादित करनी गीतार्थ-गणधरपद योग्य करके, पश्चात् जो तुमको इष्ट हो वह चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो अनाथशाला में औषधि की करो।
गवेषणा होनी चाहिए। For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International