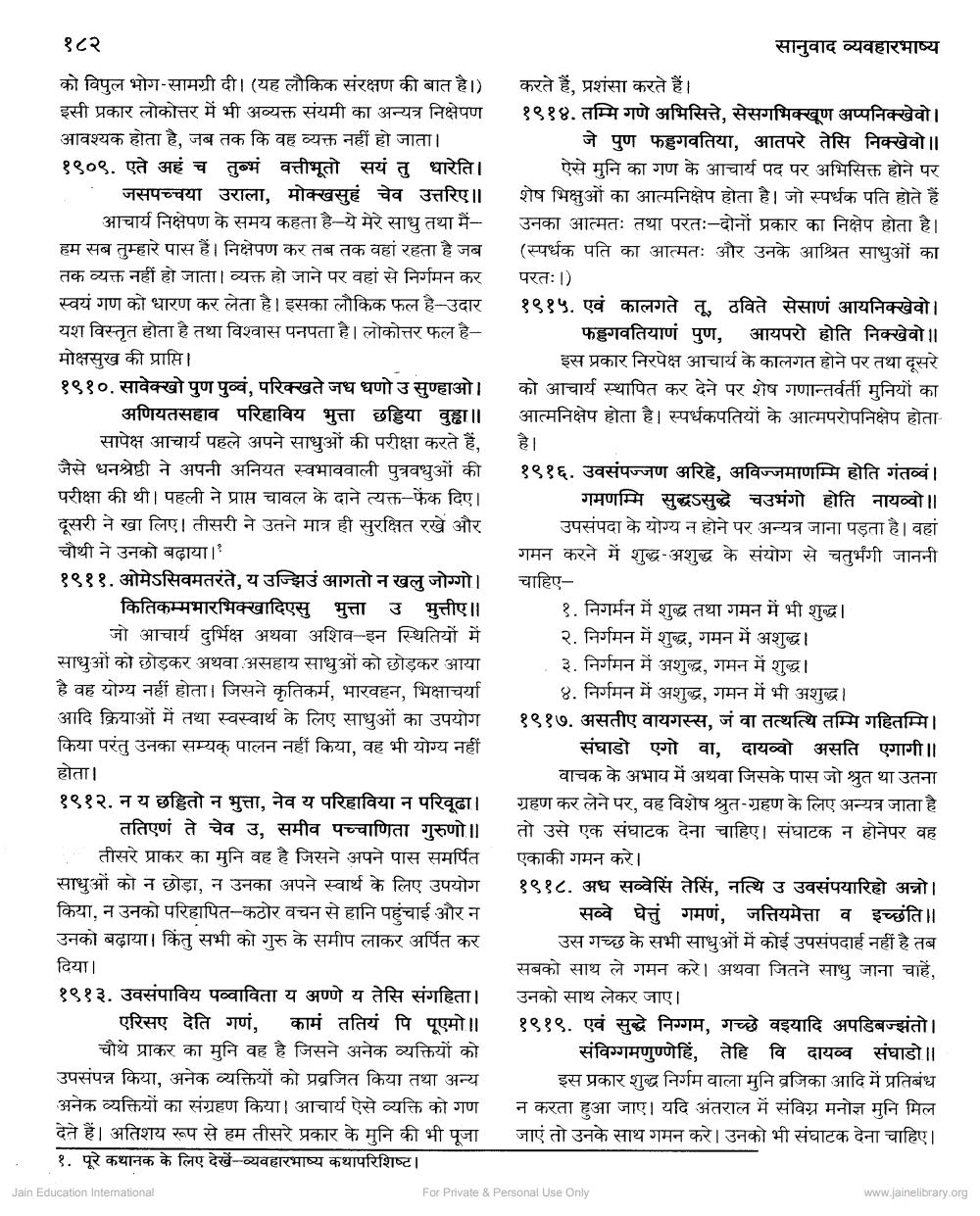________________
१८२
को विपुल भोग सामग्री दी (यह लौकिक संरक्षण की बात है।) इसी प्रकार लोकोत्तर में भी अव्यक्त संयमी का अन्यत्र निक्षेपण आवश्यक होता है, जब तक कि वह व्यक्त नहीं हो जाता । १९०९. एते अहं च तुब्भं वत्तीभूतो सयं तु धारेति । जसपच्चया उराला मोक्खसुहं चेव उत्तरिए || आचार्य निक्षेपण के समय कहता है-ये मेरे साधु तथा मैंहम सब तुम्हारे पास हैं। निक्षेपण कर तब तक वहां रहता है जब तक व्यक्त नहीं हो जाता। व्यक्त हो जाने पर वहां से निर्गमन कर स्वयं गण को धारण कर लेता है। इसका लौकिक फल है-उदार यश विस्तृत होता है तथा विश्वास पनपता है। लोकोत्तर फल हैमोक्षसुख की प्राप्ति ।
१९१०. सावेक्खो पुण पुव्यं, परिक्खते जघ घणो उ सुण्हाओ। अणियतसहाव परिहाविय भुत्ता छडिया वुड्डा ॥ सापेक्ष आचार्य पहले अपने साधुओं की परीक्षा करते हैं, जैसे धन श्रेष्ठी ने अपनी अनियत स्वभाववाली पुत्रवधुओं की परीक्षा की थी पहली ने प्राप्त चावल के दाने त्यक्त-फेंक दिए। दूसरी ने खा लिए तीसरी ने उतने मात्र ही सुरक्षित रखें और चौथी ने उनको बढ़ाया।
१९११. ओमेऽसिवमतरंते, य उज्झिउं आगतो न खलु जोग्गो । कितिकम्मभारभिक्खादिएसु भुत्ता उ भुत्तीए ॥
जो आचार्य दुर्भिक्ष अथवा अशिव-इन स्थितियों में साधुओं को छोड़कर अथवा असहाय साधुओं को छोड़कर आया है वह योग्य नहीं होता जिसने कृतिकर्म, भारवहन, मिक्षाचर्या आदि क्रियाओं में तथा स्वस्वार्थ के लिए साधुओं का उपयोग किया परंतु उनका सम्यक् पालन नहीं किया, वह भी योग्य नहीं होता।
१९१२. न य छड्डितो न भुत्ता, नेव य परिहाविया न परिवूढा । ततिएणं ते चैव उ, समीव पच्चाणिता गुरुणो ॥ तीसरे प्राकर का मुनि वह है जिसने अपने पास समर्पित साधुओं को न छोड़ा, न उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया, न उनको परिहापित-कठोर वचन से हानि पहुंचाई और न उनको बढ़ाया। किंतु सभी को गुरु के समीप लाकर अर्पित कर दिया ।
१९१३. उवसंपाविय पव्वाविता य अण्णे य तेसि संगहिता । एरिसए देति गणं, कामं ततियं पि पूएमो ॥ चौथे प्राकर का मुनि वह है जिसने अनेक व्यक्तियों को उपसंपन्न किया, अनेक व्यक्तियों को प्रबजित किया तथा अन्य अनेक व्यक्तियों का संग्रहण किया। आचार्य ऐसे व्यक्ति को गण देते हैं अतिशय रूप से हम तीसरे प्रकार के मुनि की भी पूजा १. पूरे कथानक के लिए देखें-व्यवहारभाष्य कथापरिशिष्ट ।
Jain Education International
सानुवाद व्यवहारभाष्य
करते हैं, प्रशंसा करते हैं।
१९१४. तम्मि गणे अभिसित्ते, सेसगभिक्खूण अप्पनिक्खेवो । जे पुण फडगवतिया, आतपरे तेसि निक्खेवो ॥ ऐसे मुनि का गण के आचार्य पद पर अभिसिक्त होने पर शेष भिक्षुओं का आत्मनिक्षेप होता है जो स्पर्धक पति होते हैं। 1 उनका आत्मतः तथा परतः - दोनों प्रकार का निक्षेप होता है। ( स्पर्धक पति का आत्मतः और उनके आश्रित साधुओं का परतः ।)
१९१५. एवं कालगते तू, ठविते सेसाणं आयनिक्खेवो । फगवतियाणं पुण, आयपरो होति निक्खेवो ॥
इस प्रकार निरपेक्ष आचार्य के कालगत होने पर तथा दूसरे को आचार्य स्थापित कर देने पर शेष गणान्तर्वर्ती मुनियों का आत्मनिक्षेप होता है। स्पर्धकपतियों के आत्मपरोपनिक्षेप होताहै।
१९१६. उवसंपज्जण अरिहे, अविज्जमाणम्मि होति गंतव्वं । गमणम्मि सुखसुद्धे चउमंगो होति नायव्वो । उपसंपदा के योग्य न होने पर अन्यत्र जाना पड़ता है। वहां गमन करने में शुद्ध - अशुद्ध के संयोग से चतुभंगी जाननी चाहिए
१. निगर्मन में शुद्ध तथा गमन में भी शुद्ध २. निर्गमन में शुद्ध, गमन में अशुद्ध ।
३. निर्गमन में अशुद्ध, गमन में शुद्ध ४. निर्गमन में अशुद्ध, गमन में भी अशुद्ध
१९१७. असतीए वायगस्स, जं वा तत्थत्थि तम्मि गहितम्मि । संघाडो एगो वा, दायव्वो असति एगागी ॥ वाचक के अभाव में अथवा जिसके पास जो श्रुत था उतना ग्रहण कर लेने पर, वह विशेष श्रुत-ग्रहण के लिए अन्यत्र जाता है। तो उसे एक संघाटक देना चाहिए। संघाटक न होनेपर वह एकाकी गमन करे।
१९१८. अध सव्वेसिं तेसिं, नत्थि उ उवसंपयारिहो अन्नो ।
सव्वे घेतुं गमणं, जत्तियमेत्ता व इच्छति ॥
उस गच्छ के सभी साधुओं में कोई उपसंपदा नहीं है तब सबको साथ ले गमन करे। अथवा जितने साधु जाना चाहें, उनको साथ लेकर जाए।
१९१९. एवं सुद्धे निग्गम, गच्छे वइयादि अपडिबज्झतो ।
संविग्गमणुण्णेहिं, तेहि वि दायव्व संघाडो ॥ इस प्रकार शुद्ध निर्गम वाला मुनि व्रजिका आदि में प्रतिबंध न करता हुआ जाए। यदि अंतराल में संविग्र मनोज मुनि मिल जाएं तो उनके साथ गमन करे उनको भी संघाटक देना चाहिए।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org