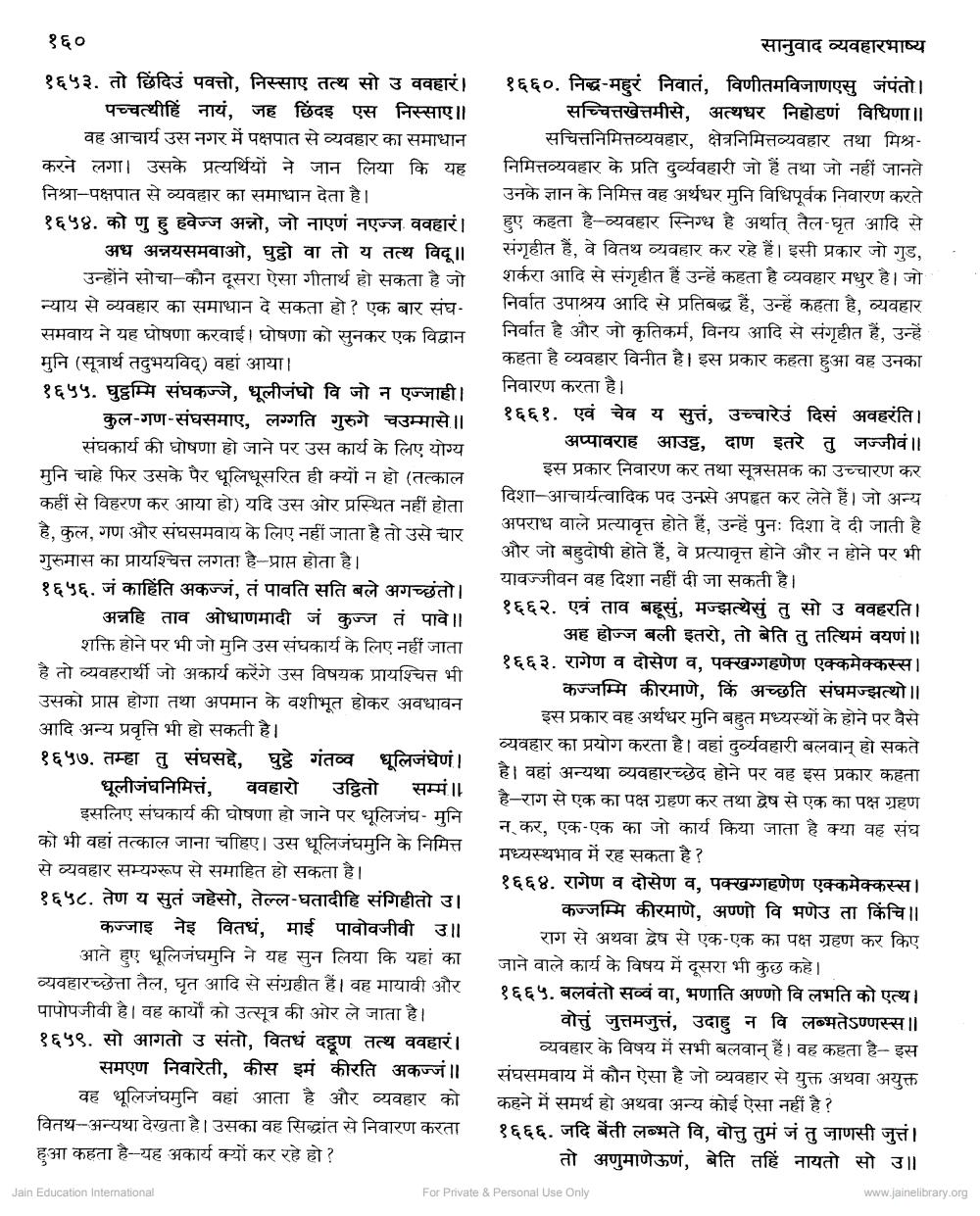________________
१६०
2
१६५३. तो छिंविडं पवत्तो, निस्साए तत्थ सो उ ववहारं । पच्चत्थीहिं नायं जह छिंदइ एस निस्साए । वह आचार्य उस नगर में पक्षपात से व्यवहार का समाधान करने लगा। उसके प्रत्यर्थियों ने जान लिया कि यह निश्रा पक्षपात से व्यवहार का समाधान देता है। १६५४. को णु हु हवेज्ज अन्नो, जो नाएणं नएज्ज ववहारं ।
अध अन्नयसमवाओ, घुट्ठो वा तो य तत्थ विदू ॥ उन्होंने सोचा- कौन दूसरा ऐसा गीतार्थ हो सकता है जो न्याय से व्यवहार का समाधान दे सकता हो ? एक बार संघ - समवाय ने यह घोषणा करवाई। घोषणा को सुनकर एक विद्वान मुनि (सूत्रार्थ तदुभयविद्) वहां आया। १६५५. घुट्ठम्मि संघकज्जे, धूलीजंघो वि जो न एज्जाही ।
कुल गण संघसमाए, लग्गति गुरुगे चउम्मासे ॥ संघकार्य की घोषणा हो जाने पर उस कार्य के लिए योग्य मुनि चाहे फिर उसके पैर धूलिधूसरित ही क्यों न हो (तत्काल कहीं से विहरण कर आया हो) यदि उस ओर प्रस्थित नहीं होता है, कुल, गण और संघसमवाय के लिए नहीं जाता है तो उसे चार गुरुमास का प्रायश्चित्त लगता है-प्राप्त होता है। १६५६. जं काहिंति अकज्जं, तं पावति सति बले अगच्छंतो ।
अन्नहि ताव ओघाणमादी जं कुज्ज तं पावे ॥ शक्ति होने पर भी जो मुनि उस संघकार्य के लिए नहीं जाता है तो व्यवहरार्थी जो अकार्य करेंगे उस विषयक प्रायश्चित्त भी उसको प्राप्त होगा तथा अपमान के वशीभूत होकर अवधावन आदि अन्य प्रवृत्ति भी हो सकती है।
१६५७. तम्हा तु संघसद्दे, घुट्टे गंतव्य धूलिजंघेणं । धूलीजंघनिमित्तं, यवहारो उडितो
इसलिए संघकार्य की घोषणा हो जाने पर धूलिजंघ - मुनि को भी वहां तत्काल जाना चाहिए। उस धूलिजंघमुनि के निमित्त से व्यवहार सम्यग्रूप से समाहित हो सकता है। १६५८. तेण य सुतं जसो, तेल्ल घतादीहि संगिडीतो उ। कज्जाह नेह वितधं, माई पावोवजीवी उ॥
आते हुए धूलिजंघमुनि ने यह सुन लिया कि यहां का व्यवहारच्छेत्ता तैल, घृत आदि से संग्रहीत हैं। वह मायावी और पापोपजीबी है वह कार्यों को उत्सूत्र की ओर ले जाता है। १६५९. सो आगतो उ संतो, वितधं दट्ठूण तत्थ ववहारं ।
समएण निवारेती, कीस इमं कीरति अकज्जं ॥ वह धूलिजंघमुनि वहां आता है और व्यवहार को वितथ-अन्यथा देखता है। उसका वह सिद्धांत से निवारण करता हुआ कहता है- यह अकार्य क्यों कर रहे हो ?
Jain Education International
सानुवाद व्यवहारभाष्य
१६६०. निद्र-महुरं निवातं, विणीतमविजाणएस जंपतो । सच्चित्तखेत्तमीसे, अत्थधर निहोडणं विधिणा ॥ सचित्तनिमित्तव्यवहार, क्षेत्रनिमित्तव्यवहार तथा मिश्र निमित्तव्यवहार के प्रति दुर्व्यवहारी जो हैं तथा जो नहीं जानते उनके ज्ञान के निमित्त वह अर्थधर मुनि विधिपूर्वक निवारण करते हुए कहता है-व्यवहार स्निग्ध है अर्थात् तैल-घृत आदि से संगृहीत हैं, वे वितथ व्यवहार कर रहे हैं। इसी प्रकार जो गुड, शर्करा आदि से संगृहीत हैं उन्हें कहता है व्यवहार मधुर है जो निर्वात उपाश्रय आदि से प्रतिबद्ध हैं, उन्हें कहता है, व्यवहार निर्वात है और जो कृतिकर्म, विनय आदि से संगृहीत हैं, उन्हें कहता है व्यवहार विनीत है। इस प्रकार कहता हुआ वह उनका निवारण करता है।
१६६१. एवं चेव य सुत्तं, उच्चारेडं दिसं अवहरति ।
अप्पावराह आउट्ट, दाण इतरे तु जज्जीवं ॥ इस प्रकार निवारण कर तथा सूत्रसप्तक का उच्चारण कर दिशा - आचार्यत्वादिक पद उनसे अपहृत कर लेते हैं। जो अन्य अपराध वाले प्रत्यावृत्त होते हैं, उन्हें पुनः दिशा दे दी जाती है और जो बहुदोषी होते हैं, वे प्रत्यावृत्त होने और न होने पर भी यावज्जीवन वह दिशा नहीं दी जा सकती है। १६६२. एवं ताव बहुसुं, मज्झत्येसुं तु सो उ ववहरति ।
अह होज्ज बली इतरो, तो बेति तु तत्थिमं वयणं ॥ १६६३. रागेण व दोसेण व पक्खग्गहणेण एक्कमेक्कस्स | कज्जम्मि कीरमाणे, किं अच्छति संघमज्झत्थो ।
इस प्रकार वह अर्थधर मुनि बहुत मध्यस्थों के होने पर वैसे व्यवहार का प्रयोग करता है। वहां दुर्व्यवहारी बलवान् हो सकते है। वहां अन्यथा व्यवहारच्छेद होने पर वह इस प्रकार कहता है - राग से एक का पक्ष ग्रहण कर तथा द्वेष से एक का पक्ष ग्रहण न कर, एक एक का जो कार्य किया जाता है क्या वह संघ मध्यस्थभाव में रह सकता है ?
१६६४. रागेण व दोसेण व, पक्खम्गहणेण एक्कमेक्कस्स
कज्जम्मि कीरमाणे, अण्णो वि भणेउ ता किंचि ॥ राग से अथवा द्वेष से एक-एक का पक्ष ग्रहण कर किए जाने वाले कार्य के विषय में दूसरा भी कुछ कहे। १६६५. बलवंतो सव्वं वा, भणाति अण्णो वि लगति को एत्थ ।
वोत्तुं जुत्तमजुत्तं, उदाहु न वि लब्भतेऽण्णस्स ॥ व्यवहार के विषय में सभी बलवान् हैं। वह कहता है- इस संघसमवाय में कौन ऐसा है जो व्यवहार से युक्त अथवा अयुक्त कहने में समर्थ हो अथवा अन्य कोई ऐसा नहीं है? १६६६. जदि बेंती लब्भते वि, वोत्तु तुमं जं तु जाणसी जुत्तं । तो अणुमाणेऊणं, बेति तर्हि नावतो सो उ॥
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org