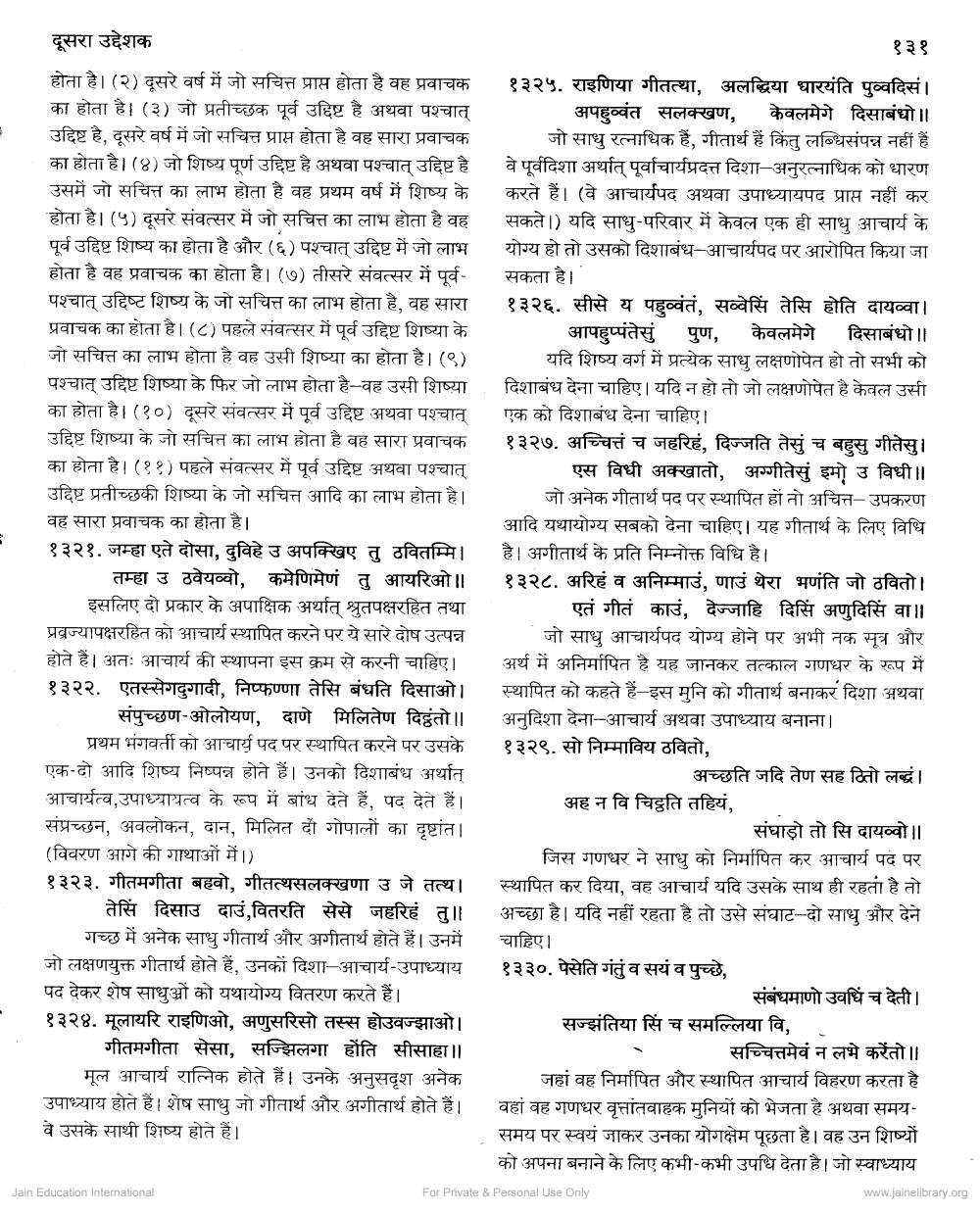________________
दूसरा उद्देशक
१३१
होता है। (२) दूसरे वर्ष में जो सचित्त प्राप्त होता है वह प्रवाचक १३२५. राइणिया गीतत्था, अलद्धिया धारयंति पुव्वदिसं। का होता है। (३) जो प्रतीच्छक पूर्व उद्दिष्ट है अथवा पश्चात्
अपहुव्वंत सलक्खण, केवलमेगे दिसाबंधो॥ उद्दिष्ट है, दूसरे वर्ष में जो सचित्त प्राप्त होता है वह सारा प्रवाचक जो साधु रत्नाधिक हैं, गीतार्थ हैं किंतु लब्धिसंपन्न नहीं हैं का होता है। (४) जो शिष्य पूर्ण उद्दिष्ट है अथवा पश्चात् उद्दिष्ट है वे पूर्वदिशा अर्थात् पूर्वाचार्यप्रदत्त दिशा-अनुरत्नाधिक को धारण उसमें जो सचित्त का लाभ होता है वह प्रथम वर्ष में शिष्य के करते हैं। (वे आचार्यपद अथवा उपाध्यायपद प्राप्त नहीं कर होता है। (५) दूसरे संवत्सर में जो सचित्त का लाभ होता है वह सकते।) यदि साधु-परिवार में केवल एक ही साधु आचार्य के पूर्व उद्दिष्ट शिष्य का होता है और (६) पश्चात् उद्दिष्ट में जो लाभ योग्य हो तो उसको दिशाबंध-आचार्यपद पर आरोपित किया जा होता है वह प्रवाचक का होता है। (७) तीसरे संवत्सर में पूर्व- सकता है। पश्चात् उद्दिष्ट शिष्य के जो सचित्त का लाभ होता है, वह सारा १३२६. सीसे य पहुव्वंतं, सव्वेसिं तेसि होति दायव्वा। प्रवाचक का होता है। (८) पहले संवत्सर में पूर्व उद्दिष्ट शिष्या के ___ आपहुप्पंतेसुं पुण, केवलमेगे दिसाबंधो।। जो सचित्त का लाभ होता है वह उसी शिष्या का होता है। (९) यदि शिष्य वर्ग में प्रत्येक साधु लक्षणोपेत हो तो सभी को पश्चात् उद्दिष्ट शिष्या के फिर जो लाभ होता है-वह उसी शिष्या दिशाबंध देना चाहिए। यदि न हो तो जो लक्षणोपेत है केवल उसी का होता है। (१०) दूसरे संवत्सर में पूर्व उद्दिष्ट अथवा पश्चात् एक को दिशाबंध देना चाहिए। उद्दिष्ट शिष्या के जो सचित्त का लाभ होता है वह सारा प्रवाचक १३२७. अच्चित्तं च जहरिहं, दिज्जति तेसुं च बहुसु गीतेसु। का होता है। (११) पहले संवत्सर में पूर्व उद्दिष्ट अथवा पश्चात्
एस विधी अक्खातो, अग्गीतेसुं इमो उ विधी।। उद्दिष्ट प्रतीच्छकी शिष्या के जो सचित्त आदि का लाभ होता है। जो अनेक गीतार्थ पद पर स्थापित हों तो अचित्त-उपकरण वह सारा प्रवाचक का होता है।
आदि यथायोग्य सबको देना चाहिए। यह गीतार्थ के लिए विधि १३२१. जम्हा एते दोसा, दुविहे उ अपक्खिए तु ठवितम्मि। है। अगीतार्थ के प्रति निम्नोक्त विधि है।।
तम्हा उ ठवेयव्वो, कमेणिमेणं तु आयरिओ॥ १३२८. अरिहं व अनिम्माउं, णाउं थेरा भणंति जो ठवितो। इसलिए दो प्रकार के अपाक्षिक अर्थात् श्रुतपक्षरहित तथा
एतं गीतं काउं, देज्जाहि दिसिं अणुदिसिं वा।। प्रव्रज्यापक्षरहित को आचार्य स्थापित करने पर ये सारे दोष उत्पन्न जो साधु आचार्यपद योग्य होने पर अभी तक सूत्र और होते हैं। अतः आचार्य की स्थापना इस क्रम से करनी चाहिए। अर्थ में अनिर्मापित है यह जानकर तत्काल गणधर के रूप में १३२२. एतस्सेगदुगादी, निष्फण्णा तेसि बंधति दिसाओ। स्थापित को कहते हैं-इस मुनि को गीतार्थ बनाकर दिशा अथवा
संपुच्छण-ओलोयण, दाणे मिलितेण दिटुंतो॥ अनुदिशा देना-आचार्य अथवा उपाध्याय बनाना। प्रथम भंगवर्ती को आचार्य पद पर स्थापित करने पर उसके १३२९. सो निम्माविय ठवितो, एक-दो आदि शिष्य निष्पन्न होते हैं। उनको दिशाबंध अर्थात
अच्छति जदि तेण सह ठितो लद्धं । आचार्यत्व,उपाध्यायत्व के रूप में बांध देते हैं, पद देते हैं।
अह न वि चिट्ठति तहियं, संप्रच्छन, अवलोकन, दान, मिलित दो गोपालों का दृष्टांत।
संघाड़ो तो सि दायव्वो।। (विवरण आगे की गाथाओं में।)
जिस गणधर ने साधु को निर्मापित कर आचार्य पद पर १३२३. गीतमगीता बहवो, गीतत्थसलक्खणा उ जे तत्थ। स्थापित कर दिया, वह आचार्य यदि उसके साथ ही रहता है तो
तेसिं दिसाउ दाउं,वितरति सेसे जहरिहं तु॥ अच्छा है। यदि नहीं रहता है तो उसे संघाट-दो साधु और देने
गच्छ में अनेक साधु गीतार्थ और अगीतार्थ होते हैं। उनमें चाहिए। जो लक्षणयुक्त गीतार्थ होते हैं, उनकों दिशा-आचार्य-उपाध्याय १३३०. पेसेति गंतुंव सयं व पुच्छे, पद देकर शेष साधुओं को यथायोग्य वितरण करते हैं।
संबंधमाणो उवधिं च देती। १३२४. मूलायरि राइणिओ, अणुसरिसो तस्स होउवज्झाओ। सज्झंतिया सिं च समल्लिया वि, गीतमगीता सेसा, सज्झिलगा होंति सीसाहा॥
सच्चित्तमेवं न लभे करेंतो॥ मूल आचार्य रात्निक होते हैं। उनके अनुसदृश अनेक जहां वह निर्मापित और स्थापित आचार्य विहरण करता है उपाध्याय होते हैं। शेष साधु जो गीतार्थ और अगीतार्थ होते हैं। वहां वह गणधर वृत्तांतवाहक मुनियों को भेजता है अथवा समयवे उसके साथी शिष्य होते हैं।
समय पर स्वयं जाकर उनका योगक्षेम पूछता है। वह उन शिष्यों
को अपना बनाने के लिए कभी-कभी उपधि देता है। जो स्वाध्याय For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International