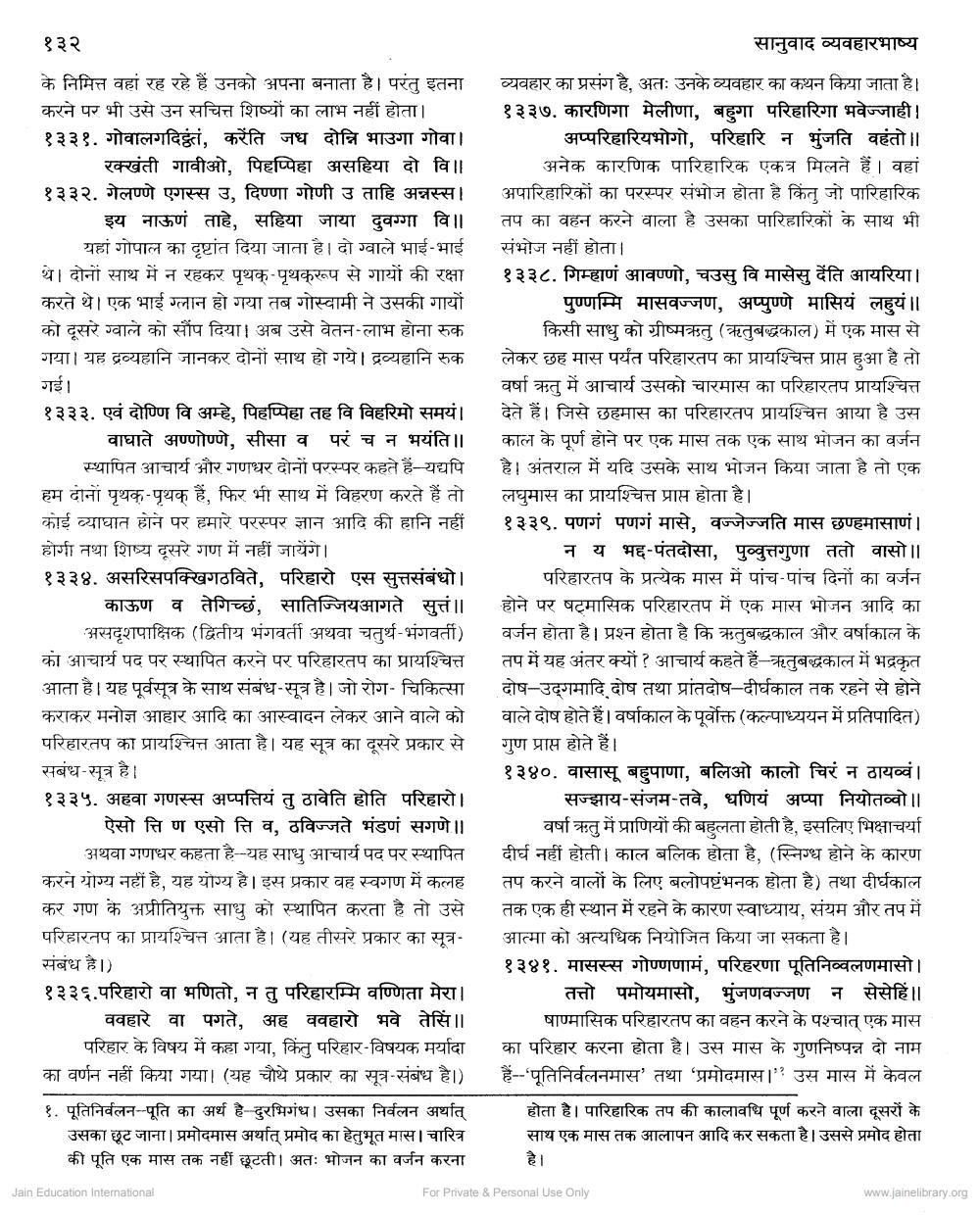________________
सानुवाद व्यवहारभाष्य
१३२ के निमित्त वहां रह रहे हैं उनको अपना बनाता है। परंतु इतना करने पर भी उसे उन सचित्त शिष्यों का लाभ नहीं होता। १३३१. गोवालगदिद्वंतं, करेंति जध दोन्नि भाउगा गोवा।
रक्खंती गावीओ, पिहप्पिहा असहिया दो वि॥ १३३२. गेलण्णे एगस्स उ, दिण्णा गोणी उ ताहि अन्नस्स।
__ इय नाऊणं ताहे, सहिया जाया दुवग्गा वि॥
यहां गोपाल का दृष्टांत दिया जाता है। दो ग्वाले भाई-भाई थे। दोनों साथ में न रहकर पृथक्-पृथकरूप से गायों की रक्षा करते थे। एक भाई ग्लान हो गया तब गोस्वामी ने उसकी गायों को दूसरे ग्वाले को सौंप दिया। अब उसे वेतन-लाभ होना रुक गया। यह द्रव्यहानि जानकर दोनों साथ हो गये। द्रव्यहानि रुक गई। १३३३. एवं दोणि वि अम्हे, पिहप्पिहा तह वि विहरिमो समयं।
वाघाते अण्णोण्णे, सीसा व परं च न भयंति॥
स्थापित आचार्य और गणधर दोनों परस्पर कहते हैं-यद्यपि हम दोनों पृथक-पृथक् हैं, फिर भी साथ में विहरण करते हैं तो कोई व्याघात होने पर हमारे परस्पर ज्ञान आदि की हानि नहीं होगी तथा शिष्य दूसरे गण में नहीं जायेंगे। १३३४. असरिसपक्खिगठविते, परिहारो एस सुत्तसंबंधो।
काऊण व तेगिच्छं, सातिज्जियआगते सुत्तं।
असदृशपाक्षिक (द्वितीय भंगवर्ती अथवा चतुर्थ-भंगवर्ती) का आचार्य पद पर स्थापित करने पर परिहारतप का प्रायश्चित्त आता है। यह पूर्वसूत्र के साथ संबंध-सूत्र है। जो रोग- चिकित्सा कराकर मनोज्ञ आहार आदि का आस्वादन लेकर आने वाले को परिहारतप का प्रायश्चित्त आता है। यह सूत्र का दूसरे प्रकार से सबंध-सूत्र है। १३३५. अहवा गणस्स अप्पत्तियं तु ठावेति होति परिहारो।
ऐसो त्ति ण एसो त्ति व, ठविज्जते भंडणं सगणे॥
अथवा गणधर कहता है-यह साधु आचार्य पद पर स्थापित करने योग्य नहीं है, यह योग्य है। इस प्रकार वह स्वगण में कलह कर गण के अप्रीतियुक्त साधु को स्थापित करता है तो उसे परिहारतप का प्रायश्चित्त आता है। (यह तीसरे प्रकार का सूत्रसंबंध है। १३३६.परिहारो वा भणितो, न तु परिहारम्मि वण्णिता मेरा।
ववहारे वा पगते, अह ववहारो भवे तेसिं।। परिहार के विषय में कहा गया, किंतु परिहार-विषयक मर्यादा का वर्णन नहीं किया गया। (यह चौथे प्रकार का सूत्र-संबंध है।) १. पूतिनिर्वलन--पूति का अर्थ है-दुरभिगंध। उसका निर्वलन अर्थात्
उसका छूट जाना। प्रमोदमास अर्थात् प्रमोद का हेतुभूत मास। चारित्र की पूति एक मास तक नहीं छूटती। अतः भोजन का वर्जन करना
व्यवहार का प्रसंग है, अतः उनके व्यवहार का कथन किया जाता है। १३३७. कारणिगा मेलीणा, बहुगा परिहारिगा भवेज्जाही।
- अप्परिहारियभोगो, परिहारि न भुंजति वहंतो।।
अनेक कारणिक पारिहारिक एकत्र मिलते हैं। वहां अपारिहारिकों का परस्पर संभोज होता है किंतु जो पारिहारिक तप का वहन करने वाला है उसका पारिहारिकों के साथ भी संभोज नहीं होता। १३३८. गिम्हाणं आवण्णो, चउसु वि मासेसु देंति आयरिया।
पुण्णम्मि मासवज्जण, अप्पुण्णे मासियं लहुयं ।। किसी साधु को ग्रीष्मऋतु (ऋतुबद्धकाल) में एक मास से लेकर छह मास पर्यंत परिहारतप का प्रायश्चित्त प्राप्त हुआ है तो वर्षा ऋतु में आचार्य उसको चारमास का परिहारतप प्रायश्चित्त देते हैं। जिसे छहमास का परिहारतप प्रायश्चित्त आया है उस काल के पूर्ण होने पर एक मास तक एक साथ भोजन का वर्जन है। अंतराल में यदि उसके साथ भोजन किया जाता है तो एक लघुमास का प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। १३३९. पणगं पणगं मासे, वज्जेज्जति मास छण्हमासाणं।
न य भद्द-पंतदोसा, पुव्वुत्तगुणा ततो वासो।।
परिहारतप के प्रत्येक मास में पांच-पांच दिनों का वर्जन होने पर षट्मासिक परिहारतप में एक मास भोजन आदि का वर्जन होता है। प्रश्न होता है कि ऋतुबद्धकाल और वर्षाकाल के तप में यह अंतर क्यों ? आचार्य कहते हैं-ऋतुबद्धकाल में भद्रकृत दोष-उद्गमादि दोष तथा प्रांतदोष-दीर्घकाल तक रहने से होने वाले दोष होते हैं। वर्षाकाल के पूर्वोक्त (कल्पाध्ययन में प्रतिपादित) गुण प्राप्त होते हैं। १३४०. वासासू बहुपाणा, बलिओ कालो चिरं न ठायव्वं ।
__ सज्झाय-संजम-तवे, धणियं अप्पा नियोतव्वो।।
वर्षा ऋतु में प्राणियों की बहुलता होती है, इसलिए भिक्षाचर्या दीर्घ नहीं होती। काल बलिक होता है, (स्निग्ध होने के कारण तप करने वालों के लिए बलोपष्टंभनक होता है) तथा दीर्घकाल तक एक ही स्थान में रहने के कारण स्वाध्याय, संयम और तप में आत्मा को अत्यधिक नियोजित किया जा सकता है। १३४१. मासस्स गोण्णणामं, परिहरणा पूतिनिव्वलणमासो।
तत्तो पमोयमासो, भुंजणवज्जण न सेसेहिं।। पाण्मासिक परिहारतप का वहन करने के पश्चात् एक मास का परिहार करना होता है। उस मास के गुणनिष्पन्न दो नाम हैं-- पूतिनिर्वलनमास' तथा 'प्रमोदमास।" उस मास में केवल
होता है। पारिहारिक तप की कालावधि पूर्ण करने वाला दूसरों के साथ एक मास तक आलापन आदि कर सकता है। उससे प्रमोद होता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org