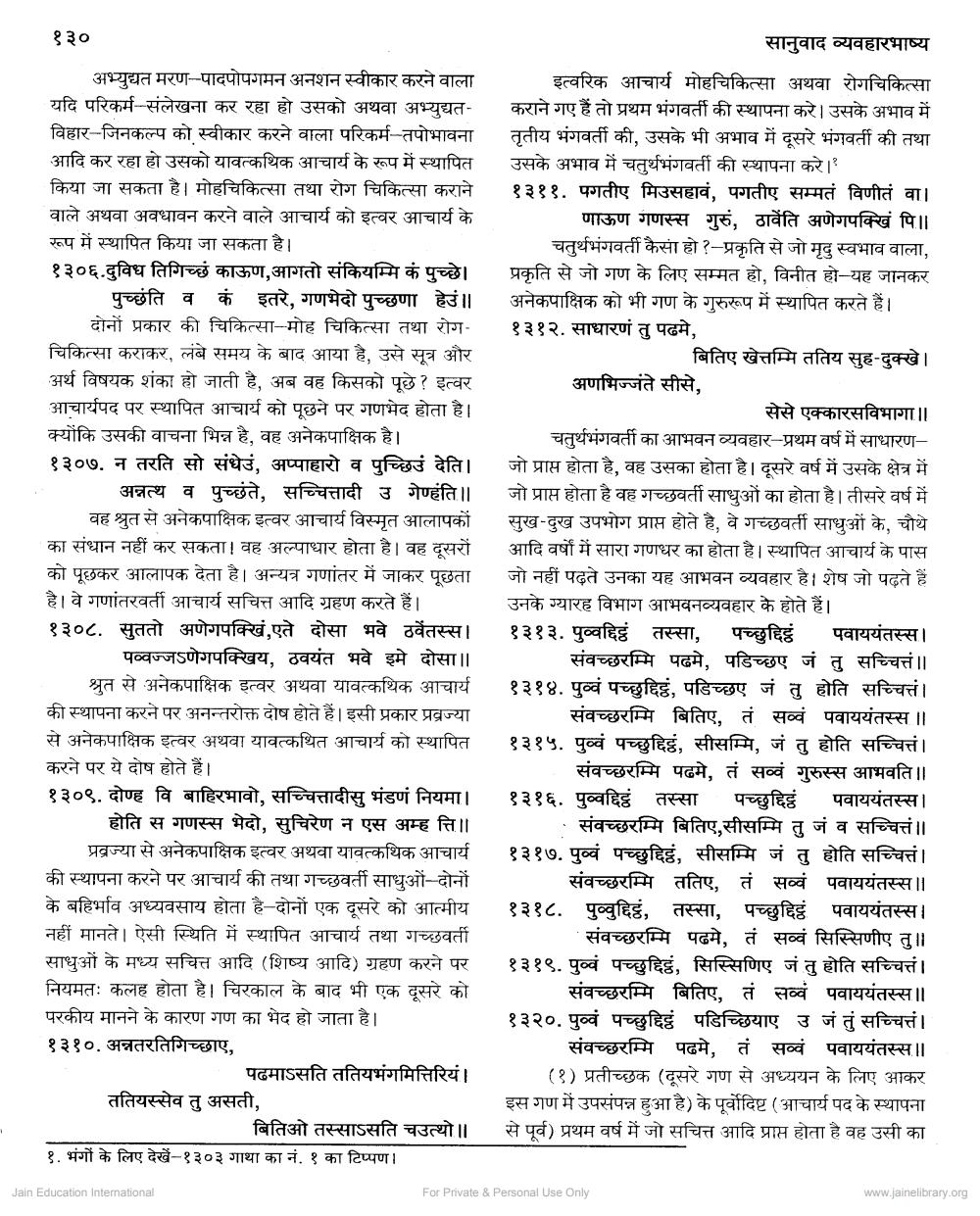________________
१३०
अभ्युद्यत मरण-पादपोपगमन अनशन स्वीकार करने वाला यदि परिकर्म-संलेखना कर रहा हो उसको अथवा अभ्युद्यत- विहार-जिनकल्प को स्वीकार करने वाला परिकर्म-तपोभावना ।
आदि कर रहा हो उसको यावत्कथिक आचार्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मोहचिकित्सा तथा रोग चिकित्सा कराने वाले अथवा अवधावन करने वाले आचार्य को इत्वर आचार्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। १३०६.दुविध तिगिच्छं काऊण,आगतो संकियम्मि कं पुच्छे।
पुच्छंति व कं इतरे, गणभेदो पुच्छणा हेउं॥
दोनों प्रकार की चिकित्सा-मोह चिकित्सा तथा रोग- चिकित्सा कराकर, लंबे समय के बाद आया है, उसे सूत्र और अर्थ विषयक शंका हो जाती है, अब वह किसको पूछे ? इत्वर आचार्यपद पर स्थापित आचार्य को पूछने पर गणभेद होता है। क्योंकि उसकी वाचना भिन्न है, वह अनेकपाक्षिक है। १३०७. न तरति सो संधेलं, अप्पाहारो व पुच्छिउं देति।
अन्नत्थ व पुच्छंते, सच्चित्तादी उ गेण्हति॥ वह श्रुत से अनेकपाक्षिक इत्वर आचार्य विस्मृत आलापकों का संधान नहीं कर सकता। वह अल्पाधार होता है। वह दूसरों को पूछकर आलापक देता है। अन्यत्र गणांतर में जाकर पूछता है। वे गणांतरवर्ती आचार्य सचित्त आदि ग्रहण करते हैं। १३०८. सुततो अणेगपक्खिं,एते दोसा भवे ठवेंतस्स।
पव्वज्जणेगपक्खिय, ठवयंत भवे इमे दोसा।। श्रुत से अनेकपाक्षिक इत्वर अथवा यावत्कथिक आचार्य की स्थापना करने पर अनन्तरोक्त दोष होते हैं। इसी प्रकार प्रव्रज्या से अनेकपाक्षिक इत्वर अथवा यावत्कथित आचार्य को स्थापित करने पर ये दोष होते हैं। १३०९. दोण्ह वि बाहिरभावो, सच्चित्तादीसु भंडणं नियमा।
होति स गणस्स भेदो, सुचिरेण न एस अम्ह ति॥ प्रव्रज्या से अनेकपाक्षिक इत्वर अथवा यावत्कथिक आचार्य की स्थापना करने पर आचार्य की तथा गच्छवर्ती साधुओं-दोनों के बहिर्भाव अध्यवसाय होता है दोनों एक दूसरे को आत्मीय नहीं मानते। ऐसी स्थिति में स्थापित आचार्य तथा गच्छवर्ती साधुओं के मध्य सचित्त आदि (शिष्य आदि) ग्रहण करने पर नियमतः कलह होता है। चिरकाल के बाद भी एक दूसरे को परकीय मानने के कारण गण का भेद हो जाता है। १३१०. अन्नतरतिगिच्छाए,
पढमाऽसति ततियभंगमित्तिरियं। ततियस्सेव तु असती,
बितिओ तस्साऽसति चउत्थो॥ १. भंगों के लिए देखें-१३०३ गाथा का नं. १ का टिप्पण।
सानुवाद व्यवहारभाष्य इत्वरिक आचार्य मोहचिकित्सा अथवा रोगचिकित्सा कराने गए हैं तो प्रथम भंगवर्ती की स्थापना करे। उसके अभाव में तृतीय भंगवर्ती की, उसके भी अभाव में दूसरे भंगवर्ती की तथा उसके अभाव में चतुर्थभंगवर्ती की स्थापना करे। १३११. पगतीए मिउसहावं, पगतीए सम्मतं विणीतं वा।
णाऊण गणस्स गुरूं, ठावेंति अणेगपक्खिं पि॥ चतुर्थभंगवर्ती कैसा हो?-प्रकृति से जो मृदु स्वभाव वाला, प्रकृति से जो गण के लिए सम्मत हो, विनीत हो-यह जानकर अनेकपाक्षिक को भी गण के गुरुरूप में स्थापित करते हैं। १३१२. साधारणं तु पढमे,
बितिए खेत्तम्मि ततिय सुह-दुक्खे। अणभिज्जंते सीसे,
सेसे एक्कारसविभागा॥ चतुर्थभंगवर्ती का आभवन व्यवहार-प्रथम वर्ष में साधारणजो प्राप्त होता है, वह उसका होता है। दूसरे वर्ष में उसके क्षेत्र में जो प्राप्त होता है वह गच्छवर्ती साधुओं का होता है। तीसरे वर्ष में सुख-दुख उपभोग प्राप्त होते है, वे गच्छवर्ती साधुओं के, चौथे आदि वर्षों में सारा गणधर का होता है। स्थापित आचार्य के पास जो नहीं पढ़ते उनका यह आभवन व्यवहार है। शेष जो पढ़ते हैं उनके ग्यारह विभाग आभवनव्यवहार के होते हैं। १३१३. पुव्वद्दिढें तस्सा, पच्छुद्दिटुं पवाययंतस्स।
संवच्छरम्मि पढमे, पडिच्छए जं तु सच्चित्तं ।। १३१४. पुव्वं पच्छुद्दिटुं, पडिच्छए जं तु होति सच्चित्तं।
संवच्छरम्मि बितिए, तं सव्वं पवाययंतस्स ।। १३१५. पुव्वं पच्छुद्दिठं, सीसम्मि, जं तु होति सच्चित्तं ।
संवच्छरम्मि पढमे, तं सव्वं गुरुस्स आभवति ।। १३१६. पुव्वद्दिटुं तस्सा पच्छुद्दिष्टुं पवाययंतस्स।
• संवच्छरम्मि बितिए,सीसम्मि तु जं व सच्चित्तं॥ १३१७. पुव्वं पच्छुद्दिष्ठं, सीसम्मि जं तु होति सच्चित्तं।
संवच्छरम्मि ततिए, तं सव्वं पवाययंतस्स। १३१८. पुव्वुद्दिटुं, तस्सा, पच्छुद्दिटुं पवाययंतस्स।
संवच्छरम्मि पढमे, तं सव्वं सिस्सिणीए तु॥ १३१९. पुव्वं पच्छुद्दिटुं, सिस्सिणिए जंतु होति सच्चित्तं।
संवच्छरम्मि बितिए, तं सव्वं पवाययंतस्स। १३२०. पुव्वं पच्छुद्दिष्टुं पडिच्छियाए उ जं तुं सच्चित्तं।
संवच्छरम्मि पढमे, तं सव्वं पवाययंतस्स। (१) प्रतीच्छक (दूसरे गण से अध्ययन के लिए आकर इस गण में उपसंपन्न हुआ है) के पूर्वोदिष्ट (आचार्य पद के स्थापना से पूर्व) प्रथम वर्ष में जो सचित्त आदि प्राप्त होता है वह उसी का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org