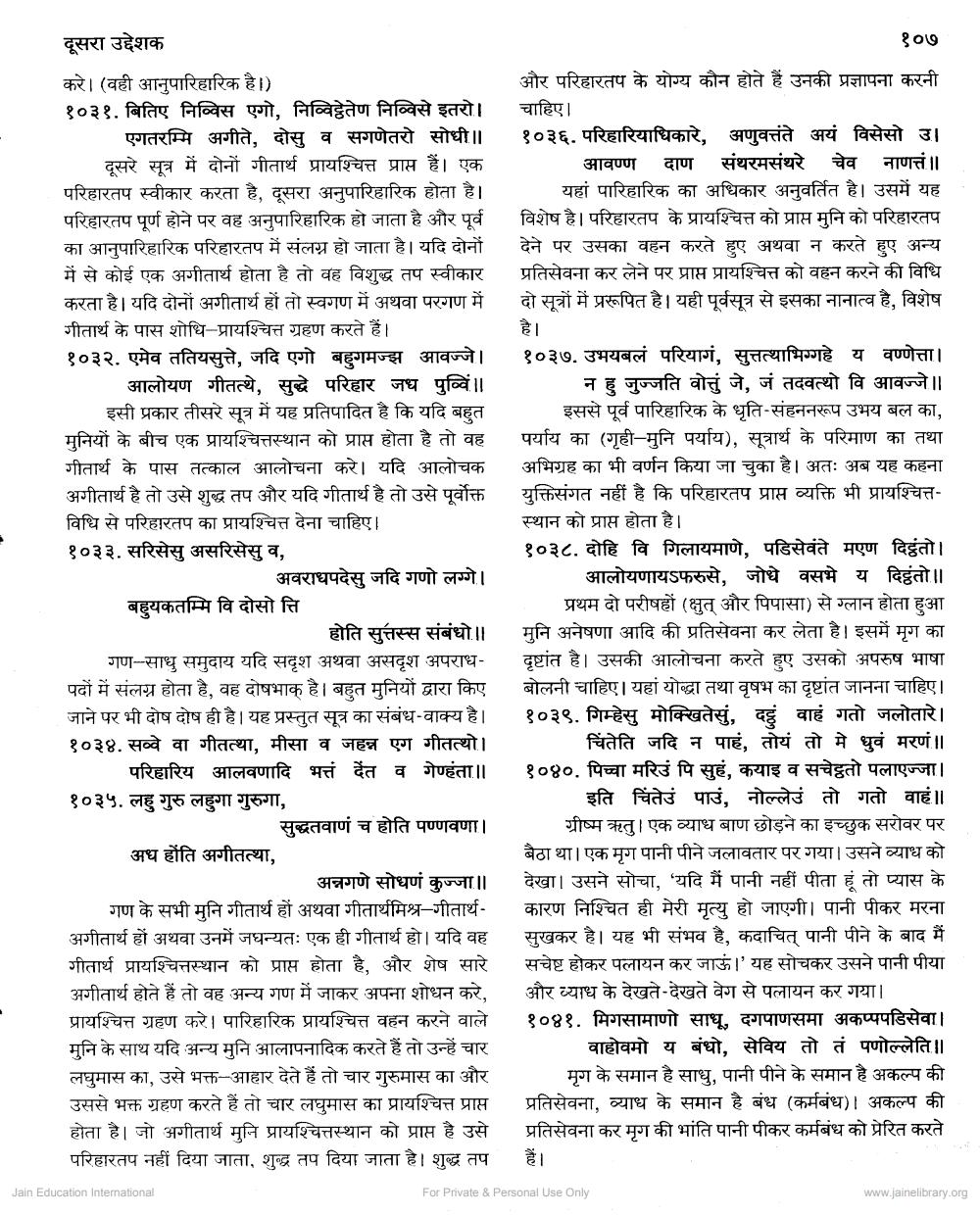________________
दूसरा उद्देशक
करे। (वही आनुपारिहारिक है ।) १०३१. बितिए निव्विस एगो, निव्विट्ठेतेण निव्विसे इतरो । एगतरम्मि अगीते, दोसु व सगणेतरो सोधी । दूसरे सूत्र में दोनों गीतार्थ प्रायश्चित्त प्राप्त हैं। एक परिहारतप स्वीकार करता है, दूसरा अनुपारिहारिक होता है। परिहारतप पूर्ण होने पर वह अनुपारिहारिक हो जाता है और पूर्व का आनुपारिहारिक परिहारतप में संलग्न हो जाता है। यदि दोनों में से कोई एक अगीतार्थ होता है तो वह विशुद्ध तप स्वीकार करता है। यदि दोनों अगीतार्थ हों तो स्वगण में अथवा परगण में गीतार्थ के पास शोधि- प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैं। १०३२. एमेव ततियसुत्ते, जदि एगो बहुगमज्झ आवज्जे । आलोयण गीतत्थे, सुद्धे परिहार जध पुव्विं ॥ इसी प्रकार तीसरे सूत्र में यह प्रतिपादित है कि यदि बहुत मुनियों के बीच एक प्रायश्चित्तस्थान को प्राप्त होता है तो वह गीतार्थ के पास तत्काल आलोचना करे। यदि आलोचक अगीतार्थ है तो उसे शुद्ध तप और यदि गीतार्थ है तो उसे पूर्वोक्त विधि से परिहारतप का प्रायश्चित्त देना चाहिए। १०३३. सरिसेसु असरिसेसु व,
अवराधपदेसु जदि गणो लग्गे । बहुकतम्मि वि दोसो ति
होति सुत्तस्स संबंधो । गण- साधु समुदाय यदि सदृश अथवा असदृश अपराधपदों में संलग्न होता है, वह दोषभाक् है । बहुत मुनियों द्वारा किए जाने पर भी दोष दोष ही है। यह प्रस्तुत सूत्र का संबंध वाक्य है। १०३४. सव्वे वा गीतत्था, मीसा व जहन्न एग गीतत्थो । परिहारिय आलवणादि भत्तं देंत व गेण्हंता ।। १०३५. लहु गुरु लहुगा गुरुगा,
सुद्धतवाणं च होति पण्णवणा ।
अध होंति अगीतत्था,
अन्नगणे सोधणं कुज्जा ॥
गण के सभी मुनि गीतार्थ हों अथवा गीतार्थमिश्र - गीतार्थ - अगीतार्थ हों अथवा उनमें जघन्यतः एक ही गीतार्थ हो । यदि वह गीतार्थ प्रायश्चित्तस्थान को प्राप्त होता है, और शेष सारे अगीतार्थ होते हैं तो वह अन्य गण में जाकर अपना शोधन करे, प्रायश्चित्त ग्रहण करे। पारिहारिक प्रायश्चित्त वहन करने वाले मुनि के साथ यदि अन्य मुनि आलापनादिक करते हैं तो उन्हें चार लघुमास का, उसे भक्त आहार देते हैं तो चार गुरुमास का और उससे भक्त ग्रहण करते हैं तो चार लघुमास का प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। जो अगीतार्थ मुनि प्रायश्चित्तस्थान को प्राप्त है उसे परिहारतप नहीं दिया जाता, शुद्ध तप दिया जाता है। शुद्ध तप
Jain Education International
१०७ और परिहारतप के योग्य कौन होते हैं उनकी प्रज्ञापना करनी चाहिए।
१०३६. परिहारियाधिकारे, अणुवत्तंते अयं विसेसो उ । आवण्ण दाण संथरमसंथरे चेव नाणत्तं ॥ यहां पारिहारिक का अधिकार अनुवर्तित है। उसमें यह विशेष है। परिहारतप के प्रायश्चित्त को प्राप्त मुनि को परिहार प देने पर उसका वहन करते हुए अथवा न करते हुए अन्य प्रतिसेवना कर लेने पर प्राप्त प्रायश्चित्त को वहन करने की विधि दो सूत्रों में प्ररूपित है। यही पूर्वसूत्र से इसका नानात्व है, विशेष है।
१०३७. उभयबलं परियागं, सुत्तत्थाभिग्गहे य वण्णेत्ता ।
न हु जुज्जति वोत्तुं जे, जं तदवत्थो वि आवज्जे ॥ इससे पूर्व पारिहारिक के धृति - संहननरूप उभय बल का, पर्याय का (गृही - मुनि पर्याय), सूत्रार्थ के परिमाण का तथा अभिग्रह का भी वर्णन किया जा चुका है। अतः अब यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि परिहारतप प्राप्त व्यक्ति भी प्रायश्चित्तस्थान को प्राप्त होता है।
१०३८. दोहि वि गिलायमाणे, पडिसेवंते मएण दिट्टंतो । आलोयणायऽफरुसे, जोधे वसभे य दिट्ठतो ॥
प्रथम दो परीषों (क्षुत् और पिपासा) से ग्लान होता हुआ मुनि अनेषणा आदि की प्रतिसेवना कर लेता है। इसमें मृग का दृष्टांत है। उसकी आलोचना करते हुए उसको अपरुष भाषा बोलनी चाहिए। यहां योद्धा तथा वृषभ का दृष्टांत जानना चाहिए। १०३९. गिम्हेसु मोक्खितेसुं, दडुं वाहं गतो जलोतारे ।
चिंतेति जदि न पाहं, तोयं तो मे धुवं मरणं ॥ १०४०. पिच्चा मरिउं पि सुहं, कयाइ व सचेट्ठतो पलाएज्जा । इति चिंतेउं पाउं, नोल्लेउं तो गतो वाहं ॥ ग्रीष्म ऋतु । एक व्याध बाण छोड़ने का इच्छुक सरोवर पर बैठा था। एक मृग पानी पीने जलावतार पर गया। उसने व्याध को देखा। उसने सोचा, ‘यदि मैं पानी नहीं पीता हूं तो प्यास के कारण निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। पानी पीकर मरना सुखकर है। यह भी संभव है, कदाचित् पानी पीने के बाद मैं सचेष्ट होकर पलायन कर जाऊं।' यह सोचकर उसने पानी पीया और व्याध के देखते-देखते वेग से पलायन कर गया। १०४१. मिगसामाणो साधू, दगपाणसमा अकप्पपडिसेवा ।
वाहोमो य बंधो, सेविय तो तं पणोल्लेति । मृग के समान है साधु, पानी पीने के समान है अकल्प की प्रतिसेवना, व्याध के समान है बंध (कर्मबंध) । अकल्प की प्रतिसेवना कर मृग की भांति पानी पीकर कर्मबंध को प्रेरित करते हैं।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org