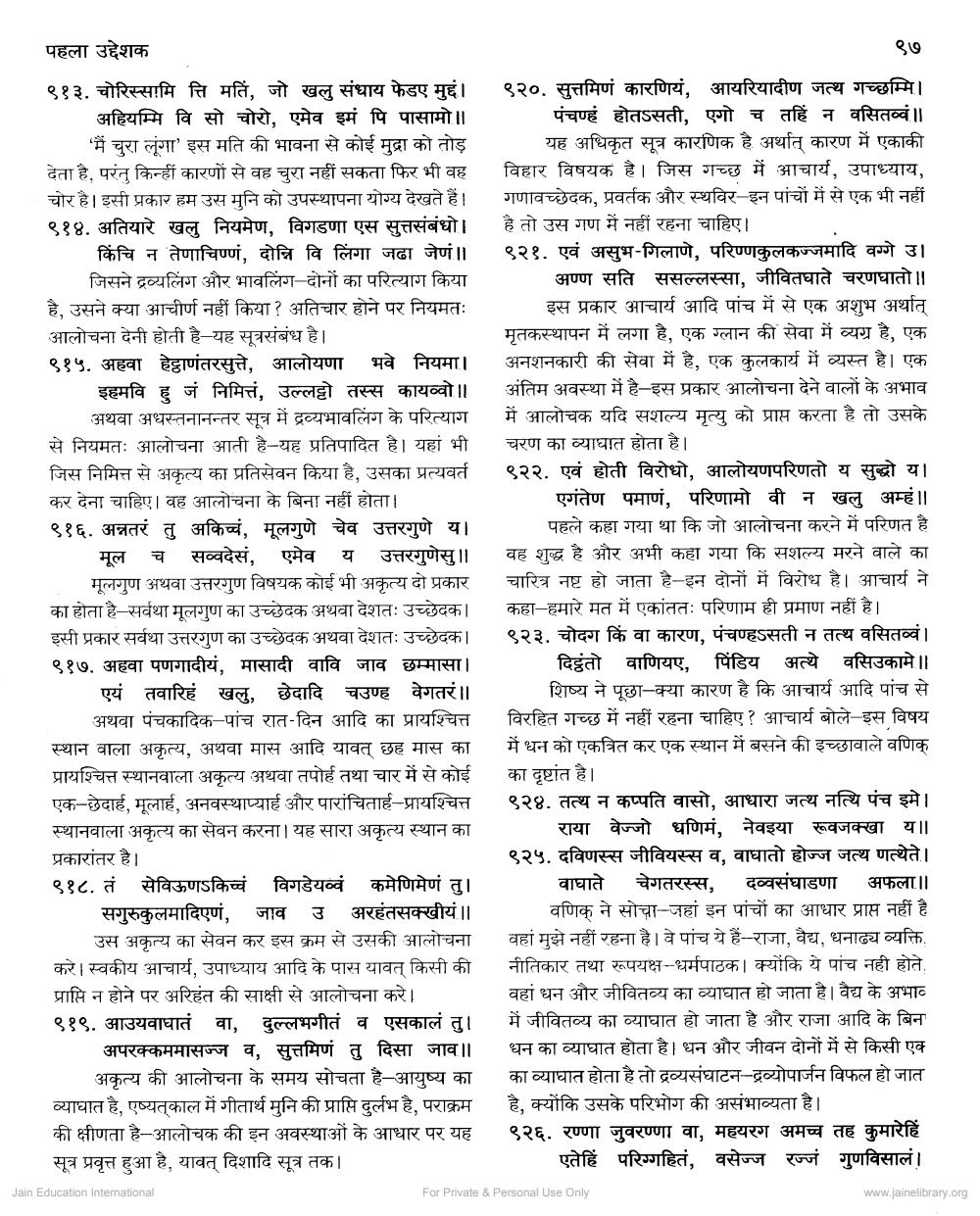________________
पहला उद्देशक
९७
९१३. चोरिस्सामि त्ति मतिं, जो खलु संधाय फेडए मुई। ९२०. सुत्तमिणं कारणियं, आयरियादीण जत्थ गच्छम्मि।
अहियम्मि वि सो चोरो, एमेव इमं पि पासामो॥ पंचण्हं होतऽसती, एगो च तहिं न वसितव्वं ।। 'मैं चुरा लूंगा' इस मति की भावना से कोई मुद्रा को तोड़ यह अधिकृत सूत्र कारणिक है अर्थात् कारण में एकाकी देता है, परंतु किन्हीं कारणों से वह चुरा नहीं सकता फिर भी वह विहार विषयक है। जिस गच्छ में आचार्य, उपाध्याय, चोर है। इसी प्रकार हम उस मुनि को उपस्थापना योग्य देखते हैं। गणावच्छेदक, प्रवर्तक और स्थविर-इन पांचों में से एक भी नहीं ९१४. अतियारे खलु नियमेण, विगडणा एस सुत्तसंबंधो। है तो उस गण में नहीं रहना चाहिए।
किंचि न तेणाचिण्णं, दोन्नि वि लिंगा जढा जेणं॥ ९२१. एवं असुभ-गिलाणे, परिण्णकुलकज्जमादि वग्गे उ। जिसने द्रव्यलिंग और भावलिंग-दोनों का परित्याग किया
अण्ण सति ससल्लस्सा, जीवितघाते चरणघातो।। है, उसने क्या आचीर्ण नहीं किया? अतिचार होने पर नियमतः इस प्रकार आचार्य आदि पांच में से एक अशुभ अर्थात् आलोचना देनी होती है-यह सूत्रसंबंध है।
मृतकस्थापन में लगा है, एक ग्लान की सेवा में व्यग्र है, एक ९१५. अहवा हेट्ठाणंतरसुत्ते, आलोयणा भवे नियमा। अनशनकारी की सेवा में है, एक कुलकार्य में व्यस्त है। एक
इहमवि हु जं निमित्तं, उल्लट्टो तस्स कायव्वो।।। अंतिम अवस्था में है-इस प्रकार आलोचना देने वालों के अभाव
अथवा अधस्तनानन्तर सूत्र में द्रव्यभावलिंग के परित्याग में आलोचक यदि सशल्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके से नियमतः आलोचना आती है-यह प्रतिपादित है। यहां भी चरण का व्याघात होता है। जिस निमित्त से अकृत्य का प्रतिसेवन किया है, उसका प्रत्यवर्त ९२२. एवं होती विरोधो, आलोयणपरिणतो य सुद्धो य। कर देना चाहिए। वह आलोचना के बिना नहीं होता।
____एगतेण पमाणं, परिणामो वी न खलु अम्हं।। ९१६. अन्नतरं तु अकिच्चं, मूलगुणे चेव उत्तरगुणे य। पहले कहा गया था कि जो आलोचना करने में परिणत है
मूल च सव्वदेस, एमेव य उत्तरगुणेसु॥ वह शुद्ध है और अभी कहा गया कि सशल्य मरने वाले का
मूलगुण अथवा उत्तरगुण विषयक कोई भी अकृत्य दो प्रकार चारित्र नष्ट हो जाता है-इन दोनों में विरोध है। आचार्य ने का होता है सर्वथा मूलगुण का उच्छेदक अथवा देशतः उच्छेदक। कहा-हमारे मत में एकांततः परिणाम ही प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार सर्वथा उत्तरगुण का उच्छेदक अथवा देशतः उच्छेदक। ९२३. चोदग किं वा कारण, पंचण्हऽसती न तत्थ वसितव्वं । ९१७. अहवा पणगादीयं, मासादी वावि जाव छम्मासा। दिद्रुतो वाणियए, पिंडिय अत्थे वसिउकामे।
एयं तवारिहं खलु, छेदादि चउण्ह वेगतरं।। शिष्य ने पूछा-क्या कारण है कि आचार्य आदि पांच से
अथवा पंचकादिक-पांच रात-दिन आदि का प्रायश्चित्त विरहित गच्छ में नहीं रहना चाहिए? आचार्य बोले- इस विषय स्थान वाला अकृत्य, अथवा मास आदि यावत् छह मास का में धन को एकत्रित कर एक स्थान में बसने की इच्छावाले वणिक् प्रायश्चित्त स्थानवाला अकृत्य अथवा तपोर्ह तथा चार में से कोई का दृष्टांत है। एक-छेदाई, मूलाई, अनवस्थाप्यारी और पारांचितार्ह-प्रायश्चित्त ९२४. तत्थ न कप्पति वासो, आधारा जत्थ नत्थि पंच इमे। स्थानवाला अकृत्य का सेवन करना। यह सारा अकृत्य स्थान का
राया वेज्जो धणिमं, नेवइया रूवजक्खा य॥ प्रकारांतर है।
९२५. दविणस्स जीवियस्स व, वाघातो होज्ज जत्थ णत्थेते। ९१८. तं सेविऊण किच्चं विगडेयव्वं कमेणिमेणं तु। वाघाते चेगतरस्स, दव्वसंघाडणा अफला॥
सगुरुकुलमादिएणं, जाव उ अरहंतसक्खीयं ।। वणिक् ने सोचा-जहां इन पांचों का आधार प्राप्त नहीं है
उस अकृत्य का सेवन कर इस क्रम से उसकी आलोचना वहां मुझे नहीं रहना है। वे पांच ये हैं-राजा, वैद्य, धनाढ्य व्यक्ति करे। स्वकीय आचार्य, उपाध्याय आदि के पास यावत् किसी की नीतिकार तथा रूपयक्ष-धर्मपाठक। क्योंकि ये पांच नही होते. प्राप्ति न होने पर अरिहंत की साक्षी से आलोचना करे।
वहां धन और जीवितव्य का व्याघात हो जाता है। वैद्य के अभाव ९१९. आउयवाघातं वा, दुल्लभगीतं व एसकालं तु। में जीवितव्य का व्याघात हो जाता है और राजा आदि के बिन
अपरक्कममासज्ज व, सुत्तमिणं तु दिसा जाव॥ धन का व्याघात होता है। धन और जीवन दोनों में से किसी एक
अकृत्य की आलोचना के समय सोचता है-आयुष्य का का व्याघात होता है तो द्रव्यसंघाटन-द्रव्योपार्जन विफल हो जात व्याघात है, एष्यत्काल में गीतार्थ मुनि की प्राप्ति दुर्लभ है, पराक्रम है, क्योंकि उसके परिभोग की असंभाव्यता है। की क्षीणता है-आलोचक की इन अवस्थाओं के आधार पर यह ९२६. रण्णा जुवरण्णा वा, महयरग अमच्च तह कुमारेहिं सूत्र प्रवृत्त हुआ है, यावत् दिशादि सूत्र तक।
एतेहिं परिग्गहितं, वसेज्ज रज्जं गुणविसालं। Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org