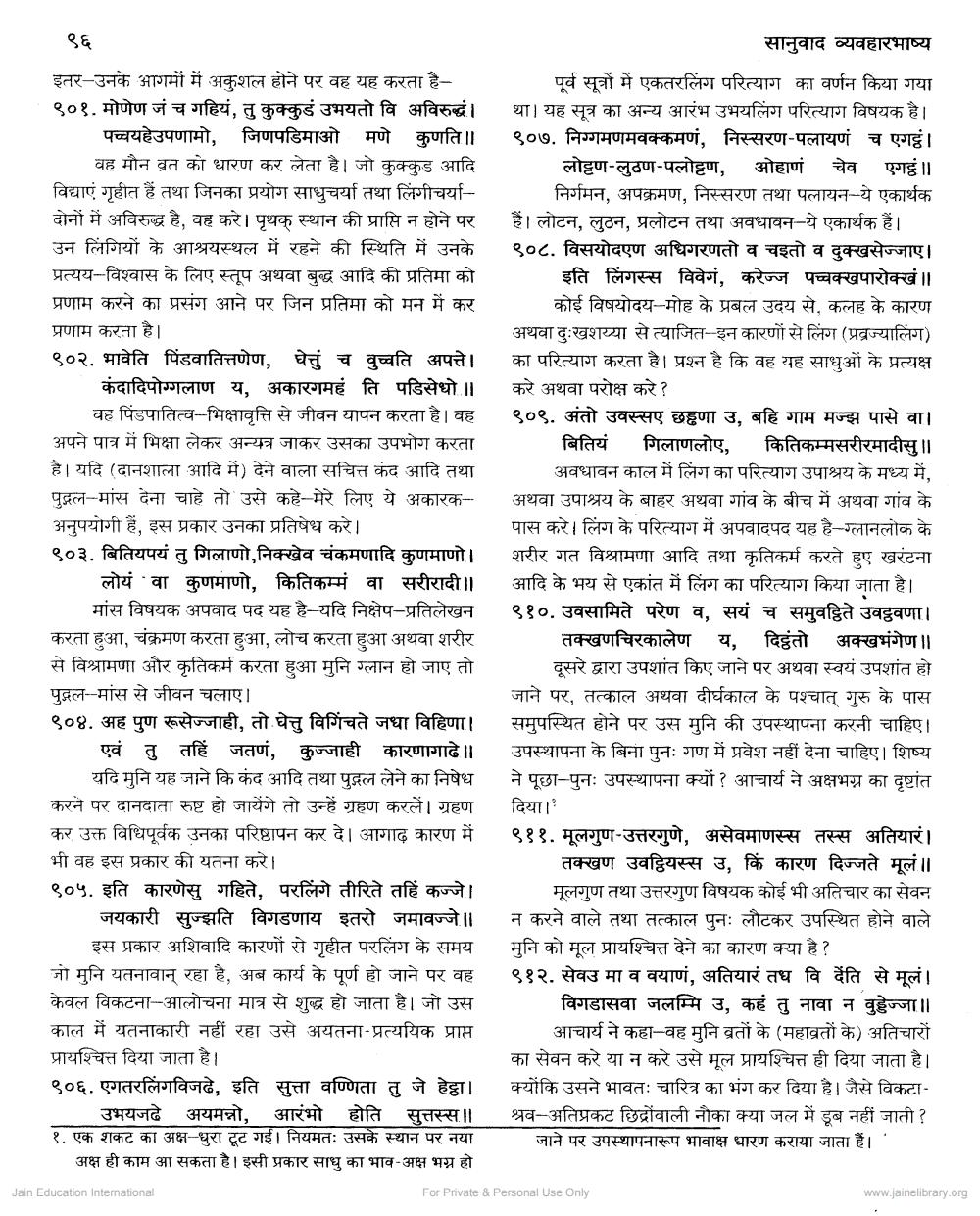________________
९६
3
इतर- उनके आगमों में अकुशल होने पर वह यह करता है९०१. मोणेण जं च गहियं तु कुक्कुडं उभयतो वि अविरुद्धं । पच्चयहेउपणामो, जिणपडिमाओ मणे कुणति ॥ वह मौन व्रत को धारण कर लेता है। जो कुक्कुड आदि विद्याएं गृहीत हैं तथा जिनका प्रयोग साधुचर्या तथा लिंगीचर्यादोनों में अविरुद्ध है, वह करे | पृथक् स्थान की प्राप्ति न होने पर उन लिंगियों के आश्रयस्थल में रहने की स्थिति में उनके प्रत्यय - विश्वास के लिए स्तूप अथवा बुद्ध आदि की प्रतिमा को प्रणाम करने का प्रसंग आने पर जिन प्रतिमा को मन में कर प्रणाम करता है।
९०२. भावेति पिंडवातित्तणेण घेतुं च बुच्चति अपत्ते । कंदादिपोग्गलाण य, अकारगमहं ति पडिसेधो ॥ वह पिंडपातित्व- भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता है। वह अपने पात्र में भिक्षा लेकर अन्यत्र जाकर उसका उपभोग करता है। यदि (दानशाला आदि में) देने वाला सचित्त कंद आदि तथा पुद्गल - मांस देना चाहे तो उसे कहे मेरे लिए ये अकारकअनुपयोगी हैं, इस प्रकार उनका प्रतिषेध करे । ९०३. वितियपयं तु गिलाणो, निक्खेव चंकमणादि कुणमाणो ।
लोयं वा कुणमाणो, कितिकम्मं वा सरीरादी ॥ मांस विषयक अपवाद पद यह है-यदि निक्षेप प्रतिलेखन करता हुआ, चंक्रमण करता हुआ, लोच करता हुआ अथवा शरीर से विश्रामणा और कृतिकर्म करता हुआ मुनि ग्लान हो जाए तो पुत्रल-मांस से जीवन चलाए।
९०४. अह पुण रूसेज्जाही, तो घेत्तु विगिंचते जधा विहिणा । एवं तु तहिं जतणं, कुज्जाही कारणागाढे ॥ यदि मुनि यह जाने कि कंद आदि तथा पुद्गल लेने का निषेध करने पर दानदाता रुष्ट हो जायेंगे तो उन्हें ग्रहण करलें । ग्रहण कर उक्त विधिपूर्वक उनका परिष्ठापन कर दे। आगाढ़ कारण में भी वह इस प्रकार की यतना करे।
९०५ इति कारणेसु गहिते, परलिंगे तीरिते तहिं कज्जे
जयकारी सुज्झति विगडणाय इतरो जमावज्जे ॥ इस प्रकार अशिवादि कारणों से गृहीत परलिंग के समय जो मुनि यतनावान् रहा है, अब कार्य के पूर्ण हो जाने पर वह केवल विकटना-आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाता है। जो उस काल में यतनाकारी नहीं रहा उसे अयतना- प्रत्ययिक प्राप्त प्रायश्चित्त दिया जाता है।
९०६. एगतरलिंगविजढे इति सुत्ता वण्णिता तु जे हेट्ठा । उभयजढे अयमन्नो, आरंभो होति सुत्तस्स ॥ १. एक शकट का अक्ष-धुरा टूट गई। नियमतः उसके स्थान पर नया अक्ष ही काम आ सकता है। इसी प्रकार साधु का भाव अक्ष भग्न हो
-
Jain Education International
सानुवाद व्यवहारभाष्य
पूर्व सूत्रों में एकतरलिंग परित्याग का वर्णन किया गया था। यह सूत्र का अन्य आरंभ उभयलिंग परित्याग विषयक है। ९०७. निग्गमणमवक्कमणं, निस्सरण पलायणं च एगई।
लोट्टण - लुठण- पलोट्टण, ओहाणं चेव एग ॥ निर्गमन, अपक्रमण, निस्सरण तथा पलायन-ये एकार्थक हैं लोटन, लुठन, प्रलोटन तथा अवधावन-ये एकार्थक हैं। ९०८. विसयोदपण अधिगरणतो व चइतो व दुक्खसेज्जाए।
इति लिंगस्स विवेगं, करेज्ज पच्चक्खपारोक्खं ॥ कोई विषयोदय-मोह के प्रबल उदय से, कलह के कारण अथवा दुःखशय्या से त्याजित- इन कारणों से लिंग (प्रव्रज्यालिंग) का परित्याग करता है। प्रश्न है कि वह यह साधुओं के प्रत्यक्ष करे अथवा परोक्ष करे ?
९०९. अंतो उवस्सए छहुणा उ, बहि गाम मज्झ पासे वा । बिलियं गिलाणलोए, कितिकम्मसरीरमादीसु ॥ अवधावन काल में लिंग का परित्याग उपाश्रय के मध्य में, अथवा उपाश्रय के बाहर अथवा गांव के बीच में अथवा गांव के पास करे। लिंग के परित्याग में अपवादपद यह है-ग्लानलोक के शरीर गत विश्रामणा आदि तथा कृतिकर्म करते हुए खरंटना आदि के भय से एकांत में लिंग का परित्याग किया जाता है। ९१०. उवसामिते परेण व, सयं च समुवट्ठिते उवट्ठवणा ।
तक्खणचिरकालेण य, दिवंतो अक्खभंगेण ॥
दूसरे द्वारा उपशांत किए जाने पर अथवा स्वयं उपशांत हो जाने पर, तत्काल अथवा दीर्घकाल के पश्चात् गुरु के पास समुपस्थित होने पर उस मुनि की उपस्थापना करनी चाहिए। उपस्थापना के बिना पुनः गण में प्रवेश नहीं देना चाहिए। शिष्य ने पूछा–पुनः उपस्थापना क्यों ? आचार्य ने अक्षभग्न का दृष्टांत दिया । "
९११. मूलगुण- उत्तरगुणे, असेवमाणस्स तस्स अतियारं ।
तक्खण उवट्ठियस्स उ, किं कारण दिज्जते मूलं ॥ मूलगुण तथा उत्तरगुण विषयक कोई भी अतिचार का सेवन न करने वाले तथा तत्काल पुनः लौटकर उपस्थित होने वाले नको मूल प्रायश्चित्त देने का कारण क्या है ? ९१२. सेवउ मा व वयाणं, अतियारं तध वि देंति से मूलं ।
विगडासवा जलम्मि उ कहं तु नावा न बुझेज्जा ॥ आचार्य ने कहा- वह मुनि व्रत के महाव्रतों के) अतिचारों का सेवन करे या न करे उसे मूल प्रायश्चित्त ही दिया जाता है। क्योंकि उसने भावतः चारित्र का भंग कर दिया है। जैसे विकटाश्रव-अतिप्रकट छिद्रोंवाली नौका क्या जल में डूब नहीं जाती ? जाने पर उपस्थापनारूप भावाक्ष धारण कराया जाता हैं।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org