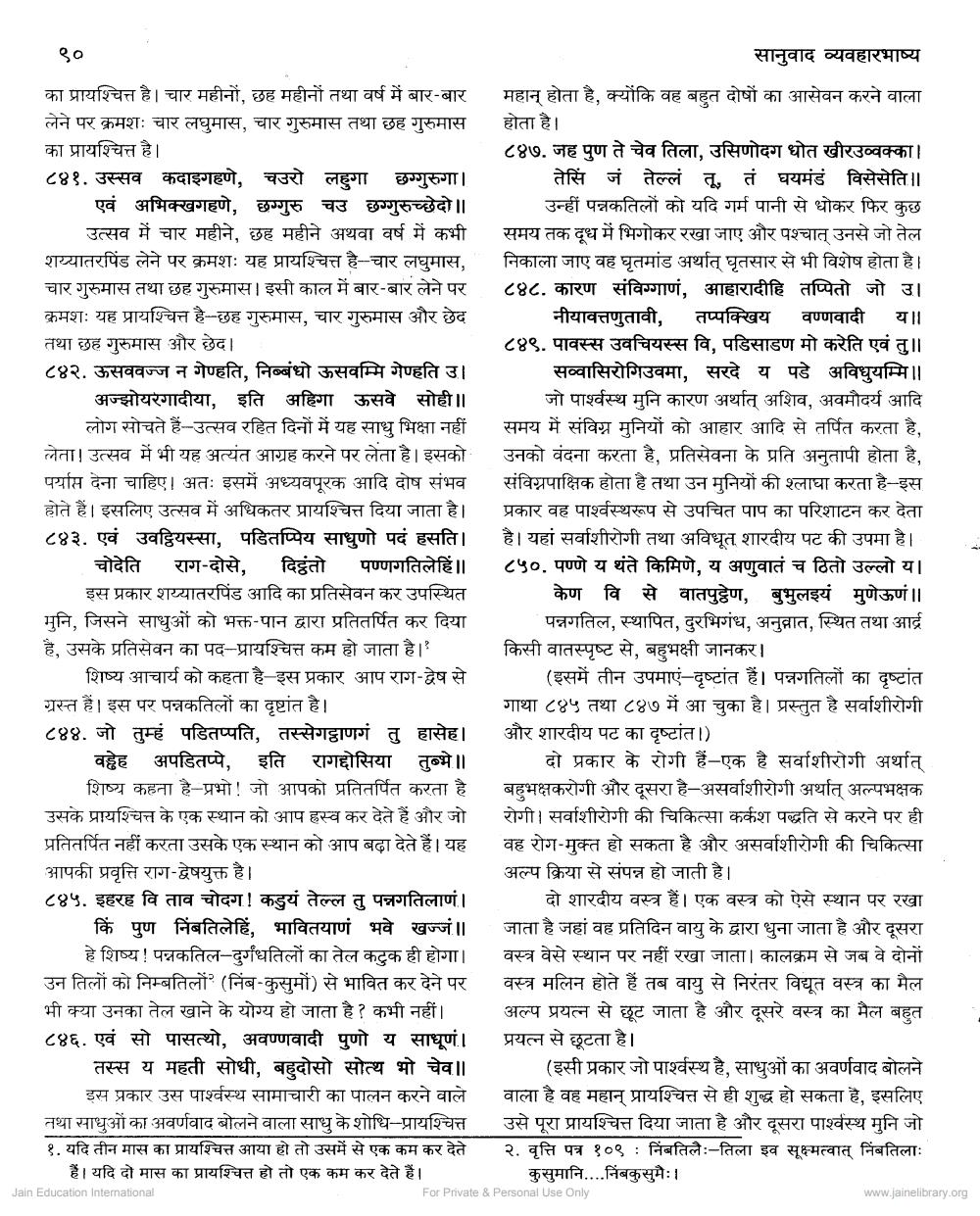________________
९०
का प्रायश्चित्त है। चार महीनों, छह महीनों तथा वर्ष में बार-बार लेने पर क्रमशः चार लघुमास, चार गुरुमास तथा छह गुरुमास का प्रायश्चित्त है। ८४१. उस्सव कदाइगहणे, चउरो लहुगा छग्गुरुगा।
एवं अभिक्खगहणे, छग्गुरु चउ छग्गुरुच्छेदो।
उत्सव में चार महीने, छह महीने अथवा वर्ष में कभी शय्यातरपिंड लेने पर क्रमशः यह प्रायश्चित्त है-चार लघुमास, चार गुरुमास तथा छह गुरुमास। इसी काल में बार-बार लेने पर क्रमशः यह प्रायश्चित्त है-छह गुरुमास, चार गुरुमास और छेद तथा छह गुरुमास और छेद। ८४२. ऊसववज्ज न गेण्हति, निब्बंधो ऊसवम्मि गेण्हति उ।
अज्झोयरगादीया, इति अहिगा ऊसवे सोही।।
लोग सोचते हैं-उत्सव रहित दिनों में यह साधु भिक्षा नहीं लेता। उत्सव में भी यह अत्यंत आग्रह करने पर लेता है। इसको पर्याप्त देना चाहिए। अतः इसमें अध्यवपूरक आदि दोष संभव होते हैं। इसलिए उत्सव में अधिकतर प्रायश्चित्त दिया जाता है। ८४३. एवं उवट्ठियस्सा, पडितप्पिय साधुणो पदं हसति।
चोदेति राग-दोसे, दिर्सेतो पण्णगतिलेहिं॥
इस प्रकार शय्यातरपिंड आदि का प्रतिसेवन कर उपस्थित मुनि, जिसने साधुओं को भक्त-पान द्वारा प्रतितर्पित कर दिया है, उसके प्रतिसेवन का पद-प्रायश्चित्त कम हो जाता है।
शिष्य आचार्य को कहता है इस प्रकार आप राग-द्वेष से ग्रस्त हैं। इस पर पन्नकतिलों का दृष्टांत है। ८४४. जो तुम्हं पडितप्पति, तस्सेगट्ठाणगं तु हासेह।
वड्ढेह अपडितप्पे, इति रागद्दोसिया तुब्भे॥
शिष्य कहता है-प्रभो! जो आपको प्रतितर्पित करता है उसके प्रायश्चित्त के एक स्थान को आप ह्रस्व कर देते हैं और जो प्रतितर्पित नहीं करता उसके एक स्थान को आप बढ़ा देते हैं। यह आपकी प्रवृत्ति राग-द्वेषयुक्त है। ८४५. इहरह वि ताव चोदग! कडुयं तेल्ल तु पन्नगतिलाणं।
किं पुण निंबतिलेहिं, भावितयाणं भवे खज्जं॥
हे शिष्य ! पन्नकतिल-दुर्गंधतिलों का तेल कटुक ही होगा। उन तिलों को निम्बतिलों (निंब-कुसुमों) से भावित कर देने पर भी क्या उनका तेल खाने के योग्य हो जाता है ? कभी नहीं। ८४६. एवं सो पासत्थो, अवण्णवादी पुणो य साधूणं।
तस्स य महती सोधी, बहुदोसो सोत्थ भो चेव॥
इस प्रकार उस पार्श्वस्थ सामाचारी का पालन करने वाले तथा साधुओं का अवर्णवाद बोलने वाला साधु के शोधि-प्रायश्चित्त १. यदि तीन मास का प्रायश्चित्त आया हो तो उसमें से एक कम कर देते
हैं। यदि दो मास का प्रायश्चित्त हो तो एक कम कर देते हैं।
सानुवाद व्यवहारभाष्य महान् होता है, क्योंकि वह बहुत दोषों का आसेवन करने वाला होता है। ८४७. जह पुण ते चेव तिला, उसिणोदग धोत खीरउव्वक्का।
तेसिं जं तेल्लं तू, तं घयमंडं विसेसेति।।
उन्हीं पन्नकतिलों को यदि गर्म पानी से धोकर फिर कुछ समय तक दूध में भिगोकर रखा जाए और पश्चात् उनसे जो तेल निकाला जाए वह घृतमांड अर्थात् घृतसार से भी विशेष होता है। ८४८. कारण संविग्गाणं, आहारादीहि तप्पितो जो उ।
नीयावत्तणुतावी, तप्पक्खिय वण्णवादी य॥ ८४९. पावस्स उवचियस्स वि, पडिसाडण मो करेति एवं तु।।
सव्वासिरोगिउवमा, सरदे य पडे अविधुयम्मि।।
जो पार्श्वस्थ मुनि कारण अर्थात् अशिव, अवमौदर्य आदि समय में संविग्न मुनियों को आहार आदि से तर्पित करता है, उनको वंदना करता है, प्रतिसेवना के प्रति अनुतापी होता है, संविग्नपाक्षिक होता है तथा उन मुनियों की श्लाघा करता है-इस प्रकार वह पार्श्वस्थरूप से उपचित पाप का परिशाटन कर देता है। यहां सर्वाशीरोगी तथा अविधूत शारदीय पट की उपमा है। ८५०. पण्णे य यंते किमिणे, य अणुवातं च ठितो उल्लो य।
केण वि से वातपुतॄण, बुभुलइयं मुणेऊणं ।।
पन्नगतिल, स्थापित, दुरभिगंध, अनुनात, स्थित तथा आर्द्र किसी वातस्पृष्ट से, बहुभक्षी जानकर।
(इसमें तीन उपमाएं-दृष्टांत हैं। पन्नगतिलों का दृष्टांत गाथा ८४५ तथा ८४७ में आ चुका है। प्रस्तुत है सर्वाशीरोगी और शारदीय पट का दृष्टांत।)
दो प्रकार के रोगी हैं-एक है सर्वाशीरोगी अर्थात् बहुभक्षकरोगी और दूसरा है-असर्वाशीरोगी अर्थात् अल्पभक्षक रोगी। सर्वाशीरोगी की चिकित्सा कर्कश पद्धति से करने पर ही वह रोग-मुक्त हो सकता है और असर्वाशीरोगी की चिकित्सा अल्प क्रिया से संपन्न हो जाती है।
दो शारदीय वस्त्र हैं। एक वस्त्र को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां वह प्रतिदिन वायु के द्वारा धुना जाता है और दूसरा वस्त्र वेसे स्थान पर नहीं रखा जाता। कालक्रम से जब वे दोनों वस्त्र मलिन होते हैं तब वायु से निरंतर विद्यूत वस्त्र का मैल अल्प प्रयत्न से छूट जाता है और दूसरे वस्त्र का मैल बहुत प्रयत्न से छूटता है।
(इसी प्रकार जो पार्श्वस्थ है, साधुओं का अवर्णवाद बोलने वाला है वह महान् प्रायश्चित्त से ही शुद्ध हो सकता है, इसलिए उसे पूरा प्रायश्चित्त दिया जाता है और दूसरा पार्श्वस्थ मुनि जो २. वृत्ति पत्र १०९ : निंबतिलैः-तिला इव सूक्ष्मत्वात् निंबतिलाः कुसुमानि....निंबकुसुमैः।
www.jainelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only