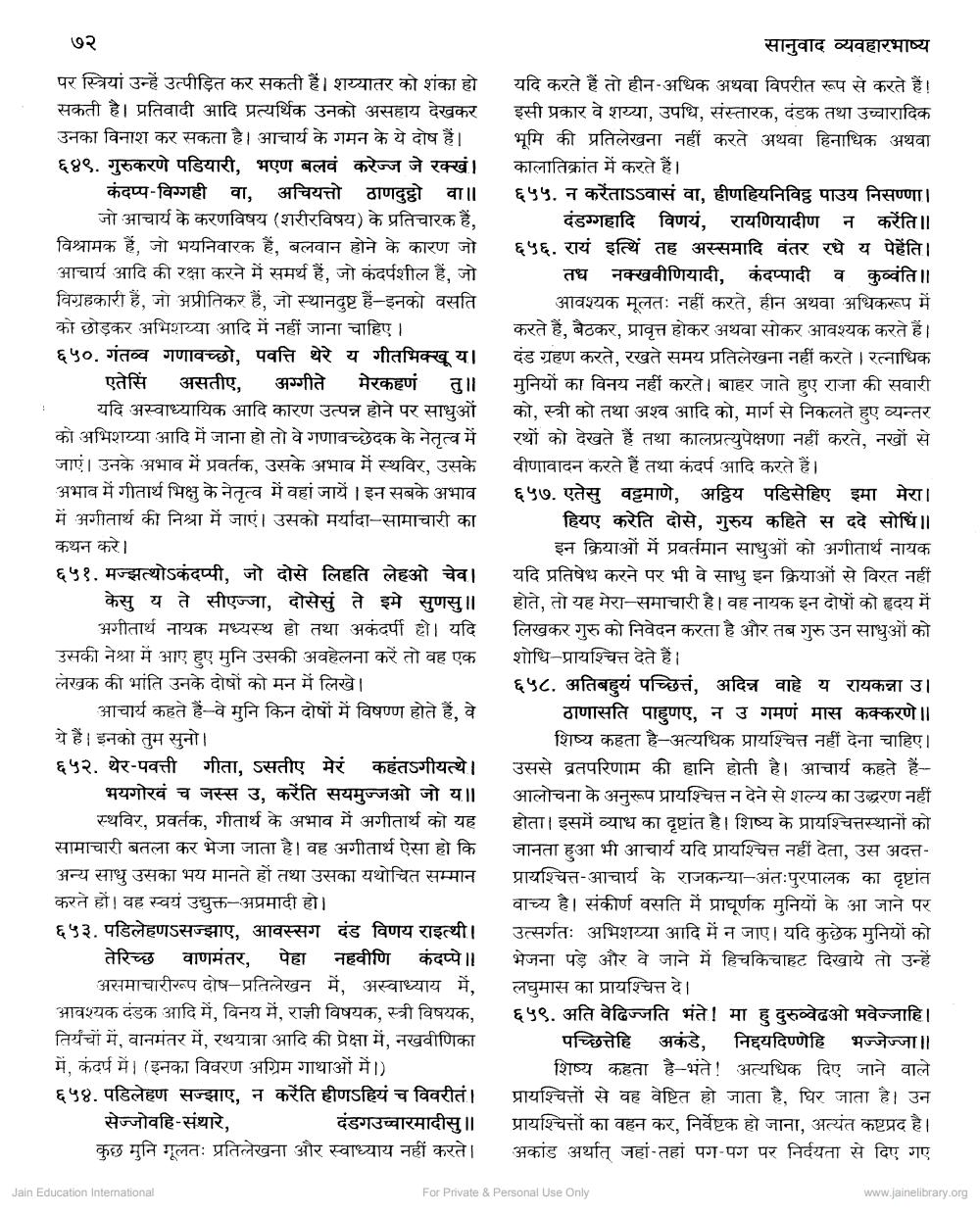________________
७२
पर स्त्रियां उन्हें उत्पीड़ित कर सकती हैं। शय्यातर को शंका हो सकती है। प्रतिवादी आदि प्रत्यर्थिक उनको असहाय देखकर उनका विनाश कर सकता है। आचार्य के गमन के ये दोष हैं। ६४९. गुरुकरणे पडियारी, भएण बलवं करेज्ज जे रक्खं । कंदप्प - विग्गही वा, अचियत्तो ठाणदुट्ठो वा ॥ जो आचार्य के करणविषय (शरीरविषय) के प्रतिचारक हैं, विश्रामक हैं, जो भयनिवारक हैं, बलवान होने के कारण जो आचार्य आदि की रक्षा करने में समर्थ हैं, जो कंदर्पशील हैं, जो विग्रहकारी हैं, जो अप्रीतिकर हैं, जो स्थानदुष्ट हैं- इनको वसति को छोड़कर अभिशय्या आदि में नहीं जाना चाहिए। ६५०.
गंतव्व गणावच्छो, पवत्ति थेरे य गीतभिक्खू य एतेसिं असतीए, अग्गीते मेरकहणं तु ॥ यदि अस्वाध्यायिक आदि कारण उत्पन्न होने पर साधुओं को अभिशय्या आदि में जाना हो तो वे गणावच्छेदक के नेतृत्व में जाएं। उनके अभाव में प्रवर्तक, उसके अभाव में स्थविर, उसके अभाव में गीतार्थ भिक्षु के नेतृत्व में वहां जायें। इन सबके अभाव में अगीतार्थ की निश्रा में जाएं। उसको मर्यादा -सामाचारी का कथन करे।
६५१. मज्झत्थोऽकंदप्पी, जो दोसे लिहति लेहओ चेव । केसु य ते सीएज्जा, दोसेसुं ते इमे सुणसु ॥ अगीतार्थ नायक मध्यस्थ हो तथा अकंदर्पी हो। यदि उसकी नेश्रा में आए हुए मुनि उसकी अवहेलना करें तो वह एक लेखक की भांति उनके दोषों को मन में लिखे ।
आचार्य कहते हैं - वे मुनि किन दोषों में विषण्ण होते हैं, वे ये हैं । इनको तुम सुनो।
६५२. थेर-पवत्ती गीता, ऽसतीए मेरं
कहंतऽगीयत्थे । भयगोरवं च जस्स उ, करेंति सयमुज्जओ जो य ॥ स्थविर, प्रवर्तक, गीतार्थ के अभाव में अगीतार्थ को यह सामाचारी बतला कर भेजा जाता है। वह अगीतार्थ ऐसा हो कि अन्य साधु उसका भय मानते हों तथा उसका यथोचित सम्मान करते हों। वह स्वयं उद्युक्त-अप्रमादी हो ।
६५३. पडिलेहणऽसज्झाए, आवस्सग दंड विणय राइत्थी ।
तेरिच्छ वाणमंतर, पेहा नहवीणि कंदप्पे ॥ असमाचारीरूप दोष - प्रतिलेखन में अस्वाध्याय में, आवश्यक दंडक आदि में, विनय में, राज्ञी विषयक, स्त्री विषयक, तिर्यंचों में, वानमंतर में, रथयात्रा आदि की प्रेक्षा में, नखवीणिका में, कंदर्प में। (इनका विवरण अग्रिम गाथाओं में ।)
६५४. पडिलेहण सज्झाए, न करेंति हीणऽहियं च विवरीतं । सेज्जोवहि-संथारे, दंडगउच्चारमादीसु ॥ कुछ मुनि मूलतः प्रतिलेखना और स्वाध्याय नहीं करते।
Jain Education International
सानुवाद व्यवहारभाष्य
यदि करते हैं तो हीन अधिक अथवा विपरीत रूप से करते हैं। इसी प्रकार वे शय्या, उपधि, संस्तारक, दंडक तथा उच्चारादिक भूमि की प्रतिलेखना नहीं करते अथवा हिनाधिक अथवा कालातिक्रांत में करते हैं।
६५५. न करेंताऽऽवासं वा, हीणहियनिविट्ठ पाउय निसण्णा । दंडग्गहादि विणयं, रायणियादीण न करेंति ॥ ६५६. रायं इत्थिं तह अस्समादि वंतर रधे य पेहेंति ।
तध नक्खवीणियादी, कंदप्पादी व कुव्वंति ॥ आवश्यक मूलतः नहीं करते, हीन अथवा अधिकरूप में करते हैं, बैठकर, प्रावृत्त होकर अथवा सोकर आवश्यक करते हैं। दंड ग्रहण करते, रखते समय प्रतिलेखना नहीं करते । रत्नाधिक मुनियों का विनय नहीं करते। बाहर जाते हुए राजा की सवारी को, स्त्री को तथा अश्व आदि को, मार्ग से निकलते हुए व्यन्तर रथों को देखते हैं तथा कालप्रत्युपेक्षणा नहीं करते, नखों से वीणावादन करते हैं तथा कंदर्प आदि करते हैं। ६५७. एतेसु वट्टमाणे, अट्ठिय पडिसेहिए इमा मेरा ।
हियए करेति दोसे, गुरुय कहिते स ददे सोधिं ॥ इन क्रियाओं में प्रवर्तमान साधुओं को अगीतार्थ नायक यदि प्रतिषेध करने पर भी वे साधु इन क्रियाओं से विरत नहीं होते, तो यह मेरा - समाचारी है। वह नायक इन दोषों को हृदय में लिखकर गुरु को निवेदन करता है और तब गुरु उन साधुओं को शोधि- प्रायश्चित्त देते हैं।
६५८. अतिबहुयं पच्छित्तं, अदिन्न वाहे य रायकन्ना उ ।
ठाणासति पाहुणए, न उ गमणं मास कक्करणे ॥ शिष्य कहता है-अत्यधिक प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए । उससे व्रतपरिणाम की हानि होती है। आचार्य कहते हैंआलोचना के अनुरूप प्रायश्चित्त न देने से शल्य का उद्धरण नहीं होता। इसमें व्याध का दृष्टांत है। शिष्य के प्रायश्चित्तस्थानों को जानता हुआ भी आचार्य यदि प्रायश्चित्त नहीं देता, उस अदत्तप्रायश्चित्त-आचार्य के राजकन्या - अंतःपुरपालक का दृष्टांत वाच्य है। संकीर्ण वसति में प्राघूर्णक मुनियों के आ जाने पर उत्सर्गतः अभिशय्या आदि में न जाए। यदि कुछेक मुनियों को भेजना पड़े और वे जाने में हिचकिचाहट दिखाये तो उन्हें लघुमास का प्रायश्चित्त दे। ६५९. अति वेढिज्जति भंते! मा हु दुरुव्वेढओ भवेज्जाहि । पच्छित्तेहि अकंडे, निद्दयदिण्णेहि शिष्य कहता है- भंते! अत्यधिक दिए जाने वाले प्रायश्चित्तों से वह वेष्टित हो जाता है, घिर जाता है। उन प्रायश्चित्तों का वहन कर, निर्वेष्टक हो जाना, अत्यंत कष्टप्रद है। अकांड अर्थात् जहां-तहां पग-पग पर निर्दयता से दिए गए
भज्जेज्जा ॥
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org