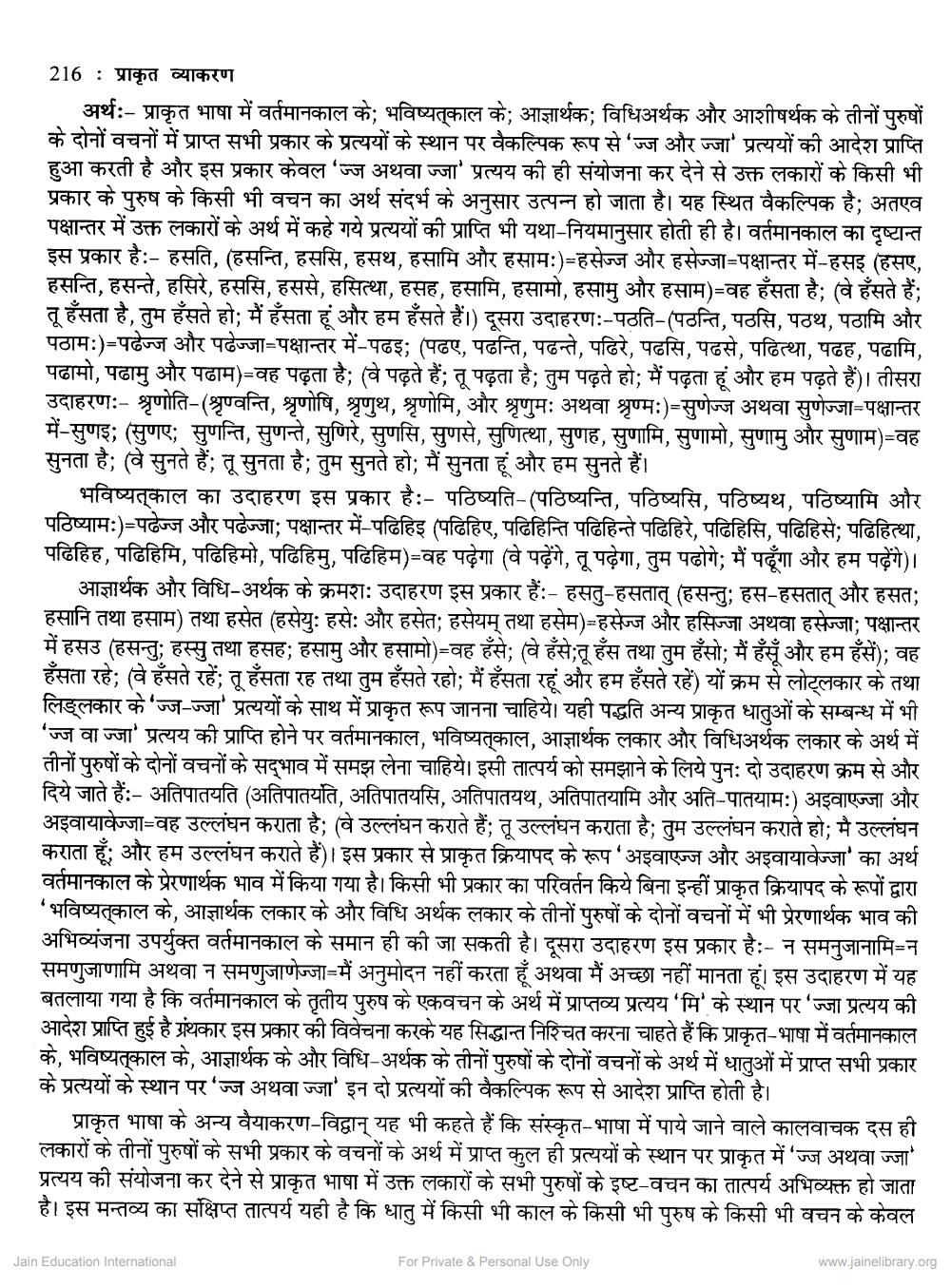________________
216 : प्राकृत व्याकरण __ अर्थः- प्राकृत भाषा में वर्तमानकाल के; भविष्यत्काल के; आज्ञार्थक; विधिअर्थक और आशीषर्थक के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में प्राप्त सभी प्रकार के प्रत्ययों के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'ज्ज और ज्जा' प्रत्ययों की आदेश प्राप्ति हुआ करती है और इस प्रकार केवल 'ज्ज अथवा ज्जा' प्रत्यय की ही संयोजना कर देने से उक्त लकारों के किसी भी प्रकार के पुरुष के किसी भी वचन का अर्थ संदर्भ के अनुसार उत्पन्न हो जाता है। यह स्थित वैकल्पिक है; अतएव पक्षान्तर में उक्त लकारों के अर्थ में कहे गये प्रत्ययों की प्राप्ति भी यथा-नियमानुसार होती ही है। वर्तमानकाल का दृष्टान्त इस प्रकार है:- हसति, (हसन्ति, हससि, हसथ, हसामि और हसामः) हसेज्ज और हसेज्जा=पक्षान्तर में-हसइ (हसए, हसन्ति, हसन्ते, हसिरे, हससि, हससे, हसित्था, हसह, हसामि, हसामो, हसामु और हसाम) वह हँसता है; (वे हँसते हैं; तू हँसता है, तुम हँसते हो; मैं हँसता हूं और हम हँसते हैं।) दूसरा उदाहरणः-पठति-(पठन्ति, पठसि, पठथ, पठामि और पठामः)=पढेज्ज और पढेज्जा पक्षान्तर में-पढइ; (पढए, पढन्ति, पढन्ते, पढिरे, पढसि, पढसे, पढित्था, पढह, पढामि, पढामो, पढामु और पढाम)-वह पढ़ता है; (वे पढ़ते हैं; तू पढ़ता है; तुम पढ़ते हो; मैं पढ़ता हूं और हम पढ़ते हैं)। तीसरा उदाहरण:- श्रृणोति-(श्रृण्वन्ति, श्रृणोषि, श्रृणुथ, श्रृणोमि, और श्रृणुमः अथवा श्रृण्मः)-सुणेज्ज अथवा सुणेज्जा-पक्षान्तर में-सुणइ; (सुणए; सुणन्ति, सुणन्ते, सुणिरे, सुणसि, सुणसे, सुणित्था, सुणह, सुणामि, सुणामो, सुणामु और सुणाम)-वह सुनता है; (वे सुनते हैं; तू सुनता है; तुम सुनते हो; मैं सुनता हूं और हम सुनते हैं।
भविष्यत्काल का उदाहरण इस प्रकार है:- पठिष्यति-(पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यामि और पठिष्यामः) पढेज्ज और पढेज्जा; पक्षान्तर में पढिहिइ (पढिहिए, पढिहिन्ति पढिहिन्ते पढिहिरे, पढिहिसि, पढिहिसे; पढिहित्था, पढिहिह, पढिहिमि, पढिहिमो, पढिहिमु, पढिहिम)-वह पढ़ेगा (वे पढ़ेंगे, तू पढ़ेगा, तुम पढोगे; मैं पढूँगा और हम पढ़ेंगे)।
आज्ञार्थक और विधि-अर्थक के क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैं:- हसतु-हसतात् (हसन्तु; हस-हसतात् और हसत; हसानि तथा हसाम) तथा हसेत (हसेयुः हसेः और हसेत; हसेयम् तथा हसेम)-हसेज्ज और हसिज्जा अथवा हसेज्जा; पक्षान्तर में हसउ (हसन्तु; हस्सु तथा हसह; हसामु और हसामो)=वह हँसे; (वे हँसे;तू हँस तथा तुम हँसो; मैं हँसूं और हम हँसें); वह हँसता रहे; (वे हँसते रहें; तू हँसता रह तथा तुम हँसते रहो; मैं हँसता रहूं और हम हँसते रहें) यो क्रम से लोट्लकार के तथा लिङ्लकार के 'ज्ज-ज्जा' प्रत्ययों के साथ में प्राकृत रूप जानना चाहिये। यही पद्धति अन्य प्राकृत धातुओं के सम्बन्ध में भी 'ज्ज वा ज्जा' प्रत्यय की प्राप्ति होने पर वर्तमानकाल, भविष्यत्काल, आज्ञार्थक लकार और विधिअर्थक लकार के अर्थ में तीनों पुरुषों के दोनों वचनों के सदभाव में समझ लेना चाहिये। इसी तात्पर्य को समझाने के लिये पनः दो उदाहरण क्रम से और दिये जाते हैं:- अतिपातयति (अतिपातयति, अतिपातयसि, अतिपातयथ, अतिपातयामि और अति-पातयामः) अइवाएज्जा और अइवायावेज्जा वह उल्लंघन कराता है; (वे उल्लंघन कराते हैं; तू उल्लंघन कराता है; तुम उल्लंघन कराते हो; मै उल्लंघन कराता हूँ; और हम उल्लंघन कराते हैं)। इस प्रकार से प्राकृत क्रियापद के रूप 'अइवाएज्ज और अइवायावेज्जा' का अर्थ वर्तमानकाल के प्रेरणार्थक भाव में किया गया है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये बिना इन्हीं प्राकृत क्रियापद के रूपों द्वारा 'भविष्यत्काल के, आज्ञार्थक लकार के और विधि अर्थक लकार के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में भी प्रेरणार्थक भाव की अभिव्यंजना उपर्युक्त वर्तमानकाल के समान ही की जा सकती है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है:- न समनुजानामिन समणुजाणामि अथवा न समणुजाणेज्जा=मैं अनुमोदन नहीं करता हूँ अथवा मैं अच्छा नहीं मानता हूं। इस उदाहरण में यह बतलाया गया है कि वर्तमानकाल के तृतीय पुरुष के एकवचन के अर्थ में प्राप्तव्य प्रत्यय 'मि' के स्थान पर 'ज्जा प्रत्यय की आदेश प्राप्ति हुई है ग्रंथकार इस प्रकार की विवेचना करके यह सिद्धान्त निश्चित करना चाहते हैं कि प्राकृत भाषा में वर्तमानकाल के, भविष्यत्काल के, आज्ञार्थक के और विधि-अर्थक के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों के अर्थ में धातुओं में प्राप्त सभी प्रकार के प्रत्ययों के स्थान पर 'ज्ज अथवा ज्जा' इन दो प्रत्ययों की वैकल्पिक रूप से आदेश प्राप्ति होती है।
प्राकृत भाषा के अन्य वैयाकरण-विद्वान् यह भी कहते हैं कि संस्कृत-भाषा में पाये जाने वाले कालवाचक दस ही लकारों के तीनों पुरुषों के सभी प्रकार के वचनों के अर्थ में प्राप्त कुल ही प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में 'ज्ज अथवा ज्जा' प्रत्यय की संयोजना कर देने से प्राकृत भाषा में उक्त लकारों के सभी पुरुषों के इष्ट-वचन का तात्पर्य अभिव्यक्त हो जाता है। इस मन्तव्य का संक्षिप्त तात्पर्य यही है कि धातु में किसी भी काल के किसी भी पुरुष के किसी भी वचन के केवल
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org