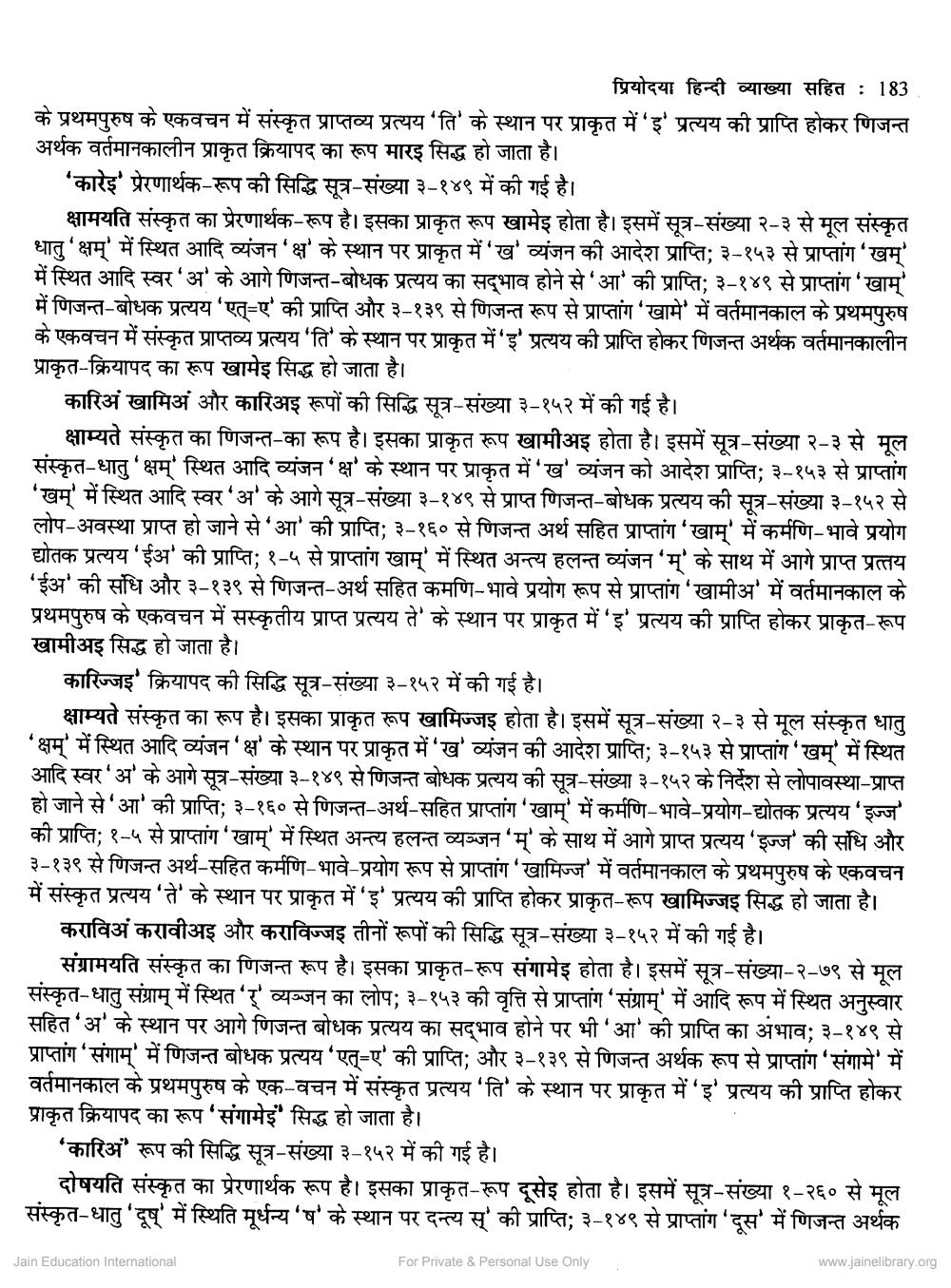________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 183. के प्रथमपुरुष के एकवचन में संस्कृत प्राप्तव्य प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर णिजन्त अर्थक वर्तमानकालीन प्राकृत क्रियापद का रूप मारइ सिद्ध हो जाता है। 'कारेइ प्रेरणार्थक-रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१४९ में की गई है।
क्षामयति संस्कृत का प्रेरणार्थक-रूप है। इसका प्राकृत रूप खामेइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या २-३ से मूल संस्कृत धातु 'क्षम्' में स्थित आदि व्यंजन 'क्ष' के स्थान पर प्राकृत में 'ख' व्यंजन की आदेश प्राप्ति; ३-१५३ से प्राप्तांग 'खम्' में स्थित आदि स्वर 'अ' के आगे णिजन्त-बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से 'आ' की प्राप्ति; ३-१४९ से प्राप्तांग 'खाम्' में णिजन्त-बोधक प्रत्यय ‘एत्=ए' की प्राप्ति और ३-१३९ से णिजन्त रूप से प्राप्तांग 'खामे में वर्तमानकाल के प्रथमपुरुष के एकवचन में संस्कृत प्राप्तव्य प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर णिजन्त अर्थक वर्तमानकालीन प्राकृत-क्रियापद का रूप खामेइ सिद्ध हो जाता है।
कारिअं खामिअं और कारिअइ रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१५२ में की गई है।
क्षाम्यते संस्कृत का णिजन्त-का रूप है। इसका प्राकृत रूप खामीअइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या २-३ से मूल संस्कृत-धातु 'क्षम् स्थित आदि व्यंजन 'क्ष' के स्थान पर प्राकृत में 'ख' व्यंजन को आदेश प्राप्ति; ३-१५३ से प्राप्तांग 'खम्' में स्थित आदि स्वर 'अ' के आगे सूत्र-संख्या ३-१४९ से प्राप्त णिजन्त-बोधक प्रत्यय की सूत्र-संख्या ३-१५२ से लोप-अवस्था प्राप्त हो जाने से 'आ' की प्राप्ति; ३-१६० से णिजन्त अर्थ सहित प्राप्तांग 'खाम्' में कर्मणि-भावे प्रयोग द्योतक प्रत्यय 'ईअ' की प्राप्ति; १-५ से प्राप्तांग खाम्' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यंजन 'म्' के साथ में आगे प्राप्त प्रत्तय 'ईअ' की संधि और ३-१३९ से णिजन्त-अर्थ सहित कमणि-भावे प्रयोग रूप से प्राप्तांग 'खामीअ में वर्तमानकाल के प्रथमपुरुष के एकवचन में सस्कृतीय प्राप्त प्रत्यय ते' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत-रूप खामीअइ सिद्ध हो जाता है।
कारिज्जइ' क्रियापद की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१५२ में की गई है।
क्षाम्यते संस्कृत का रूप है। इसका प्राकृत रूप खामिज्जइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या २-३ से मूल संस्कृत धातु 'क्षम्' में स्थित आदि व्यंजन 'क्ष' के स्थान पर प्राकृत में 'ख' व्यंजन की आदेश प्राप्ति; ३-१५३ से प्राप्तांग 'खम् में स्थित
आदि स्वर 'अ' के आगे सूत्र-संख्या ३-१४९ से णिजन्त बोधक प्रत्यय की सूत्र-संख्या ३-१५२ के निर्देश से लोपावस्था प्राप्त हो जाने से 'आ' की प्राप्ति; ३-१६० से णिजन्त-अर्थ-सहित प्राप्तांग 'खाम्' में कर्मणि-भावे-प्रयोग-द्योतक प्रत्यय 'इज्ज' की प्राप्ति; १-५ से प्राप्तांग 'खाम्' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 'म्' के साथ में आगे प्राप्त प्रत्यय 'इज्ज' की संधि और ३-१३९ से णिजन्त अर्थ-सहित कर्मणि-भावे-प्रयोग रूप से प्राप्तांग 'खामिज्ज' में वर्तमानकाल के प्रथमपुरुष के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'ते' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत-रूप खामिज्जइ सिद्ध हो जाता है।
कराविअंकरावीअइ और कराविज्जइ तीनों रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१५२ में की गई है।
संग्रामयति संस्कृत का णिजन्त रूप है। इसका प्राकृत-रूप संगामेइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या-२-७९ से मूल संस्कृत-धातु संग्राम में स्थित 'र' व्यञ्जन का लोप; ३-१५३ की वृत्ति से प्राप्तांग संग्राम्' में आदि रूप में स्थित अनुस्वार सहित 'अ' के स्थान पर आगे णिजन्त बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने पर भी 'आ' की प्राप्ति का अभाव; ३-१४९ से प्राप्तांग 'संगाम्' में णिजन्त बोधक प्रत्यय 'एत्-ए' की प्राप्ति; और ३-१३९ से णिजन्त अर्थक रूप से प्राप्तांग 'संगामे' में वर्तमानकाल के प्रथमपुरुष के एक-वचन में संस्कृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राकृत क्रियापद का रूप 'संगामेई सिद्ध हो जाता है।
'कारिअं रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१५२ में की गई है।
दोषयति संस्कृत का प्रेरणार्थक रूप है। इसका प्राकृत-रूप दूसेइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-२६० से मूल संस्कृत-धातु 'दूष' में स्थिति मूर्धन्य 'ष' के स्थान पर दन्त्य स्' की प्राप्ति; ३-१४९ से प्राप्तांग 'दूस' में णिजन्त अर्थक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org