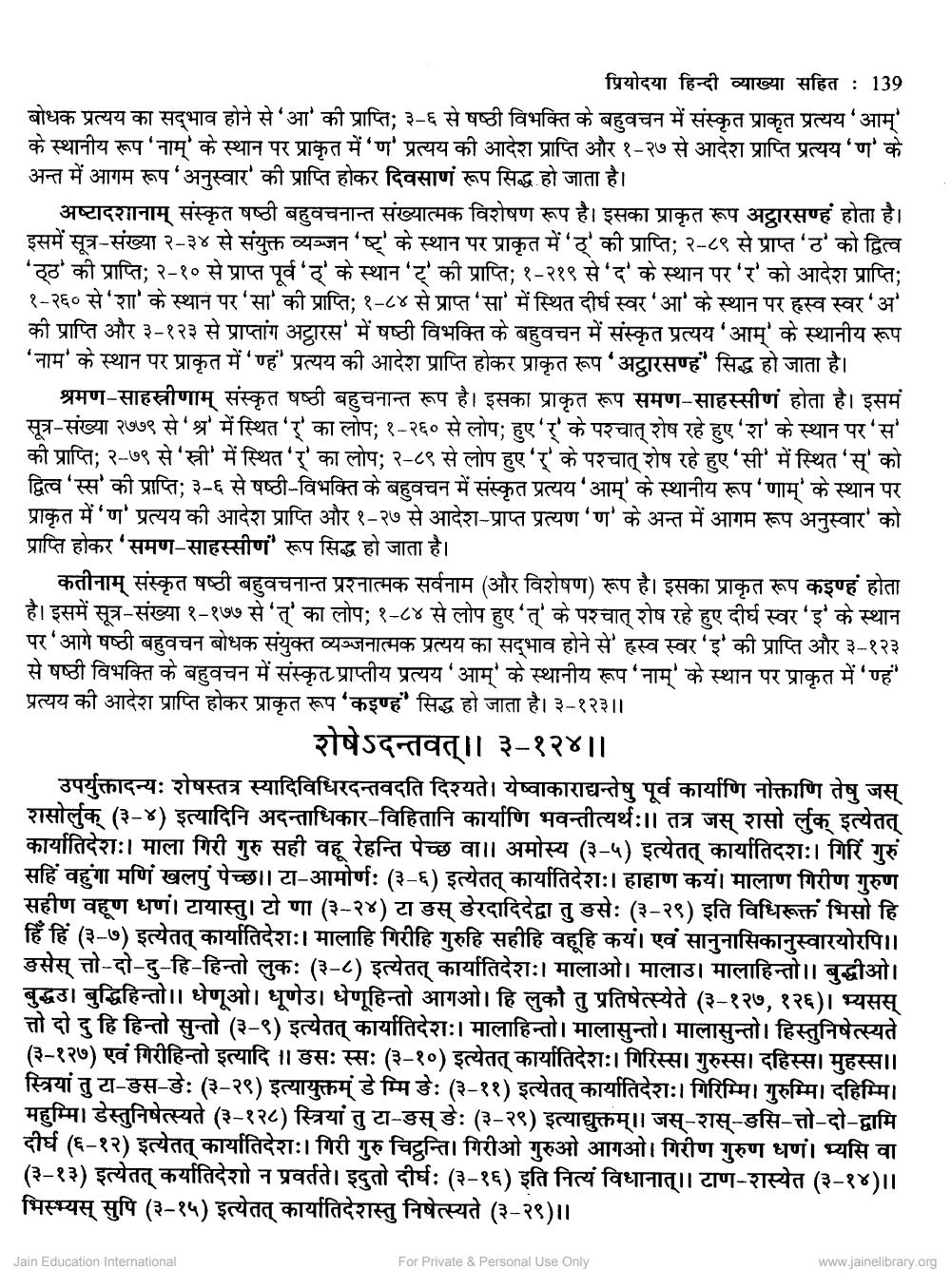________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 139 बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से 'आ' की प्राप्ति; ३-६ से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत प्राकृत प्रत्यय 'आम्' के स्थानीय रूप 'नाम्' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति और १-२७ से आदेश प्राप्ति प्रत्यय 'ण' के अन्त में आगम रूप अनुस्वार' की प्राप्ति होकर दिवसाणं रूप सिद्ध हो जाता है। ___ अष्टादशानाम् संस्कृत षष्ठी बहुवचनान्त संख्यात्मक विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप अट्ठारसण्हं होता है। इसमें सूत्र-संख्या २-३४ से संयुक्त व्यञ्जन 'ष्ट्' के स्थान पर प्राकृत में 'ठ्' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त 'ठ' को द्वित्व 'ठ्ठ की प्राप्ति; २-१० से प्राप्त पूर्व'' के स्थान 'ट् की प्राप्ति; १-२१९ से 'द' के स्थान पर 'र' को आदेश प्राप्ति; १-२६० से 'शा' के स्थान पर 'सा' की प्राप्ति; १-८४ से प्राप्त 'सा' में स्थित दीर्घ स्वर 'आ' के स्थान पर हस्व स्वर 'अ' की प्राप्ति और ३-१२३ से प्राप्तांग अटारस' में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत प्रत्यय 'आम्' के स्थानीय रूप 'नाम' के स्थान पर प्राकृत में 'हं' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होकर प्राकृत रूप 'अट्ठारसण्ह सिद्ध हो जाता है।
श्रमण-साहस्रीणाम् संस्कृत षष्ठी बहुचनान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप समण-साहस्सीणं होता है। इसमं सूत्र-संख्या २७७९ से 'श्र' में स्थित 'र' का लोप; १-२६० से लोप; हुए 'र' के पश्चात् शेष रहे हुए 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति; २-७९ से 'स्त्री' में स्थित 'र' का लोप; २-८९ से लोप हुए 'र' के पश्चात् शेष रहे हुए 'सी' में स्थित 'स्' को द्वित्व ‘स्स' की प्राप्ति; ३-६ से षष्ठी-विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत प्रत्यय 'आम्' के स्थानीय रूप 'णाम्' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति और १-२७ से आदेश-प्राप्त प्रत्यण 'ण' के अन्त में आगम रूप अनुस्वार' को प्राप्ति होकर 'समण-साहस्सीणं रूप सिद्ध हो जाता है। ___ कतीनाम् संस्कृत षष्ठी बहुवचनान्त प्रश्नात्मक सर्वनाम (और विशेषण) रूप है। इसका प्राकृत रूप कइण्हं होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से 'त्' का लोप; १-८४ से लोप हुए 'त्' के पश्चात् शेष रहे हुए दीर्घ स्वर 'इ' के स्थान पर आगे षष्ठी बहुवचन बोधक संयुक्त व्यञ्जनात्मक प्रत्यय का सद्भाव होने से हस्व स्वर 'इ' की प्राप्ति और ३-१२३ से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत प्राप्तीय प्रत्यय 'आम्' के स्थानीय रूप 'नाम्' के स्थान पर प्राकृत में 'व्ह' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होकर प्राकृत रूप 'कइण्ह' सिद्ध हो जाता है। ३-१२३।।
शेषेऽदन्तवत्।। ३-१२४।। उपर्युक्तादन्यः शेषस्तत्र स्यादिविधिरदन्तवदति दिश्यते। येष्वाकाराद्यन्तेषु पूर्व कार्याणि नोक्ताणि तेषु जस् शसोलुंक् (३-४) इत्यादिनि अदन्ताधिकार-विहितानि कार्याणि भवन्तीत्यर्थः।। तत्र जस् शसो लुक् इत्येतत् कार्यातिदेशः। माला गिरी गुरु सही वहू रेहन्ति पेच्छ वा।। अमोस्य (३-५) इत्येतत् कार्यातिदशः। गिरि गुरुं सहिं वहुंगा मणिं खलपुं पेच्छ।। टा-आमोर्णः (३-६) इत्येतत् कार्यातिदेशः। हाहाण कयो मालाण गिरीण गुरुण सहीण वहूण धणं। टायास्तु। टो णा (३-२४) टा डस् डेरदादिदेद्वा तु उसेः (३-२९) इति विधिरूक्तं भिसो हि हिं हिं (३-७) इत्येतत् कार्यातिदेशः। मालाहि गिरीहि गुरुहि सहीहि वहूहि कय। एवं सानुनासिकानुस्वारयोरपि।। उसेस् त्तो-दो-दु-हि-हिन्तो लुकः (३-८) इत्येतत् कार्यातिदेशः। मालाओ। मालाउ। मालाहिन्तो। बुद्धीओ। बुद्धउ। बुद्धिहिन्तो।। धेणूओ। धूणेउ। धेणूहिन्तो आगओ। हि लुकौ तु प्रतिषेत्स्येते (३-१२७, १२६)। भ्यसस् तो दो दु हि हिन्तो सुन्तो (३-९) इत्येतत् कार्यातिदेशः। मालाहिन्तो। मालासुन्तो। मालासुन्तो। हिस्तुनिषेत्स्यते (३-१२७) एवं गिरीहिन्तो इत्यादि । उसः स्सः (३-१०) इत्येतत् कार्यातिदेशः। गिरिस्स। गुरुस्स। दहिस्स। मुहस्स।। स्त्रियां तु टा-उस-डेः (३-२९) इत्यायुक्तम् डे म्मि डेः (३-११) इत्येतत् कार्यातिदेशः। गिरिम्मि। गुरुम्मि। दहिम्मि। महुम्मि। डेस्तुनिषेत्स्यते (३-१२८) स्त्रियां तु टा-डस् डेः (३-२९) इत्याधुक्तम्। जस्-शस्-डसि-त्तो-दो-द्वामि दीर्घ (६-१२) इत्येतत् कार्यातिदेशः। गिरी गुरु चिट्ठन्ति। गिरीओ गुरुओ आगओ। गिरीण गुरुण धणं। भ्यसि वा (३-१३) इत्येतत् कर्यातिदेशो न प्रवर्तते। इदुतो दीर्घः (३-१६) इति नित्यं विधानात्।। टाण-शस्येत (३-१४)।। भिस्म्यस् सुपि (३-१५) इत्येतत् कार्यातिदेशस्तु निषेत्स्यते (३-२९)।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org