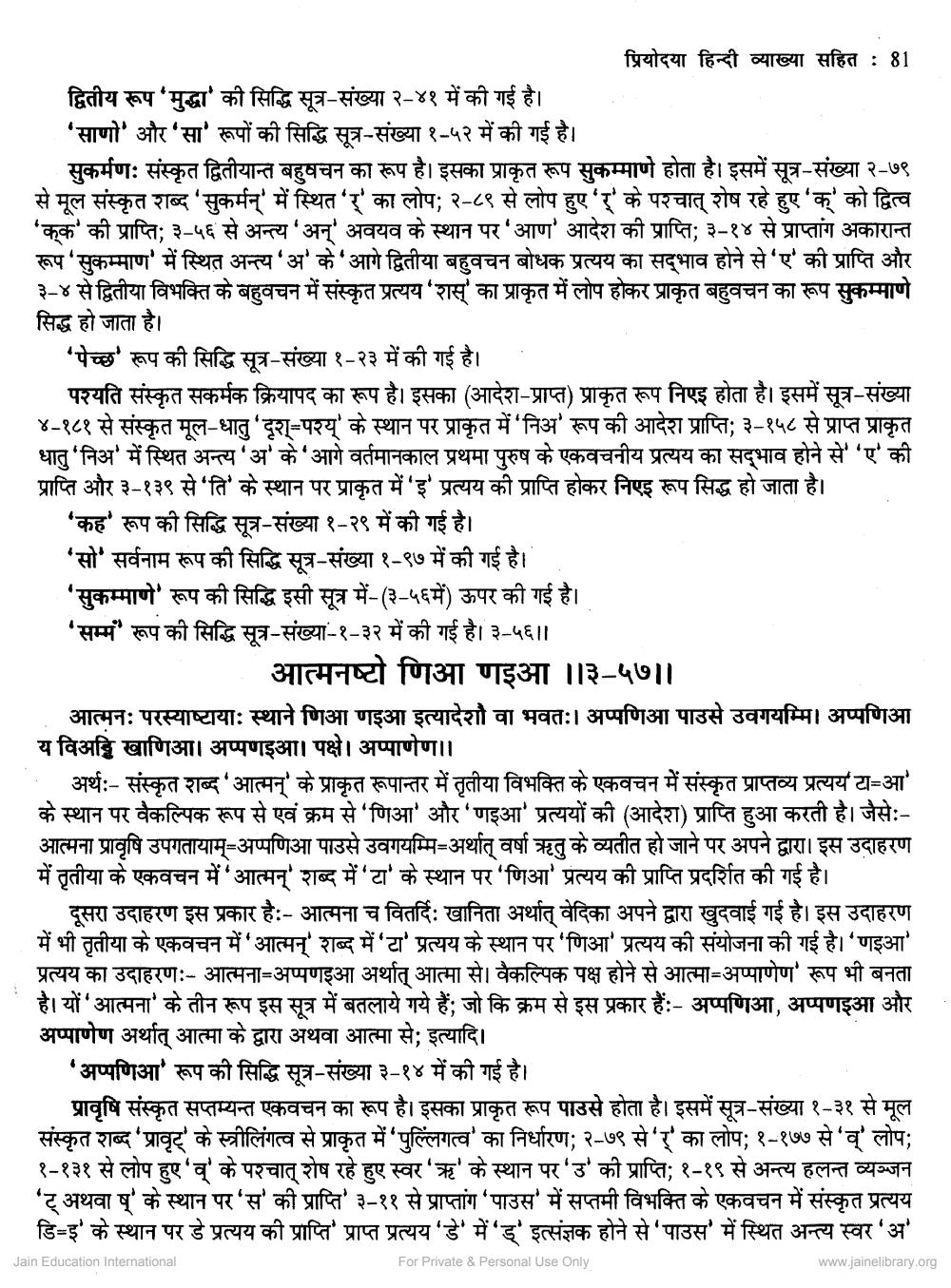________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 81 द्वितीय रूप 'मुद्धा' की सिद्धि सूत्र-संख्या २-४१ में की गई है। 'साणो' और 'सा' रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या १-५२ में की गई है।
सुकर्मणः संस्कृत द्वितीयान्त बहुषचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप सुकम्माणे होता है। इसमें सूत्र-संख्या २-७९ से मूल संस्कृत शब्द 'सुकर्मन्' में स्थित 'र' का लोप; २-८९ से लोप हुए 'र' के पश्चात् शेष रहे हुए 'क्' को द्वित्व 'क्क' की प्राप्ति; ३-५६ से अन्त्य 'अन्' अवयव के स्थान पर 'आण' आदेश की प्राप्ति; ३-१४ से प्राप्तांग अकारान्त रूप 'सुकम्माण' में स्थित अन्त्य 'अ' के आगे द्वितीया बहुवचन बोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से 'ए' की प्राप्ति और ३-४ से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत प्रत्यय 'शस्' का प्राकृत में लोप होकर प्राकृत बहुवचन का रूप सुकम्माणे सिद्ध हो जाता है।
'पेच्छ' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-२३ में की गई है।
पश्यति संस्कृत सकर्मक क्रियापद का रूप है। इसका (आदेश-प्राप्त) प्राकृत रूप निएइ होता है। इसमें सूत्र-संख्या ४-१८१ से संस्कृत मूल-धातु 'दृश्=पश्य' के स्थान पर प्राकृत में 'निअ रूप की आदेश प्राप्ति; ३-१५८ से प्राप्त प्राकृत धातु 'निअ' में स्थित अन्त्य 'अ' के 'आगे वर्तमानकाल प्रथमा पुरुष के एकवचनीय प्रत्यय का सद्भाव होने से' 'ए' की प्राप्ति और ३-१३९ से 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर निएइ रूप सिद्ध हो जाता है।
'कह' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-२९ में की गई है। 'सो' सर्वनाम रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-९७ में की गई है। 'सुकम्माणे' रूप की सिद्धि इसी सूत्र में-(३-५६में) ऊपर की गई है। 'सम्म रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या-१-३२ में की गई है। ३-५६।।
. आत्मनष्टो णिआ णइआ ॥३-५७॥ आत्मनः परस्याष्टायाः स्थाने णिआ णइआ इत्यादेशौ वा भवतः। अप्पणिआ पाउसे उवगयम्मि। अप्पणिआ य विअडि खाणिआ। अप्पणइआ। पक्षे। अप्पाणेण।। . अर्थः- संस्कृत शब्द 'आत्मन्' के प्राकृत रूपान्तर में तृतीया विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्राप्तव्य प्रत्यय टा=आ' के स्थान पर वैकल्पिक रूप से एवं क्रम से 'णिआ' और 'णइआ' प्रत्ययों की (आदेश) प्राप्ति हुआ करती है। जैसे:आत्मना प्रावृषि उपगतायाम् अप्पणिआ पाउसे उवगयम्मि अर्थात् वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने पर अपने द्वारा। इस उदाहरण में तृतीया के एकवचन में आत्मन् शब्द में 'टा' के स्थान पर 'णिआ' प्रत्यय की प्राप्ति प्रदर्शित की गई है।
दूसरा उदाहरण इस प्रकार है:- आत्मना च वितर्दिः खानिता अर्थात् वेदिका अपने द्वारा खुदवाई गई है। इस उदाहरण में भी तृतीया के एकवचन में आत्मन् शब्द में 'टा' प्रत्यय के स्थान पर 'णिआ' प्रत्यय की संयोजना की गई है। 'णइआ' प्रत्यय का उदाहरणः- आत्मना=अप्पणइआ अर्थात् आत्मा से। वैकल्पिक पक्ष होने से आत्मा अप्पाणेण' रूप भी बनता है। यों आत्मना' के तीन रूप इस सूत्र में बतलाये गये हैं; जो कि क्रम से इस प्रकार हैं:- अप्पणिआ, अप्पणइआ और अप्पाणेण अर्थात् आत्मा के द्वारा अथवा आत्मा से; इत्यादि। 'अप्पणिआ रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१४ में की गई है।
प्रावृषि संस्कृत सप्तम्यन्त एकवचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप पाउसे होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-३१ से मूल संस्कृत शब्द 'प्रावृट् के स्त्रीलिंगत्व से प्राकृत में पुल्लिगत्व' का निर्धारण; २-७९ से 'र' का लोप; १-१७७ से '' लोप; १-१३१ से लोप हुए 'व' के पश्चात् शेष रहे हुए स्वर 'ऋ' के स्थान पर 'उ' की प्राप्ति; १-१९ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 'ट् अथवा ष' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति' ३-११ से प्राप्तांग ‘पाउस' में सप्तमी विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय डि-ई' के स्थान पर डे प्रत्यय की प्राप्ति' प्राप्त प्रत्यय 'डे' में 'ड्' इत्संज्ञक होने से 'पाउस' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org