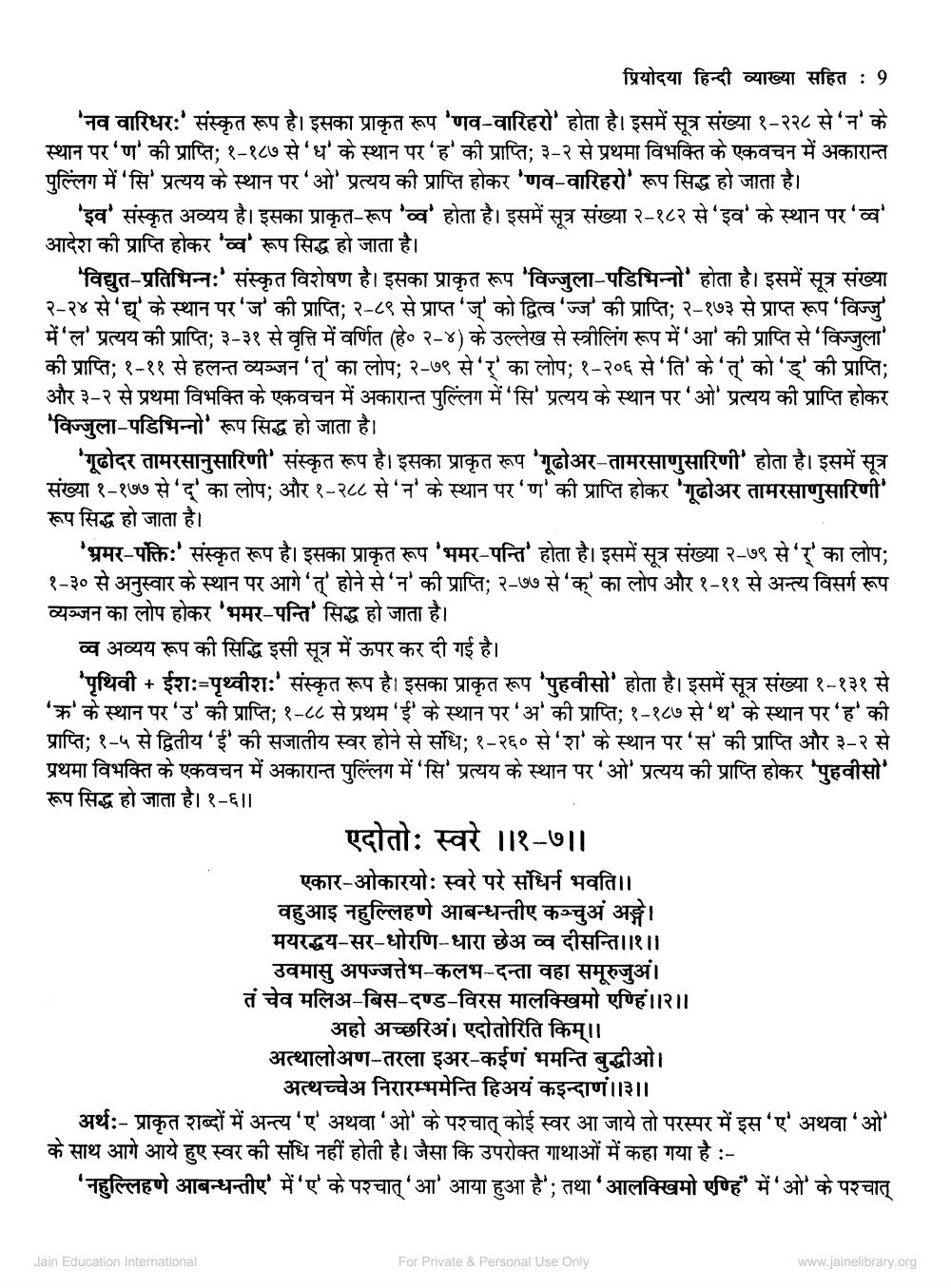________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 9 'नव वारिधरः' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'णव-वारिहरो' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-२२८ से 'न' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; १-१८७ से 'ध' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'णव-वारिहरो' रूप सिद्ध हो जाता है।
'इव' संस्कृत अव्यय है। इसका प्राकृत-रूप 'व्व' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-१८२ से 'इव' के स्थान पर 'व्व' आदेश की प्राप्ति होकर 'व्व' रूप सिद्ध हो जाता है।
"विद्युत-प्रतिभिन्नः संस्कृत विशेषण है। इसका प्राकृत रूप 'विज्जुला-पडिभिन्नो' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-२४ से 'छ्' के स्थान पर 'ज' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त 'ज्' को द्वित्व 'ज्ज' की प्राप्ति; २-१७३ से प्राप्त रूप 'विज्जु में 'ल' प्रत्यय की प्राप्ति; ३-३१ से वृत्ति में वर्णित (हे० २-४) के उल्लेख से स्त्रीलिंग रूप में 'आ' की प्राप्ति से 'विज्जुला' की प्राप्ति; १-११ से हलन्त व्यञ्जन 'त्' का लोप; २-७९ से 'र' का लोप; १-२०६ से 'ति' के 'त्' को 'ड्' की प्राप्ति; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर "विज्जुला-पडिभिन्नो' रूप सिद्ध हो जाता है।
'गूढोदर तामरसानुसारिणी' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'गूढोअर-तामरसाणुसारिणी' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१७७ से 'द्' का लोप; और १-२८८ से 'न' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति होकर 'गूढोअर तामरसाणुसारिणी' रूप सिद्ध हो जाता है।
'भ्रमर-पक्तिः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'भमर-पन्ति' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-७९ से 'र' का लोप; १-३० से अनुस्वार के स्थान पर आगे 'त्' होने से 'न' की प्राप्ति; २-७७ से 'क्' का लोप और १-११ से अन्त्य विसर्ग रूप व्यञ्जन का लोप होकर 'भमर-पन्ति' सिद्ध हो जाता है।
व्व अव्यय रूप की सिद्धि इसी सूत्र में ऊपर कर दी गई है।
'पृथिवी + ईशः पृथ्वीशः' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'पुहवीसो' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१३१ से 'क' के स्थान पर 'उ' की प्राप्ति; १-८८ से प्रथम 'ई के स्थान पर 'अ' की प्राप्ति; १-१८७ से 'थ' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; १-५ से द्वितीय 'ई' की सजातीय स्वर होने से संधि; १-२६० से 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'पुहवीसो' रूप सिद्ध हो जाता है। १-६।।
एदोतोः स्वरे ।।१-७॥ ___ एकार-ओकारयोः स्वरे परे संधिर्न भवति।। वहुआइ नहुल्लिहणे आबन्धन्तीए कञ्चुअं अङ्गे। मयरद्धय-सर-धोरणि-धारा छेअ व्व दीसन्ति।।१।।
उवमासु अपज्जत्तेभ-कलभ-दन्ता वहा समूरुजु। तं चेव मलिअ-बिस-दण्ड-विरस मालक्खिमो एण्हि।।२।।
अहो अच्छरि एदोतोरिति किम्।। अत्थालोअण-तरला इअर-कईणं भमन्ति बुद्धीओ।
अत्थच्चेअ निरारम्भमेन्ति हिअयं कइन्दाणं।।३।। अर्थः- प्राकृत शब्दों में अन्त्य 'ए' अथवा 'ओ' के पश्चात् कोई स्वर आ जाये तो परस्पर में इस 'ए' अथवा 'ओ' के साथ आगे आये हुए स्वर की संधि नहीं होती है। जैसा कि उपरोक्त गाथाओं में कहा गया है :
'नहुल्लिहणे आबन्धन्तीए' में 'ए' के पश्चात् 'आ' आया हुआ है'; तथा 'आलक्खिमो एण्हि' में 'ओ' के पश्चात्
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org