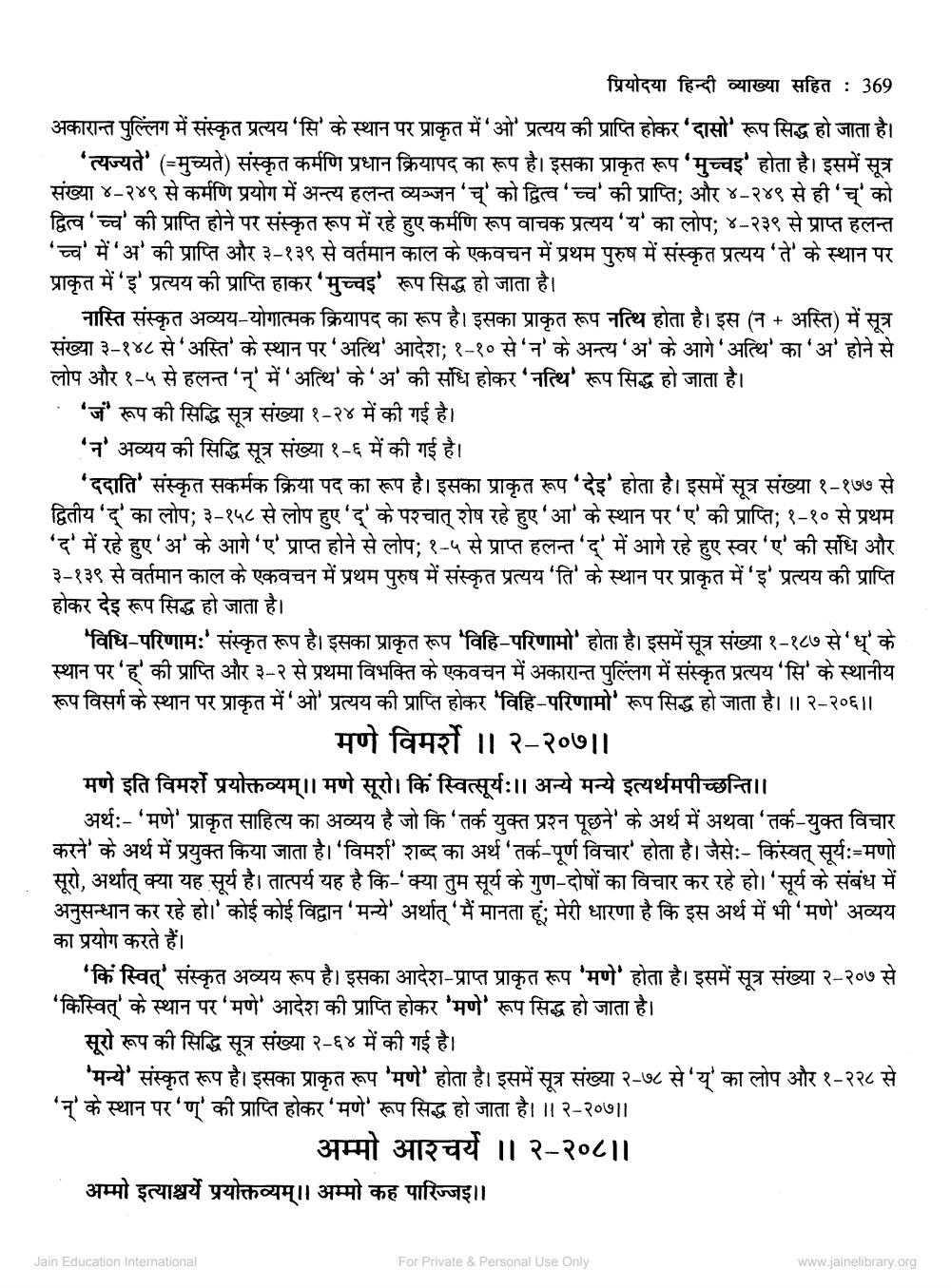________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 369 अकारान्त पुल्लिंग में संस्कृत प्रत्यय 'सि' के स्थान पर प्राकृत में 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'दासो' रूप सिद्ध हो जाता है। ___ 'त्यज्यते' (=मुच्यते) संस्कृत कर्मणि प्रधान क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'मुच्चइ' होता है। इसमें सूत्र संख्या ४-२४९ से कर्मणि प्रयोग में अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 'च' को द्वित्व 'च्च' की प्राप्ति; और ४-२४९ से ही 'च' को द्वित्व 'च्च' की प्राप्ति होने पर संस्कृत रूप में रहे हुए कर्मणि रूप वाचक प्रत्यय 'य' का लोप; ४-२३९ से प्राप्त हलन्त 'च्च' में 'अ' की प्राप्ति और ३-१३९ से वर्तमान काल के एकवचन में प्रथम पुरुष में संस्कृत प्रत्यय 'ते' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति हाकर 'मुच्चइ' रूप सिद्ध हो जाता है।
नास्ति संस्कृत अव्यय-योगात्मक क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रूप नत्थि होता है। इस (न + अस्ति) में सूत्र संख्या ३-१४८ से 'अस्ति' के स्थान पर 'अत्थि' आदेश; १-१० से 'न' के अन्त्य 'अ' के आगे 'अत्थि' का 'अ' होने से लोप और १-५ से हलन्त 'न्' में 'अत्थि' के 'अ' की संधि होकर 'नत्थि' रूप सिद्ध हो जाता है। - 'ज' रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-२४ में की गई है।
'न' अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या १-६ में की गई है।
'ददाति' संस्कृत सकर्मक क्रिया पद का रूप है। इसका प्राकृत रूप देइ' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१७७ से द्वितीय 'द्' का लोप; ३-१५८ से लोप हुए 'द्' के पश्चात् शेष रहे हुए 'आ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति; १-१० से प्रथम 'द' में रहे हुए 'अ' के आगे 'ए' प्राप्त होने से लोप; १-५ से प्राप्त हलन्त 'द्' में आगे रहे हुए स्वर 'ए' की संधि और ३-१३९ से वर्तमान काल के एकवचन में प्रथम पुरुष में संस्कृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर देइ रूप सिद्ध हो जाता है।
"विधि-परिणामः' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'विहि-परिणामो' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१८७ से ध्' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में संस्कृत प्रत्यय 'सि' के स्थानीय रूप विसर्ग के स्थान पर प्राकृत में 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'विहि-परिणामो' रूप सिद्ध हो जाता है। ।। २-२०६।।
मणे विमर्श ॥ २-२०७॥ मणे इति विमर्श प्रयोक्तव्यम्। मणे सूरो। किं स्वित्सूर्यः।। अन्ये मन्ये इत्यर्थमपीच्छन्ति।।
अर्थः- 'मणे' प्राकृत साहित्य का अव्यय है जो कि 'तर्क युक्त प्रश्न पूछने' के अर्थ में अथवा 'तर्क-युक्त विचार करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। 'विमर्श' शब्द का अर्थ 'तर्क-पूर्ण विचार होता है। जैसे:- किंस्वत् सूर्यः=मणो सूरो, अर्थात् क्या यह सूर्य है। तात्पर्य यह है कि-'क्या तुम सूर्य के गुण-दोषों का विचार कर रहे हो। सूर्य के संबंध में अनुसन्धान कर रहे हो। कोई कोई विद्वान 'मन्ये' अर्थात् 'मैं मानता हूं; मेरी धारणा है कि इस अर्थ में भी 'मणे' अव्यय का प्रयोग करते हैं। __'किं स्वित्' संस्कृत अव्यय रूप है। इसका आदेश-प्राप्त प्राकृत रूप 'मणे' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-२०७ से 'किस्वित्' के स्थान पर 'मणे' आदेश की प्राप्ति होकर 'मणे' रूप सिद्ध हो जाता है।
सूरो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या २-६४ में की गई है।
'मन्ये संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'मणे' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-७८ से 'य' का लोप और १-२२८ से 'न्' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति होकर 'मणे' रूप सिद्ध हो जाता है। ।। २-२०७॥
अम्मो आश्चर्य ।। २-२०८॥ अम्मो इत्याश्चर्ये प्रयोक्तव्यम्।। अम्मो कह पारिज्जइ।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org