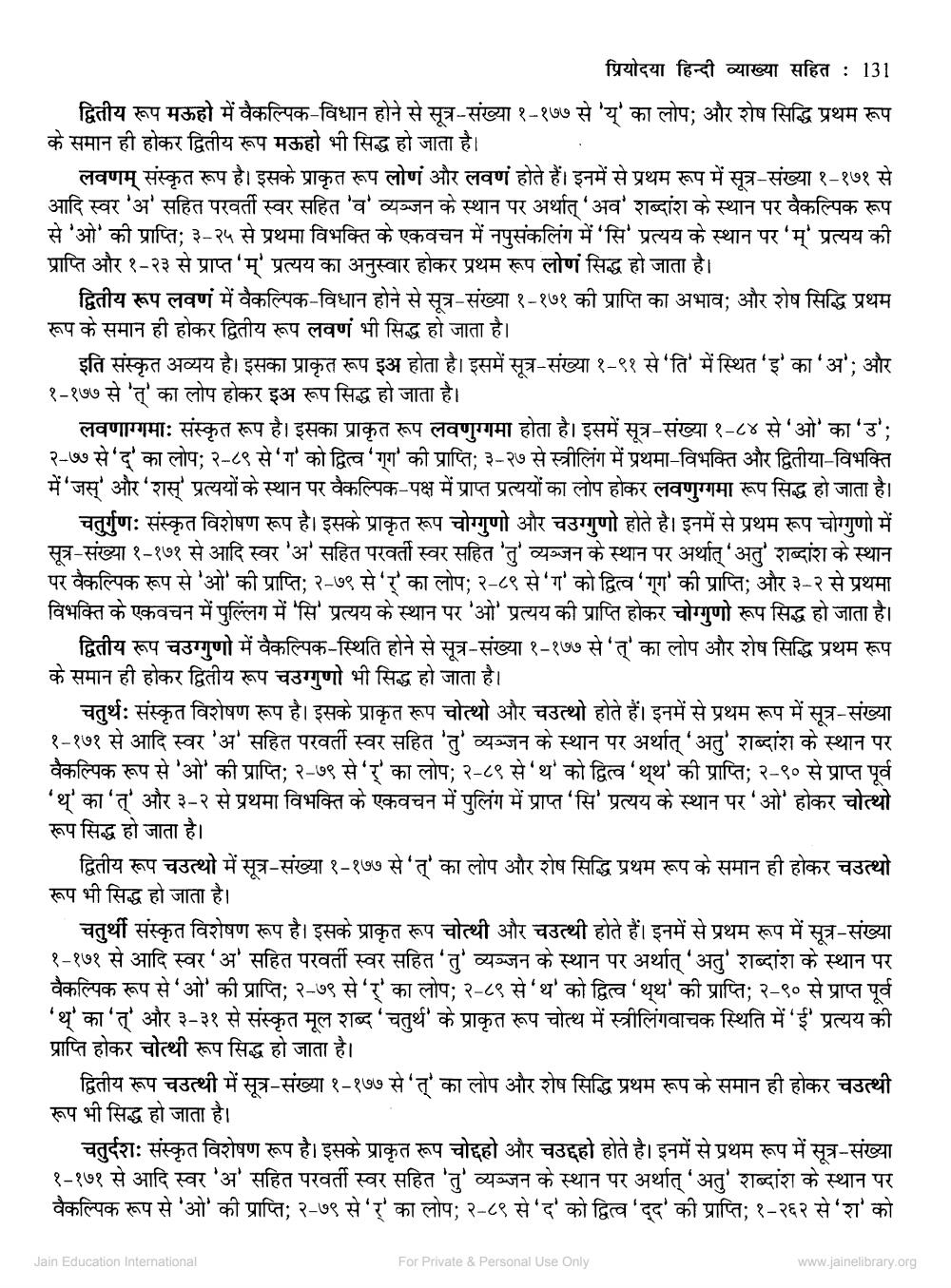________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 131 द्वितीय रूप मऊहो में वैकल्पिक-विधान होने से सूत्र-संख्या १-१७७ से 'य' का लोप; और शेष सिद्धि प्रथम रूप के समान ही होकर द्वितीय रूप मऊहो भी सिद्ध हो जाता है।
लवणम् संस्कृत रूप है। इसके प्राकृत रूप लोणं और लवणं होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-१७१ से
स्वर 'अ' सहित परवर्ती स्वर सहित 'व' व्यञ्जन के स्थान पर अर्थात् 'अव' शब्दांश के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'ओ' की प्राप्ति: ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में नपसंकलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'म्' प्रत्यय का अनुस्वार होकर प्रथम रूप लोणं सिद्ध हो जाता है।
द्वितीय रूप लवणं में वैकल्पिक-विधान होने से सूत्र-संख्या १-१७१ की प्राप्ति का अभाव; और शेष सिद्धि प्रथम रूप के समान ही होकर द्वितीय रूप लवणं भी सिद्ध हो जाता है।
इति संस्कृत अव्यय है। इसका प्राकृत रूप इअ होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-९१ से 'ति' में स्थित 'इ' का 'अ'; और १-१७७ से 'त्' का लोप होकर इअ रूप सिद्ध हो जाता है।
लवणाग्गमाः संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप लवणुग्गमा होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-८४ से 'ओ' का 'उ'; २-७७ से 'द्' का लोप; २-८९ से 'ग' को द्वित्व 'ग्ग' की प्राप्ति; ३-२७ से स्त्रीलिंग में प्रथमा-विभक्ति और द्वितीया-विभक्ति में 'जस्' और 'शस्' प्रत्ययों के स्थान पर वैकल्पिक-पक्ष में प्राप्त प्रत्ययों का लोप होकर लवणुग्गमा रूप सिद्ध हो जाता है। __ चतुर्गुणः संस्कृत विशेषण रूप है। इसके प्राकृत रूप चोग्गुणो और चउग्गुणो होते है। इनमें से प्रथम रूप चोग्गुणो में सूत्र-संख्या १-१७१ से आदि स्वर 'अ' सहित परवर्ती स्वर सहित 'तु' व्यञ्जन के स्थान पर अर्थात् 'अतु' शब्दांश के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'ओ' की प्राप्ति; २-७९ से 'र' का लोप; २-८९ से 'ग' को द्वित्व 'ग्ग' की प्राप्ति; और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर चोग्गुणो रूप सिद्ध हो जाता है।
द्वितीय रूप चउग्गुणो में वैकल्पिक-स्थिति होने से सूत्र-संख्या १-१७७ से 'त्' का लोप और शेष सिद्धि प्रथम रूप के समान ही होकर द्वितीय रूप चउग्गुणो भी सिद्ध हो जाता है।
चतुर्थः संस्कृत विशेषण रूप है। इसके प्राकृत रूप चोत्थो और चउत्थो होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-१७१ से आदि स्वर 'अ' सहित परवर्ती स्वर सहित 'तु' व्यञ्जन के स्थान पर अर्थात् 'अतु' शब्दांश के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'ओ' की प्राप्ति; २-७९ से 'र' का लोप; २-८९ से 'थ' को द्वित्व 'थ्थ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'थ्' का 'त्' और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पुलिंग में प्राप्त 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' होकर चोत्थो रूप सिद्ध हो जाता है।
द्वितीय रूप चउत्थो में सूत्र-संख्या १-१७७ से 'त्' का लोप और शेष सिद्धि प्रथम रूप के समान ही होकर चउत्थो रूप भी सिद्ध हो जाता है। __चतुर्थी संस्कृत विशेषण रूप है। इसके प्राकृत रूप चोत्थी और चउत्थी होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-१७१ से आदि स्वर 'अ' सहित परवर्ती स्वर सहित 'तु' व्यञ्जन के स्थान पर अर्थात् 'अतु' शब्दांश के स्थान पर
वैकल्पिक रूप से 'ओ' की प्राप्ति; २-७९ से 'र' का लोप; २-८९ से 'थ' को द्वित्व 'थ्थ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'थ्' का 'त्' और ३-३१ से संस्कृत मूल शब्द 'चतुर्थ' के प्राकृत रूप चोत्थ में स्त्रीलिंगवाचक स्थिति में 'ई' प्रत्यय की प्राप्ति होकर चोत्थी रूप सिद्ध हो जाता है।
द्वितीय रूप चउत्थी में सूत्र-संख्या १-१७७ से 'त्' का लोप और शेष सिद्धि प्रथम रूप के समान ही होकर चउत्थी रूप भी सिद्ध हो जाता है।
चतुर्दशः संस्कृत विशेषण रूप है। इसके प्राकृत रूप चोद्दहो और चउद्दहो होते है। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-१७१ से आदि स्वर 'अ' सहित परवर्ती स्वर सहित 'तु' व्यञ्जन के स्थान पर अर्थात् 'अतु' शब्दांश के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'ओ' की प्राप्ति; २-७९ से 'र' का लोप; २-८९ से 'द' को द्वित्व द्द' की प्राप्ति; १-२६२ से 'श' को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org