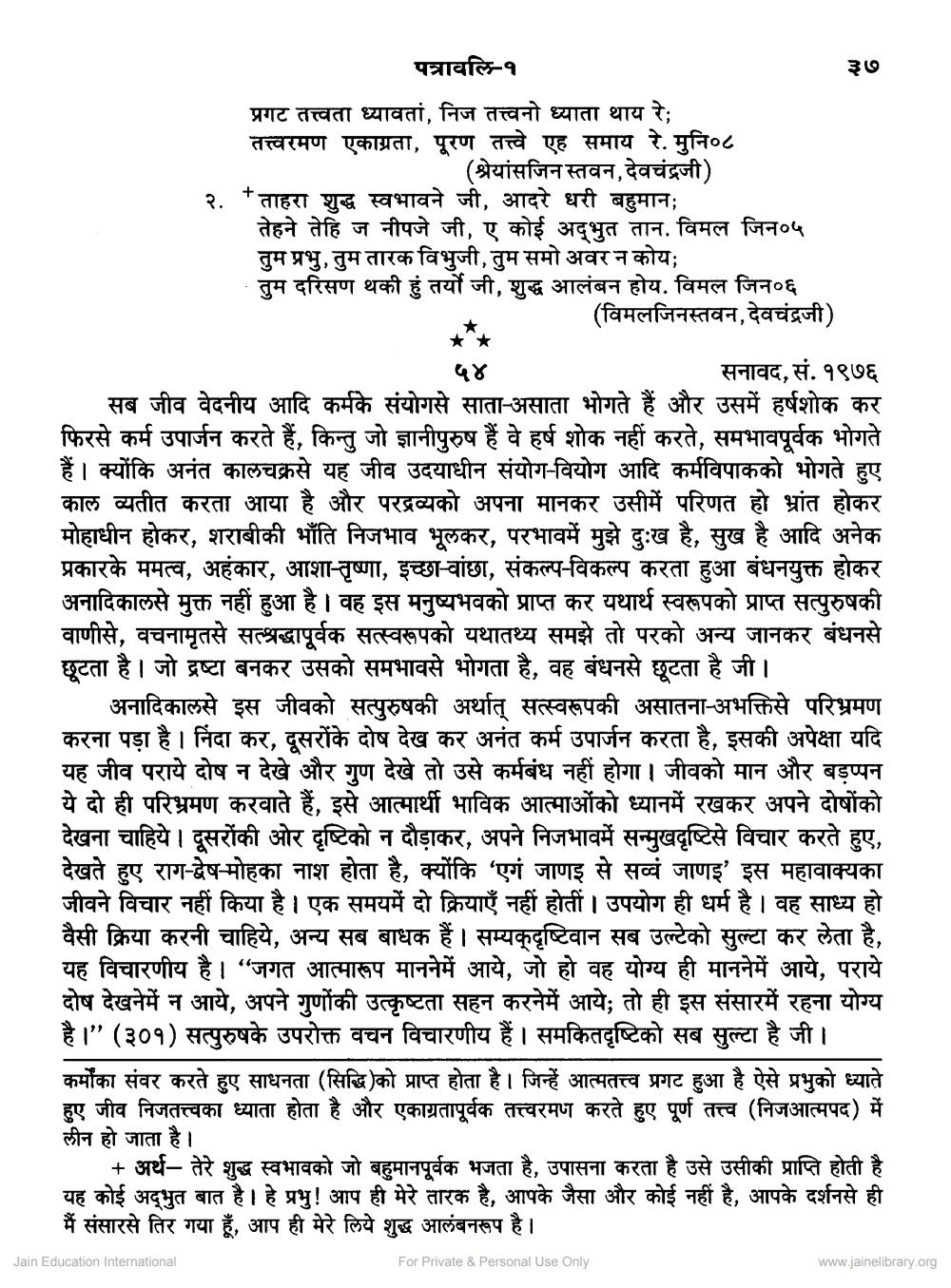________________
पत्रावलि - १
प्रगट तत्त्वता ध्यावतां, निज तत्त्वनो ध्याता थाय रे;
तत्त्वरमण एकाग्रता, पूरण तत्त्वे एह समाय रे. मुनि०८ (श्रेयांसजिन स्तवन, देवचंद्रजी )
+ २.
ताहरा शुद्ध स्वभावने जी, आदरे धरी बहुमान; तेहने तेहि ज नीपजे जी, ए कोई अद्भुत तान. विमल जिन०५ तुम प्रभु, तुम तारक विभुजी, तुम समो अवर न कोय;
तुम दरिसण थकी हुं तर्यो जी, शुद्ध आलंबन होय. विमल जिन०६ (विमलजिनस्तवन, देवचंद्रजी )
३७
५४
सनावद, सं. १९७६
सब जीव वेदनीय आदि कर्मके संयोगसे साता - असाता भोगते हैं और उसमें हर्षशोक कर फिरसे कर्म उपार्जन करते हैं, किन्तु जो ज्ञानीपुरुष हैं वे हर्ष शोक नहीं करते, समभावपूर्वक भोगते हैं। क्योंकि अनंत कालचक्रसे यह जीव उदयाधीन संयोग-वियोग आदि कर्मविपाकको भोगते हुए काल व्यतीत करता आया है और परद्रव्यको अपना मानकर उसीमें परिणत हो भ्रांत होकर मोहाधीन होकर, शराबीकी भाँति निजभाव भूलकर, परभावमें मुझे दुःख है, सुख है आदि अनेक प्रकारके ममत्व, अहंकार, आशा तृष्णा, इच्छा-वांछा, संकल्प-विकल्प करता हुआ बंधनयुक्त होकर अनादिकालसे मुक्त नहीं हुआ है । वह इस मनुष्यभवको प्राप्त कर यथार्थ स्वरूपको प्राप्त सत्पुरुषकी वाणीसे, वचनामृतसे सत्श्रद्धापूर्वक सत्स्वरूपको यथातथ्य समझे तो परको अन्य जानकर बंधनसे छूटता है । जो द्रष्टा बनकर उसको समभावसे भोगता है, वह बंधनसे छूटता है जी ।
अनादिकाल से इस जीवको सत्पुरुषकी अर्थात् सत्स्वरूपकी असातना - अभक्तिसे परिभ्रमण करना पड़ा है । निंदा कर, दूसरोंके दोष देख कर अनंत कर्म उपार्जन करता है, इसकी अपेक्षा यदि यह जीव पराये दोष न देखे और गुण देखे तो उसे कर्मबंध नहीं होगा । जीवको मान और बड़प्पन ये दो ही परिभ्रमण करवाते हैं, इसे आत्मार्थी भाविक आत्माओंको ध्यानमें रखकर अपने दोषोंको देखना चाहिये। दूसरोंकी ओर दृष्टिको न दौड़ाकर, अपने निजभावमें सन्मुखदृष्टिसे विचार करते हुए, देखते हुए राग-द्वेष-मोहका नाश होता है, क्योंकि 'एगं जाणइ से सव्वं जाणइ' इस महावाक्यका जीवने विचार नहीं किया है । एक समयमें दो क्रियाएँ नहीं होतीं । उपयोग ही धर्म है । वह साध्य हो वैसी क्रिया करनी चाहिये, अन्य सब बाधक हैं । सम्यकदृष्टिवान सब उल्टेको सुल्टा कर लेता है, यह विचारणीय है । " जगत आत्मारूप माननेमें आये, जो हो वह योग्य ही माननेमें आये, पराये दोष देखने में न आये, अपने गुणोंकी उत्कृष्टता सहन करनेमें आये; तो ही इस संसारमें रहना योग्य है ।" (३०१) सत्पुरुषके उपरोक्त वचन विचारणीय हैं । समकितदृष्टिको सब सुल्टा है जी ।
कर्मोंका संवर करते हुए साधनता (सिद्धि ) को प्राप्त होता है । जिन्हें आत्मतत्त्व प्रगट हुआ है ऐसे प्रभुको ध्या हुए जीव निजतत्त्वका ध्याता होता है और एकाग्रतापूर्वक तत्त्वरमण करते हुए पूर्ण तत्त्व (निजआत्मपद) में लीन हो जाता है ।
+ अर्थ - तेरे शुद्ध स्वभावको जो बहुमानपूर्वक भजता है, उपासना करता है उसे उसीकी प्राप्ति होती है यह कोई अद्भुत बात है । हे प्रभु! आप ही मेरे तारक है, आपके जैसा और कोई नहीं है, आपके दर्शनसे ही मैं संसारसे तिर गया हूँ, आप ही मेरे लिये शुद्ध आलंबनरूप है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org