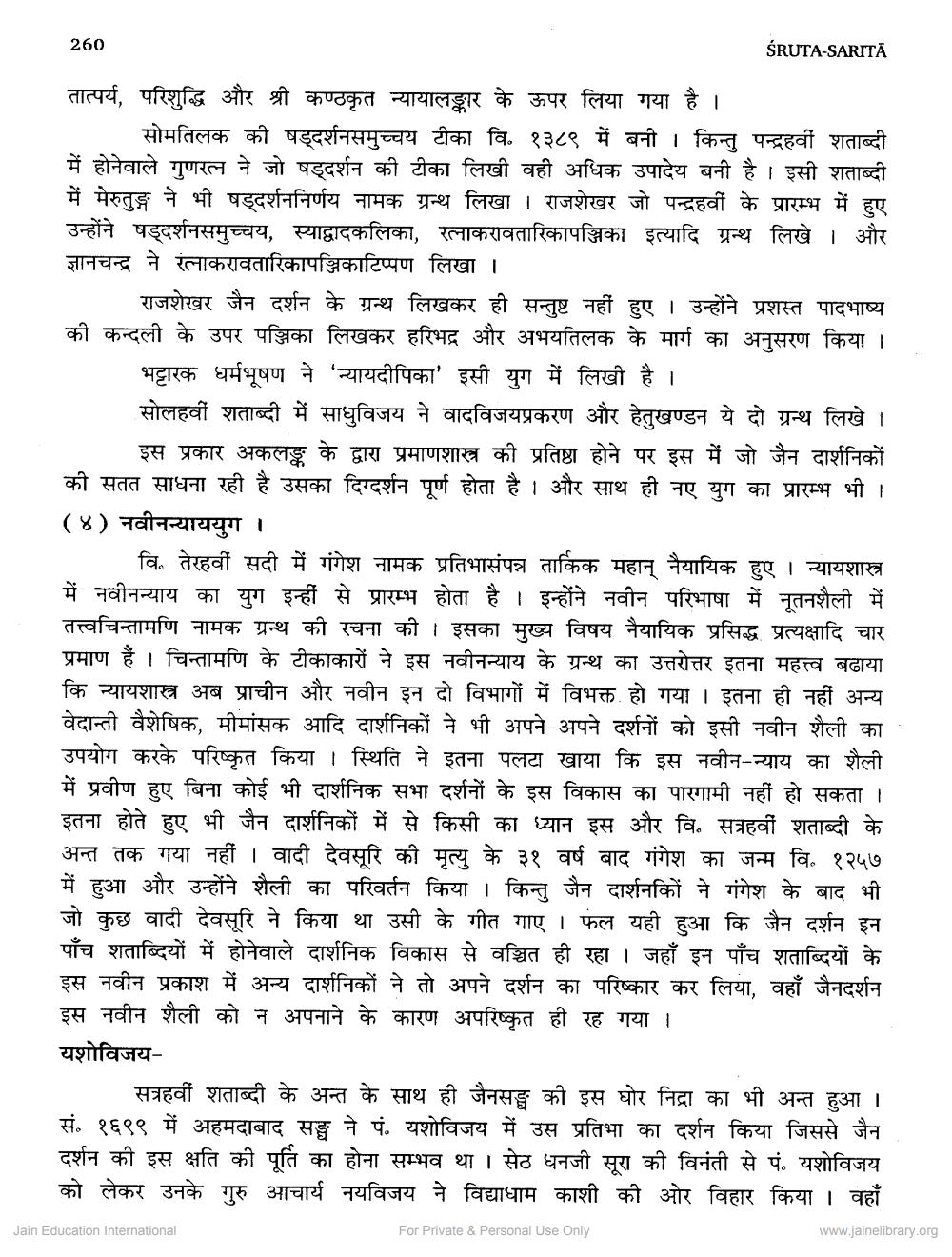________________
260
ŚRUTA-SARITĀ
ऊपर लिया गया है ।
तात्पर्य, परिशुद्धि और श्री कण्ठकृत न्यायालङ्कार के सोमतिलक की षड्दर्शनसमुच्चय टीका वि. १३८९ में बनी । किन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी में होनेवाले गुणरत्न ने जो षड्दर्शन की टीका लिखी वही अधिक उपादेय बनी है । इसी शताब्दी में मेरुतुङ्ग ने भी षड्दर्शननिर्णय नामक ग्रन्थ लिखा । राजशेखर जो पन्द्रहवीं के प्रारम्भ में हुए उन्होंने षड्दर्शनसमुच्चय, स्याद्वादकलिका, रत्नाकरावतारिकापञ्जिका इत्यादि ग्रन्थ लिखे । और ज्ञानचन्द्र ने रत्नाकरावतारिकापञ्जिकाटिप्पण लिखा ।
राजशेखर जैन दर्शन के ग्रन्थ लिखकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्होंने प्रशस्त पादभाष्य की कन्दली के उपर पञ्जिका लिखकर हरिभद्र और अभयतिलक के मार्ग का अनुसरण किया । भट्टारक धर्मभूषण ने 'न्यायदीपिका' इसी युग में लिखी है ।
सोलहवीं शताब्दी में साधुविजय ने वादविजयप्रकरण और हेतुखण्डन ये दो ग्रन्थ लिखे । इस प्रकार अकलङ्क के द्वारा प्रमाणशास्त्र की प्रतिष्ठा होने पर इस में जो जैन दार्शनिकों की सतत साधना रही है उसका दिग्दर्शन पूर्ण होता है । और साथ ही नए युग का प्रारम्भ भी । (४) नवीनन्याययुग ।
वि. तेरहवीं सदी में गंगेश नामक प्रतिभासंपन्न तार्किक महान् नैयायिक हुए । न्यायशास्त्र में नवीनन्याय का युग इन्हीं से प्रारम्भ होता है । इन्होंने नवीन परिभाषा में नूतनशैली में तत्त्वचिन्तामणि नामक ग्रन्थ की रचना की । इसका मुख्य विषय नैयायिक प्रसिद्ध प्रत्यक्षादि चार प्रमाण हैं । चिन्तामणि के टीकाकारों ने इस नवीनन्याय के ग्रन्थ का उत्तरोत्तर इतना महत्त्व बढाया कि न्यायशास्त्र अब प्राचीन और नवीन इन दो विभागों में विभक्त हो गया । इतना ही नहीं अन्य वेदान्ती वैशेषिक, मीमांसक आदि दार्शनिकों ने भी अपने-अपने दर्शनों को इसी नवीन शैली का उपयोग करके परिष्कृत किया । स्थिति ने इतना पलटा खाया कि इस नवीन न्याय का शैली
प्रवीण हुए बिना कोई भी दार्शनिक सभा दर्शनों के इस विकास का पारगामी नहीं हो सकता । इतना होते हुए भी जैन दार्शनिकों में से किसी का ध्यान इस और वि० सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक गया नहीं । वादी देवसूरि की मृत्यु के ३१ वर्ष बाद गंगेश का जन्म वि. १२५७ में हुआ और उन्होंने शैली का परिवर्तन किया । किन्तु जैन दार्शनकों ने गंगेश के बाद भी जो कुछ वादी देवसूरि ने किया था उसी के गीत गाए । फल यही हुआ कि जैन दर्शन इन पाँच शताब्दियों में होनेवाले दार्शनिक विकास से वञ्चित ही रहा । जहाँ इन पाँच शताब्दियों के इस नवीन प्रकाश में अन्य दार्शनिकों तो अपने दर्शन का परिष्कार कर लिया, वहाँ जैनदर्शन इस नवीन शैली को न अपनाने के कारण अपरिष्कृत ही रह गया ।
यशोविजय
सत्रहवीं शताब्दी के अन्त के साथ ही जैनसङ्घ की इस घोर निद्रा का भी अन्त हुआ । सं. १६९९ में अहमदाबाद सङ्घ ने पं. यशोविजय में उस प्रतिभा का दर्शन किया जिससे जैन दर्शन की इस क्षति की पूर्ति का होना सम्भव था । सेठ धनजी सूरा की विनंती से पं. यशोविजय को लेकर उनके गुरु आचार्य नयविजय ने विद्याधाम काशी की ओर विहार किया । वहाँ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org