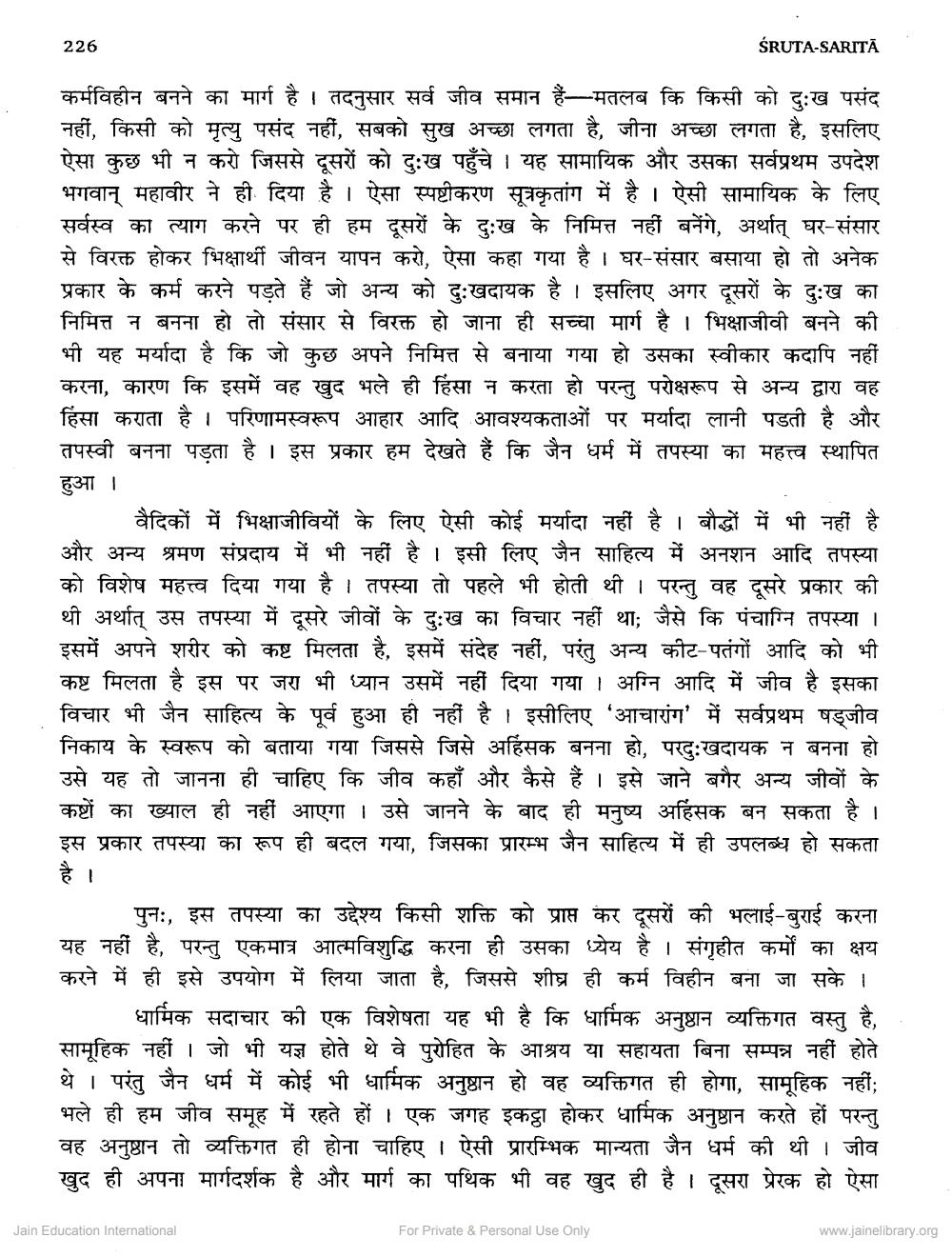________________
ŚRUTA-SARITĀ
कर्मविहीन बनने का मार्ग है । तदनुसार सर्व जीव समान हैं— मतलब कि किसी को दुःख पसंद नहीं, किसी को मृत्यु पसंद नहीं, सबको सुख अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा कुछ भी न करो जिससे दूसरों को दुःख पहुँचे । यह सामायिक और उसका सर्वप्रथम उपदेश भगवान् महावीर ने ही दिया है। ऐसा स्पष्टीकरण सूत्रकृतांग में है । ऐसी सामायिक के लिए सर्वस्व का त्याग करने पर ही हम दूसरों के दुःख के निमित्त नहीं बनेंगे, अर्थात् घर-संसार से विरक्त होकर भिक्षार्थी जीवन यापन करो, ऐसा कहा गया है। घर-संसार बसाया हो तो अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं जो अन्य को दुःखदायक है । इसलिए अगर दूसरों के दुःख का निमित्त न बनना हो तो संसार से विरक्त हो जाना ही सच्चा मार्ग है । भिक्षाजीवी बनने की भी यह मर्यादा है कि जो कुछ अपने निमित्त से बनाया गया हो उसका स्वीकार कदापि नहीं करना, कारण कि इसमें वह खुद भले ही हिंसा न करता हो परन्तु परोक्षरूप से अन्य द्वारा वह हिंसा कराता है । परिणामस्वरूप आहार आदि आवश्यकताओं पर मर्यादा लानी पडती है और तपस्वी बनना पड़ता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म में तपस्या का महत्त्व स्थापित हुआ ।
226
वैदिकों में भिक्षाजीवियों के लिए ऐसी कोई मर्यादा नहीं है । बौद्धों में भी नहीं है और अन्य श्रमण संप्रदाय में भी नहीं है । इसी लिए जैन साहित्य में अनशन आदि तपस्या को विशेष महत्त्व दिया गया है । तपस्या तो पहले भी होती थी । परन्तु वह दूसरे प्रकार की थी अर्थात् उस तपस्या में दूसरे जीवों के दुःख का विचार नहीं था; जैसे कि पंचाग्नि तपस्या । इसमें अपने शरीर को कष्ट मिलता है, इसमें संदेह नहीं, परंतु अन्य कीट-पतंगों आदि को भी कष्ट मिलता है इस पर जरा भी ध्यान उसमें नहीं दिया गया । अग्नि आदि में जीव है इसका विचार भी जैन साहित्य के पूर्व हुआ ही नहीं है । इसीलिए 'आचारांग' में सर्वप्रथम षड्जीव निकाय के स्वरूप को बताया गया जिससे जिसे अहिंसक बनना हो, परदुःखदायक न बनना हो उसे यह तो जानना ही चाहिए कि जीव कहाँ और कैसे हैं । इसे जाने बगैर अन्य जीवों के कष्टों का ख्याल ही नहीं आएगा । उसे जानने के बाद ही मनुष्य अहिंसक बन सकता है । इस प्रकार तपस्या का रूप ही बदल गया, जिसका प्रारम्भ जैन साहित्य में ही उपलब्ध हो सकता है ।
पुनः, इस तपस्या का उद्देश्य किसी शक्ति को प्राप्त कर दूसरों की भलाई - बुराई करना यह नहीं है, परन्तु एकमात्र आत्मविशुद्धि करना ही उसका ध्येय है । संगृहीत कर्मों का क्षय करने में ही इसे उपयोग में लिया जाता है, जिससे शीघ्र ही कर्म विहीन बना जा सके । धार्मिक सदाचार की एक विशेषता यह भी है कि धार्मिक अनुष्ठान व्यक्तिगत वस्तु है, सामूहिक नहीं । जो भी यज्ञ होते थे वे पुरोहित के आश्रय या सहायता बिना सम्पन्न नहीं होते थे । परंतु जैन धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो वह व्यक्तिगत ही होगा, सामूहिक नहीं; भले ही हम जीव समूह में रहते हों । एक जगह इकट्ठा होकर धार्मिक अनुष्ठान करते हों परन्तु वह अनुष्ठान तो व्यक्तिगत ही होना चाहिए । ऐसी प्रारम्भिक मान्यता जैन धर्म की थी । जीव खुद ही अपना मार्गदर्शक है और मार्ग का पथिक भी वह खुद ही है । दूसरा प्रेरक हो ऐसा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org