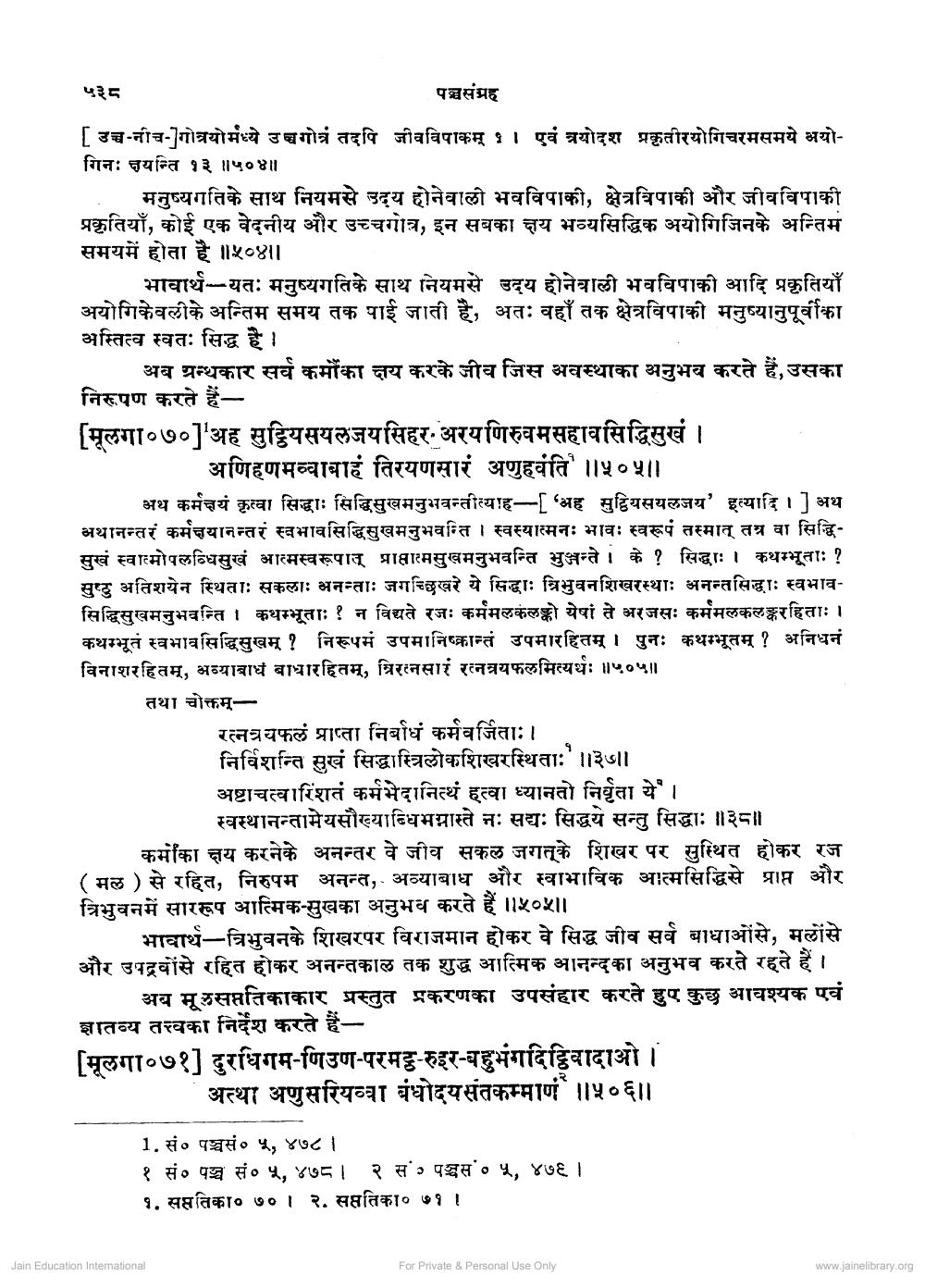________________
५३८
पञ्चसंग्रह
[ उच्च-नीच-गोत्रयोमध्ये उच्चगोत्रं तदपि जीवविपाकम् । एवं त्रयोदश प्रकृतीरयोगिचरमसमये अयोगिनः जयन्ति १३ ॥५०४॥ ... मनुष्यगतिके साथ नियमसे उदय होनेवाली भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियाँ, कोई एक वेदनीय और उच्चगोत्र, इन सबका क्षय भव्यसिद्धिक अयोगिजिनके अन्तिम समयमें होता है ॥५०४।।
भावार्थ-यतः मनुष्यगतिके साथ नियमसे उदय होनेवाली भवविपाकी आदि प्रकृतियाँ अयोगिकेवलीके अन्तिम समय तक पाई जाती है, अतः वहाँ तक क्षेत्रविपाकी मनुष्यानुपूर्वीका अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। ___अब ग्रन्थकार सर्व कर्मोंका क्षय करके जीव जिस अवस्थाका अनुभव करते हैं, उसका निरूपण करते हैं[मूलगा०७०]'अह सुट्टियसयलजयसिहर अरयणिरुवमसहावसिद्धिसुखं ।
अणिहणमव्वाबाहं तिरयणसारं अणुहवंति ॥५०॥ अथ कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धाः सिद्धिसुखमनुभवन्तीत्याह-['अह मुठियसयलजय' इत्यादि । ] अथ अथानन्तरं कर्मक्षयानन्तरं स्वभावसिद्धिसुखमनुभवन्ति । स्वस्यात्मनः भावः स्वरूपं तस्मात् तत्र वा सिद्धिसुखं स्वात्मोपलब्धिसुखं आत्मस्वरूपात् प्रातात्मसुखमनुभवन्ति भुञ्जन्ते । के ? सिद्धाः। कथम्भूताः? सुष्टु अतिशयेन स्थिताः सकलाः अनन्ताः जगच्छिखरे ये सिद्धाः त्रिभुवनशिखरस्थाः अनन्तसिद्धाः स्वभावसिद्धिसखमनभवन्ति । कथम्भूताः१ न विद्यते रजः कर्ममलकलतो येषां ते अरजसः कर्ममलकलङ्करहिताः । कथम्भूतं स्वभावसिद्धिसुखम् ? निरूपमं उपमानिष्क्रान्तं उपमारहितम् । पुनः कथम्भूतम् ? अनिधनं विनाशरहितम्, अव्याबा, बाधारहितम्, त्रिरत्नसारं रत्नत्रयफलमित्यर्थः ॥५०५॥ तथा चोक्तम्
रत्नत्रयफलं प्राप्ता निर्बाधं कर्मवर्जिताः। निर्विशन्ति सुखं सिद्धास्त्रिलोकशिखरस्थिताः ॥३७॥ अष्टाचत्वारिंशतं कर्मभेदानित्थं हत्वा ध्यानतो निर्वृता ये।
स्वस्थानन्तामेयसौख्याब्धिमनास्ते नः सद्यः सिद्धये सन्तु सिद्धाः ॥३८॥ कर्मीका क्षय करनेके अनन्तर वे जीव सकल जगत्के शिखर पर सुस्थित होकर रज ( मल ) से रहित, निरुपम अनन्त, अव्याबाध और स्वाभाविक आत्मसिद्धिसे प्राप्त और त्रिभुवनमें साररूप आत्मिक-सुखका अनुभव करते हैं ।।५०५।।
भावार्थ-त्रिभुवनके शिखरपर विराजमान होकर वे सिद्ध जीव सर्व बाधाओंसे, मलोंसे और उपद्रवोंसे रहित होकर अनन्तकाल तक शुद्ध आत्मिक आनन्दका अनुभव करते रहते हैं।
_अब मूलसप्ततिकाकार प्रस्तुत प्रकरणका उपसंहार करते हुए कुछ आवश्यक एवं ज्ञातव्य तत्त्वका निर्देश करते हैं[मूलगा०७१] दुरधिगम-णिउण-परमट्ठ-रुइर-बहुभंगदिढिवादाओ।
अत्था अणुसरियव्या बंधोदयसंतकम्माणं ॥५०६॥
1. सं० पञ्चसं० ५, ४७८ । १ सं० पञ्च सं०५, ४७८। २ स पञ्चस० ५, ४७६ । १. सप्ततिका० ७० । २. सप्ततिका० ७१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org