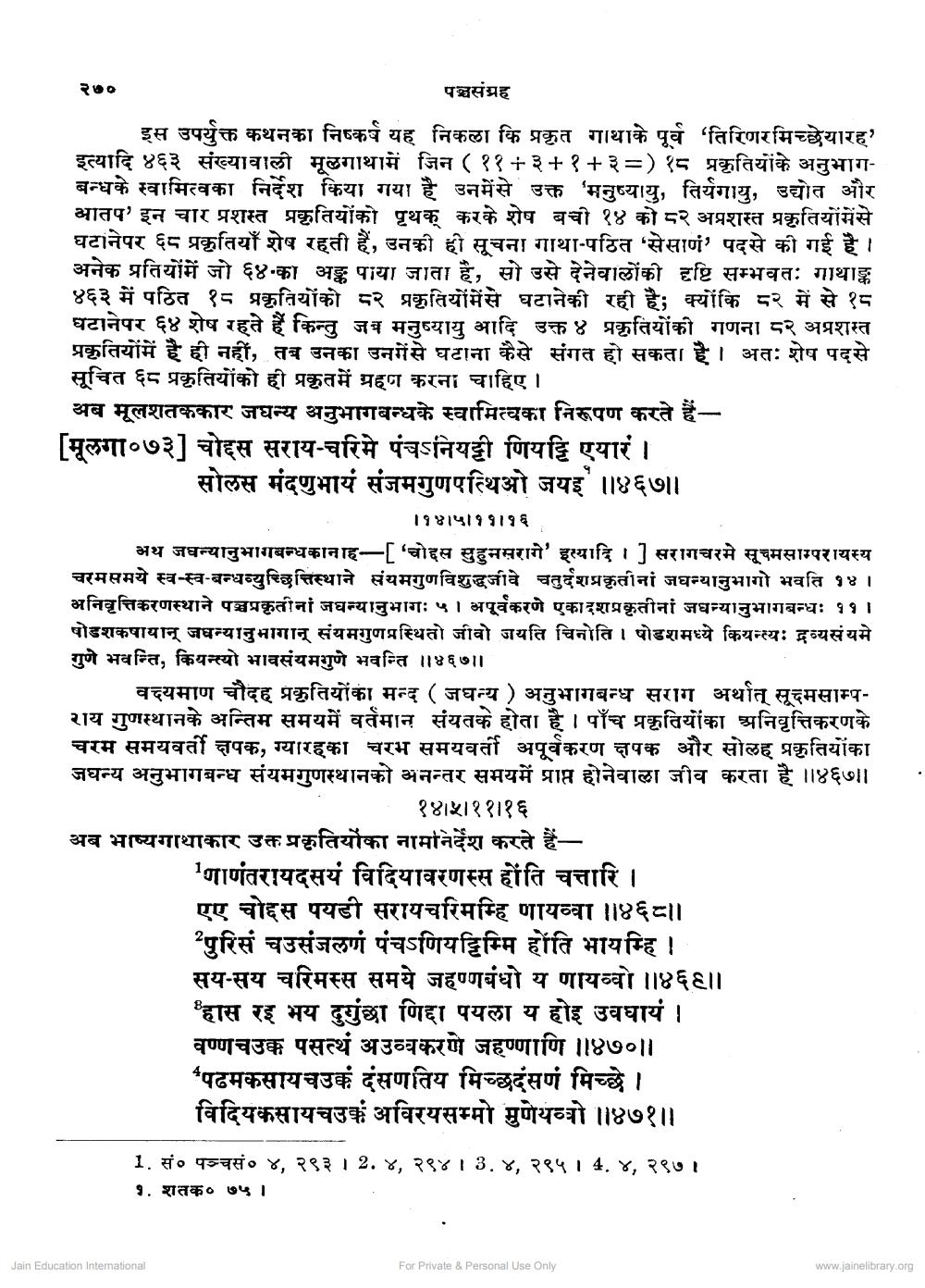________________
पञ्चसंग्रह
इस उपर्युक्त कथनका निष्कर्ष यह निकला कि प्रकृत गाथाके पूर्व 'तिरिणरमिच्छेयारह' इत्यादि ४६३ संख्यावाली मूलगाथामें जिन (११+३+१+३=) १८ प्रकृतियोंके अनुभागबन्धके स्वामित्वका निर्देश किया गया है उनमें से उक्त 'मनुष्यायु, तिर्यगायु, उद्योत और आतप' इन चार प्रशस्त प्रकृतियोंको पृथक् करके शेष बची १४ को ८२ अप्रशस्त प्रकृतियोंमेंसे घटानेपर ६८ प्रकृतियाँ शेष रहती हैं, उनकी ही सूचना गाथा-पठित 'सेसाणं' पदसे की गई है। अनेक प्रतियोंमें जो ६४.का अङ्क पाया जाता है, सो उसे देनेवालोंकी दृष्टि सम्भवतः गाथाङ्क ४६३ में पठित १८ प्रकृतियोंको ८२ प्रकृतियोंमेंसे घटानेकी रही है। क्योंकि ८२ में से १८ घटानेपर ६४ शेष रहते हैं किन्तु जब मनुष्यायु आदि उक्त ४ प्रकृतियोंकी गणना ८२ अप्रशस्त प्रकृतियोंमें है ही नहीं, तब उनका उनमेंसे घटाना कैसे संगत हो सकता है। अतः शेष पदसे सूचित ६८ प्रकृतियोंको ही प्रकृतमें ग्रहण करना चाहिए । अब मूलशतककार जघन्य अनुभागबन्धके स्वामित्वका निरूपण करते हैं[मूलगा०७३] चोदस सराय-चरिमे पंचनियट्टी णियट्टि एयारं । सोलस मंदणुभायं संजमगुणपत्थिओ जयइ ॥४६७॥
।१४।५।११।१६ अथ जघन्यानुभागबन्धकानाह-['चोद्दस सुहुनसरागे' इत्यादि । ] सरागचरमे सूचमसाम्परायस्य चरमसमये स्व-स्व-बन्धव्युच्छित्तिस्थाने संयमगुणविशुद्धजीवे चतुर्दशप्रकृतीनां जघन्यानुभागो भवति १४ । अनिवृत्तिकरणस्थाने पञ्चप्रकृतीनां जघन्यानुभागः ५। अपूर्वकरणे एकादशप्रकृतीनां जघन्यानुभागबन्धः ११ । षोडशकषायान् जघन्यानुभागान् संयमगुणप्रस्थितो जीवो जयति चिनोति । षोडशमध्ये कियन्त्यः द्रव्यसंयमे गुणे भवन्ति, कियन्स्यो भावसंयमगुणे भवन्ति ॥४६७॥
वक्ष्यमाण चौदह प्रकृतियोंका मन्द ( जघन्य ) अनुभागबन्ध सराग अर्थात् सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें वर्तमान संयतके होता है । पाँच प्रकृतियोंका अनिवृत्तिकरणके चरम समयवर्ती क्षपक, ग्यारहका चरम समयवर्ती अपूर्वकरण क्षपक और सोलह प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध संयमगुणस्थानको अनन्तर समयमें प्राप्त होनेवाला जीव करता है ॥४६७।।
१४।५।११।१६ अब भाष्यगाथाकार उक्त प्रकृतियोका नामनिर्देश करते हैं
'णाणंतरायदसयं विदियावरणस्स होंति चत्तारि । एए चोद्दस पयडी सरायचरिमम्हि णायव्वा ॥४६८॥ 'पुरिसं चउसंजलणं पंचऽणियट्टिम्मि होंति भायम्हि । सय-सय चरिमस्स समये जहण्णबंधो य णायव्वो॥४६६॥ हास रइ भय दुगुंछा णिद्दा पयला य होइ उवधायं । वण्णचउक्क पसत्थं अउव्यकरणे जहण्णाणि ॥४७०॥ 'पढमकसायचउकं दसणतिय मिच्छदंसणं मिच्छे । विदियकसायचउर्फ अविरयसम्मो मुणेयव्यो ॥४७१॥
1. सं० पञ्चसं० ४, २९३ । 2. ४, २९४ । 3. ४, २९५ । 4. ४, २९७ । १. शतक० ७५ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org