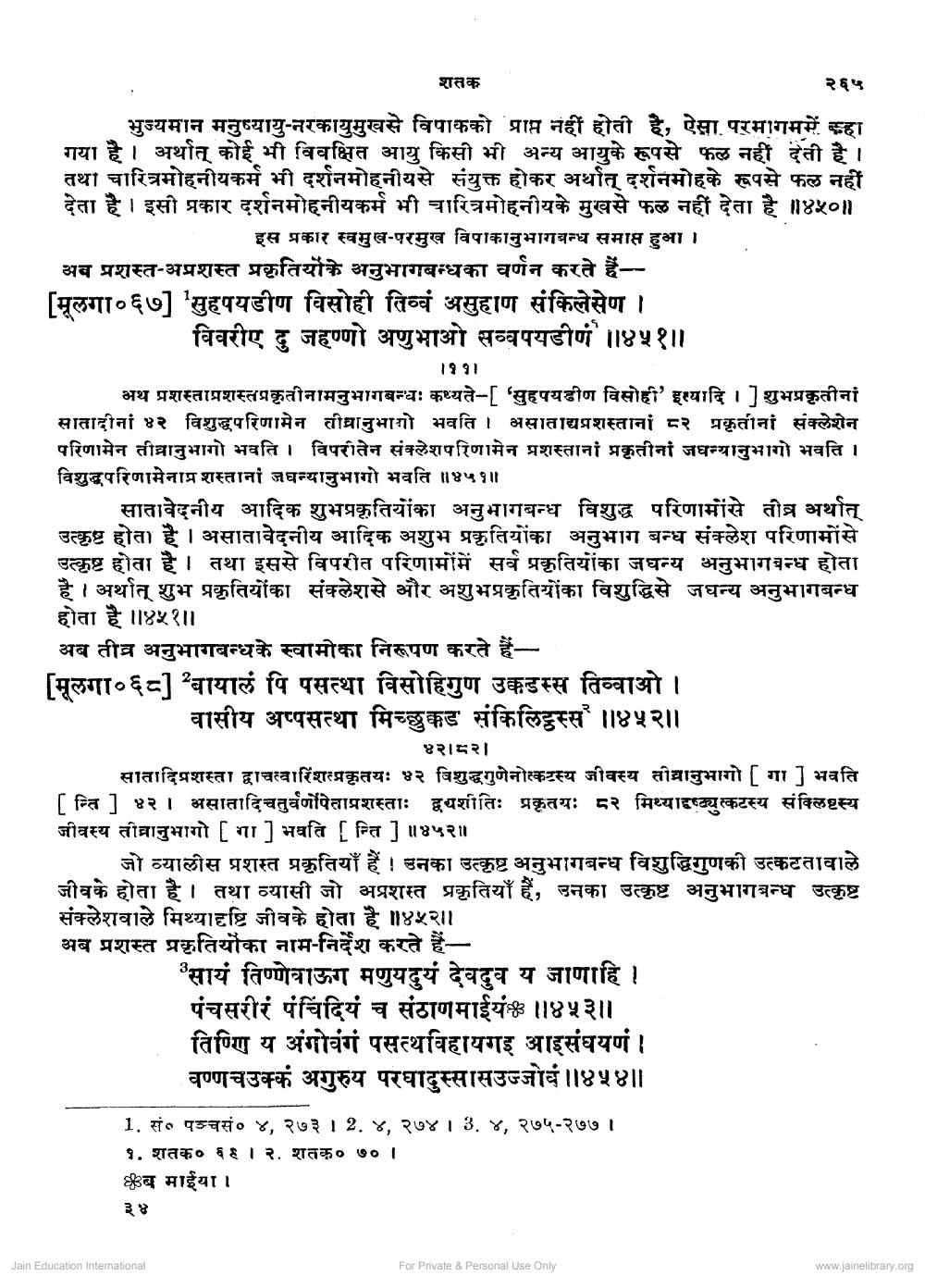________________
शतक
२६५
भुज्यमान मनुष्यायु-नरकायुमुखसे विपाकको प्राप्त नहीं होती है, ऐसा. परमागममें कहा गया है। अर्थात् कोई भी विवक्षित आयु किसी भी अन्य आयुके रूपसे फल नहीं देती है। तथा चारित्रमोहनीयकर्म भी दर्शनमोहनीयसे संयुक्त होकर अर्थात् दर्शनमोहके रूपसे फल नहीं देता है । इसी प्रकार दर्शनमोहनीयकर्म भी चारित्रमोहनीयके मुखसे फल नहीं देता है ॥४५०॥
___इस प्रकार स्वमुख-परमुख विपाकानुभागबन्ध समाप्त हुआ। अव प्रशस्त-अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागबन्धका वर्णन करते हैं-- [मूलगा०६७] 'सुहपयडीण विसोही तिव्वं असुहाण संकिलेसेण । विवरीए दु जहण्णो अणुभाओ सव्वपयडीणं ॥४५१॥
११॥ अथ प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृतीनामनुभागबन्धः कथ्यते-[ 'सुहपयढीण विसोही' इत्यादि । शुभप्रकृतीनां सातादीनां ४२ विशुद्धपरिणामेन तीवानुभागो भवति । असाताद्यप्रशस्तानां ८२ प्रकृतीनां संक्लेशेन परिणामेन तीव्रानुभागो भवति । विपरीतेन संक्लेशपरिणामेन प्रशस्तानां प्रकृतीनां जघन्यानुभागो भवति । विशुद्धपरिणामेनाप्रशस्तानां जघन्यानुभागो भवति ॥४५१॥
सातावेदनीय आदिक शुभप्रकृतियोंका अनुभागबन्ध विशुद्ध परिणामोंसे तीव्र अर्थात् उत्कृष्ट होता है । असातावेदनीय आदिक अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध संक्लेश परिणामोंसे उत्कृष्ट होता है। तथा इससे विपरीत परिणामोंमें सर्व प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध होता है । अर्थात् शुभ प्रकृतियोंका संक्लेशसे और अशुभप्रकृतियोंका विशुद्धिसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है ।।४५१॥
अब तीव्र अनुभागबन्धके स्वामोका निरूपण करते हैं[मूलगा०६८] "वायालं पि पसत्था विसोहिगुण उक्कडस्स तिव्वाओ । वासीय अप्पसत्था मिच्छुक्कड' संकिलिट्ठस्स ॥४५२।।
४२१८२ सातादिप्रशस्ता द्वाचत्वारिंशत्प्रकृतयः ४२ विशुद्धगुणेनोत्कटस्य जीवस्य तीयानुभागो[गा ] भवति [न्ति] ४२ । असातादिचतुर्वर्णोपेताप्रशस्ता: द्वयशीतिः प्रकृतयः ८२ मिथ्यादृष्ट्यत्कटस्य संक्लिष्टस्य जीवस्य तीव्रानुभागो [गा] भवति [न्ति ] ॥४५२॥
__ जो व्यालीस प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध विशुद्धिगुणकी उत्कटतावाले जीवके होता है। तथा व्यासी जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं, उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥४५२।। अब प्रशस्त प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं
"सायं तिण्णेवाऊग मणुयदुयं देवदुव य जाणाहि । पंचसरीरं पंचिंदियं च संठाणमाईयं ॥४५३॥ तिण्णि य अंगोवंगं पसत्थविहायगइ आइसंघयणं ।
वण्णचउक्कं अगुरुय परघादुस्सासउज्जोवं ॥४५४॥ 1. सं० पञ्चसं० ४, २७३ । 2. ४, २७४ । 3. ४, २७५-२७७ । १. शतक०६६ । २. शतक०७० । *ब माईया।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org