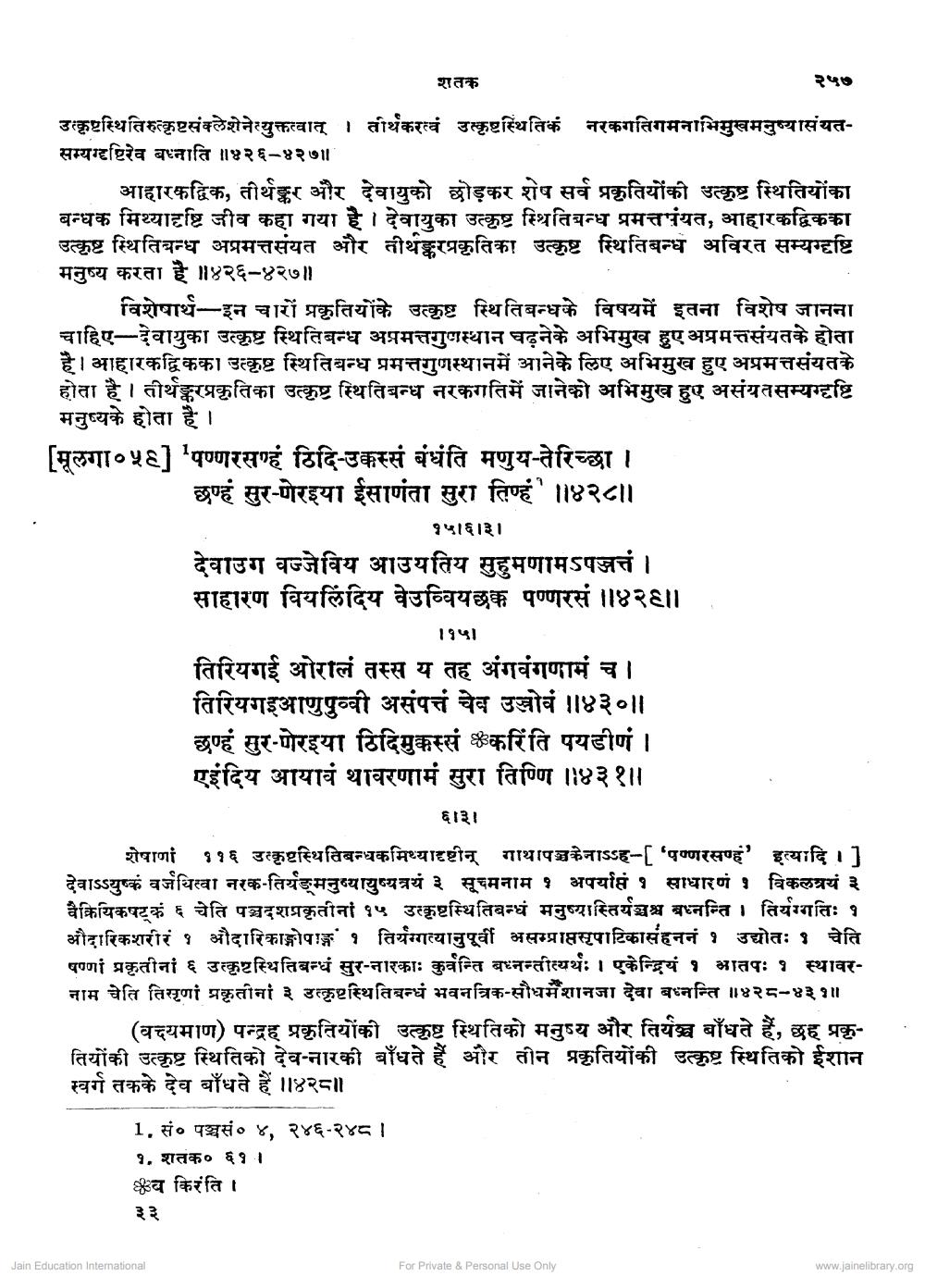________________
शतक
उत्कृष्टस्थितिरुत्कृष्टसंक्लेशेनेत्युक्तत्वात् । तीर्थकरत्वं उत्कृष्टस्थितिकं नरकगतिगमनाभिमुखमनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टिरेव बध्नाति ॥४२६-४२७॥
आहारकद्विक, तीर्थङ्कर और देवायुको छोड़कर शेष सर्व प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितियोंका बन्धक मिथ्यादृष्टि जीव कहा गया है। देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रमत्तपंयत, आहारकद्विकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अप्रमत्तसंयत और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य करता है ॥४२६-४२७॥
विशेषार्थ-इन चारों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके विषयमें इतना विशेष जानना चाहिए-देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अप्रमत्तगुणस्थान चढ़नेके अभिमुख हुए अप्रमत्तसंयतके होता है। आहारकद्विकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रमत्तगुणस्थानमें आनेके लिए अभिमुख हुए अप्रमत्तसंयतके होता है। तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नरकगतिमें जानेको अभिमुख हुए असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है। [मूलगा०५६] 'पण्णरसण्हं ठिदि-उक्कस्सं बंधंति मणुय-तेरिच्छा । छण्हं सुर-णेरड्या ईसाणंता सुरा तिण्हं ॥४२८॥
१५।६।३। देवाउग वज्जेविय आउयतिय सुहुमणामऽपजत्तं । साहारण वियलिंदिय वेउव्वियछक्क पण्णरसं ॥४२६।।
।१५। तिरियगई ओरालं तस्स य तह अंगवंगणामं च । तिरियगइआणुपुव्वी असंपत्तं चेव उखोवं ॥४३०॥ छण्हं सुर-गेरइया ठिदिमुक्कस्सं *करिंति पयडीणं । एइंदिय आयावं थावरणामं सुरा तिण्णि ॥४३१॥
६।३।
शेषाणां ११६ उत्कृष्टस्थितिबन्धकमिथ्यादृष्टीन् गाथापञ्चकेनाऽऽह-['पण्णरसण्ह' इत्यादि।1 देवाऽऽयुष्कं वर्जयित्वा नरक-तियङ्मनुष्यायुष्यत्रयं ३ सूचमनाम . अपर्याप्तं १ साधारणं, विकलत्रयं ३ वैक्रियिकषट्कं ६ चेति पञ्चदशप्रकृतीनां १५ उत्कृष्टस्थितिबन्धं मनुष्यास्तिर्यञ्चश्च बध्नन्ति । तिर्यग्गतिः १ औदारिकशरीरं १ औदारिकाङ्गोपाङ्ग तिर्यग्गत्यानुपूर्वी असम्प्राप्तसृपाटिकासंहननं १ उद्योतः १ चेति पण्णां प्रकृतीनां ६ उत्कृष्ट स्थितिबन्धं सुर-नारकाः कुर्वन्ति बध्नन्तीत्यर्थः । एकेन्द्रियं १ आतपः १ स्थावरनाम चेति तिसृणां प्रकृतीनां ३ उत्कृष्टस्थितिबन्धं भवनत्रिक-सौधर्मशानजा देवा बध्नन्ति ॥४२८-४३१॥
(वक्ष्यमाण) पन्द्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको मनुष्य और तिर्यञ्च बाँधते हैं, छह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको देव-नारकी बाँधते हैं और तीन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको ईशान स्वर्ग तकके देव बाँधते हैं ।।४२८॥
1. सं० पञ्चसं० ४, २४६-२४८ । १. शतक० ६१ कब किरंति । ३३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org