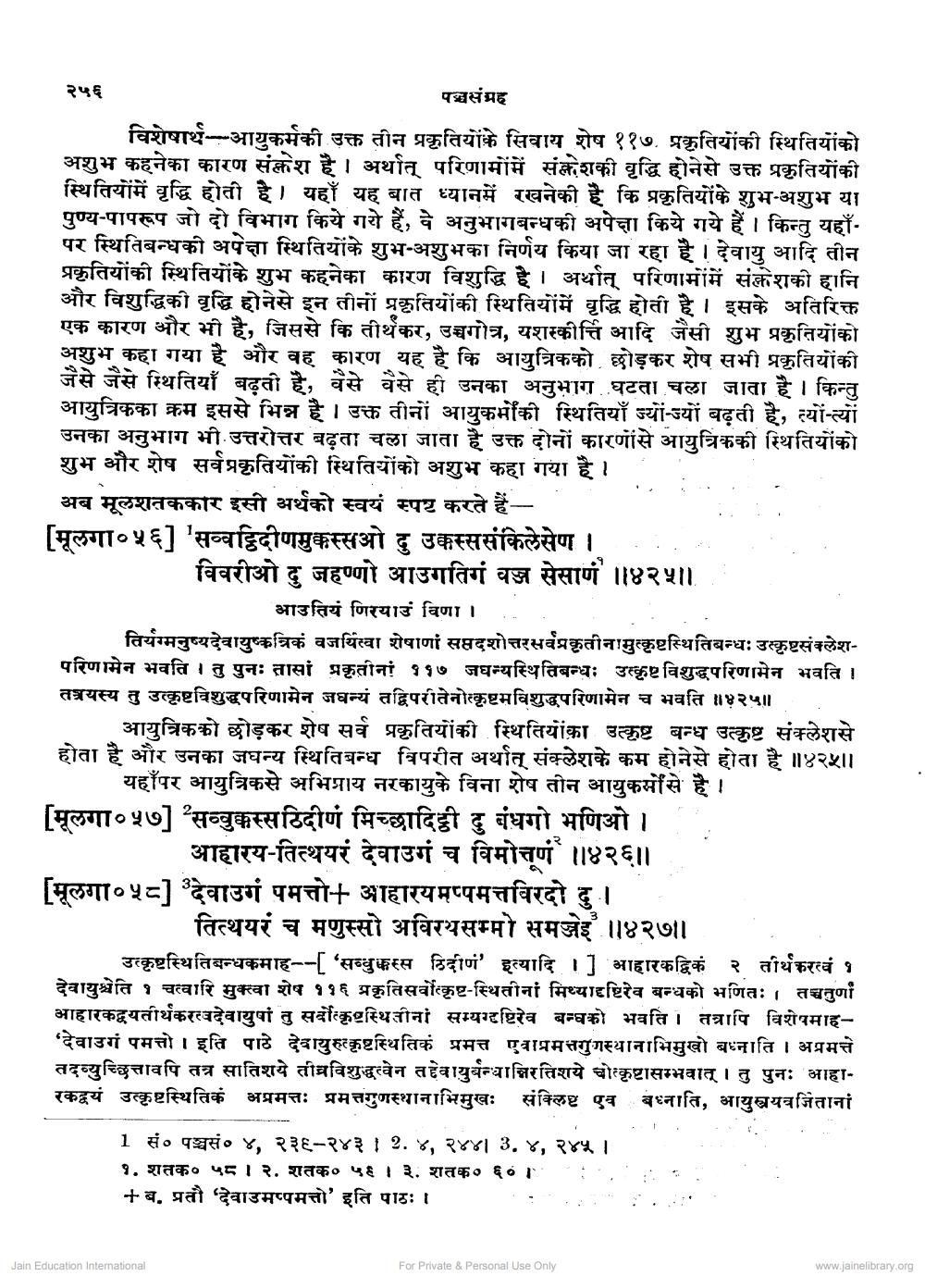________________
२५६
पञ्चसंग्रह विशेषार्थ-आयुकर्मकी उक्त तीन प्रकृतियोंके सिवाय शेष ११७. प्रकृतियोंकी स्थितियोंको अशुभ कहनेका कारण संक्लेश है। अर्थात् परिणामोंमें संलोशकी वृद्धि होनेसे उक्त प्रकृतियोंकी स्थितियोंमें वृद्धि होती है। यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि प्रकृतियोंके शुभ-अशुभ या पुण्य-पापरूप जो दो विभाग किये गये हैं, वे अनुभागबन्धकी अपेक्षा किये गये हैं। किन्तु यहाँ. पर स्थितिबन्धकी अपेक्षा स्थितियोंके शुभ-अशुभका निर्णय किया जा रहा है । देवायु आदि तीन प्रकृतियोंकी स्थितियोंके शुभ कहनेका कारण विशुद्धि है। अर्थात् परिणामोंमें संक्लेशको हानि और विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे इन तीनों प्रकृतियोंकी स्थितियों में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है, जिससे कि तीर्थकर, उच्चगोत्र, यशस्कीर्ति आदि जैसी शुभ प्रकृतियोंको अशुभ कहा गया है और वह कारण यह है कि आयुत्रिकको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियोंकी जैसे जैसे स्थितियाँ बढ़ती है, वैसे वैसे ही उनका अनुभाग घटता चला जाता है। किन्तु आयुत्रिकका क्रम इससे भिन्न है। उक्त तीनों आयुकर्मोंकी स्थितियाँ ज्यों-ज्यों बढ़ती है, त्यों-त्यों उनका अनुभाग भी उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है उक्त दोनों कारणांसे आयुत्रिककी स्थितियोंको शुभ और शेष सर्वप्रकृतियोंको स्थितियोंको अशुभ कहा गया है। अब मूलशतककार इसी अर्थको स्वयं स्पष्ट करते हैं[मूलगा०५६] 'सव्व हिदीणमुक्कस्सओ दु उकस्ससंकिलेसेण ।
विवरीओ दु जहण्णो आउगतिगं वज सेसाणं ॥४२॥
आउतियं णिरयाउं विणा। .... तिर्यग्मनुष्यदेवायुष्कत्रिकं वर्यिस्वा शेषाणां सप्तदशोत्तरसर्वप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धः उस्कृष्टसंक्लेशपरिणामेन भवति । तु पुनः तासां प्रकृतीनां ११७ जघन्यस्थितिबन्धः उस्कृष्ट विशुद्धपरिणामेन भवति । तत्रयस्य तु उत्कृष्टविशुद्धपरिणामेन जघन्यं तद्विपरीतेनोत्कृष्टमविशुद्धपरिणामेन च भवति ॥२५॥
आयुत्रिकको छोड़कर शेष सर्व प्रकृतियोंकी स्थितियोंका उत्कृष्ट बन्ध उत्कृष्ट संक्लेशसे होता है और उनका जघन्य स्थितिबन्ध विपरीत अर्थात् संक्लेशके कम होनेसे होता है ॥४२५।।
यहाँपर आयुत्रिकसे अभिप्राय नरकायुके विना शेष तीन आयुकर्मों से है। [मूलगा०५७] सव्वुक्कस्सठिदीणं मिच्छादिट्ठी दुबंधगो भणिओ।
आहारय-तित्थयरं देवाउगं च विमोत्तणं ॥४२६॥ [मूलगा०५८] 'देवाउगं पमत्तो+ आहारयमप्पमत्तविरदो दु ।
तित्थयरं च मणुस्सो अविरथसम्मो समज्जेइ ॥४२७।। उत्कृष्टस्थितिबन्धकमाह--[ 'सन्धुकस्स ठिीणं' इत्यादि । ] आहारकद्विकं २ तीर्थकरत्वं १ देवायुश्चेति १ चत्वारि मुक्त्वा शेष ११६ प्रकृतिसर्वोत्कृष्ट-स्थितीनां मिथ्यादृष्टिरेव बन्धको भणितः। तच्चतुर्णा आहारकद्वयतीर्थकरत्वदेवायुषां तु सर्वोत्कृष्टस्थितीनां सम्यग्दृष्टिरेव बन्धको भवति । तत्रापि विशेषमाह'देवाउगं पमत्तो । इति पाठे देवायुरुत्कृष्टस्थितिकं प्रमत्त एवाप्रमत्तगुगस्थानाभिमुखो बध्नाति । अप्रमत्ते तदव्युच्छित्तावपि तत्र सातिशये तीवविशुद्धत्वेन तद्देवायुबन्धान्निरतिशये चोत्कृष्टासम्भवात् । तु पुनः आहारकद्वयं उत्कृष्टस्थितिकं अप्रमत्तः प्रमत्तगुणस्थानाभिमुखः संक्लिष्ट एवं बध्नाति, आयुस्त्रयवर्जितानां
1 सं० पञ्चसं० ४, २३६-२४३ 1 2. ४, २४४| 3. ४, २४५। १. शतक० ५८ । २. शतक० ५६ । ३. शतक० ६०। . +ब, प्रतौ 'देवाउमप्पमत्तो' इति पाठः ।
....
.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org