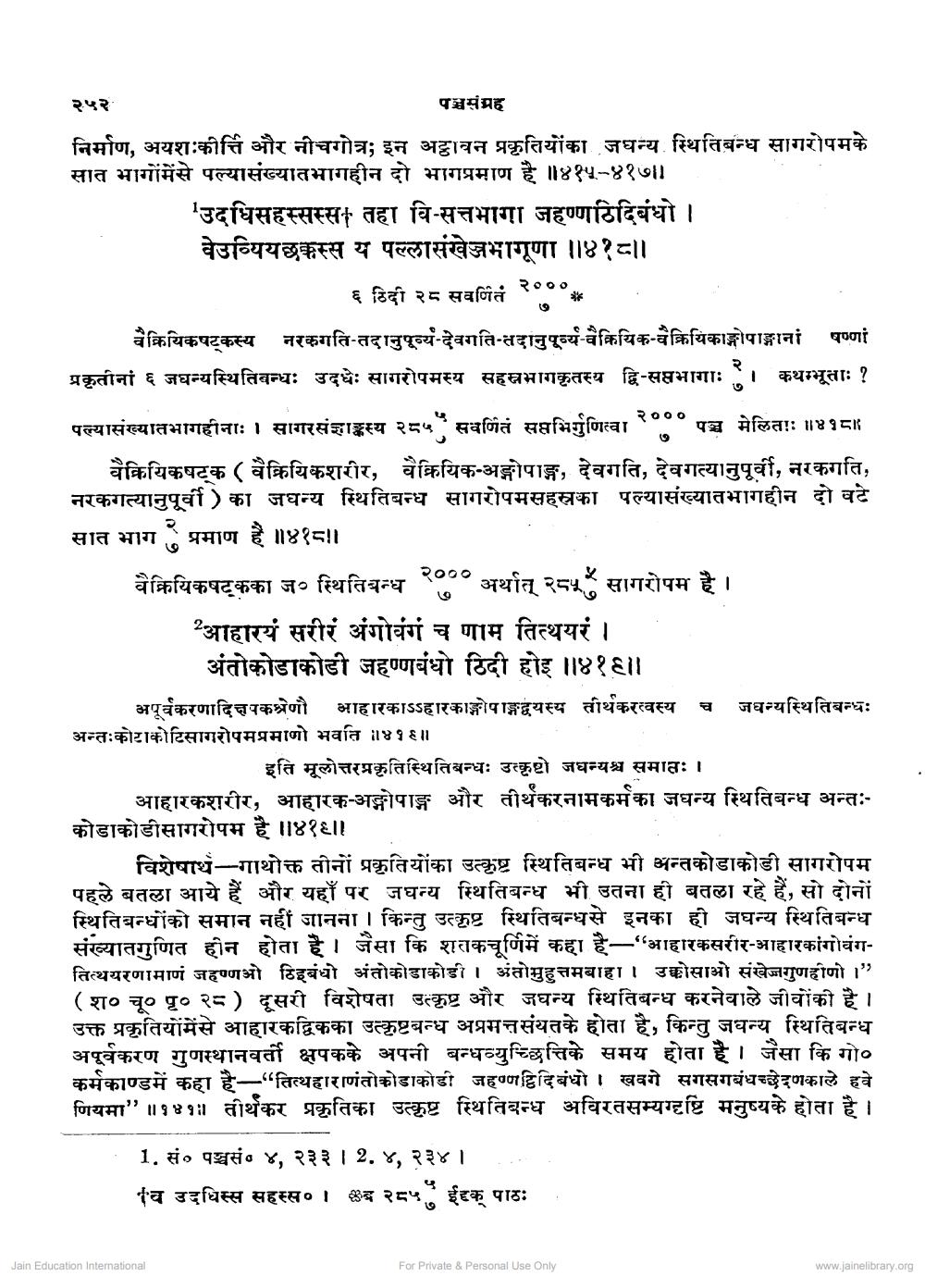________________
२५२
पञ्चसंग्रह
निर्माण, अयश कीर्ति और नीचगोत्र; इन अट्ठावन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्यासंख्यातभागहीन दो भागप्रमाण है ॥४१५-४१७।।
'उदधिसहस्सस्सा तहा वि-सत्तभागा जहण्णठिदिबंधो । वेउव्यियछकस्स य पल्लासंखेजमागूणा ॥४१८॥
___ ६ ठिदी २८ सवर्णित २०० वैक्रियिकपटकस्य नरकगति-तदानुपूर्व्य-देवगति-तदानुपूर्व-वैक्रियिक-वैक्रियिकाङ्गोपाङ्गानां षण्णां प्रकृतीनां ६ जघन्यस्थितिबन्धः उदधेः सागरोपमस्य सहस्रभागकृतस्य द्वि-सप्तभागाः । कथम्भूताः ? पल्यासंख्यातभागहीनाः । सागरसंज्ञाङ्कस्य २८५५ सवर्णित सप्तभिर्गुणित्वा २००° पञ्च मेलिताः ॥४१८॥
वैक्रियिकषट्क (वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक-अङ्गोपाङ्ग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी) का जघन्य स्थितिबन्ध सागरोपमसहस्रका पल्यासंख्यातभागहीन दो वटे सात भाग प्रमाण है ॥४१॥ वैक्रियिकपटकका ज० स्थितिबन्ध २००° अर्थात् २८५४ सागरोपम है ।
आहारयं सरीरं अंगोवंगं च णाम तित्थयरं।
अंतोकोडाकोडी जहण्णबंधो ठिदी होइ ॥४१६॥ अपूर्वकरणादिक्षपकश्रेणी आहारकाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गद्वयस्य तीर्थकरत्वस्य च जघन्यस्थितिबन्धः अन्तःकोटाकोटिसागरोपमप्रमाणो भवति ॥४१६॥
इति मूलोत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धः उत्कृष्टो जघन्यश्च समातः । आहारकशरीर, आहारक-अङ्गोपाङ्ग और तीर्थकरनामकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडीसागरोपम है ।।४१६॥
विशेषार्थ-गाथोक्त तीनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध भी अन्तकोडाकोडी सागरोपम पहले बतला आये हैं और यहाँ पर जघन्य स्थितिबन्ध भी उतना ही बतला रहे हैं, सो दोनों स्थितिबन्धोंको समान नहीं जानना । किन्तु उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे इनका ही जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणित हीन होता है। जैसा कि शतकचूर्णिमें कहा है-"आहारकसरीर-आहारकांगोवंगतित्थयरणामाणं जहण्णओ ठिइबंधो अंतोकोडाकोडी। अंतोमुत्तमबाहा। उक्कोसाओ संखेजगुणहीणो।" (श० चू० पृ०२८) दूसरी विशेषता उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्ध करनेवाले उक्त प्रकृतियोंमेंसे आहारकद्विकका उत्कृष्टबन्ध अप्रमत्तसंयतके होता है, किन्तु जघन्य स्थितिबन्ध अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती क्षपकके अपनी बन्धव्युच्छित्तिके समय होता है। जैसा कि गो० कर्मकाण्डमें कहा है-"तित्थहाराणंतोकोडाकोडी जहण्णहिदिबंधो। खवगे सगसगबंधच्छेदणकाले हवे णियमा" ॥१४१॥ तीर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है।
ध करनेवाले जीवोंकी है।
1. सं० पञ्चसं० ४, २३३ । 2. ४, २३४ । नव उदधिस्स सहस्स० । सन २८५३ ईदृक् पाठः ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org