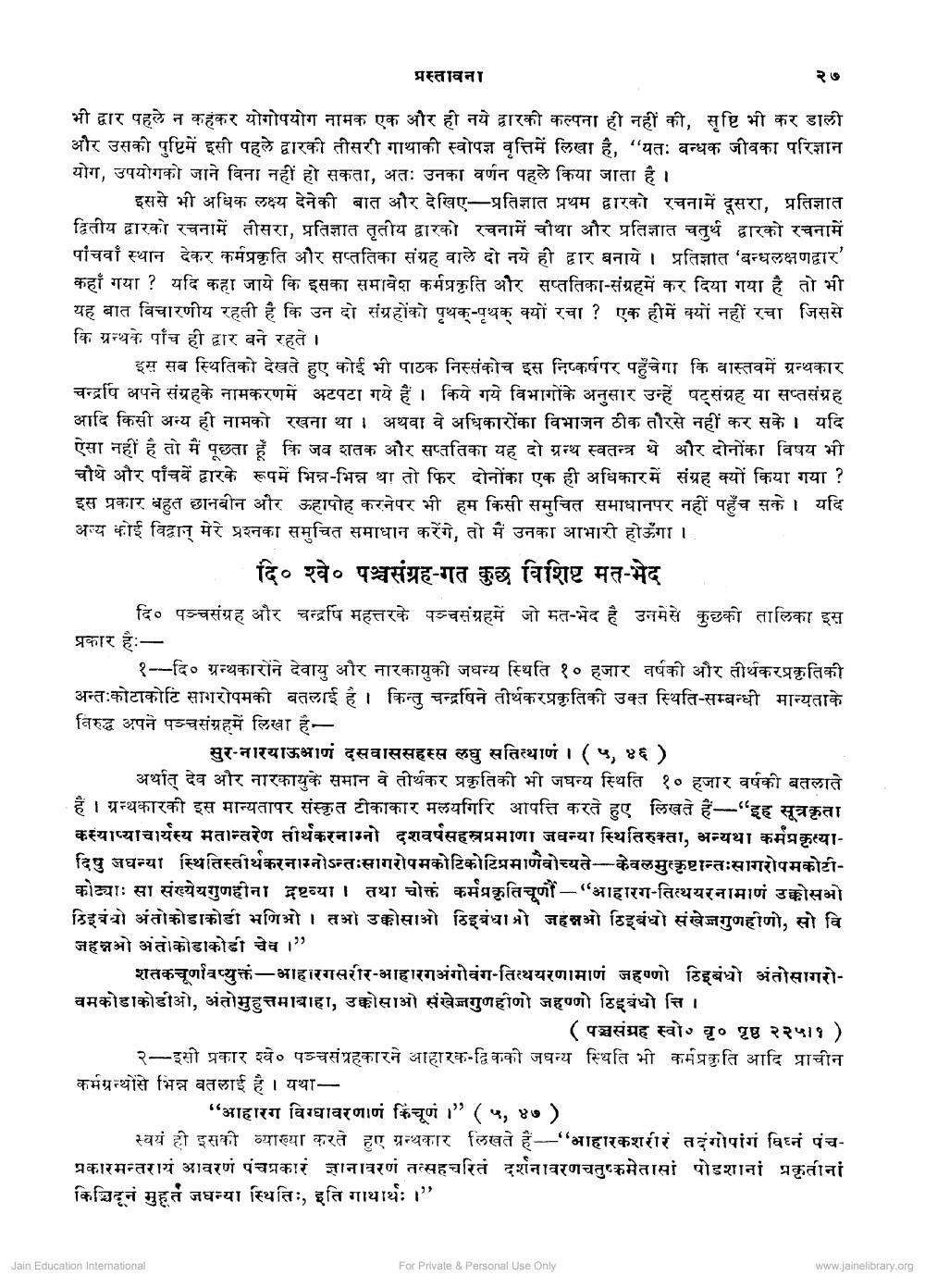________________
प्रस्तावना
भी द्वार पहले न कहकर योगोपयोग नामक एक और ही नये द्वारकी कल्पना ही नहीं की, सृष्टि भी कर डाली और उसकी पुष्टिमें इसी पहले द्वारकी तीसरी गाथाकी स्वोपज्ञ वृत्तिमें लिखा है, “यतः बन्धक जीवका परिज्ञान योग, उपयोगको जाने विना नहीं हो सकता, अतः उनका वर्णन पहले किया जाता है।
इससे भी अधिक लक्ष्य देने की बात और देखिए-प्रतिज्ञात प्रथम द्वारको रचनामें दूसरा, प्रतिज्ञात द्वितीय द्वारको रचनामें तीसरा, प्रतिज्ञात तृतीय द्वारको रचनामें चौथा और प्रतिज्ञात चतुर्थ द्वारको रचनामें पांचवां स्थान देकर कर्मप्रकृति और सप्ततिका संग्रह वाले दो नये ही द्वार बनाये। प्रतिज्ञात 'बन्धलक्षणद्वार' कहाँ गया ? यदि कहा जाये कि इसका समावेश कर्मप्रकृति और सप्ततिका-संग्रहमें कर दिया गया है तो भी यह बात विचारणीय रहती है कि उन दो संग्रहोंको पृथक्-पृथक क्यों रचा ? एक हीमें क्यों नहीं रचा जिससे कि ग्रन्थके पाँच ही द्वार बने रहते ।।
इस सब स्थितिको देखते हुए कोई भी पाठक निस्संकोच इस निष्कर्षपर पहुँचेगा कि वास्तवमें ग्रन्थकार चन्द्रपि अपने संग्रहके नामकरणमें अटपटा गये हैं। किये गये विभागोंके अनुसार उन्हें पट्संग्रह या सप्तसंग्रह आदि किसी अन्य ही नामको रखना था। अथवा वे अधिकारोंका विभाजन ठीक तौरसे नहीं कर सके। यदि ऐसा नहीं है तो मैं पूछता हूँ कि जब शतक और सप्ततिका यह दो ग्रन्थ स्वतन्त्र थे और दोनोंका विषय भी चौथे और पांचवें द्वारके रूप में भिन्न-भिन्न था तो फिर दोनोंका एक ही अधिकार में संग्रह क्यों किया गया ? इस प्रकार बहुत छानबीन और ऊहापोह करने पर भी हम किसी समुचित समाधानपर नहीं पहुँच सके। यदि अन्य कोई विद्वान् मेरे प्रश्नका समुचित समाधान करेंगे, तो मैं उनका आभारी होऊँगा ।
दि० श्वे० पञ्चसंग्रह-गत कुछ विशिष्ट मत-भेद दि० पञ्चसंग्रह और चन्द्रषि महत्तरके पञ्चसंग्रहमें जो मत-भेद है उनमेसे कुछको तालिका इस प्रकार है:
१-दि० ग्रन्थकारोंने देवायु और नारकायुकी जघन्य स्थिति १० हजार वर्षको और तीर्थकरप्रकृतिकी अन्तःकोटाकोटि सागरोपमकी बतलाई है। किन्तु चन्द्रषिने तीर्थकरप्रकृतिको उक्त स्थिति-सम्बन्धी मान्यताके विरुद्ध अपने पञ्चसंग्रहमें लिखा है
सुर-नारयाऊआणं दसवाससहस्स लघु सतित्थाणं । (५,४६) अर्थात् देव और नारकायुके समान वे तीर्थकर प्रकृतिको भी जघन्य स्थिति १० हजार वर्षकी बतलाते है । ग्रन्थकारकी इस मान्यतापर संस्कृत टीकाकार मलयगिरि आपत्ति करते हुए लिखते हैं-"इह सूत्रकृता कस्याप्याचार्यस्य मतान्तरेण तीर्थकरनाम्नो दशवर्षसहस्रप्रमाणा जघन्या स्थितिरुक्ता, अन्यथा कर्मप्रकृत्यादिपु जघन्या स्थितिस्तीर्थकरनाम्नोऽन्तःसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणवोच्यते-केवलमुत्कृष्टान्तःसागरोपमकोटीकोट्याः सा संख्येयगुणहीना द्रष्टव्या । तथा चोक्तं कर्मप्रकृतिचूणौँ- “आहारग-तित्थयरनामाणं उक्कोसो ठिइबंधो अंतोकोडाकोडी भणिो। तओ उक्कोसाओ ठिइबंधामो जहन्नओ ठिइबंधो संखेजगुणहीणो, सो वि जहन्नओ अंतोकोडाकोडी चेव ।"
शतकचूर्णावप्युक्तं-आहारगसरीर-आहारगअंगोवंग-तित्थयरणामाणं जहण्णो ठिइबंधो अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, अंतोमुत्तमाबाहा, उक्कोसाओ संखेजगुणहीणो जहण्णो ठिइबंधो त्ति ।।
(पञ्चसंग्रह स्वो वृ० पृष्ठ २२५४१) २-इसी प्रकार श्वे० पञ्चसंग्रहकारने आहारक-द्विकको जघन्य स्थिति भी कर्मप्रकृति आदि प्राचीन कर्मग्रन्थोंसे भिन्न बतलाई है। यथा
"आहारग विग्यावरणाणं किंचूणं।” (५, ४७) स्वयं ही इसकी व्याख्या करते हए ग्रन्थकार लिखते है-"भाहारकशरीरं तदंगोपांगं विघ्नं पंचप्रकारमन्तरायं आवरणं पंचप्रकारं ज्ञानावरणं तत्सहचरितं दर्शनावरणचतुष्कमेतासां पोडशानां प्रकृतीनां किञ्चिदनं मुहत जघन्या स्थितिः, इति गाथार्थः।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org