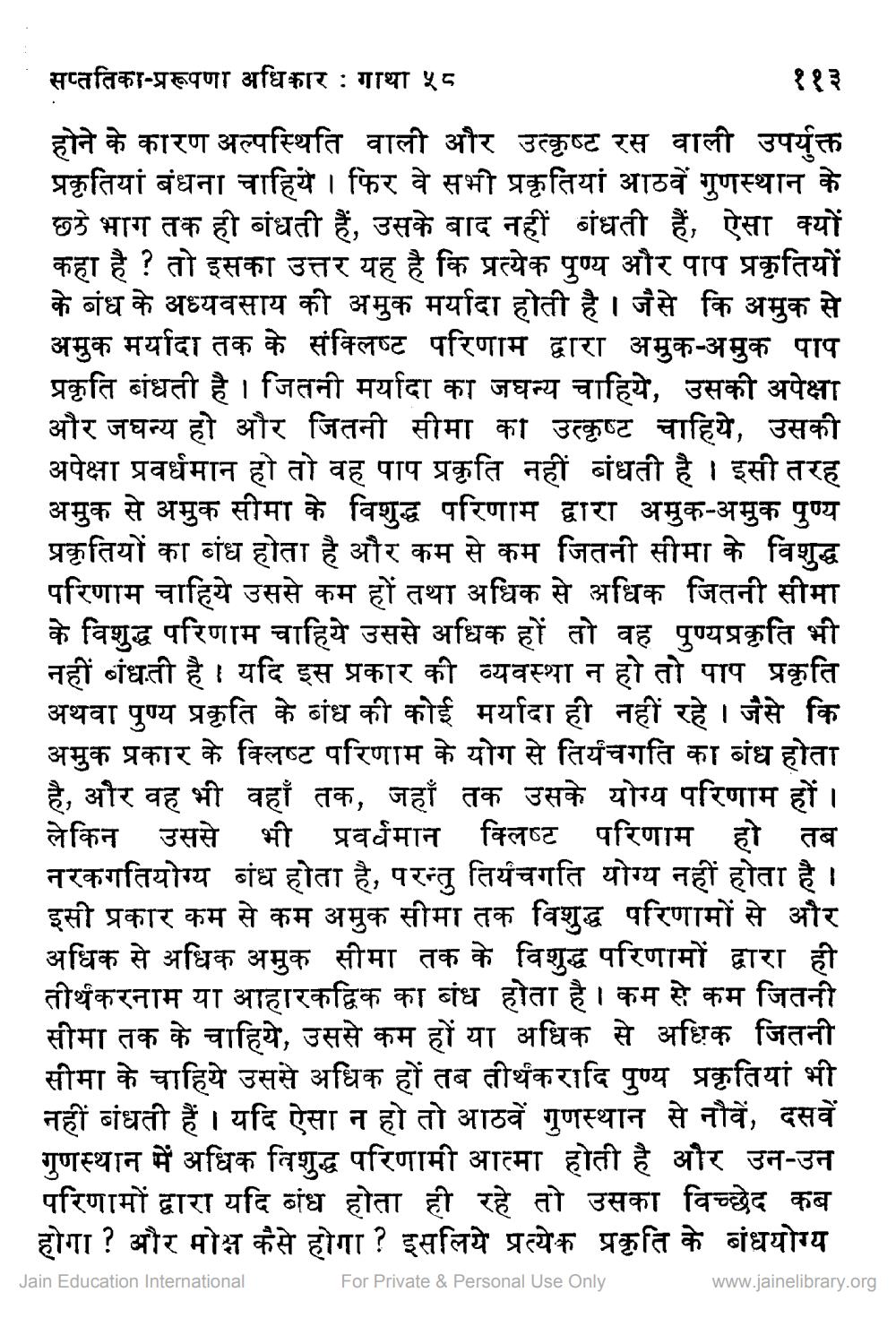________________
सप्ततिका-प्ररूपणा अधिकार : गाथा ५८
११३
सके बाद नहीं पूण्य और पाप प्रमुक से
बंध के अध्यवसायलष्ट परिणाम द्वारा
उसकी अपेक्षा
* का बंधामा के विशुद्ध प्रकृति नहीं हष्ट चाहिये, अपेक्षा
होने के कारण अल्पस्थिति वाली और उत्कृष्ट रस वाली उपर्युक्त प्रकृतियां बंधना चाहिये । फिर वे सभी प्रकृतियां आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक ही बंधती हैं, उसके बाद नहीं बंधती हैं, ऐसा क्यों कहा है ? तो इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक पुण्य और पाप प्रकृतियों के बंध के अध्यवसाय की अमुक मर्यादा होती है। जैसे कि अमुक से अमुक मर्यादा तक के संक्लिष्ट परिणाम द्वारा अमुक-अमुक पाप प्रकृति बंधती है। जितनी मर्यादा का जघन्य चाहिये, उसकी अपेक्षा और जघन्य हो और जितनी सीमा का उत्कृष्ट चाहिये, उसकी अपेक्षा प्रवर्धमान हो तो वह पाप प्रकृति नहीं बंधती है । इसी तरह अमुक से अमुक सीमा के विशुद्ध परिणाम द्वारा अमुक-अमुक पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है और कम से कम जितनी सीमा के विशुद्ध परिणाम चाहिये उससे कम हों तथा अधिक से अधिक जितनी सीमा के विशुद्ध परिणाम चाहिये उससे अधिक हों तो वह पुण्यप्रकृति भी नहीं बांधती है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था न हो तो पाप प्रकृति अथवा पुण्य प्रकृति के बंध की कोई मर्यादा ही नहीं रहे । जैसे कि अमुक प्रकार के क्लिष्ट परिणाम के योग से तिर्यंचगति का बंध होता है, और वह भी वहाँ तक, जहाँ तक उसके योग्य परिणाम हों। लेकिन उससे भी प्रवर्वमान क्लिष्ट परिणाम हो तब नरकगतियोग्य बंध होता है, परन्तु तिर्यंचगति योग्य नहीं होता है। इसी प्रकार कम से कम अमुक सीमा तक विशुद्ध परिणामों से और अधिक से अधिक अमुक सीमा तक के विशुद्ध परिणामों द्वारा ही तीर्थकरनाम या आहारकद्विक का बंध होता है। कम से कम जितनी सीमा तक के चाहिये, उससे कम हों या अधिक से अधिक जितनी सीमा के चाहिये उससे अधिक हों तब तीर्थंकरादि पुण्य प्रकृतियां भी नहीं बंधती हैं । यदि ऐसा न हो तो आठवें गुणस्थान से नौवें, दसवें गुणस्थान में अधिक विशुद्ध परिणामी आत्मा होती है और उन-उन परिणामों द्वारा यदि बांध होता ही रहे तो उसका विच्छेद कब होगा? और मोक्ष कैसे होगा? इसलिये प्रत्येक प्रकृति के बंधयोग्य Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org