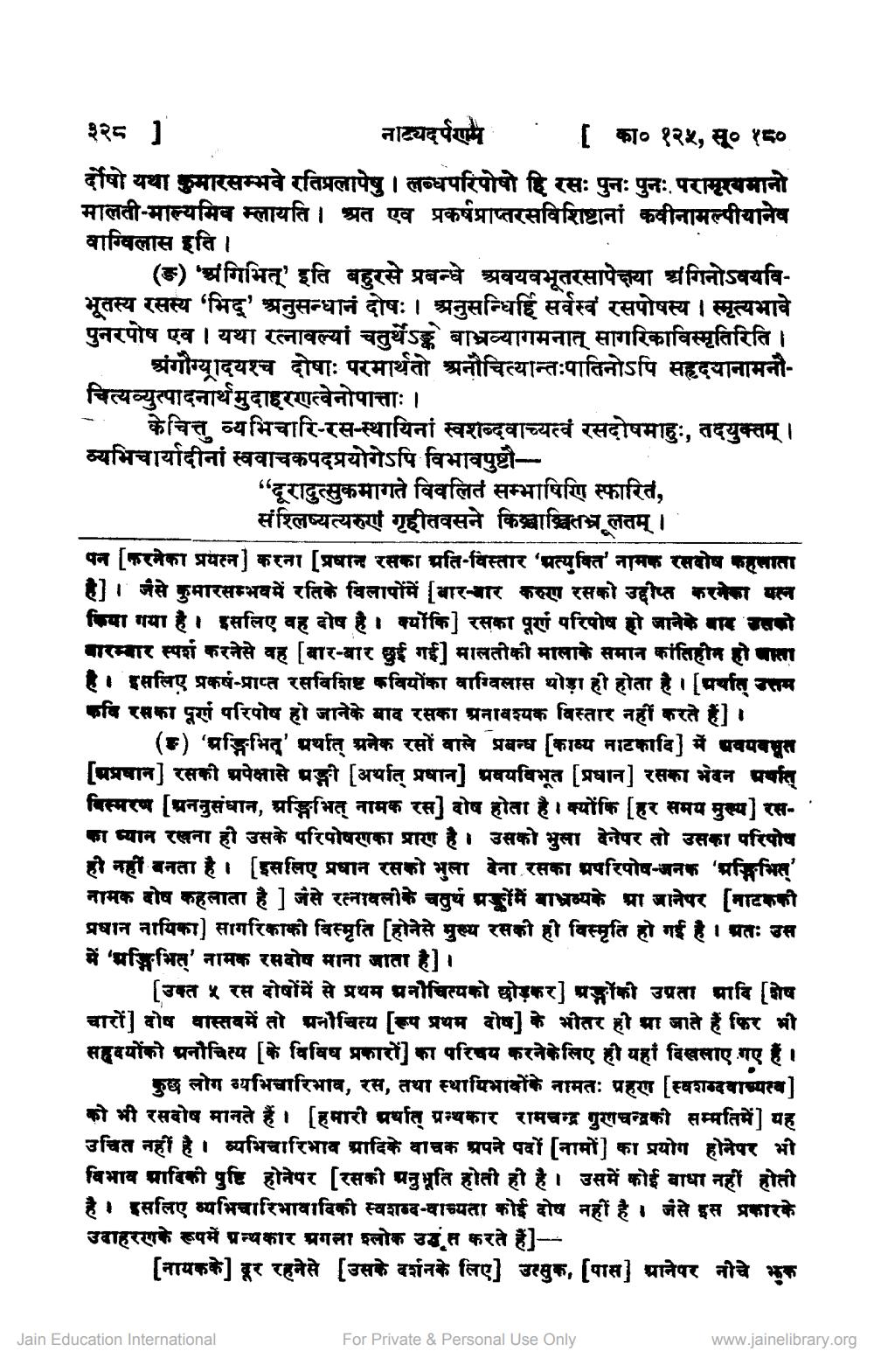________________
३२८ ]
नाट्यदर्पणम [ का० १२५, सू० १८० र्दोषो यथा कुमारसम्भवे रतिप्रलापेषु । लब्धपरिपोषो हि रसः पुनः पुनः परामश्वमानो मालती-माल्यमिव म्लायति । अत एव प्रकर्षप्राप्तरसविशिष्टानां कवीनामल्पीयानेव वाग्विलास इति ।
(ङ) 'अंगिभित्' इति बहुरसे प्रबन्धे अवयवभूतरसापेक्षया अंगिनोऽवयविभूतस्य रसस्य 'भिद्' अनुसन्धानं दोषः । अनुसन्धिर्हि सर्वस्वं रसपोषस्य । स्मृत्यभावे पुनरपोष एव । यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क बाभ्रव्यागमनात् सागरिकाविस्मृतिरिति ।
अंगौग्यादयश्च दोषाः परमार्थतो अनौचित्यान्तःपातिनोऽपि सहृदयानामनौचित्यव्युत्पादनार्थमुदाहरणत्वेनोपात्ताः।
केचित्तु व्यभिचारि-रस-स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं रसदोषमाहुः, तदयुक्तम् । व्यभिचार्यादीनां स्ववाचकपदप्रयोगेऽपि विभावपुष्टौ
"दूरादुत्सुकमागते विवलित सम्भाषिणि स्फारित,
संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किश्वाचित लतम् । पन [करनेका प्रयत्न करना [प्रधान रसका प्रति-विस्तार 'प्रत्युक्ति' नामक रसदोष कहलाता है] । जैसे कुमारसम्भवमें रतिके विलापोंमें बार-बार करुण रसको उद्दीप्त करमेका यत्न किया गया है। इसलिए वह दोष है। क्योंकि] रसका पूर्ण परिपोष हो जानेके बाद उसको बारम्बार स्पर्श करनेसे वह [बार-बार छुई गई] मालतीको मालाके समान कांतिहीन हो पाता है। इसलिए प्रकर्ष-प्राप्त रसविशिष्ट कवियोंका वाग्विलास थोड़ा ही होता है। [अर्थात उत्तम कवि रसका पूर्ण परिपोष हो जानेके बाव रसका अनावश्यक विस्तार नहीं करते हैं ।
(8) 'मङ्गिभित्' अर्थात् अनेक रसों वाले प्रबन्ध [काव्य नाटकादि] में अवयवभूत [पप्रधान] रसकी अपेक्षासे प्रङ्गी [अर्थात् प्रधान] प्रवयविभूत [प्रधान] रसका भेदन अर्थात् विस्मरण [अननुसंधान, अङ्गिभित् नामक रस] दोष होता है। क्योंकि [हर समय मुख्य रसका ध्यान रखना ही उसके परिपोषणका प्राण है। उसको भुला देनेपर तो उसका परिपोष हो नहीं बनता है। [इसलिए प्रधान रसको भुला देना रसका अपरिपोष-जनक 'प्रङ्गिभित्' नामक दोष कहलाता है ] जैसे रत्नावलीके चतुर्थ प्रथों में बाभ्रव्यके प्रा जानेपर [नाटककी प्रधान नायिका सागरिकाको विस्मृति [होनेसे मुख्य रसकी ही विस्मृति हो गई है । अतः उस में 'मणिभित्' नामक रसदोष माना जाता है ।
[उक्त ५ रस दोषों में से प्रथम प्रनौचित्यको छोड़कर] प्रङ्गोंकी उप्रता प्रादि [शेष चारों दोष वास्तवमें तो अनौचित्य [रूप प्रथम दोष] के भीतर ही मा जाते हैं फिर भी सहदयोंको अनौचित्य [के विविध प्रकारों का परिचय करनेके लिए ही यहां दिखलाए गए हैं।
कुछ लोग व्यभिचारिभाव, रस, तथा स्थायिभावोंके नामतः प्रहण [स्वशम्दवाध्यत्व] को भी रसदोष मानते हैं। [हमारी अर्थात् ग्रन्थकार रामचन्द्र गुणचन्द्रको सम्मतिमें] यह उचित नहीं है। व्यभिचारिभाव प्रादिके वाचक अपने पदों [नामों का प्रयोग होनेपर भी विभाव माविकी पुष्टि होनेपर [रसकी अनुभूति होती ही है। उसमें कोई बाधा नहीं होती है। इसलिए व्यभिचारिभावादिको स्वशब्द-वाच्यता कोई दोष नहीं है। जैसे इस प्रकारके उदाहरणके रूपमें प्रन्थकार अगला श्लोक उबंत करते हैं]--
[नायकके] दूर रहनेसे [उसके दर्शनके लिए] उत्सुक, [पास] मानेपर नीचे झुक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org