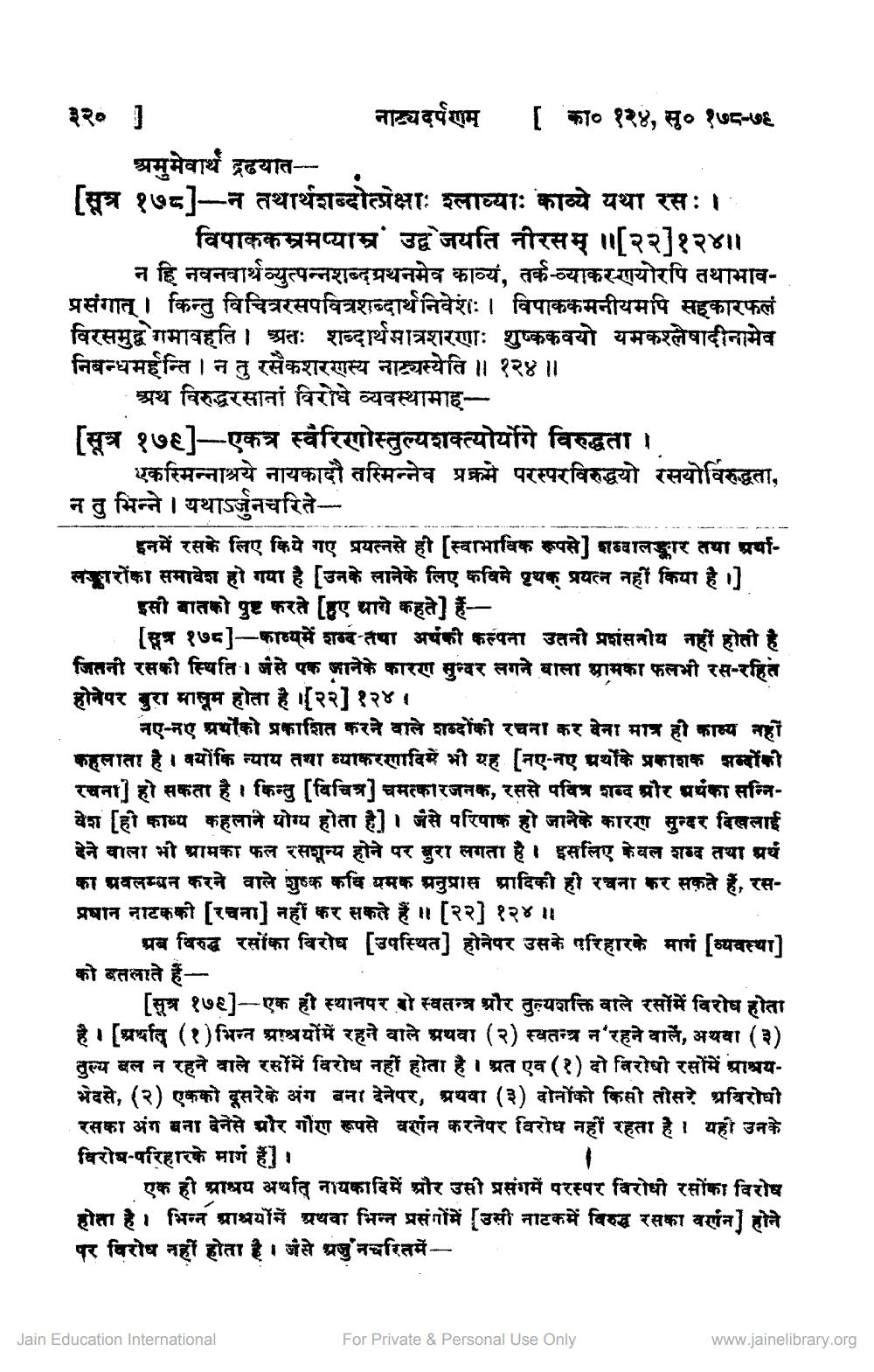________________
३२०
नाट्यदर्पणम [ का० १२४, सु० १७८-७६ अमुमेवार्थ द्रढयात[सूत्र १७८]-न तथार्थशब्दोत्प्रेक्षाः श्लाघ्याः काव्ये यथा रसः ।
विपाककम्रमप्यानं उद्वजयति नीरसम् ॥[२२] १२४॥ न हि नवनवार्थव्युत्पन्नशब्दग्रथनमेव काव्यं, तर्क-व्याकरणयोरपि तथाभावप्रसंगात् । किन्तु विचित्ररसपवित्रशब्दार्थनिवेशः । विपाककमनीयमपि सहकारफलं विरसमुद्व गमावहति । अतः शब्दार्थमात्रशरणाः शुष्ककवयो यमकश्लेषादीनामेव निबन्धमर्हन्ति । न तु रसैकशरणस्य नाट्यस्येति ॥ १२४ ॥
अथ विरुद्धरसानां विरोधे व्यवस्थामाह[सूत्र १७६]-एकत्र स्वैरिणोस्तुल्यशक्त्योर्योगे विरुद्धता।
एकस्मिन्नाश्रये नायकादौ तस्मिन्नेव प्रक्रमे परस्परविरुद्धयो रसयोविरुद्धता, न तु भिन्ने । यथाऽर्जुनचरिते--
इनमें रसके लिए किये गए प्रयत्नसे ही [स्वाभाविक रूपसे] शब्दालङ्कार तथा प्रर्यालकारोंका समावेश हो गया है [उनके लानेके लिए कविने पृथक् प्रयत्न नहीं किया है।]
इसी बातको पुष्ट करते [हए धागे कहते हैं
[सूत्र १७८]-काव्यमें शब्द तथा अर्थको कल्पना उतनी प्रशंसनीय नहीं होती है जितनी रसको स्थिति । जैसे पक जानेके कारण सुन्दर लगने वाला प्रामका फलभी रस-रहित होनेपर बुरा मालूम होता है ।[२२] १२४ ॥
नए-नए प्रयोको प्रकाशित करने वाले शब्दोंकी रचना कर देना मात्र ही काव्य नहीं कहलाता है। क्योंकि न्याय तथा व्याकरणाविमें भी यह [नए-नए प्रोंके प्रकाशक भन्दोंकी रचना हो सकता है। किन्तु [विचित्र चमत्कारजनक, रससे पवित्र शब्द और अर्थका सन्निवेशही काव्य कहलाने योग्य होता है। जैसे परिपाक हो जानेके कारण सुन्दर दिखलाई देने वाला भी प्रामका फल रसशून्य होने पर सुरा लगता है। इसलिए केवल शम्द तथा अर्थ का अवलम्बन करने वाले शुष्क कवि यमक अनुप्रास प्रादिकी ही रचना कर सकते हैं, रसप्रषान नाटकको [रचना नहीं कर सकते हैं । [२२] १२४॥
अब विरुद्ध रसोंका विरोध [उपस्थित होनेपर उसके परिहारके मार्ग [व्यवस्था को बतलाते हैं
[सूत्र १७९]-एक ही स्थानपर को स्वतन्त्र और तुल्यशक्ति वाले रसोंमें विरोध होता है। [अर्थात् (१)भिन्न प्राश्रयों में रहने वाले अथवा (२) स्वतन्त्र न रहने वालें, अथवा (३) तुल्य बल न रहने वाले रसों में विरोध नहीं होता है । अत एव (१) दो विरोधी रसोंमें पाश्रयभेदसे, (२) एकको दूसरेके अंग बना देनेपर, अथवा (३) वोनोंको किसी तीसरे अविरोधी रसका अंग बना देनेसे और गौण रूपसे वर्णन करनेपर विरोध नहीं रहता है। यही उनके विरोध-परिहारके मार्ग हैं।
एक ही पाश्रय अर्थात् नायकादिमें और उसी प्रसंगमें परस्पर विरोधी रसोंका विरोध होता है। भिन्न प्राश्रयोंने अथवा भिन्न प्रसंगोंमें [उसी नाटकमें विरुख रसका वर्णन होने पर विरोध नहीं होता है । जैसे अर्जुनचरितमें
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org