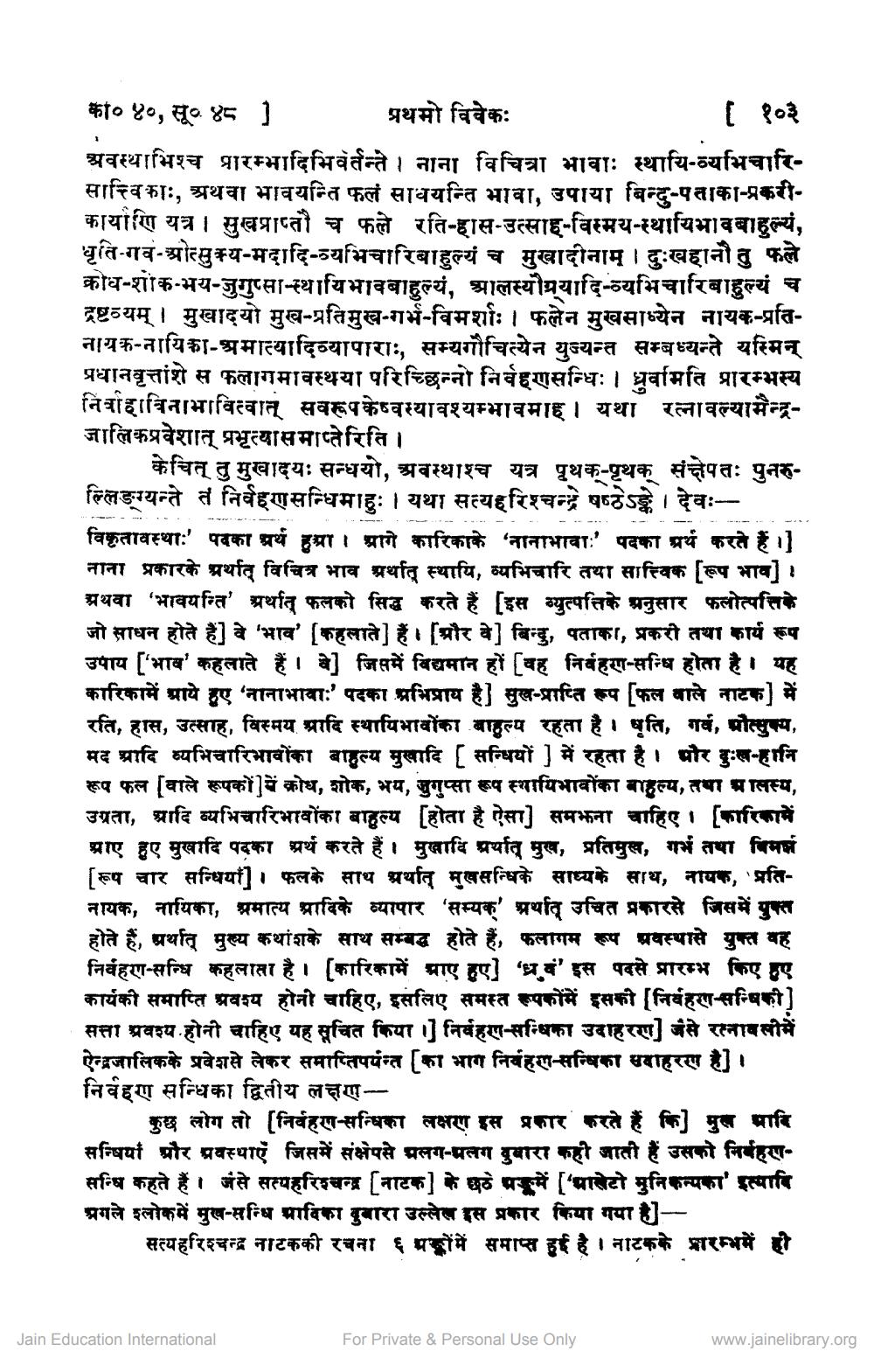________________
का०४०, सू०४८ ] प्रथमो विवेकः अवस्थाभिश्च प्रारम्भादिभिवर्तन्ते । नाना विचित्रा भावाः स्थायि-व्यभिचारिसात्त्विकाः, अथवा भावयन्ति फलं साधयन्ति भावा, उपाया बिन्दु-पताका-प्रकरीकार्याणि यत्र । सुखप्राप्तौ च फले रति-हास-उत्साह-विस्मय-स्थायिभावबाहुल्यं, धृति-गव-प्रोत्सुक्य-मदादि-व्यभिचारिबाहुल्यं च मुखादीनाम् । दुःखहानौ तु फले क्रोध-शोक-भय-जुगुप्सा-स्थायिभावबाहुल्यं, आलस्योग्र्यादि-व्यभिचारिबाहुल्यं च द्रष्टव्यम् । मुखादयो मुख-प्रतिमुख-गर्भ-विमर्शाः। फलेन मुखसाध्येन नायक-प्रतिनायक-नायिका-अमात्यादिव्यापाराः, सम्यगौचित्येन युज्यन्त सम्बध्यन्ते यस्मिन् प्रधानवृत्तांशे स फलागमावस्थया परिच्छिन्नो निर्वहणसन्धिः । ध्रुवमिति प्रारम्भस्य निर्वाहाविनाभावित्वात् सवरूपकेष्वस्यावश्यम्भावमाह । यथा रत्नावल्यामैन्द्रजालिकप्रवेशात् प्रभृत्यासमाप्तेरिति ।
केचित् तु मुखादयः सन्धयो, अवस्थाश्च यत्र पृथक-पृथक् संक्षेपतः पुनरुल्लिङ्ग्यन्ते त निर्वहणसन्धिमाहुः । यथा सत्यहरिश्चन्द्रे षष्ठेऽङ्के । देवःविकृतावस्थाः' पदका अर्थ हुआ। प्रागे कारिकाके 'नानाभावाः' पदका प्रर्य करते हैं।] नाना प्रकारके अर्थात् विचित्र भाव अर्थात् स्थायि, व्यभिचारि तथा सात्त्विक [रूप भाव । अथवा 'भावयन्ति' अर्थात् फलको सिद्ध करते हैं [इस व्युत्पत्तिके अनुसार फलोत्पत्तिके जो साधन होते हैं] वे 'भाव' कहलाते हैं। और वे] बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य रूप उपाय ['भाव' कहलाते हैं। वे] जिसमें विद्यमान हों [वह निर्वहरण-सन्धि होता है। यह कारिकामें पाये हुए 'नानाभावाः' पदका अभिप्राय है] सुख प्राप्ति रूप [फल वाले नाटक में रति, हास, उत्साह, विस्मय प्रादि स्थायिभावोंका बाहुल्य रहता है। धृति, गर्व, प्रोत्सुक्य, मद प्रादि व्यभिचारिभावोंका बाहुल्य मुखादि [ सन्धियों ] में रहता है। पौर दुःख-हानि रूप फल [वाले रूपकों] में क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा रूप स्थायिभावोंका बाहुल्य, तथा प्रालस्य, उग्रता, प्रादि व्यभिचारिभावोंका बाहुल्य [होता है ऐसा] समझना चाहिए। [कारिकामें प्राए हुए मुखादि पदका अर्थ करते हैं। मुखादि अर्थात् मुख, प्रतिमुख, गर्भ तथा विमर्श [रूप चार सन्धियाँ] । फलके साथ अर्थात् मुखसन्धिके साध्यके साथ, नायक, 'प्रतिनायक, नायिका, अमात्य प्रादिके व्यापार 'सम्यक्' अर्थात् उचित प्रकारसे जिसमें पुक्त होते हैं, अर्थात् मुख्य कथांशके साथ सम्बद्ध होते हैं, फलागम रूप अवस्थासे युक्त वह निर्वहरण-सन्धि कहलाता है। [कारिकामें पाए हुए] 'ध्र वं" इस पदसे प्रारम्भ किए हए कार्यको समाप्ति अवश्य होनी चाहिए, इसलिए समस्त रूपकोंमें इसकी [निर्वहण-सन्धिकी] सत्ता अवश्य होनी चाहिए यह सूचित किया। निर्वहरण-सन्धिका उदाहरण] जैसे रत्नावलीमें ऐन्द्रजालिकके प्रवेशसे लेकर समाप्तिपर्यन्त [का भाग निर्वहरण-सन्धिका सदाहरण है। निर्वहण सन्धिका द्वितीय लक्षण
कुछ लोग तो [निर्वहरण-सन्धिका लक्षण इस प्रकार करते हैं कि मुख पारि सन्धियां और अवस्थाएँ जिसमें संक्षेपसे अलग-अलग दुबारा कही जाती हैं उसको निर्वहरणसन्धि कहते हैं। जैसे सत्यहरिश्चन्द्र [नाटक के छठे महमें ['माटो मुनिकन्यका' इत्यादि अगले इलोकमें मुख-सन्धि माविका दुबारा उल्लेख इस प्रकार किया गया है]
सत्यहरिश्चन्द्र नाटककी रचना ६ पड़ों में समाप्त हुई है । नाटकके प्रारम्भमें ही
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org