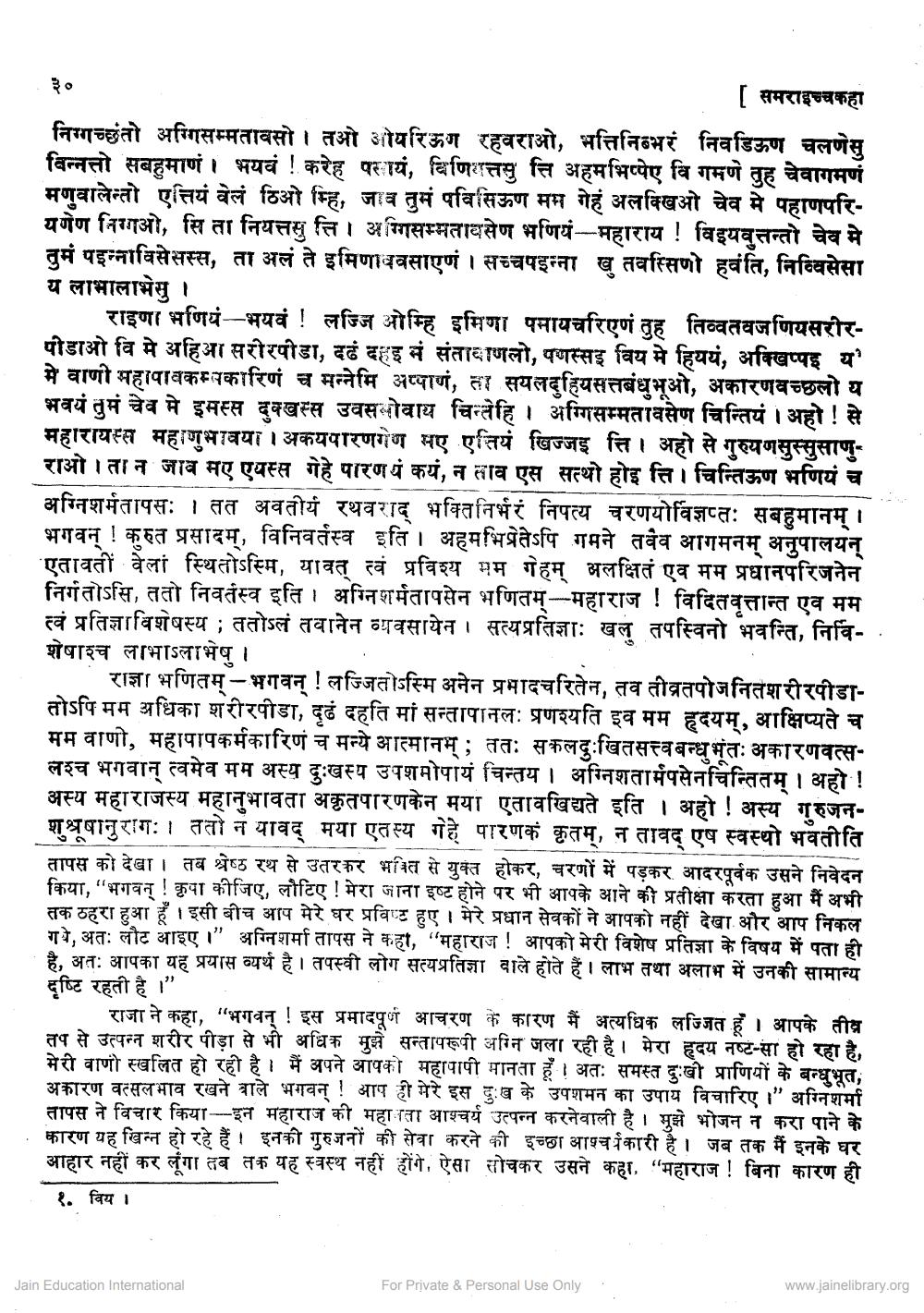________________
[ समराइच्चकहा
निग्गच्छंतो अग्गिसम्मतावसो । तओ ओयरिऊग रहवराओ, भत्तिनिब्भरं निवडिऊण चलणेसु विन्नत्तो सबहुमाणं । भयवं ! करेह पसायं, विणिवत्तसु ति अहमभिप्पेए वि गमणे तुह चेवागमणं मवान्तो एत्तियं वेलं ठिओ म्हि, जाव तुमं पविसिऊण मम गेहं अलक्खिओ चेव मे पहाणपरियण नगओ, सिता नियत्तसु ति । अग्गिसम्मतावसेण भणियं - महाराय ! विइयवुत्तन्तो चेव मे तुमं पइन्नाविसेसस्स, ता अलं ते इमिणाववसाएणं । सच्चपइन्ना खु तवस्तिणो हवंति, निव्विसेसा य लाभालाभे
३०
।
राणा भणियं - भयवं ! लज्जि ओम्हि इमिणा पमायचरिएणं तुह तिव्वतवजणियसरीरपीडाओ वि मे अहिआ सरीरपीडा, दढं दहइ नं संतावाणलो, वणस्सइ विय मे हिययं, अक्खिप्पर य मेवाणी महापातकम्पकारिणं च मन्नेमि अध्यानं, ता सयलदुहियसत्तबंधुभूओ, अकारणवच्छलो य भवयं तुमं चैव मे इमस्स दुक्खस्स उवसलोवाय चिन्तेहि । अग्गिसम्मतावसेण चिन्तियं । अहो ! से महारायस्त महाणुभावया । अकयवारणगेण मए एतियं खिज्जइ त्ति । अहो से गुरुयण सुस्सुसाणुराओ । तान जाब मए एक्स्स गेहे पारणयं कयं, न ताव एस सत्थो होइ ति । चिन्तिऊण भणियं च अग्निशर्मतापसः । तत अवतीर्य रथवराद् भक्तिनिर्भरं निपत्य चरणयोविज्ञप्तः सबहुमानम् । भगवन् ! कुरुत प्रसादम्, विनिवर्तस्व इति । अहमभिप्रेतेऽपि गमने तवैव आगमनम् अनुपालयन् एतावतीं वेलां स्थितोऽस्मि, यावत् त्वं प्रविश्य मम गेहम् अलक्षितं एव मम प्रधानपरिजनेन निर्गतोऽसि ततो निवर्तस्व इति । अग्निर्मतापसेन भणितम् - महाराज ! विदितवृत्तान्त एव मम त्वं प्रतिज्ञाविशेषस्य ; ततोऽलं तवानेन व्यवसायेन । सत्यप्रतिज्ञाः खलु तपस्विनो भवन्ति, निर्वि शेषाश्च लाभालाभेषु ।
2
राज्ञा भणितम् - भगवन् ! लज्जितोऽस्मि अनेन प्रमादचरितेन तव तीव्रतपोजनितशरीरपीडातोऽपि मम अधिका शरीरपीडा, दृढं दहति मां सन्तापानलः प्रणश्यति इव मम हृदयम्, आक्षिप्यते च मम वाणी, महापापकर्मकारिणं च मन्ये आत्मानम् ; ततः सकलदुःखितसत्त्व बन्धु भूतः अकारणवत्सलश्च भगवान् त्वमेव मम अस्य दुःखस्य उपशमोपायं चिन्तय । अग्निशतापसेनचिन्तितम् । अहो ! अस्य महाराजस्य महानुभावता अकृतपारणकेन मया एतावखिद्यते इति । अहो ! अस्य गुरुजनशुश्रूषानुरागः । ततो न यावद् मया एतस्य गेहे पारणकं कृतम्, न तावद् एष स्वस्थो भवतीति तापस को देखा । तब श्रेष्ठ रथ से उतरकर भक्ति से युक्त होकर, चरणों में पड़कर आदरपूर्वक उसने निवेदन किया, "भगवन् ! कृपा कीजिए, लौटिए ! मेरा जाना इष्ट होने पर भी आपके आने की प्रतीक्षा करता हुआ मैं अभी तक ठहरा हुआ हूँ । इसी बीच आप मेरे घर प्रविष्ट हुए। मेरे प्रधान सेवकों ने आपको नहीं देखा और आप निकल गये, अतः लौट आइए ।" अग्निशर्मा तापस ने कहा, "महाराज ! आपको मेरी विशेष प्रतिज्ञा के विषय में पता ही है, अतः आपका यह प्रयास व्यर्थ है । तपस्वी लोग सत्यप्रतिज्ञा वाले होते हैं। लाभ तथा अलाभ में उनकी सामान्य दृष्टि रहती है ।"
राजा ने कहा, "भगवन् ! इस प्रमादपूर्ण आचरण के कारण मैं अत्यधिक लज्जित हूँ । आपके तीव्र तप से उत्पन्न शरीर पीड़ा से भी अधिक मुझे सन्तापरूपी अग्नि जला रही है । मेरा हृदय नष्ट-सा हो रहा है, मेरी वाणी स्खलित हो रही है । मैं अपने आपको महापापी मानता हूँ । अतः समस्त दुःखी प्राणियों के बन्धुभूत, अकारण वत्सलभाव रखने वाले भगवन् ! आप ही मेरे इस दुःख के उपशमन का उपाय विचारिए ।" अग्निशर्मा तापस ने विचार किया - इन महाराज की महानता आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है । मुझे भोजन न करा पाने के कारण यह खिन्न हो रहे हैं। इनकी गुरुजनों की सेवा करने की इच्छा आश्चर्यकारी है। जब तक मैं इनके घर आहार नहीं कर लूंगा तब तक यह स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसा सोचकर उसने कहा, "महाराज ! बिना कारण ही
१. विय ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org