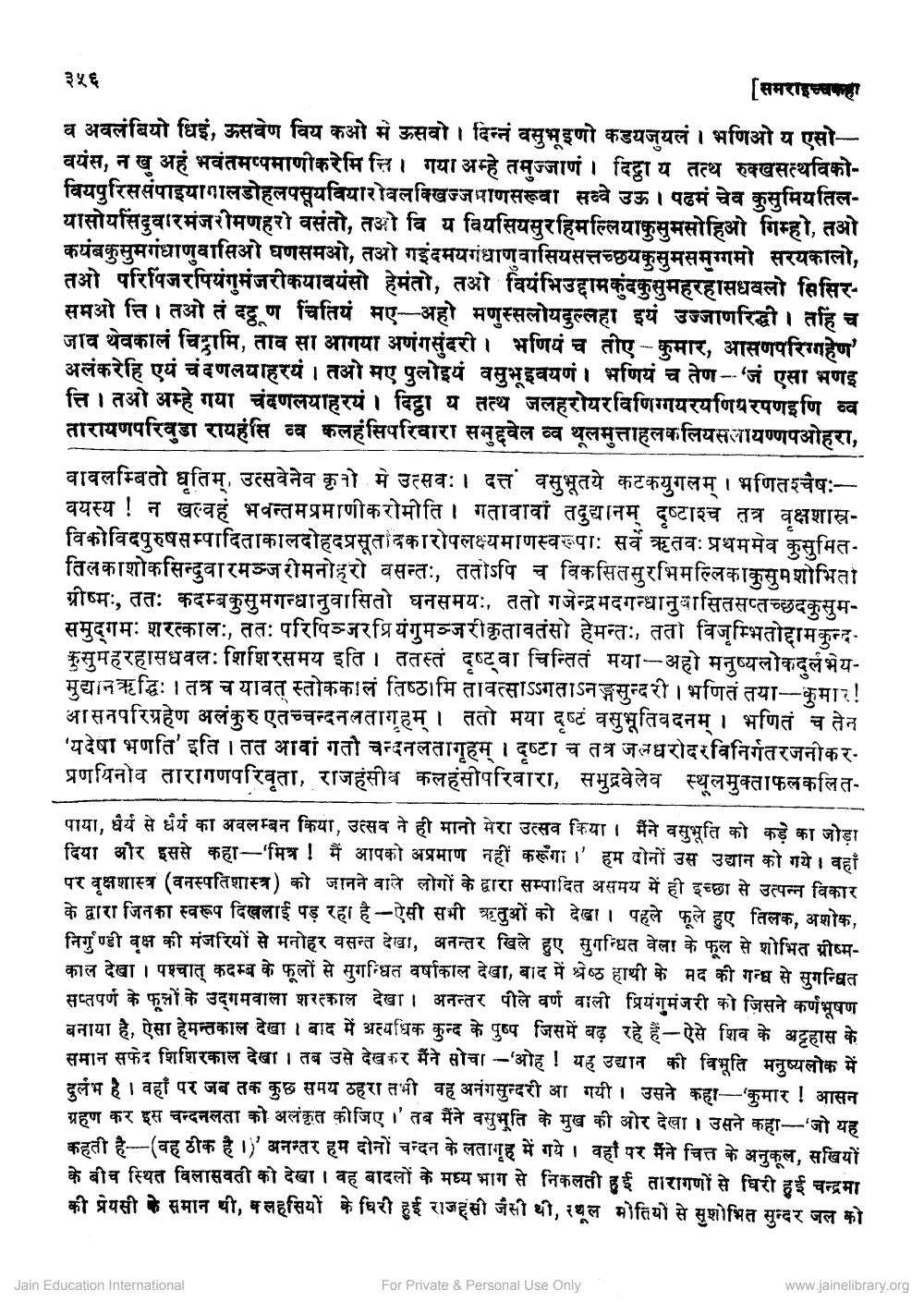________________
३५६
[समराइच्चकहा व अवलंबियो धिई, ऊसवेण विय कओ मे ऊसवो। दिन्नं वसुभूइणो कडयजुयलं । भणिओ य एसोवयंस, न खु अहं भवंतमप्पमाणीकरेमि ति। गया अम्हे तमुज्जाणं । दिवा य तत्थ रुक्खसत्थविकोवियपुरिससंपाइयागालडोहलपसूयवियारोवलक्खिज्जमाणसख्वा सव्वे उऊ । पढमं चेव कुसुमियतिलयासोयसिंदुवारमंजरीमणहरो वसंतो, तओ वि य वियसियसुरहिमल्लियाकुसुमसोहिओ गिम्हो, तओ कयंबकुसुमगंधाणुवासिओ घणसमओ, तओ गइंदमयगंधाणुवासियसत्तच्छयकुसुमसमुग्गमो सरयकालो, तओ परिपिंजरपियंगमंजरीकयावयंसो हेमंतो, तओ वियंभिउद्दामकुंदकुसुमहरहासधवलो सिसिरसमओ त्ति । तओ तं दट्ट ण चितियं मए-अहो मणुस्सलोयदुल्लहा इयं उज्जाणरिद्धी। तहिं च जाव थेवकालं चिट्ठामि, ताव सा आगया अणंगसुंदरी। भणियं च तीए-कुमार, आसणपरिग्गहेण' अलंकरेहि एवं चंदणलयाहरयं । तओ मए पुलोइयं वसुभइवयणं। भणियं च तेण-- 'जं एसा भणइ त्ति । तओ अम्हे गया चंदणलयाहरयं । दिट्ठा य तत्थ जलहरोयरविणिग्गयरयणियरपणइणि व्व तारायणपरिवुडा रायहंसि व्व कलहंसिपरिवारा समुद्दवेल व्व थूलमुत्ताहलकलियसलायण्णपओहरा, वावलम्बितो धृतिम्, उत्सवेनेव कृतो मे उत्सवः । दत्तं वसुभूतये कटकयुगलम् । भणितश्चैषःवयस्य ! न खल्वहं भवन्तमप्रमाणीकरोमोति । गतावावां तदुद्यानम् दृष्टाश्च तत्र वृक्षशास्रविकोविदपुरुषसम्पादिताकालदोहदप्रसूता दकारोपलक्ष्यमाणस्वरूपा: सर्वे ऋतवः प्रथममेव कुसुमित. तिलकाशोकसिन्दुवारमञ्जरीमनोहरो वसन्तः, ततोऽपि च विकसितसुरभिमल्लिकाकुसुमशोभिता ग्रीष्मः, ततः कदम्बकुसुमगन्धानुवासितो घनसमयः, ततो गजेन्द्रमदगन्धानुवासितसप्तच्छदकुसुमसमुद्गमः शरत्काल:, ततः परिपिञ्जरप्रियंगुमञ्जरीकृतावतंसो हेमन्तः, ततो विजृम्भितोदामकुन्दकुसुमहरहासधवलः शिशिरसमय इति । ततस्तं दृष्ट्वा चिन्तितं मया-अहो मनुष्यलोकदुर्लभेयमुद्यानऋद्धिः । तत्र च यावत् स्तोककालं तिष्ठामि तावत्साऽऽगताऽनङ्गसुन्दरी । भणितं तया-कुमार! आसनपरिग्रहेण अलंकुरु एतच्चन्दनलतागृहम् । ततो मया दृष्टं वसुभूतिवदनम् । भणितं च तेन 'यदेषा भणति' इति । तत आवां गतौ चन्दनलतागृहम् । दृष्टा च तत्र जलधरोदरविनिर्गतरजनीकर. प्रणयिनोव तारागणपरिवृता, राजहंसीव कलहंसीपरिवारा, समुद्रवेलेव स्थूलमुक्ताफल कलितपाया, धैर्य से धैर्य का अवलम्बन किया, उत्सव ने ही मानो मेरा उत्सव किया। मैंने वसुभूति को कड़े का जोड़ा दिया और इससे कहा-'मित्र! मैं आपको अप्रमाण नहीं करूंगा।' हम दोनों उस उद्यान को गये। वहाँ पर वृक्षशास्त्र (वनस्पतिशास्त्र) को जानने वाले लोगों के द्वारा सम्पादित असमय में ही इच्छा से उत्पन्न विकार के द्वारा जिनका स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है-ऐसी सभी ऋतुओं को देखा। पहले फूले हुए तिलक, अशोक, निर्गुण्डी वृक्ष की मंजरियों से मनोहर वसन्त देखा, अनन्तर खिले हुए सुगन्धित वेला के फूल से शोभित ग्रीष्मकाल देखा । पश्चात् कदम्ब के फूलों से सुगन्धित वर्षाकाल देखा, बाद में श्रेष्ठ हाथी के मद की गन्ध से सुगन्धित सप्तपर्ण के फूलों के उद्गमवाला शरत्काल देखा। अनन्तर पीले वर्ण वाली प्रियंगुमंजरी को जिसने कर्णभूषण बनाया है, ऐसा हेमन्तकाल देखा । बाद में अत्यधिक कुन्द के पुष्प जिसमें बढ़ रहे हैं-ऐसे शिव के अट्टहास के समान सफेद शिशिरकाल देखा । तब उसे देखकर मैंने सोचा -'ओह ! यह उद्यान की विभूति मनुष्यलोक में दुर्लभ है । वहाँ पर जब तक कुछ समय ठहरा तभी वह अनंगसुन्दरी आ गयी। उसने कहा-'कुमार ! आसन ग्रहण कर इस चन्दनलता को अलंकृत कीजिए।' तब मैंने वसुभूति के मुख की ओर देखा। उसने कहा-'जो यह कहती है---(वह ठीक है ।) अनन्तर हम दोनों चन्दन के लतागृह में गये। वहां पर मैंने चित्त के अनुकूल, सखियों के बीच स्थित विलासवती को देखा । वह बादलों के मध्य भाग से निकलती हुई तारागणों से घिरी हुई चन्द्रमा की प्रेयसी के समान थी, कलहसियों के घिरी हुई राजहंसी जैसी थी, रथूल मोतियों से सुशोभित सुन्दर जल को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org