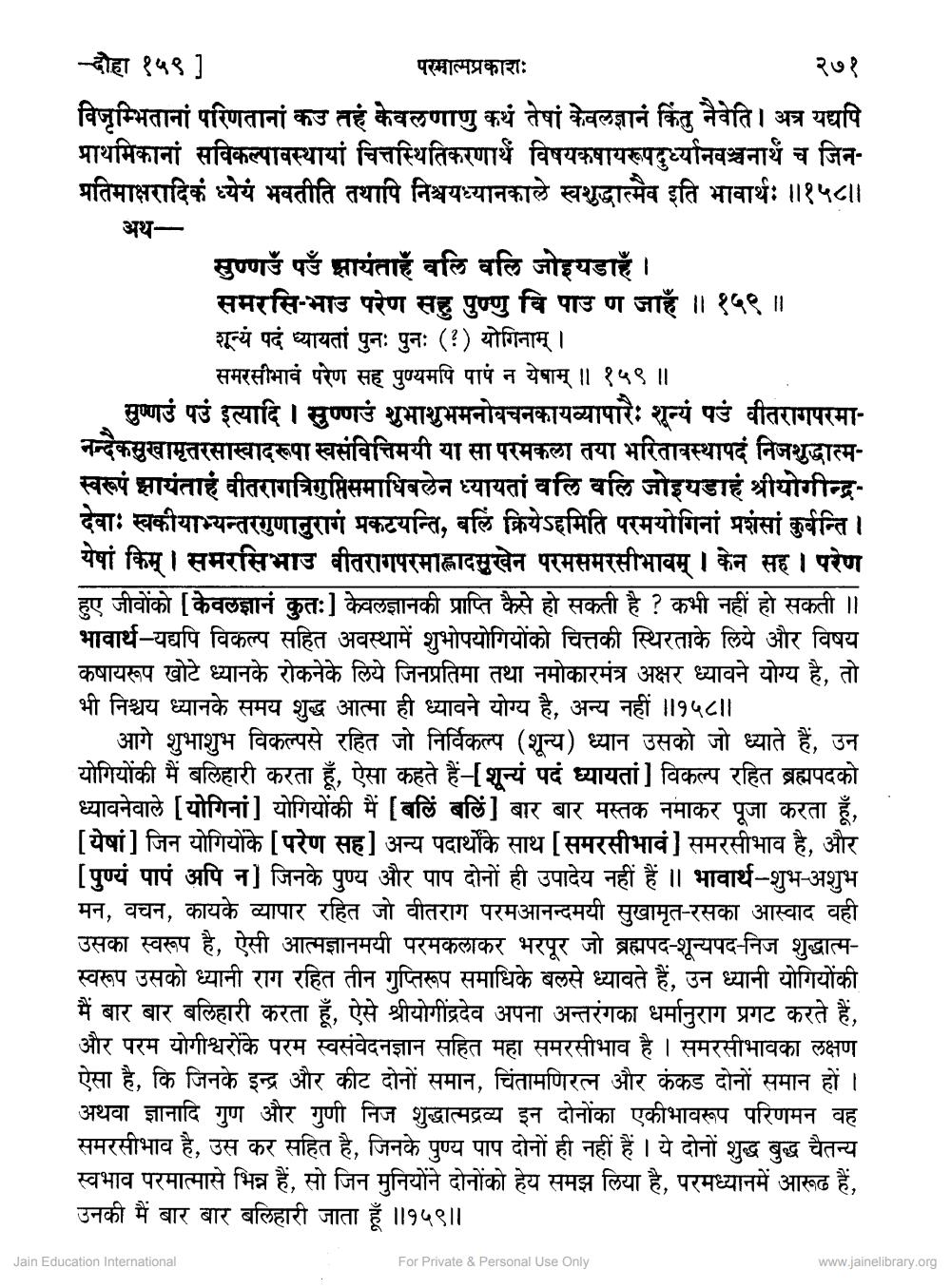________________
परमात्मप्रकाशः
-दोहा १५९]
२७१ विजृम्भितानां परिणतानां कउ तहं केवलणाणु कथं तेषां केवलज्ञानं किंतु नैवेति। अत्र यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थितिकरणार्थ विषयकषायरूपदानवञ्चनार्थं च जिनप्रतिमाक्षरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निश्चयध्यानकाले स्वशुद्धात्मैव इति भावार्थः ।।१५८।। अथ
सुण्णउँ पउँ झायंताहँ वलि वलि जोइयडाहँ। समरसि-भाउ परेण सह पुण्णु वि पाउ ण जाहँ ॥ १५९ ॥ शून्यं पदं ध्यायतां पुनः पुनः (१) योगिनाम् ।।
समरसीभावं परेण सह पुण्यमपि पापं न येषाम् ॥ १५९ ॥ सुण्णउं पउं इत्यादि । सुण्णउं शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैः शून्यं परं वीतरागपरमानन्देकमुखामृतरसास्वादरूपा स्वसंवित्तिमयी या सा परमकला तया भरितावस्थापदं निजशुद्धात्मस्वरूपं झायंताहं वीतरागत्रिगुप्तिसमाधिबलेन ध्यायतां वलि वलि जोइयडाहं श्रीयोगीन्द्रदेवाः स्वकीयाभ्यन्तरगुणानुरागं प्रकटयन्ति, बलिं क्रियेऽहमिति परमयोगिनां प्रशंसां कुर्वन्ति । येषां किम् । समरसिभाउ वीतरागपरमाह्लादमुखेन परमसमरसीभावम् । केन सह । परेण हुए जीवोंको [केवलज्ञानं कुतः] केवलज्ञानकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? कभी नहीं हो सकती ॥ भावार्थ-यद्यपि विकल्प सहित अवस्थामें शुभोपयोगियोंको चित्तकी स्थिरताके लिये और विषय कषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये जिनप्रतिमा तथा नमोकारमंत्र अक्षर ध्यावने योग्य है, तो भी निश्चय ध्यानके समय शुद्ध आत्मा ही ध्यावने योग्य है, अन्य नहीं ॥१५८॥ __ आगे शुभाशुभ विकल्पसे रहित जो निर्विकल्प (शून्य) ध्यान उसको जो ध्याते हैं, उन योगियोंकी मैं बलिहारी करता हूँ, ऐसा कहते हैं-शून्यं पदं ध्यायतां] विकल्प रहित ब्रह्मपदको ध्यावनेवाले [योगिनां] योगियोंकी मैं [बलिं बलिं] बार बार मस्तक नमाकर पूजा करता हूँ, [येषां] जिन योगियोंके [परेण सह] अन्य पदार्थोंके साथ [समरसीभावं] समरसीभाव है, और [पुण्यं पापं अपि न] जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं हैं । भावार्थ-शुभ-अशुभ मन, वचन, कायके व्यापार रहित जो वीतराग परमआनन्दमयी सुखामृत-रसका आस्वाद वही उसका स्वरूप है, ऐसी आत्मज्ञानमयी परमकलाकर भरपूर जो ब्रह्मपद-शून्यपद-निज शुद्धात्मस्वरूप उसको ध्यानी राग रहित तीन गुप्तिरूप समाधिके बलसे ध्यावते हैं, उन ध्यानी योगियोंकी मैं बार बार बलिहारी करता हूँ, ऐसे श्रीयोगींद्रदेव अपना अन्तरंगका धर्मानुराग प्रगट करते हैं,
और परम योगीश्वरोंके परम स्वसंवेदनज्ञान सहित महा समरसीभाव है । समरसीभावका लक्षण ऐसा है, कि जिनके इन्द्र और कीट दोनों समान, चिंतामणिरत्न और कंकड दोनों समान हो । अथवा ज्ञानादि गुण और गुणी निज शुद्धात्मद्रव्य इन दोनोंका एकीभावरूप परिणमन वह समरसीभाव है, उस कर सहित है, जिनके पुण्य पाप दोनों ही नहीं हैं । ये दोनों शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मासे भिन्न हैं, सो जिन मुनियोंने दोनोंको हेय समझ लिया है, परमध्यानमें आरूढ हैं, उनकी मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ ॥१५९।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org