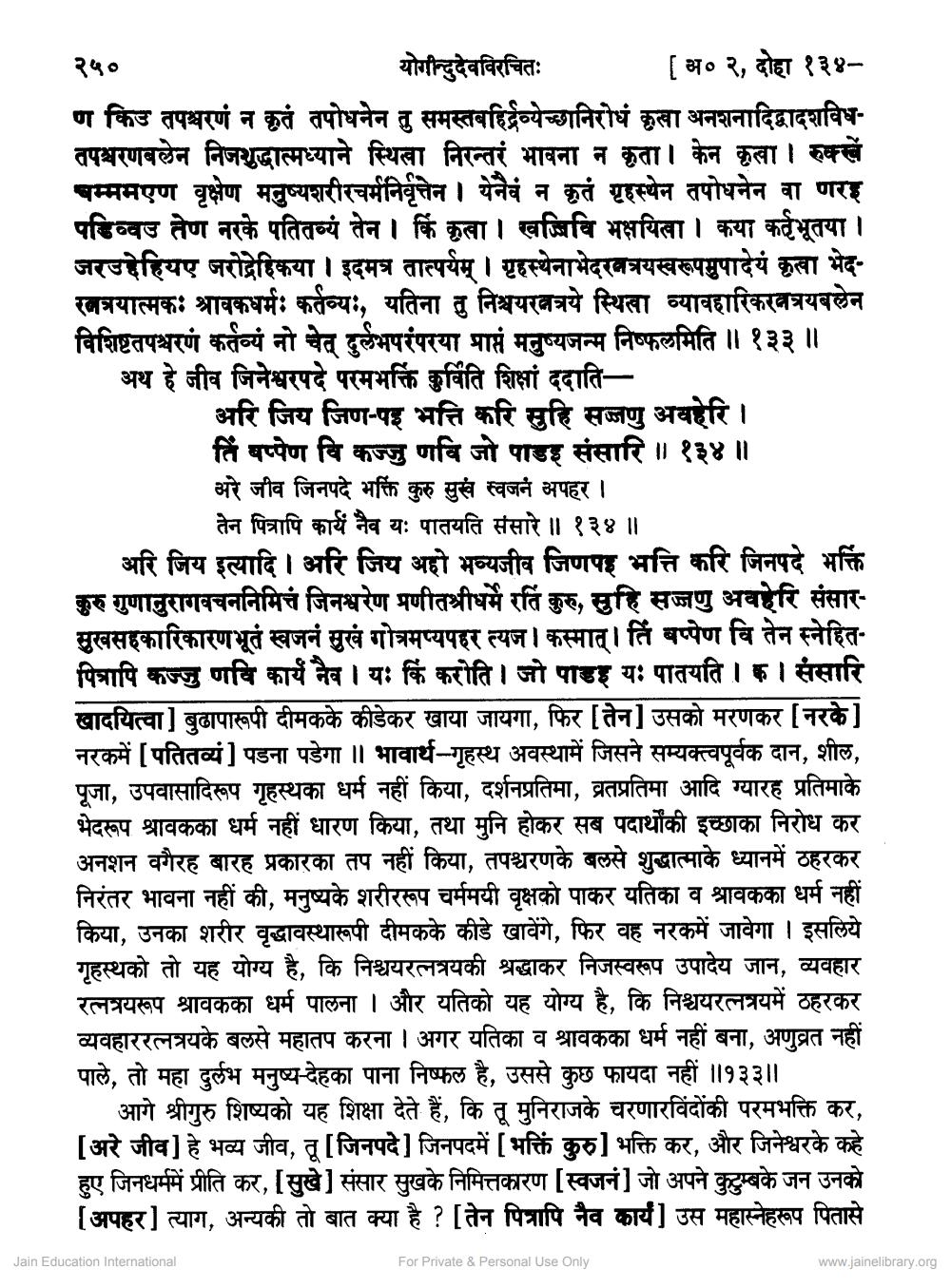________________
२५०
योगीन्दुदेवविरचितः [अ० २, दोहा १३४ण किउ तपश्चरणं न कृतं तपोधनेन तु समस्तबहिर्द्रव्येच्छानिरोधं कृखा अनशनादिद्वादशविधतपश्चरणबलेन निजशुद्धात्मध्याने स्थिता निरन्तरं भावना न कृता। केन कृता । रुक्खें चम्ममएण वृक्षण मनुष्यशरीरचर्मनिवृत्तेन । येनैवं न कृतं गृहस्थेन तपोधनेन वा णरह पडिव्वउ तेण नरके पतितव्यं तेन । किं कृता । खजिवि भक्षयिखा । कया कर्तृभूतया । जरउद्देहियए जरोदेहिकया । इदमत्र तात्पर्यम् । गृहस्थेनाभेदरबत्रयस्वरूपमुपादेयं कृत्वा भेदरजत्रयात्मकः श्रावकधर्मः कर्तव्यः, यतिना तु निश्चयरत्नत्रये स्थिखा व्यावहारिकरवत्रयबलेन विशिष्टतपश्चरणं कर्तव्यं नो चेत् दुर्लभपरंपरया प्राप्तं मनुष्यजन्म निष्फलमिति ॥ १३३ ॥ अथ हे जीव जिनेश्वरपदे परमभक्तिं कुर्विति शिक्षां ददाति
अरि जिय जिण-पइ भत्ति करि सहि सज्जणु अवहेरि । ति बप्पेण वि कज्जु णवि जो पाडइ संसारि ॥ १३४ ॥ अरे जीव जिनपदे भक्तिं कुरु सुखं स्वजनं अपहर।।
तेन पित्रापि कार्य नैव यः पातयति संसारे ॥ १३४ ॥ अरि जिय इत्यादि । अरि जिय अहो भव्यजीव जिणपइ भत्ति करि जिनपदे भक्तिं कुरु गुणानुरागवचननिमित्तं जिनश्चरेण प्रणीतश्रीधर्म रतिं कुरु, सुहि सज्जणु अवहेरि संसारसुखसहकारिकारणभूतं स्वजनं सुखं गोत्रमप्यपहर त्यज । कस्मात् । ति बप्पेण वि तेन स्नेहितपित्रापि कज्जु णवि कार्य नैव । यः किं करोति । जो पाडइ यः पातयति । क । संसारि खादयित्वा] बुढापारूपी दीमकके कीडेकर खाया जायगा, फिर [तेन] उसको मरणकर [नरके] नरकमें [पतितव्यं] पडना पडेगा ॥ भावार्थ-गृहस्थ अवस्थामें जिसने सम्यक्त्वपूर्वक दान, शील, पूजा, उपवासादिरूप गृहस्थका धर्म नहीं किया, दर्शनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा आदि ग्यारह प्रतिमाके भेदरूप श्रावकका धर्म नहीं धारण किया, तथा मुनि होकर सब पदार्थोंकी इच्छाका निरोध कर अनशन वगैरह बारह प्रकारका तप नहीं किया, तपश्चरणके बलसे शुद्धात्माके ध्यानमें ठहरकर निरंतर भावना नहीं की, मनुष्यके शरीरस्प चर्ममयी वृक्षको पाकर यतिका व श्रावकका धर्म नहीं किया, उनका शरीर वृद्धावस्थारूपी दीमकके कीडे खावेंगे, फिर वह नरकमें जावेगा । इसलिये गृहस्थको तो यह योग्य है, कि निश्चयरत्नत्रयकी श्रद्धाकर निजस्वरूप उपादेय जान, व्यवहार रत्नत्रयरूप श्रावकका धर्म पालना । और यतिको यह योग्य है, कि निश्चयरत्नत्रयमें ठहरकर व्यवहाररत्नत्रयके बलसे महातप करना । अगर यतिका व श्रावकका धर्म नहीं बना, अणुव्रत नहीं पाले, तो महा दुर्लभ मनुष्य-देहका पाना निष्फल है, उससे कुछ फायदा नहीं ॥१३३।। ___ आगे श्रीगुरु शिष्यको यह शिक्षा देते हैं, कि तू मुनिराजके चरणारविंदोंकी परमभक्ति कर, [अरे जीव] हे भव्य जीव, तू [जिनपदे] जिनपदमें [भक्तिं कुरु] भक्ति कर, और जिनेश्वरके कहे हुए जिनधर्ममें प्रीति कर, [सुखे] संसार सुखके निमित्तकारण [स्वजनं] जो अपने कुटुम्बके जन उनको [अपहर] त्याग, अन्यकी तो बात क्या है ? [तेन पित्रापि नैव कार्य] उस महास्नेहरूप पितासे
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org