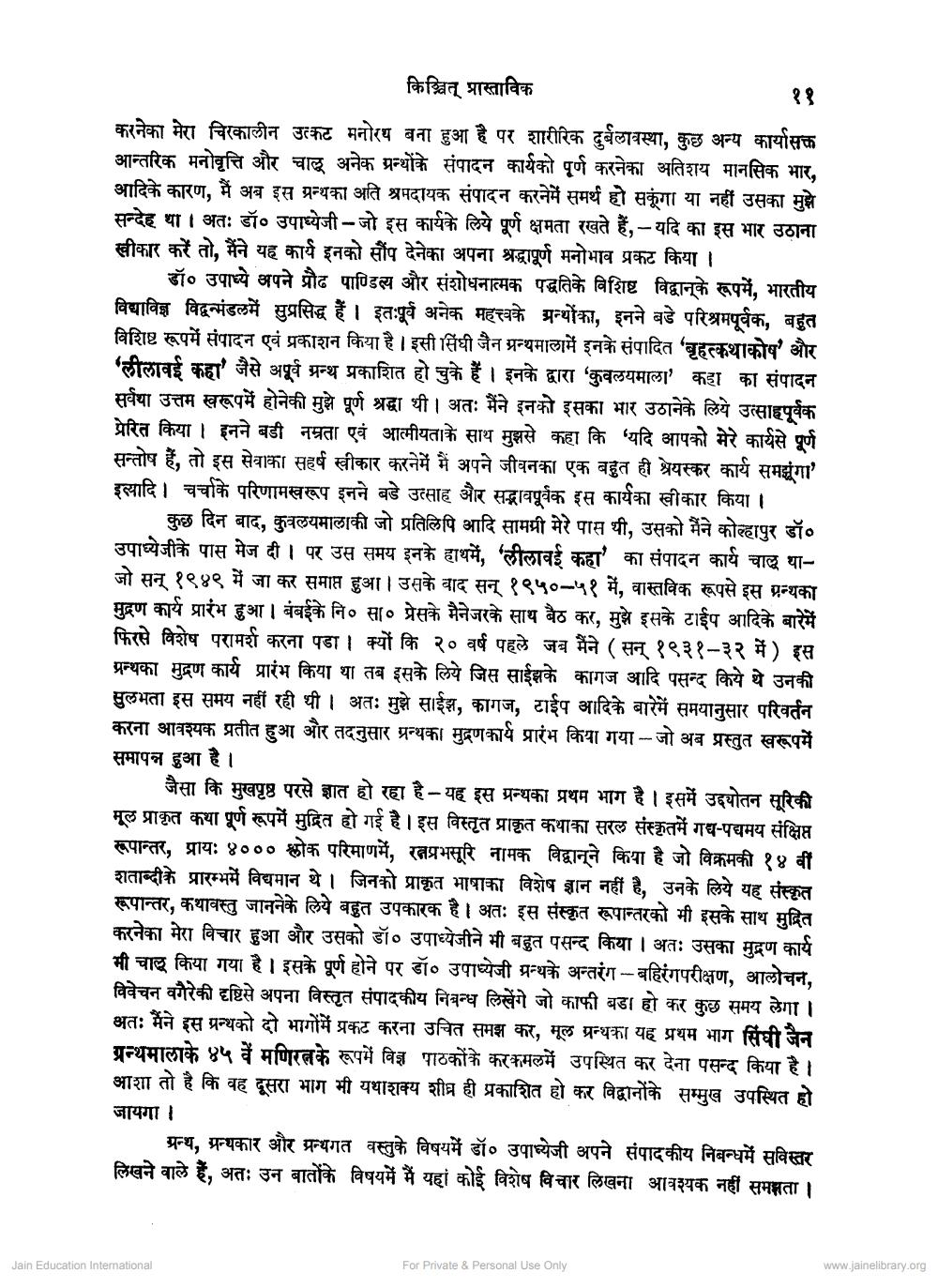________________
किञ्चित् प्रास्ताविक
११
करनेका मेरा चिरकालीन उत्कट मनोरथ बना हुआ है पर शारीरिक दुर्बलावस्था, कुछ अन्य कार्यासक्त आन्तरिक मनोवृत्ति और चालू अनेक ग्रन्थोंके संपादन कार्यको पूर्ण करनेका अतिशय मानसिक भार, आदिके कारण, अब इस ग्रन्थका अति श्रमदायक संपादन करनेमें समर्थ हो सकूंगा या नहीं उसका मुझे सन्देह था । अतः डॉ० उपाध्येजी- जो इस कार्यके लिये पूर्ण क्षमता रखते हैं, - यदि का इस भार उठाना स्वीकार करें तो, मैंने यह कार्य इनको सौंप देनेका अपना श्रद्धापूर्ण मनोभाव प्रकट किया ।
डॉ० उपाध्ये अपने प्रौढ पाण्डित्य और संशोधनात्मक पद्धतिके विशिष्ट विद्वान्के रूपमें, भारतीय विद्याविज्ञ विद्वन्मंडलमें सुप्रसिद्ध हैं । इतः पूर्व अनेक महत्त्व के ग्रन्थोंका, इनने बडे परिश्रमपूर्वक, बहुत विशिष्ट रूपमें संपादन एवं प्रकाशन किया है। इसी सिंघी जैन ग्रन्थमालामें इनके संपादित 'बृहत्कथा कोष' और 'लीलावई कहा' जैसे अपूर्व ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । इनके द्वारा 'कुवलयमाला' कहा का संपादन सर्वथा उत्तम स्वरूपमें होनेकी मुझे पूर्ण श्रद्धा थी । अतः मैंने इनको इसका भार उठानेके लिये उत्साहपूर्वक प्रेरित किया । इनने बडी नम्रता एवं आत्मीयता के साथ मुझसे कहा कि 'यदि आपको मेरे कार्य से पूर्ण सन्तोष हैं, तो इस सेवाका सहर्ष स्वीकार करनेमें मैं अपने जीवनका एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य समझंगा' इत्यादि । चर्चाके परिणामस्वरूप इनने बडे उत्साह और सद्भावपूर्वक इस कार्यका स्वीकार किया ।
कुछ दिन बाद, कुवलयमालाकी जो प्रतिलिपि आदि सामग्री मेरे पास थी, उसको मैंने कोल्हापुर डॉ० उपाध्येजीके पास मेज दी । पर उस समय इनके हाथमें, 'लीलावई कहा' का संपादन कार्य चालू थाजो सन् १९४९ में जा कर समाप्त हुआ । उसके बाद सन् १९५०-५१ में, वास्तविक रूपसे इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ। बंबईके नि० सा० प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर, मुझे इसके टाईप आदिके बारेमें फिरसे विशेष परामर्श करना पडा । क्यों कि २० वर्ष पहले जब मैंने ( सन् १९३१ - ३२ में ) इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ किया था तब इसके लिये जिस साईझके कागज आदि पसन्द किये थे उनकी सुलभता इस समय नहीं रही थी । अतः मुझे साईझ, कागज, टाईप आदिके बारेमें समयानुसार परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ और तदनुसार ग्रन्थका मुद्रणकार्य प्रारंभ किया गया - जो अब प्रस्तुत स्वरूपमें समापन हुआ है ।
1
जैसा कि मुखपृष्ठ परसे ज्ञात हो रहा है - यह इस ग्रन्थका प्रथम भाग है । इसमें उदयोतन सूरिकी मूल प्राकृत कथा पूर्ण रूपमें मुद्रित हो गई है। इस विस्तृत प्राकृत कथाका सरल संस्कृतमें गद्य-पद्यमय संक्षिप्त रूपान्तर, प्रायः ४००० श्लोक परिमाणमें, रत्नप्रभसूरि नामक विद्वान् ने किया है जो विक्रमकी १४ वीं शताब्दी के प्रारम्भमें विद्यमान थे। जिनको प्राकृत भाषाका विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिये यह संस्कृत रूपान्तर, कथावस्तु जाननेके लिये बहुत उपकारक है । अतः इस संस्कृत रूपान्तरको भी इसके साथ मुद्रित करनेका मेरा विचार हुआ और उसको डॉ० उपाध्येजीने भी बहुत पसन्द किया । अतः उसका मुद्रण कार्य मी चालू किया गया है। इसके पूर्ण होने पर डॉ० उपाध्येजी ग्रन्थके अन्तरंग - बहिरंगपरीक्षण, आलोचन, विवेचन वगैरेकी दृष्टिसे अपना विस्तृत संपादकीय निबन्ध लिखेंगे जो काफी बडा हो कर कुछ समय लेगा । अतः मैंने इस ग्रन्थको दो भागों में प्रकट करना उचित समझ कर, मूल ग्रन्थका यह प्रथम भाग सिंघी जैन ग्रन्थमाला ४५ वें मणिरत्न के रूपमें विज्ञ पाठकोंके करकमलमें उपस्थित कर देना पसन्द किया है । आशा तो है कि वह दूसरा भाग भी यथाशक्य शीघ्र ही प्रकाशित हो कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित हो
जायगा ।
ग्रन्थ, ग्रन्थकार और ग्रन्थगत वस्तुके विषयमें डॉ० उपाध्येजी अपने संपादकीय निबन्धमें सविस्तर लिखने वाले हैं, अतः उन बातोंके विषय में मैं यहां कोई विशेष विचार लिखना आवश्यक नहीं समझता ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org