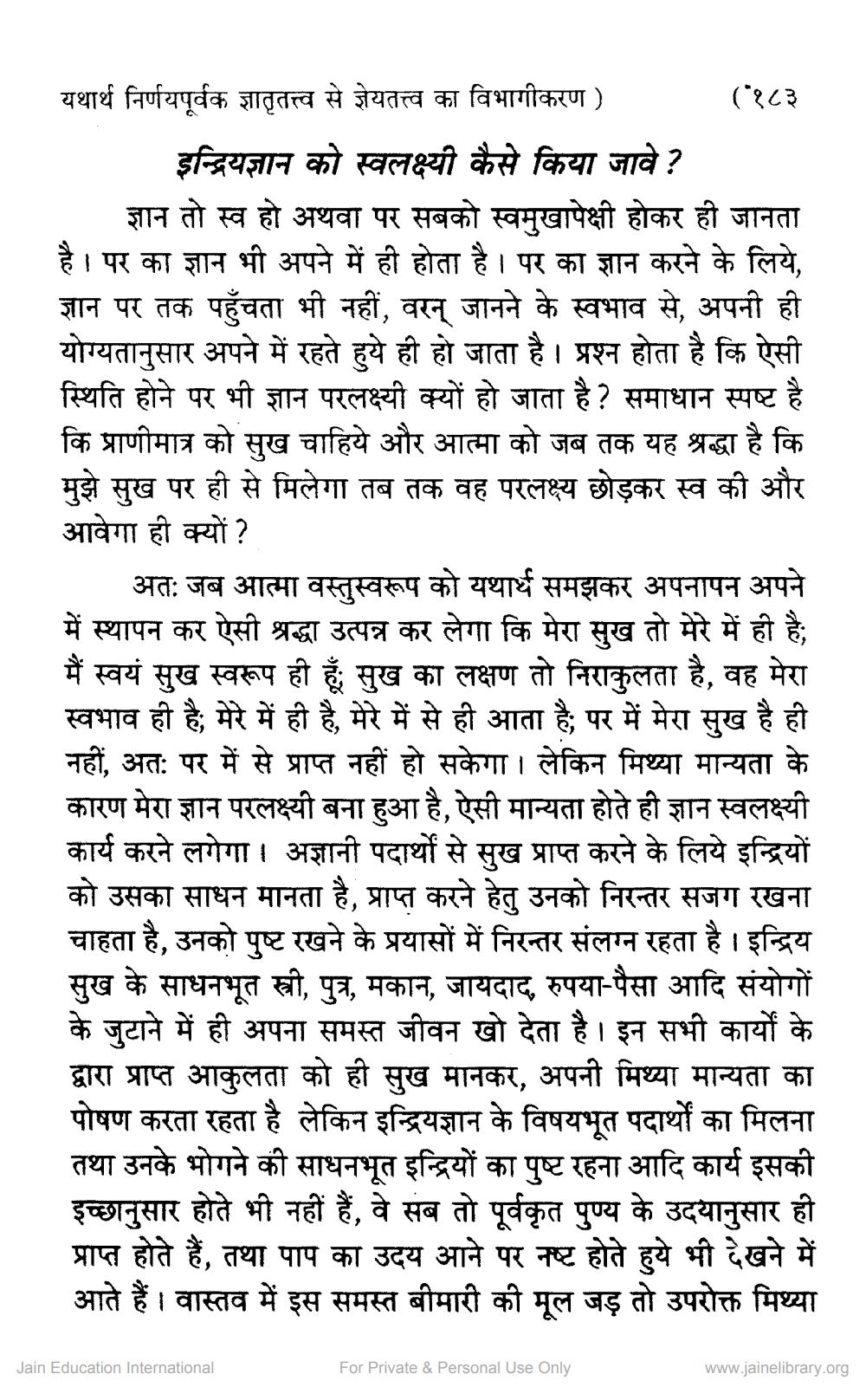________________
यथार्थ निर्णयपूर्वक ज्ञातृतत्त्व से ज्ञेयतत्त्व का विभागीकरण) (१८३
इन्द्रियज्ञान को स्वलक्ष्यी कैसे किया जावे? ज्ञान तो स्व हो अथवा पर सबको स्वमुखापेक्षी होकर ही जानता है। पर का ज्ञान भी अपने में ही होता है। पर का ज्ञान करने के लिये, ज्ञान पर तक पहुँचता भी नहीं, वरन् जानने के स्वभाव से, अपनी ही योग्यतानुसार अपने में रहते हुये ही हो जाता है। प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति होने पर भी ज्ञान परलक्ष्यी क्यों हो जाता है? समाधान स्पष्ट है कि प्राणीमात्र को सुख चाहिये और आत्मा को जब तक यह श्रद्धा है कि मुझे सुख पर ही से मिलेगा तब तक वह परलक्ष्य छोड़कर स्व की और आवेगा ही क्यों?
अत: जब आत्मा वस्तुस्वरूप को यथार्थ समझकर अपनापन अपने में स्थापन कर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कर लेगा कि मेरा सुख तो मेरे में ही है, मैं स्वयं सुख स्वरूप ही हूँ; सुख का लक्षण तो निराकुलता है, वह मेरा स्वभाव ही है; मेरे में ही है, मेरे में से ही आता है; पर में मेरा सुख है ही नहीं, अत: पर में से प्राप्त नहीं हो सकेगा। लेकिन मिथ्या मान्यता के कारण मेरा ज्ञान परलक्ष्यी बना हुआ है, ऐसी मान्यता होते ही ज्ञान स्वलक्ष्यी कार्य करने लगेगा। अज्ञानी पदार्थों से सुख प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों को उसका साधन मानता है, प्राप्त करने हेतु उनको निरन्तर सजग रखना चाहता है, उनको पुष्ट रखने के प्रयासों में निरन्तर संलग्न रहता है । इन्द्रिय सुख के साधनभूत स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया-पैसा आदि संयोगों के जुटाने में ही अपना समस्त जीवन खो देता है। इन सभी कार्यों के द्वारा प्राप्त आकुलता को ही सुख मानकर, अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करता रहता है लेकिन इन्द्रियज्ञान के विषयभूत पदार्थों का मिलना तथा उनके भोगने की साधनभूत इन्द्रियों का पुष्ट रहना आदि कार्य इसकी इच्छानुसार होते भी नहीं हैं, वे सब तो पूर्वकृत पुण्य के उदयानुसार ही प्राप्त होते हैं, तथा पाप का उदय आने पर नष्ट होते हुये भी देखने में आते हैं। वास्तव में इस समस्त बीमारी की मूल जड़ तो उपरोक्त मिथ्या
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org