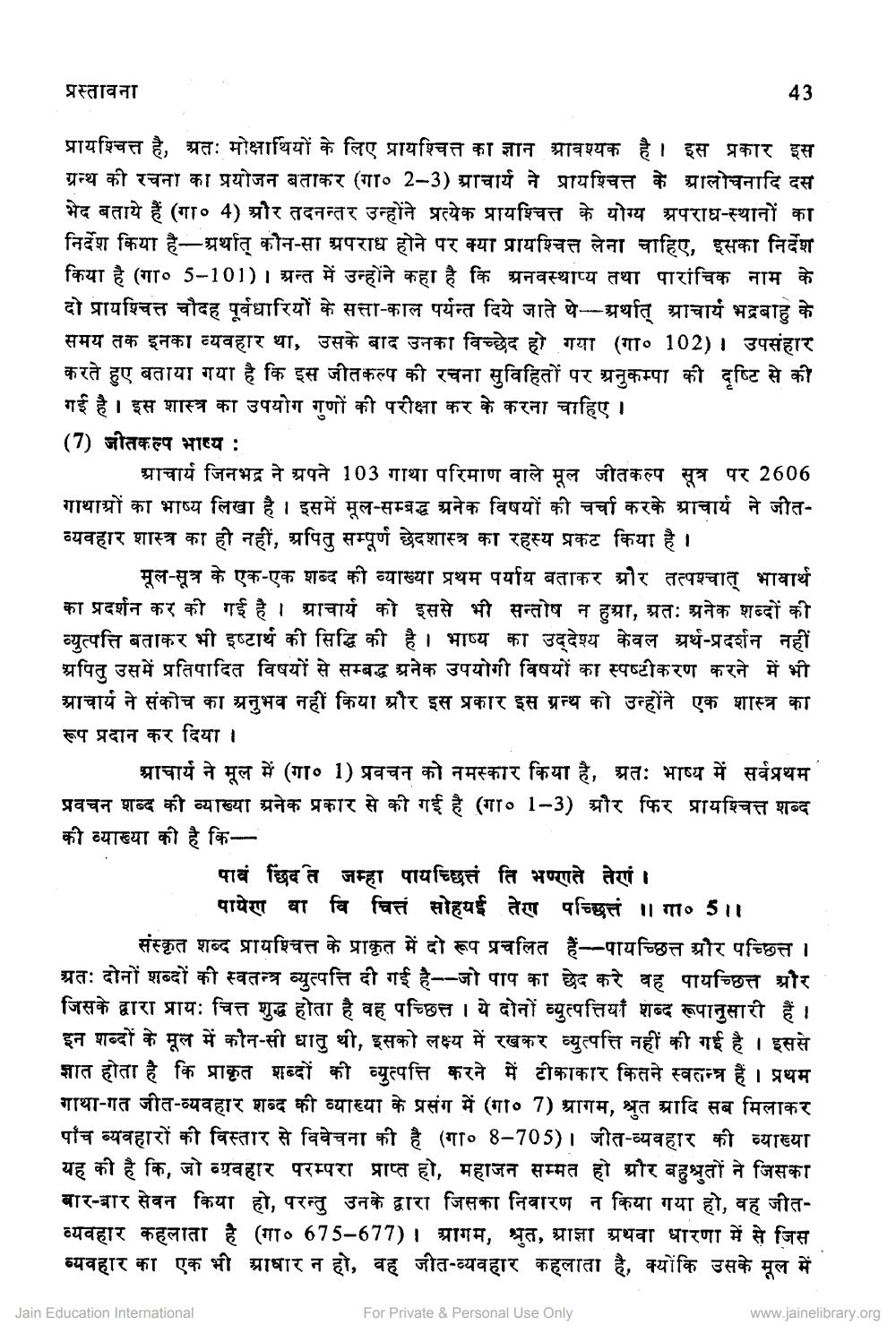________________
प्रस्तावना
प्रायश्चित्त है, अतः मोक्षार्थियों के लिए प्रायश्चित्त का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना का प्रयोजन बताकर (गा० 2-3) प्राचार्य ने प्रायश्चित्त के पालोचनादि दस भेद बताये हैं (गा० 4) और तदनन्तर उन्होंने प्रत्येक प्रायश्चित्त के योग्य अपराध-स्थानों का निर्देश किया है-अर्थात् कौन-सा अपराध होने पर क्या प्रायश्चित्त लेना चाहिए, इसका निर्देश किया है (गा० 5-101)। अन्त में उन्होंने कहा है कि अनवस्थाप्य तथा पारांचिक नाम के दो प्रायश्चित्त चौदह पूर्वधारियों के सत्ता-काल पर्यन्त दिये जाते थे----अर्थात् प्राचार्य भद्रबाहु के समय तक इनका व्यवहार था, उसके बाद उनका विच्छेद हो गया (गा० 102)। उपसंहार करते हुए बताया गया है कि इस जीतकल्प की रचना सुविहितों पर अनुकम्पा की दृष्टि से की गई है । इस शास्त्र का उपयोग गुणों की परीक्षा कर के करना चाहिए । (7) जीतकल्प भाष्य :
आचार्य जिनभद्र ने अपने 103 गाथा परिमाण वाले मूल जीतकल्प सूत्र पर 2606 गाथानों का भाष्य लिखा है । इसमें मूल-सम्बद्ध अनेक विषयों की चर्चा करके प्राचार्य ने जीतव्यवहार शास्त्र का ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण छेदशास्त्र का रहस्य प्रकट किया है ।
मूल-सूत्र के एक-एक शब्द की व्याख्या प्रथम पर्याय बताकर और तत्पश्चात् भावार्थ का प्रदर्शन कर की गई है। प्राचार्य को इससे भी सन्तोष न हुअा, अतः अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति बताकर भी इष्टार्थ की सिद्धि की है। भाष्य का उद्देश्य केवल अर्थ-प्रदर्शन नहीं अपितु उसमें प्रतिपादित विषयों से सम्बद्ध अनेक उपयोगी विषयों का स्पष्टीकरण करने में भी आचार्य ने संकोच का अनुभव नहीं किया और इस प्रकार इस ग्रन्थ को उन्होंने एक शास्त्र का रूप प्रदान कर दिया।
प्राचार्य ने मूल में (गा० 1) प्रवचन को नमस्कार किया है, अतः भाष्य में सर्वप्रथम प्रवचन शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है (गा० 1-3) और फिर प्रायश्चित्त शब्द की व्याख्या की है कि
पावं छिद त जम्हा पायच्छित्तं ति भण्णते तेणं ।
पायेण वा वि चित्तं सोहयई तेण पच्छित्तं ॥ गा० 5॥ संस्कृत शब्द प्रायश्चित्त के प्राकृत में दो रूप प्रचलित हैं-पायच्छित्त और पच्छित्त । अतः दोनों शब्दों की स्वतन्त्र व्युत्पत्ति दी गई है--जो पाप का छेद करे वह पायच्छित्त और जिसके द्वारा प्रायः चित्त शुद्ध होता है वह पच्छित्त । ये दोनों व्युत्पत्तियाँ शब्द रूपानुसारी हैं। इन शब्दों के मूल में कौन-सी धातु थी, इसको लक्ष्य में रखकर व्युत्पत्ति नहीं की गई है । इससे ज्ञात होता है कि प्राकृत शब्दों की व्युत्पत्ति करने में टीकाकार कितने स्वतन्त्र हैं । प्रथम गाथा-गत जीत-व्यवहार शब्द की व्याख्या के प्रसंग में (गा० 7) आगम, श्रुत आदि सब मिलाकर पाँच ब्यवहारों की विस्तार से विवेचना की है (गा० 8-705)। जीत-व्यवहार की व्याख्या यह की है कि, जो व्यवहार परम्परा प्राप्त हो, महाजन सम्मत हो और बहुश्रुतों ने जिसका बार-बार सेवन किया हो, परन्तु उनके द्वारा जिसका निवारण न किया गया हो, वह जीतव्यवहार कहलाता है (गा० 675-677)। आगम, श्रुत, प्राज्ञा अथवा धारणा में से जिस व्यवहार का एक भी आधार न हो, वह जीत-व्यवहार कहलाता है, क्योंकि उसके मूल में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org